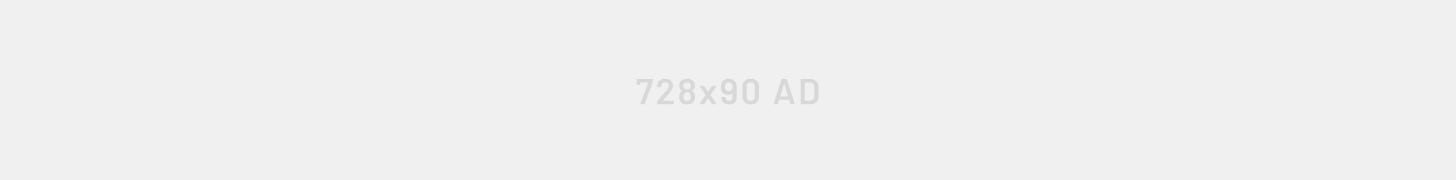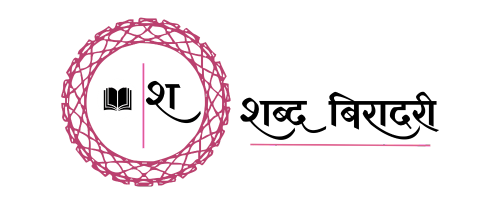‘कानपुर का जो ज़िक्र किया तूने हमनशीं
इक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय !’
अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है Amazing जिसका हिंदी तर्जुमा अद्भुत है और उर्दू में इसे हैरत अंगेज़ कहतें हैं। लेकिन हमारे लिए इन तीनों का असल मतलब कानपुर है! इस बात को वही समझ सकता है जो या तो कनपुरिया है या फिर उसने कानपुर में कुछ समय बिताया हो।
हमारी बचपन की कानपुर की यादें एक ऐसे शहर की है जहां इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर से टेक्सटाइल मिलें थीं और मजदूरों की कॉलोनीज़ हुआ करतीं थीं। और तीन चार बड़ी बाज़ारें थीं। कानपुर में तब मल्टी स्टोरीज़ नहीं होती थीं। ज़्यादा से ज़्यादा दो मंज़िले मकान ही थे।। पहली बार जब मॉल रोड पर मेघदूत होटल खुला तो सात मंज़िले होटल के रूफटॉप रेस्तरां में लिफ्ट यूज़ करने के लिए हमें लिफ्ट मैन को बुलाने की ज़रूरत पड़ी। इसका इल्म नहीं था कि लिफ्ट चलती कैसे है और रुकती कैसे है। मेघदूत कानपुर का सबसे बड़ा होटल था। शायद 3 स्टार। हमारे एक कॉलेज फ्रेंड थे रियाज़ सैय्यद रूफ़ी वाक़ी। एशिया टैनरी के मालिक के नवासे थे। चमड़े के बिजनेस में उनका दिल नहीं लगता था। चमड़े के व्यापारी अपने घर के लड़कों को ट्रेनिंग के लिए पहले कुछ साल चमड़ा मंडी भेज करते थे जिससे उन्हें चमड़े की जानकारी हो सके। टैनरी में उन्हें बाद में लगाया जाता था। रूफ़ी के नाना उन्हें हर सुबह चमड़ा मंडी विज़िट करने के लिए हर रोज दो सौ रुपए देते थे। बाक़ी के खर्चे अलग थे। रूफ़ी ने अपने मुंशी को पटा लिया था और बस दस्तख़त कर दफ़्तर से भाग आते थे। उन पैसों को जोड़ कर हर दूसरे तीसरे हमें मेघदूत ले जाते।
मेघदूत के पहले कानपुर के सिविल लाइन्स में बर्कले हाउस हुआ करता था। ब्रिटीशर्स के ज़माने का। अक्सर इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वहीं ठहराए जाते थे। इंग्लिश क्रिकेट टीम जब कानपुर आती तो वो बीआईसी के अंग्रेज़ अफसरों के घरों में रुकती थी।
कानपुर में ब्रिटीशर्स के बड़े बंगले सिविल लाइन्स, पार्वती बागला रोड या फिर मैकरॉबर्ट्स गंज,जहां हम लोग रहते थे, से लेकर तिलक नगर के बीच थे।
चार पांच बड़ी मार्केट्स थीं। मॉल रोड, पीपीएन मार्केट, नवीन मार्केट या फिर परेड। ब्रांड स्टोर्स तब कानपुर क्या हिंदुस्तान में ही नहीं थे। मॉल रोड सबसे हाई एन्ड थी। शाम को चहलक़दमी के लिए हम लोग नवीन मार्केट ही जाते थे। क्राइस्ट चर्च सबसे इलीट को – एड कॉलेज हुआ करता था। लेकिन आपस मे इतना सेग्रिगेशन था कि साथ पढ़ने वाले लड़के – लड़कियां अपनी फैमिलीज़ के बीच जब शाम को नवीन मार्केट में टकराते तो एक दूसरे को पहचानने से गुरेज़ करते।
तो बात कानपुर के अमेज़िंग होने की थी। इसका सबसे बेहतरीन एग्ज़ामपिल परेड की बाज़ार थी। नवीन मार्केट के सामने एक बहुत बड़ा परेड ग्राउंड था जहां बारहों महीने टेम्पोररी दुकानें लगी रहतीं थीं। रोज़मर्रा की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो परेड में ना मिलती हो। ग्राउंड में अलग अलग सेक्शन्स थे। एक तरफ पुरानी किताबों की दुकानें थीं। हमारी पोलिटिकल साइंस , हिस्टिरी और इंग्लिश लिटरेचर की तक़रीबन सारी किताबें परेड ग्राउंड से खरीदी गईं थीं। क्राइस्ट चर्च से आते जाते हम अक़्सर परेड बाज़ार में घंटों बिताते थे। एक एक सी नायाब किताबें मिल जाती थीं। ये वो दौर था जब ख़ास क़िताबों के रीप्रिंट्स नहीं आते या आसानी से नहीं मिल पाते। इसी बाज़ार से हमें डॉक्टर जॉनसन की बॉसवेल की लिखी बायोग्रेफी, कीट्स के अपनी मंगेतर फैनी ब्रॉन को लिखे ख़तों का कमपाईलेशन और स्टेनली लेनपूल की इंडियन हिस्ट्री की किताबें मिली थीं। बाँसबल्ली से लेकर सस्ते कपड़ों , चश्मों, बैग्स – झोलों, बर्तन, बरसाती – पॉलीथीन , मुर्ग़ा, मछली, गोश्त सब कुछ आस पास एक ही ग्राउंड में मुहैय्या था। इनमें सबसे दिलचस्प चिड़ियों और एक्वेरियम फिश की बाज़ार थी। हमारी दादी के पहाड़ी तोते यहीं से आते थे। हमारे वालिद ने घर मे एक बड़ा सा बर्ड हाउस बनवाया था। लाल मुनिया हम इसी परेड बाज़ार से लाते। दुकानदार दो लाल मुनिया रुमाल में ढीले से बांध देता औऱ हम हैंडल में फंसा कर आहिस्ता आहिस्ता साईकल से घर ले आते।
बड़ा अनरुली शहर था कानपुर। ट्रैफिक के कोई रूल नहीं थे। आज भी नहीं हैं। जो जिधर चाहे उधर गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा, तांगा घुसेड़ दे। जहां चाहे फुटपाथ घेर कर दुकान लगा ले। शहर में फुटपाथ थे लेकिन वो आम पैदल चलने वालों के लिए नहीं। खोन्चों, पानी के ठेलों, दुकानों के आगे समान के फैलाव के लिए थे। शहर के लोगों को इससे कोई दिक़्क़त भी नहीं थी। बल्कि इन चीजों को लोकल्स इंजॉय करते थे।
बड़े मलंग तबियत के होते थे कानपुर वाले! बेहद बेफ़िक्री के आलम में। मौजूदा वक़्त में जीने वाले। कल के लिए बेपरवाह। झगड़ा लड़ाई , कहा सुनी आम बात थी। जो मिनटों में निपट भी जाती और जिससे वे क़तई डिस्टर्ब भी ना होते। लफ़्फ़ाज़ी में एक नम्बर! इतनी बड़ी बड़ी लंतरानी की सुनने वाला बोर हो जाएं, सुनाने वाला थके ना। ‘नक़्शेबाज़’ कानपुर का टर्म है। जो ज़रा बन संवर कर निकले या ऊंची ले वो ‘नक़्शेबाज़’ हो जाता। और उसके लिए एक टाइटल होता, ‘झाड़े रहो कलक्टर गंज!’ कानपुर की लोकल ज़ुबान लखनवी ज़ुबान से कितनी अलहदा है इसके कुछ एग्ज़ामपिल हैं जैसे कानपुर में झांपड नहीं ‘कंटाप’ मारा जाता है।यहां किसी का रुतबा ‘भौकाल’ कहलाता है। कोई चीज़ अच्छी है, हसीन या क्वालिटी की है तो वो ‘धांसू’ कहलाती है। मूर्ख या बेवकूफ़ को बग़ैर किसी झिझक के तड़ से ‘चूतिया’ क़रार कर दिया जाता । कानपुर में कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनता बल्कि वो ‘चौडीयाता’ है। बड़े बेझिझक हैं कानपुर के लोग। लेकिन उनके लिए ये बातें आम फ़हम है। दूसरी ज़ुबान या तहज़ीब से ना आशनाई इसकी एक वजह हो सकती है। बड़े बेख़ौफ़ भी होते हैं कानपुर के लोग। क्राइस्ट चर्च में हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी उसके बाप कानपुर शहर कोतवाल थे। बड़ा जाबिर कोतवाल था। वैसे कानपुर का कोतवाल जाबिर ही होकर टिक सकता है। कोतवाली हमारे क्राइस्ट चर्च कॉलेज से लगी हुई थी। एक बार कॉलेज में लड़कों ने हंगामा कर दिया। कोतवाल ने पकड़ कर लौंडों की तुड़ाई कर दी। हम सीनियर थे तो मजबूरन कोतवाली जाना पड़ा। जूनियर्स के सामने कस के चौड़िया के लौटे। कोतवाल पहचानते थे इसलिए बस छोड़ ही दिया। दूसरे दिन कोतवाल की बेटी मुंह फुलाए, नाराज़ होकर छिटक गई। ज़ाहिर है बाप ने क्लास ली होगी कि , ‘ किन लोफरों के बीच उठती बैठती हो!’
कानपुर का असल मिज़ाज मिलता है यहां के मशहूर ‘ठग्गू के लड्डू’ और ‘बदनाम कुल्फ़ी’ में। ये दोनों प्रोडक्ट एक ही इंसान की दिमाग़ की ईजाद है। अब तो ये लड्डू और कुल्फ़ी पूरे हिंदुस्तान में कानपुर की पहचान बन कर मशहूर है वरना जब हम पढ़ते थे तो बड़े चौराहे पर उर्सला अस्पताल के पास फुटपाथ पर ठग्गू के लड्डू का एक छोटा सा ठीहा हुआ करता था जहां एक बड़े बोर्ड पर लिखा रहता, ‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको मैंने ठगा नहीं’। ठग्गू के लड्डू को शोहरत उसकी इसी टैग लाइन से मिली। इसी सक्सेस को देख कर इन मोहतरम ने ‘बदनाम कुल्फ़ी’ लांच की। क्वालिटी मिठाइयों की दुकान तिवारी स्वीट्स बिरहाना रोड पर कुछ बाद में आई। उनदिनोँ लोकल अखबारों में छपता था कि दिवाली पर तिवारी स्वीट्स ने 3 करोड़ का बिजनेस किया। ये कानपुर की लोकल न्यूज़ होती थी!
मॉल रोड का क्वालिटी रेस्टारेंट ख़ासा आइकोनिक हुआ करता। वहां कानपुर की क्रीम पहुंचती। आम लोगों के लिए भाटिया रेस्टॉरेंट था। हमारे घर के पास आर्यनगर में घोष स्वीट हाउस था।पता नहीं अब है या नहीं। घोष का रसगुल्ला और मिष्टी दोई जैसा दोबारा कहीं देखने को नहीं मिला। कोलकाता में भी नहीं!
उनदिनोँ कानपुर में तीन चार क्लब्स ही थे। कानपुर क्लब डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स और शहर के बड़े बिज़नेस मैन के लिए था। कमला क्लब जेके इंडस्ट्रीज़ के लोगों का था। बीआईसी क्लब ब्रिटिश इंडिया कॉर्पिरेशन के सीनियर ऑफिसर्स का एक्सक्लूसिव क्लब था और गैंजिस क्लब कानपुर के प्रोफेशनल बिरादरी के लिए था। बकिया लोगों के लिए चौराहे बाज़ी और मोहल्ले के खटिया क्लब के अड्डे थे। वैसे कानपुर के खटिया क्लब पर एक अलहदा राइट अप बनता है जो कभी बाद में !
कानपुर में टीवी 78 के बाद आया जब वहां मोतीझील में टीवी टावर लगाई गई। उसके पहले आम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के नाम पर साल में तीन चार महीनों के लिए लगने वाली सर्कस थी जो हमारे घर के पास बृजेन्द्र स्वरुप पार्क में लगती या फिर या पांच छह सिनेमा हॉल्स थे। ये सभी सिनेमा हॉल्स एक सीधी सड़क पर थे। चुन्नीगंज में विवेक टॉकीज से लेकर मॉल रोड पर हीर पैलेस। हीर पैलेस उनदिनोँ सबसे अच्छा हॉल था। कूलर की आवाज़ धीमी होती थी और कुर्सियां भी उम्दा पुश बैक गद्दे दार थीं। निशात टॉकीज क्राइस्ट चर्च के सामने था और विवेक हमारे घर के रास्ते में। जहां हम जब चाहते किसी भी समय फ़िल्म के बीच मे बग़ैर टिकट धंस लेते।
कहते हैं ना कि अपनो के सौ ख़ून मुआफ़! आज जब ट्रेन से कानपुर के सफ़र पर हैं तो जैसे जैसे अपना शहर नज़दीक आ रहा है कानपुर बहुत याद आ रहा है! लाज़िम है। पैदाइश से लेकर ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो यहां बीता है! जहां ख़ाबों की इब्तिदा हुई! जहां हम कभी ‘ चौड़िया ‘ कर चले होंगे! और कितनी बार ‘झाड़े रहो कलक्टरगंज ‘ से बुलाए गए होंगे!
ना चाहते हुए भी उन सभी जगहों को एक साथ देखना चाहते हैं, वहां जाना चाहतें हैं जो हमारी ज़िंदगी के किसी ना किसी पहलू से जुड़ी रहीं।
पता नहीं जा भी पाएंगे। देख भी पाएंगे! बड़ी हिम्मत जो चाहिए। बड़ा कलेजा चाहिए। शायद इसलिए कि कानपुर में पाया कम, खोया ज़्यादा है!
शेष अगले भाग में…