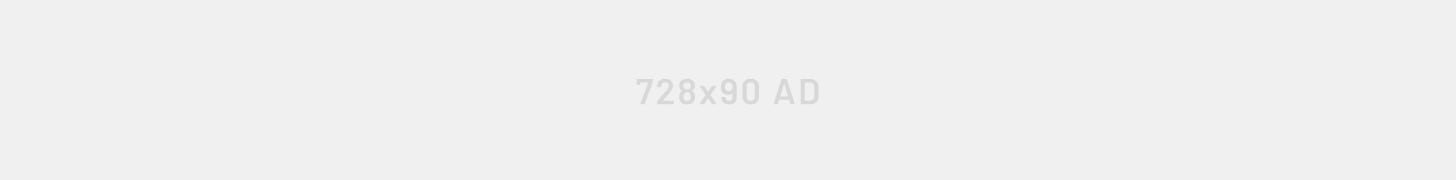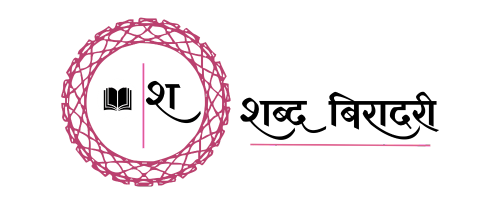यह मैं हूं या शाख पर टिका आखिरी पत्ता
यह पतझड़ का मौसम या शुष्क हवा जागती सी
देखना है कृशकाया मेरी चीर देगी पवन का रुख
या कि रुख़सत होने की घड़ी आ गई करीब
धुंधला धुंधला सा वलय सूक्ष्म से स्थूल घेरता
घेरा यह लेता अपनी परिधि में
हवा, पानी, आकाश, अग्नि, धरा को
मानव तन और समूचा वातायन
बढ़ते ही जाता, गिरफ्त में लेता साँसें
फिर भी जाने क्यों सुट्टा मारना चाहे मन
जब उज्जैन से चली थी यह सवारी
पच्चीस बोगियाँ जुड़ी थी वर्षों की
स्टीम इंजन से गूंजती हुई आती सीटी
चीर कर रख देती थी
अनुभूतियों का सन्नाटा
अनुभव का शिशु चौक पड़ता यकसाँ
नींद से
इक्का-दुक्का पहचाने चेहरे
डॉ. जोशी, प्रभाकर माचवे उतरते मंगलनाथ के रास्ते
भैरोनाथ के आसपास, वेधशाला के पीछे
सूखी वापी जिसके भीतर धँसती सीढ़ियाँ
मुहाने तक जमीं हरी-कच्च काई
नीचे तल में बहुत कम जल
अनाथ कीट-पतंगों और टिड्डों की शरणस्थली वह
जैसे जल तल पर सोया पड़ा हो शब्द
एकांत यह धँसता जाता भीतर गाड़ियों में, भीड़ में
अजनबी चेहरे आशंकित, उत्साहित, भौचक्के से
स्वयं को अभिव्यक्त करते मुखौटे
बहुत-बहुत घूमें भर्तृहरि की गुफा के रास्ते
श्मशान घाट के पास दिन पर दिन और रातें भी
अंतहीन-बहसें, चर्चाएँ दर्शन-राजनीति और साहित्य पर
स्पष्ट कर आरंभ से ही चला था
कि सफलता नहीं सार्थकता चाहिए
सार्थकता की राह बढ़ चला जीवन
पीछे झूठे महाकाल, भस्म-आरती,
जागरण करते जन
मदिरा-भोग, आस्था आदि
कुमारसंभव और कालिदास
कब तक निभाते साथ ?
कह गए — आएंगे कभी कविता में, स्वप्न में, नींद में
किंतु नहीं, मिथ्या ही सिद्ध हुए उनके उद्घोष
चले आए भीतर धँसकर संग-साथ
अपना सौंदर्यबोध ले
जैसे अलसाई आँखों में चली आती है लज्जा
तभी तो यह बोध तलाशता रहा सौंदर्य
समय की शक्ल में आता रहा समक्ष
जूनी इंदौर के टूटे-फूटे पुलों पर
किशनपुरे की चंद्रभागा नदी के तट
पुरातन देवालयों, दरगाहों, मस्जिदों, खंडहरों,वीरान रास्तों
आदिम वृद्ध इमलियों के तलदेशों, निर्जन टापूओं पर
विचरण करते हर एक चीज़ में वही-वही
सौंदर्य के जाने कितने आयामों के अन्वेषण
अनावरण करते अस्तित्व कि उद्घाटित होता सत्य
अस्तित्व की तलाश भीतर जारी रही दरहमेश
‘हंस’ के साथ करना चाहा दूध का दूध, पानी का पानी
बनारस, कलकत्ता, जबलपुर नक्षत्रों की तरह चमके
लुप्त हुए धूमकेतु-से आकाशगंगाओं के बीच
आकांक्षाओं के बिम्ब दिखें फिर हो गए
एक गहरी-सी ऊब अभाव व संघर्ष ले आता
कर्ण का पिता अभिशापित करता
आशाओं की कुंती को प्रतिदिन
और स्वप्नों के शिशु तिरोहित हो जाते
अंततः नया खून ले आया नागपुर
कोठारिया वह छोटी-सी झनझनाते पायदान
खाली कनस्तर से बजते जल-पात्र
जैसे काँवड़ ढो रहा श्रवण
दिनचर्या की शुरुआत यह
दातुन मुँह में दबाए देखता आकाश
संतरे के मौसम में छौंक दाल या गिलकी-तुरई
साग कोई जंगली …कि मेनर का काढ़ा
टिक्कड़ मोटे-मोटे, दो चार ग्रास ले चल पड़ता
दफ्तर की मारामारी, यंत्रवत दिनचर्या
अखबारनवीसी की दुनिया का आगाज यूँ
वक़्त निकाल इसी में लिखता ख़त-ख़तूत
दोस्तों को नत्थी कर भेजता रिज्यूम
एक अदद छोटी सी नौकरी की चाह
कमबख़्त यह जिद्दी ज़िंदगी!
बलवती होती कहीं टिककर रहने की इच्छा
धूल उड़ाती पवन आक्रोशी, लू चलती,
जलाती त्वचा धूप
भीतर कलेजा इतना पथरीला कि सुट्टा मारना चाहे मन
हड्डियों के ढांचे पर चमड़ी मढ़ी ज्यों काया
गुजरती ट्रैफिक से बेसाख़्ता, बेपरवाह बेनाम
जैसे कांच की रोशनी धुंध चीर नहीं पाती
गुजरता वह मद्धिम-मद्धिम
देखता अपने ही जैसे शरीर फुटपाथिए
भीतर मार्क्स देता दस्तकें, डार्विन सोता
बाहर फ्रायड थपथपाता कंधा
जुंग हिलाता धमनियों-सी जड़ें
कि देर रात लौटने पर भी दीखेंगी यहीं सोते
असुविधा, अभाव में लिथड़ी ये मानव देह
दूभर क्यों हुए टिक्कड़-तरकारी इनसे
कि सुट्टे का स्वप्न भी दूर-दूरस्थ
बाट जोहते पखवाड़ा बीता,न आए नरेश मेहता
क्यूँ खिन्न हुए वाम से नरेशों के मन
क्यूँ नहीं दिख रहा सड़कों पर दु:ख
भला कैसे जा सकेगा कोई अंतस में रमने
भीतर के उस वियावान में
कि सुन सकेगा कोमल तान
अवश्यम्भावी है भीतर भी घेर रहा हो को कुहासा
जैसे धुआँ धुआँ हुआ जा रहा अंतस्थल
क़दमताल करता शुक्रवारी तालाब तक
मिल बैठते दोस्त यार शैलेंद्र, विद्रोही वगैरह
मूंगफली खरीद लौटते उन्हीं रास्ते समर्थ भाऊ के साथ
विचरते खुले आकाश में दो बगुले
कि छोटे भाई का जिक्र छिड़ते ही
विचलित हो जाता मन
वह अधिक सौभाग्यशाली अधिक संपन्न
यहाँ तो स्वयं को परिभाषित करने में निष्फल
ओजवान कलाकार, आखिर क्यों ?
मित्रों के षड्यंत्र और संपादकों की उपेक्षा
क्या अंदेशा है उन निकटतम मित्रों को ?
पांडुलिपि भी खो गई उपन्यास की
जैसे सिर पर चश्मा लगा भूल जाए कोई,
ढूंढता रहे सर्वत्र
प्रकाशकों की कारगुजारियां ओफ्फ…ओह!
सच, डिग्रियों की बैशाखियों के बिना
नहीं चला जाता बुद्धिजीवियों से डग भर
बांध दिए हों जैसे घोड़े के पैर गिरमे से
पंद्रह वर्ष बाद दी फिर स्नातकोत्तर परीक्षा
इतनी अवधि में तो लौट आए थे राघव अयोध्या
परित्याग कर चुके थे वैदेही का
रचा जा चुका था योग वशिष्ठ
पर धिक् हाय-हाय वही द्वितीय श्रेणी
कितनी पृथक पृथक है
साहित्य और समाज की दुनिया
कि इस नींद से जागना कठिनतर कितना
छूट गई पीछे संतरे की नगरी
आया राजनांदगांव कस्बानुमा शहर
नया-नया महाविद्यालय
बड़ा सा मकान हवेलीनुमा
घनी छाँह बरगद की
अतल गहराइयों वाली बावड़ी नापना मुश्किल
मन की भी एक, थाह पाना मुश्किल
जादुई संसार खुलता सामने
अब करीने से दिखा भावी अतीत
फिर कनेरों पर टिका सूरज व्यतीत
याद आती बारहा वह हर घड़ी
दीवारों में जड़ें धँसाता बरगद
इठलाता है अजगरी भुजायें फैला सहस्त्रबाहु-सा
चक्करदार जीनों से उतरता स्वत्व
बावरियों में निहारता स्वमेव
एक अजगर और है जो लीलता वय
एक मदारी प्रतिबंधित करता है किताबें
एक मन भीतर से कहता धिक् समय
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा
जागरण के काल में युग सो रहा
चुनौतियां अब सामने हैं अत्यधिक
और हैं पर्याप्त खुले
अभिव्यक्ति के अवसर भी.
-- मोहन सगोरिया