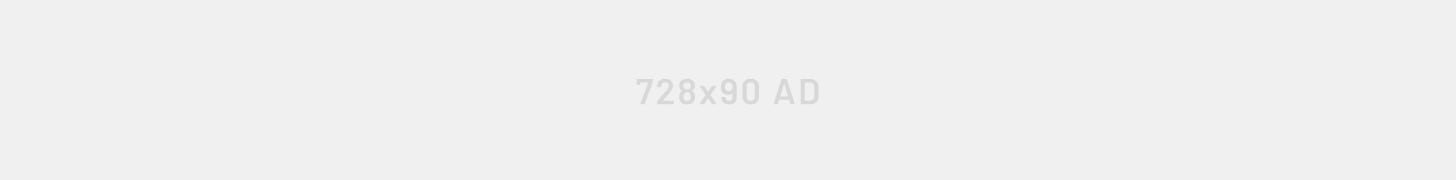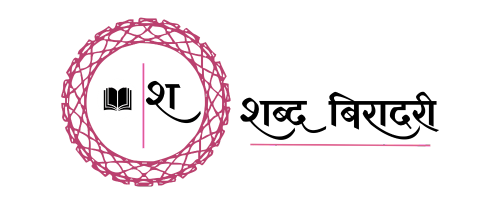कानपुर के मुशायरे
यूं तो शेरी नशिस्ते साल भर होती रहतीं थीं लेकिन हल्के गुलाबी जाड़े शुरु होते ही कानपुर में मुशायरे ज़ोर पकड़ने लगते थे। मुशायरे ऑर्गनाइज़ करने में कई अदबी ऑर्गनाइज़ेशन एक्टिव थे और फाइनांशियल सपोर्ट में कॉरपोरेट्स का अहम रोल था। जिनमें बीआईसी यानि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन के अलावा जे के ग्रुप्स जैसे कई इदारे थे. पापा बीआईसी में थे और उर्दू अदब से गहरे नाते की वजह से इस में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। मुशायरे ऑर्गनाइज़ करने में तब शायद बहुत खर्च नहीं आता होगा. मुशायरे खुले बड़े मैदान में ऑर्गनाइज़ करने का चलन था. आर्गनाइज़र्स के रसूख़ से म्युनिस्पल कॉरपोरेशन, स्कूल कॉलेजों के कम्पाउंड अक्सर मुफ़्त में मिल जाया जाते थे.बीआईसी की मिलों में मुशायरे कैंपस में ही होते थे। हमने फूलबाग, हलीम डिग्री कॉलेज, एल्गिन मिलों के खुले मैदानों में कई मुशायरे अटैंड किए हैं. कानपुर में मुशायरे हमेशा से आम लोगों के लिए खुले रहते थे. वहां ऐसी रवायत आज भी है. कोई एंट्री कार्ड नहीं, कोई पास नहीं! लिहाज़ा सैकड़ों की भीड़ जुटती थी. स्टेज के सामने कुर्सियों की बस एक या दो कतारें ही रखी जाती थीं जो शहर के कुछ नामचीन बुज़ुर्ग लोगों के लिए होती थीं बाक़ी सामईन के लिए मैदान में दरी बिछाई जाती थी और लोग ज़मीन पर बैठ कर मुशायरे सुनते थे. आज के समय की तरह अच्छे कलाम पर तालियां नहीं बल्कि ‘वाह वाह’ और ‘बहौत खूब’ की भरपूर दाद मिलती थी. मुशायरे सामईन की पिछली क़तारों से उठते थे. ज़ाहिर है जिनमें ऊर्दू और शाइरी समझने की भरपूर सलाहियत हुआ करती थी. कानपुर के सामईन बेहद लुत्फ़ अंदोज़ और दिलचस्प होते थे! ख़राब शेर पर भरपूर दाद देकर मंच से शा’इरों को उखाड़ने की भी रवायत थी. कभी कभी इस तफ़रीह के माहौल में बड़े से बड़े शा’इर भी हूट हो जाया करते थे ! आज की तरह सपाट मुशायरे नहीं होते थे कि शोरा हज़रात आएं और आते ही अपना कलाम पढ़ने लगें. शा’इरों के अलावा नाज़िम भी क़िस्से कहानियों और अदबी चुटकुलों से मुशायरों का समां बांध देते थे. फ़िराक़ साहब के बारे में तो मशहूर था कि वो कलाम के पहले ज़रूर कोई चुटकुला सुनाते जो अमूमन शाइरों से जुड़ा होता था. मंच पर शाइरों के बीच ही नहीं, शा’इर और सामईन के बीच भी खींचतान चलती थी. आज की तरह शा’इरों के लिए मंच पर कभी कोई तय समय नहीं मुकर्रर होता था. शाइर अगर जम गया तो सामईन उसे उठने नहीं देते थे.
अभी हाल में आकाशवाणी का एक मुशायरा अटैंड किया तो हैरत हुई कि वक्त की कमी बताते हुए हर शायर को शुरू में ही महज़ सात मिनट का समय एलॉट किया गया! अब बताइए सात मिनट में कोई शा’इर कैसे अपने कलाम को जस्टीफ़ाई कर सकेगा? उस दौरान मुशायरों में दो दौर लाज़िम तौर से होते थे. पहला दौर अगर रात ग्यारह साढ़े ग्यारह ख़त्म हुआ तो डेढ़ दो घंटे का दूसरा दौर सीनियर शायरों के लिए मुकर्रर रहता था.
तब शायर भी मंहगे नहीं थे. बड़े शा’इर साढ़े सात सौ – हज़ार में ही आ जाते थे. शा’इर रेल या बस से चलते थे. शा’इरों को बड़े अदब से घरों में ठहराने के इंतज़ामात होते थे. शा’इर ठहरते भी क्या थे बस सीधे मुशायरों में आते और देर रात उनको घरों में लिवा लिया जाता. वहां भी सुबह होने तक महफ़िलें सजती . सुबह होने पर सबको स्टेशनों पर छोड़ दिया जाता. हां फिराक़ साहब जैसों को इलाहाबाद गाड़ी भेज कर बुलवाना पड़ता . उनका मेहनताना भी दोगुना हुआ करता था.
एक दफ़ा एल्गिन मिल -2 के मुशायरे में फ़िराक़ साहब अपना कलाम ख़त्म करते ही वालिद का घर का नाम लेकर बोले,’रज्जन कहां हैं? हमारी वापिसी के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करें और दो हज़ार का जो वादा किया है उसे कैश दें!’ पूरा मैदान ठहकों से गूंज गया था!
अब तो मुशायरों का पूरी तरह से कॉरपोरेटाइज़ेशन हो गया है! अभी हाल में एक शा’इर मिले . शा’इर क्या हैं कभी किसी समय एक न्यूज़ चैनल में कुछ करते थे फिर कुछ बड़े शा’इरों की ख़िदमत करते करते शा’इर बन गए. घटिया किस्म के शेर कहते हैं. उनके ज़्यादातर अशआर अंग्रेज़ी या दूसरी ज़ुबानों के पोएट्स के तर्जुमें होते हैं. हमसे मिले तो बोले,’दुबई और मिडिल ईस्ट से बुलव्वा है! पूरे तीन हफ़्तों का प्रोग्राम है!’ हमने पूछा,’ कमाई तो ठीक ठाक हो जानी है ना?’ तो जवाब आया,’ जावेद अख़्तर के बराबर चार्ज करता हूं!’ अब बताइए कहां ‘सुभाष बोस’ और कहां ‘** घोष’!!
मुशायरों को लेकर अब तो ‘तंज़ीमें’ बन गई हैं, बाक़ायदा अखाड़े खिंच गए हैं!! मुशायरों के आर्गनाइज़र का नाम भर पढ़ कर आप पूरी फ़ेहरिस्त को ख़ुद जान जाएंगे! एक सेट ऑफ़ पोएट्स होते हैं. ऐसा छोटे कस्बों से लेकर दिल्ली शहर के बड़े सालाना मुशायरों में होता है.नाम लेने की ज़रूरत नहीं!! यानि पूरा माहौल ‘यू स्क्रैच माई,आई स्क्रैच योर्स’ वाला है! इस माहौल को बनाने में ख़ासा रोल सो कॉल्ड ‘अलमबरदारों’ का भी है. एक दफ़ा दिल्ली के T3 एअर पोर्ट पर हम कहीं जाने के लिए थे तो देखा एक पूरा ‘गोल’ मौजूद है. मठाधीश आराम कुर्सी पर पसरे पड़े थे और चालीस पार ‘नौजवान’ या ‘उभरते’ हुए ख़िदमत में उनका झोला उठाए फ़्लाइट का अपडेट दे रहे थे!
आइए अब फिर 70 और 80 की दहाई के कानपुर चलते हैं! उस दौर में जब मालूम होता था कि कोई मुशायरा ऑर्गनाइज़ किया जाने वाला है तो तमाम उर्दू पसन्द लोगों के बीच में एक जश्न का माहौल बन जाता था. इनमें लोकल शायरों की बड़ी ज़िम्मेदारी होती थी . आज की तरह तब शा’इरो के कोई ‘गोल’, कोई ‘कॉकस ‘ नहीं होते थे. मुशायरे की कमेटी आपसी सलाह मशविरा से शा’इरों को इन्वाइट भेजती थी.
जब कभी पापा किसी मुशायरे में इन्वाल्व होते तो कई दिन पहले से ही शाम को घर पे लोकल शा’इरों की आमद शुरू हो जाती. बड़ी खुशी से ख़बर दी जाती थी कि फलां फलां ने आना कन्फर्म कर दिया .
हमनें उर्दू के शा’इरों को हमेशा ग़रीबी के आलम में ही देखा है। ज़्यादातर साईकल पर चलते थे। थोड़े हैसियत दार रिक्शा कर लेते थे। तब मोटर किसी के पास नहीं होती थी। शायद यही वजह है कि हमारे ज़हन में आज भी उर्दू शा’इर की इमेज एक ग़रीब मजबूर इंसान की ही बस गई है। जब शा’इरों को गल्फ़ से न्योते आने लगे तब कुछ हैसियत ज़रूर बढ़ गई। नूर साहब बताते थे कि गल्फ़ कंट्रीज़ की एक विज़िट में 50 – 60 हज़ार की बचत हो जाती थी। लेकिन ऐसा बहुत बाद के सालों में शुरू हुआ। और ये दौरा तब साल में एक बार ही लगता था।
मुशायरों में हमारी दिलचस्पी घर में होने वाली नाशिस्तों से पैदा हुई। हालांकि उनमें हम भाइयों का रोल चाय, पानी और पान पहुंचाने भर तक महदूद रहता था। हां कभी कभी टेप रिकार्डेड पर शायरों को रिकॉर्ड करने की ज़िम्मेदारी दी जाती थी। टेप रिकॉर्डर तब माइक वाला था। जो शा’इर पढ़ता था उसके आगे सलीके से माइक खिसकना होता था। हम घर में तब सबसे छोटे थे। ख़ाली भी थे। पढ़ाई या स्कूल होमवर्क से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता था तो लिहाज़ा पापा हमें अपने साथ मुशायरों में ले जाने लगे । हमारे साथ एक बात और थी कि हमें सुने हुए शेर बहुत जल्दी याद हो जाते थे। ये सिलसिला आजतक क़ायम है। मुशायरे के बाद अक्सर जब पापा हमसे पूछते की फ़लाने ने क्या पढ़ा और हम बता देते तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती थी।
तो पापा के साथ जब मुशायरों में जाते तो हमारा काम पनडब्बा और पानी की बोतल संभालना रहता था। हां मुशायरों की जगह गाड़ी पार्क करवाने और निकलवाने की ज़िम्मेदारी भी रहती थी। पापा अपने पर्सनल काम मे अपनी गाड़ी खुद ले जाते थे। दफ़्तर की गाड़ी ऑफिस से आते ही छोड़ देते थे। ड्राइविंग भी उन्होंने बहुत बाद में सीखी थी। वो भी शौकिया। बहुत ऐतिहात से गाड़ी चलाते। हॉर्न इतना बजाते की आगे वाला शर्मिंदा हो जाता। जब कोई हॉर्न पे भी ना हटता तो खिड़की से सर निकाल कर कहते , ‘ख़ुदा के लिए हट जाओ । नई नई चलानी सीखी है। कहीं लग गई तो ग़ज़ब हो जाएगा!’ उनके दफ़्तर एल्गिन मिल के पास ही एक पेट्रोल पंप था जहां पर ही पेट्रोल भरवाते। महीने का हिसाब होता था। पांच लीटर से ज़्यादा एक बार में कभी पेट्रोल नही भरवाते। उनका मानना था कि पेट्रोल ‘उड़’ जाता है।
पापा बैठते एल्गिन मिल नम्बर -01 में थे लेकिन बीआईसी की दो और मिलों, एल्गिन मिल नम्बर-02 और कानपुर टेक्सटाइल मिल में भी उनका दख़ल रहता था। कानपुर शहर में जो कोई थोड़ा बहुत शेर कह लेता या गाने का हुनर रखता, उसको इन मिलों में कोई ना कोई नौकरी दे देते। इस तरह उनके चाहनें वालों में शायरों की लंबी चौड़ी फ़ौज थी।
तो उस दौर में कानपुर में जो शायर थे उनमें नुशूर वाहिदी,ज़ेब ग़ौरी, फ़ना निज़ामी, क़ौसर जायसी, जलील कानपुरी, शायर फ़तेहपुरी, कमाल जायसी के नाम (जो अभी ज़हन में आ रहें हैं) थे। तब मुशायरों में शायरात की शिरकत कम या नहीं के बराबर देखने को मिलती थी. ऐसा भी कहा जाता था कि उनके उस्ताद उन्हें कलाम लिख कर देते थे जिन्हें वो तरन्नुम में पढ़ती थीं. हमारी स्टूडेंट लाइफ़ में एक शायरा थीं बरखा रानी जिन्हें अक्सर अकेले मर्द शोरा के साथ मंच पर देखा जाता था. आज के दौर में तो ख़्वातीन बहौत बढ़ चढ़ कर कह रही हैं और मर्दों मे आगे निकल रही हैं. अच्छी बात ये है कि इनमें हिन्दू ख़्वातीन की तादाद अच्छी ख़ासी है जिन्होंने ऊर्दू ज़ुबान को बाक़ायदा अपनाया है!
अभी कहीं पढ़ रहे थे कि कानपुर में कवि सम्मेलन की रवायत 1923 में गया प्रसाद सनेही ने मुशायरों की मुख़ालफ़त में शुरु की. सनेही जी ने मुशायरों के विरोध में वर्ष 1911 में कानपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की . इसमें खड़ी बोली के कवियों को जोडऩा शुरू किया. नौ साल तक इसके जनरल अधिवेशन हुए.साल 1921 में बड़ा अधिवेशन किया गया तब कवियों ने काव्य पाठ किया और कवि सम्मेलन की परंपरा चल पड़ी.सनेही जी ने सनेही मंडल की स्थापना की इसमें कई जिलों के कवियों के नाम जुड़े. सनेही जी ने ऐसा इसलिए किया था कि कानपुर में वो दौर मुशायरों का दौर था और हिन्दी के कवियों को सुनने के लिए ऑडियेंस नहीं जुटती थी.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे वालिद के साथ के होते थे वो फ़िराक़ साहब को लेकर एक क़िस्सा सुनाते थे. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुशायरे में एक बार फ़िराक़ साहब और यूनिवर्सिटी के ही उनके एक हिन्दी कवि एक साथ मंच पे थे. ऑडियंस बार उन कवि का नाम लेकर आवाज़ें लगा रही थी. फ़िराक़ साहब से ये बर्दाश्त ना हुआ. उन्होंने माइक का रुख़ अपनी तरफ़ कर के कहा,’ क्या **** **** लगा रखा है! जैसे मोटा हाथी मूते घल घल घल घल घल घल!’ पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है पर फ़िराक़ साहब बदज़बान तो थे ही!
बहरहाल ये हिन्दी – ऊर्दू का मसला धीरे धीरे ख़त्म हुआ और ख़ैर मनाइए कि मुशायरे और कवि साम्मेलन एक मंच पर होने लगे और इसे ‘गंगा – जमुनी’ नाम दिया जाने गया!
कानपुर के मुशायरों में बाहर से आने वालों में उस दौर के कुछ बड़े नाम होते थे जिनमें फिराक़ साहब, कैफ़ भोपाली, बशीर बद्र और बाद में कृष्ण बिहारी नूर शामिल थे. एक बार हमने मजरूह साहब को भी सुना था . राहत इंदौरी आते थे लेकिन इस दौर में वो उस सामईन के बीच उनका वो मुक़ाम नहीं था जो उन्होंने बाद में हासिल किया.कमोबेश वसीम बरेलवी और साग़र आज़मी भी इसी मयार के माने जाते थे . नुशूर वाहिदी साहब को हमनें मुशायरों में नहीं देखा. कानपुर के लोकल नौजवान शायरों से मुशायरों का आग़ाज़ होता था . कमाल जायसी नौजवान थे और अक्सर मुशायरों को कंडक्ट भी करते थे. एकाध आलमी मुशायरों को मलिकज़ादा मंसूर को भी कंडक्ट करते सुना . कानपुर के एक शा’इर थे फ़ना निज़ामी जिनके बड़ी सुफ़ेद दाढ़ी थी और वो तरन्नुम में गिटकिरी लगा कर कलाम पढ़ते थे.ज़्यादातर तरन्नुम में पढ़ने वाले ‘नेज़ल’ होते थे. पता नहीं क्यों आज भी कुछ ऐसा ही है! शा’इर भी दो कैटगरी के होते थे. एक मैदानी जलसों में तरन्नुम वाले जो मुशायरे लूट लिया करते थे और दूसरे अदबी नशिस्तों में तहत में पढ़ने वाले! बशीर बद्र जब शुरू के कुछ अशआर तहत में पढ़ते तो सामईन से ‘ तरन्नुम – तरन्नुम’ की आवाज़ें उठने लगतीं.
अवेलिबिल सोर्सेज़ से तो यही पता लगता है कि हिन्दुस्तान में मुशायरों की शुरुआत तरन्नुम से हुई . लेकिन ‘ख़ुदा-ए-सुख़न’ मीर तक़ी मीर तो डेफ़निटली तहत में पढ़ते होंगे जबकि मिर्ज़ा ग़ालिब तरन्नुम में! पता नहीं क्यों ऐसा माना जाने लगा कि सीरियस पोएट्री को तहत में ही पढ़ना बेहतर है! कृष्ण बिहारी नूर बताते थे कि पहले वो तरन्नुम में पढ़ते थे लेकिन फ़िराक़ साहब के कहने पर तहत पे आ गए और तरन्नुम में पढ़ना बिलकुल छोड़ दिया! लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब के तरन्नुम का जवाब नहीं था! वालिद बताते थे कि जब जिगर पढ़ने आते तो सारा ज़माना उनके साथ हो लिया करता था!!
हमने वालिद साहब के साथ कानपुर के अलावा उन्नाव, लखनऊ, फ़ैज़ाबाद और सुल्तानपुर में भी मुशायरे अटैंड किए हैं. वालिद तो हर साल डी.सी.एम शंकर शाद मुशायरा अटैंड करने दिल्ली आते थे. मुशायरों को लेकर सामईन का जो ज़ौक लखनऊ – कानपुर में देखा कमोबेश वहीं छोटे शहरों और क़स्बों में था.
मुशायरों के बाद भी उनके क़िस्से कहानियों का ज़िक्र बाद तक चलता रहता. मसलन फ़ूलबाग मुशायरे में देर से आने पर कैसे मजरूह सुल्तानपुरी साहब को अंदर जाने से रोका गया जबकि वो बार बार कहते रहे कि को मजरूह सुल्तानपुरी हैं! या हलीम कॉलेज के मुशायरे में दिलीप कुमार साहब के आने की ख़बर से इतनी भीड़ जुट गई कि उन्हें बुर्क़े में अंदर आना पड़ा! वगैरह वगैरह!! अब ये सब सच था या चंडूख़ाने की बातें, इसका कोई इल्म नहीं!
कानपुर का एक मुशायरा रसखान सोसाइटी का है जो पिछले 34 सालों से होता आ रहा है. इस मुशायरे की शुरुआत कानपुर के मशहूर सूफ़ी संत हुज़ूर शाह मंज़ूर आलम साहब ने की थी. इस साल पहली बार हमें इस मुशायरे में शिरक़त का मौका मिला. हमने अब तक दर्जनों मुशायरे अटैंड किए होंगे पर इतना क़ामयाब मुशायरा नहीं देखा. ऐसा हुज़ूर शाह मज़ूर आलम साहब के आशीर्वाद की वजह से ही मुमकिन है! हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी तहसीन मुनव्वर के लफ़्ज़ों में, ‘ये चमत्कारिक मुशायरा होता है। इस में रात भर श्रोता आते रहते हैं जैसे किसी सूफ़ी संत का आदेश उन्हें खींच लाता हो!’
अगर आपने अभी तक रसखान का मुशायरा अटैंड नहीं किया है तो इस बार कानपुर ज़रूर पहुंचिएगा ! इस मुशायरे को सूफ़ी साहब के बेटे और हमारे दोस्त मासूम अली ख़ान और कानपुर के जाने माने शाइर ज़ीशान नियाज़ी आर्गनाइज़ करते हैं. 2024 के इस मुशायरे की इत्तेला हम ही आप तक पहुंचा देंगे!