
“सुनो ना! चलो सोचना-सोचना खेलते हैं।”
“पहले तुम!”
“अच्छा चलो मान लो एक ट्रेन, एक शहर में पहुंचा दे तुम्हें, रिक्शे-तांगे, सबके सोये हुए होने के समय पर!”
“अब तुम दूधिया रौशनी वाली लैम्पपोस्ट के नीचे वाली बेंच पर बैठे सुबह को अगोरते हो! प्लेटफार्म के पीछे यूकिलिप्टस के पेड़ों का झुरमुट है। दस मीटर की दूरी पर हिचक-हिचक कर रोता हुआ पीले रंग का खिया चुका वेटिंग रूम है…जो काई व सूखी बेल लतरियों से बजबजाया हुआ है।”
“अब तुम्हें लगता है कि इन यूकिलिप्टस के झुरमुटों के सहारे इस भूरी बेंच को कभी भी पहचाना जा सकता है।”
“पर दिक्कत यह है कि झुरमुट वाले यूकिलिप्टस खंड-खंड में पूरे प्लेटफार्म की पृष्ठभूमि में फैले हुए हैं।”
“तो ठीक है न, तुम लैम्पपोस्ट के सहारे बेंच को पहचानोगे!”
“पर सारी बेंचे तो लैम्पपोस्ट की रौशनी तले ही हैं।”
“लेकिन…लेकिन यह इकलौती बेंच है जो लैम्प पोस्ट के नीचे है, और जिसकी पृष्ठभूमि में है सफेद ऊँची टहनियों वाला यूकिलिप्टस।”
“यानि कि, अब भूरे रंग वाली बेतहाशा बेंचों के बीच यूकिलिप्टस बनाम लैम्प पोस्ट वाली भूरी बेंच को कभी भी पहचाने जाने में कोई गुंजाइश शेष नहीं रहती।”
शहर को पहचानने की शुरुआत का रोमांच ‘उपभोग के सीमांत नियम’ की तरह लागू होता है और अंततः रहनवारी के आखिरी दिन जब तुम अपने बोरिया-बिस्तर समेत लौटने वाले होते हो (खत्म ना रे) स्थगित होता है, बेतहाशा भूख में पहली रोटी की संतुष्टि की तरह।
उन दिनों चंदा मामा यूँ टंगते थे आसमान में जैसे दूसरी क्लास के बच्चे ने अपनी ड्राइंग बुक में क्रमशः लेमन, येलो, और नेवी ब्लू से चाँद और बादल को रंग कर आसमान में फैला दिया हो। दिन बर्फ की तरह सरक जाता था उँगलियों से। पकी हुई पुरानी हवेली की छत की रेलिंग पर बैठने से भी रेलिंग नहीं टूटती थी और स्टील के कप से निकलने वाली सोंधी भाप के बीच शाम बीत जाती थी। शाम पीली थी, और जब सामने वाली ईमारत की बाहरी मटमैली पीली दीवारों पर उतरती थी तो संतरे जैसे हो जाती थी…जानदार, रसीली।
इन्हीं दिनों “व्योमकेश बख्शी” अखबार की कतरनों से “कांटे से कत्ल करने वाले” कातिल का पता छानता था। वो जेम्स बाँड से आगे का जासूस था, जो धोती कुरता पहनता था और रहस्यमयी यारकी वाली मुस्कुराहट के साथ सफेद खाकी वर्दी वालों से बतियाता था।
‘रजत कपूर’ अच्छा अभिनेता था, व्योमकेश बख्शी एक शातिर जासूस था। जासूसी का खेल चलता जाता था और रात गहराती जाती थी। रात काली थी, पर शाम के घिरते धुंधलके के बीच काली होती परछाईयों, घर के आँगन और बरगद की पत्तियों से कम काली थी।
चीजें तुरंत छूटी हुई ट्रेन की रफ्तार जैसी आरम्भ होती हैं और खत्म होती हैं मौन पर। नितांत अपरिचित सीने में अटका हुआ मौन…जो अटता भी नहीं और निकलता भी नहीं।
अब एक छोटी सी कल्पना और! कई-कई हजार साल बाद, जब एलियन्स पृथ्वी पर छुट्टियाँ मनाने आया करेंगे, मानव सभ्यता के उस दौर में भी हमारे-तुम्हारे जैसे सोचने वाले चिरकुट लोग, तमाम विकास यात्राओं के बाद भी चिरकुट ही बने रहेंगे! मान लोग खूब सर्दी वाली रात में तुम अपनी रजाई में पड़े हो किसी के बाहों के तकिये पर सोये हुए हो।
बेवजह ही अचानक उचटी हुई नींद के बीच तुम्हें वो छूटा हुआ छोटा सा शहर याद आता है और याद आता है। परिचय की शुरुआत का निचाट-तन्हा स्टेशन। तुम अब के अब पहली ट्रेन पकड़कर पहुंचना चाहते हो वहाँ।
सोचो वहाँ क्या होगा?
इतना घना कुहासा, इतना घना कि लैम्प पोस्ट ढिबरी की मानिंद टिमटिमा रहा होगा। प्लेटफार्म को बड़ा करने के अभियान के तहत पहला काम हुआ होगा, यह, कि, यूकिलिप्टस के पेड़ काटने पड़े हैं।
आधा अँधेरा, आधा कुहासा, और थोड़ी से मरियल पीली रौशनी के बीच टटोलते हुए तुम बेंच से टकरा जाते हो। महसूसते हो उसे हाथों से। कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे पहले तुम्हारी नजर पृष्ठभूमि पर जाती है। तमाम अँधेरे के बीच भी तुम्हें दिख जाते हैं यूकिलिप्टस के ठूँठ!
अब आश्वस्त हो तुम!
अब देखो तुम्हारा पागलपन!
तुम बैठना चाहते हो इस बेंच पर पहले की तरह, टांग पर टांगें चढ़ाकर, या अधलेटे होकर, या कि चाहे बेंच की बाँह पर पीठ का भार देकर! चाहे जैसे पर पहले की तरह, पहली बार की तरह! पर देखो, तुम तो भूल गए हो पहली बार जैसी कोई भी चीज।
“जो कार्य बहुत लम्बे समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है, वह भूल जाता है। इसी को अनभ्यास का नियम कहते हैं।”
(Douglas & Holland)
रोज रात को सोते हुए उस औरत को हमेशा से ऐसा लगता था कि जब वह सोकर उठेगी तो आश्चर्यजनक रूप से रास्ते पर कई तहों तक जम चुकी काई की परत उखड़ चुकी होगी जिनपर फिसल-फिसल कर लगातार वह गिरती रही है। ऐसा कुछ हो जाने की सम्भावना रोज जैसी ही तकरीबन नगण्य सी होती थी। पर उसे दिन-ब-दिन लगता था कि संभावना प्लस वन की रफ्तार से भागती थी।
अब ऐसे में दो बातें थीं। पहली, कि ऐसा सचमुच हो जाए, हो जाए तो फिर क्या हो?
हो यह सकता था कि जो गोलियां पुलिस वालों की बंदूकों से निकल कर निरीह गोश्तों में धंस चुकी थीं, वे उन गोश्तों से निकलकर वापस बन्दूक की नली में फिट हो जाएँ। गोश्त जो बारूद की जलन से निर्जीव हो चुके थे, पुनः सजीव होकर अपने-अपने कामों पर लग जाते।
मसलन धरने पर बैठते, नारे लगाते, चावल की खेती करते शाकाहारी गोश्त। बंदूकें थाने की सीलन वाली दीवारों से टिकी चुपचाप पड़ी होतीं। जिनके ट्रिगर वाले हिस्से पर थक्का-थक्का धूल जमी होती।
और लालझंडी वाला वह तानाशाह मुख्यमंत्री अपनी औद्योगिकीकरण की नीति पर इतरा सकता था,
“धोन्यो धान्ये पुष्पे भोरा
आम देर एई वशुंधरा!”
ऐसा न होने की स्थिति में दूसरी संभावना का अर्थ तवे पर रोटियाँ पलटने के क्रम में उँगलियों के सिरों पर भाप का लग जाना भर होता था। मजेदार बात यह कि भाप लग जाने पर उँगलियों का झटकना तक नहीं होता था, यानि कि इस कदर अभ्यस्त।
बगल कमरे से जबर्दस्ती आती हुई फुल वाल्युम में समाचार की आवाज के बीच जब कभी मिर्चें तेज भुन जाती थीं तो देर तक छींक बनी रहती थी। यानि कि दो मुंहें स्टोव के एक चूल्हे पर रोटियाँ सेंकती औरत को चूल्हे के दूसरी तरफ ठीक समय व अंदाज से कड़ाही में मिर्च का फोरन भी देना पड़ता था।
औरत इस एक साथ दो चीजों की कला में निपुण कतई नहीं थी, तो कुल जमा यह कि औरत को हमेशा स्लेटी मूड में रहने की आदत पड़ गयी थी।
वो लड़की जैसी औरत थी, गो कि उसे औरत सिर्फ इस वजह से कहा जा सकता था क्योंकि उसकी मांग में दपदपाता सिंदूर था, हाथ में शंख-पोला था और वो सलवार कुर्ता न पहनकर साड़ी पहनती थी। औरत की आँखें उसके चेहरे से बाहर भागी हुई मालूम होती थीं। मधुबनी पेंटिंग्स सरीखी खींची हुई आँखें और पूरी जिंदगी में यही ऐसी एक चीज थी जिनपर औरत नाज कर सकती थी।
औरत को हमेशा भय लगा रहता था कि अगर वो ज्यादा बोलेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास… “कि… कि…” के बाद कुछ नहीं बचेगा। सो औरत “डॉट” लगाकर आधी जगह (सम्भावनापूर्ण) खाली छोड़ देती थी।
मसलन आदमी के सेकेंड हाफ में घर वापसी का समय शाम सवा चार होता था। औरत दरवाजे की सिटकनी खोलकर, दरवाजा हल्का सा भिड़ा भर देती थी।
आदमी सायकिल की बायीं तरफ हैंडिल में सब्जियों से भरा झोला लटकाए क्वार्टर के परिसर में प्रवेश करता था।
औरत खुद झोला थाम लेती थी।
“टमाटर??” औरत मुँह से नहीं पूछती थी।
“बड़ी महँगा हथी, बीस रुपिया किलो!” आदमी को मुंह खोलकर बताना पड़ता था।
औरत पूछ सकती थी कि “कटहल कौन सस्ता हलिए?” पर औरत “डॉट-डॉट-डॉट” से भरा एक खाली स्थान चिपका देती थी साइकिल की हैंडिल पर!
क्वार्टर के अंदर साइकिल प्रविष्ट कराता आदमी सहसा ठहर जाता था चौखट पर ही।
आदमी फिर साइकिल को वापस मोड़कर बागन में लाता था, और आम गाछ से टिकाकर खड़ा कर देता था, खुद अंदर चला जाता था।
औरत जानती थी कि आदमी ने उस डॉट्स वाले खाली स्थान को साइकिल पर से उकाच कर फेंक दिया है।
ये उकाच देना औरत को बेतरह तकलीफ देता था। औरत सोचती थी कि वो किस दुकान से लाकर गोंद लगाये कि आदमी “उस डॉट्स वाले खाली स्थान को” उकाच नहीं पाए। और जो खाली स्थान आदमी को अंदर ही अंदर खूब-खूब मथ दे। इतना मथ दे, इतना…कि आदमी परेशान होकर खुद ही उस खाली स्थान पर कुछ रख दे! जैसे कि… “क्या? बोलो! हाँ! तुम!” आदि-इत्यादि।
औरत जानती थी कि आदमी अप्रैल की दोपहरी से उकता कर आएगा तो सीधा घुसेगा नहानघर में और साबुन घिस-घिस के नहाएगा। आदमी चौह्बच्चा से मग भर-भर के पानी निकलता था और देह भर का साबुन छुड़ाता था। देह का साबुन छुड़ाने के क्रम में बहुत सारा साबुन चौह्बच्चा में भी चू जाता था। बाद में टंकी में झाँकने पर पानी के ऊपर सफेद-सफेद बहुत सारा कुछ तैरता नजर आता था। औरत को इससे उबकाई आती थी। इसलिए औरत, आदमी के आने के पहले ही बाल्टी भर पानी टंकी से निकाल कर रख देती थी।
आदमी समझदार था, सब बूझता था। इसलिए बाल्टी के सारे पानी से कपड़े धो डालता था, फिर साबुन घिस-घिस के नहाता था। औरत किरोसिन के लहराने वाले स्टोव पर चाय चढ़ा देती थी। वो पिछले नौ महीने से एक ही जगह पर स्टोव रखकर चाय बनाती रही थी। लगातार स्टोव के धुएँ से रसोई की वह दीवार चीकट-काली पड़ चुकी थी…औरत ने उसे साफ करने की बहुतेरी कोशिश की पर दीवार साफ नहीं हुई।
आदमी चाय पीने से पहले भर गिलास पानी पीता था। निरा छूछा पानी। हालाँकि औरत ने पहले पहल पानी के साथ गुड़ और बताशा जैसी चीजें देने की कोशिश की थी, पर कलकत्ता दूरदर्शन पर बांग्ला खबरें सुनता आदमी उसी बेपरवाई से बताशा को अनदेखा कर पानी का गिलास थाम लिया करता था, जिस बेपरवाई से वो टमाटर को अनदेखा कर कटहल मोल लेता था।
आदमी जब भी इस औरत को देखता था तो लगातार कई जन्मों से जीते रहने की एक रस उबाहट उसके अंदर भर जाती थी।
आदमी चाय के ठंढे होने की भी प्रतीक्षा नहीं करता था और मोटी-मोटी भाप को परे धकेल कर बाकी चीज अंदर उलीच लेता था। गर्म-तरल चीज छाती में जाकर और गर्म हो जाती थी, अंदर फट-फट कुछ जलाती थी। आदमी की छनछ्नाहट बाहर नहीं आती थी। आदमी छाती जलती चीज के नीचे उतरने की प्रतीक्षा कर सकता था। जब चाय क्रमशः छाती से होती हुई पेट में रिस-रिस कर उतर जाती थी, आदमी के लिए कुछ जाहिर करना जरूरी हो जाता था। आदमी, कप को झन्न से रख देता था नीचे। आदमी साइकिल गेट से बाहर निकाल ले गया…औरत को दुःख था कि उसने अच्छे खासे क्वार्टर को सरायघर बना डाला था।
आसनसोल स्टेशन के पीछे दो कतारों में बारह-पन्द्रह क्वार्टर्स थे। ये क्वाटर्स सबसे पुराने मॉडल के थे जिनकी छतें सीधी-सपाट न होकर, बीच के किसी महीन सहारे दोनों तरफ से तिरछी थीं।
क्वाटर्स का एक कतार के सामने कोलतार की लम्बी, काली सपाट सड़क होती थी। पर एक फर्क होता था। क्वार्टर्स नीचे होते थे, सड़कें ऊपर होती थीं। सो क्वार्टर्स से निकलकर सड़क पर जाने के लिए चार या पाँच पायदानों की सीढ़ियाँ होती थीं। क्वार्टर्स के बागानों में उगे हुए आम, अमरुद, बेल व नीम की पत्तियाँ कोलतार की सड़क पर फैली रहती थीं। और बरसात भगाने वाली तेज हवा के बीच इधर-उधर उड़ती रहती थी।
दिनभर गर्म धूल हवा के साथ मिली उड़ती रहती थी। लोग-बाग लाल लाइनिंग वाली गमछियाँ माथे पर ओढ़कर खूब तेज साइकिल भगा ले जाते थे। मजदूरनियाँ पीच वाली सड़क पर ना चलकर सड़क के किनारे आवारा उगे हुए भूरे-पीले घासों पर चलती थीं। नंगे पाँव उन्हें लम्बी दूरी तय करनी होती थी। दूर-दूर तक बस काले ताड़ गाँछ के ठूँठ थे, नंगे मैदान में पीली भूरी घास थी। पाँच पायदानों वाली सीढ़ियाँ धूप में तपती रहती थीं, पर फटती नहीं थीं। सांझ के समय जब औरत इन सीढ़ियों पर पानी डालती थी तो अजब सी महक के साथ पानी गायब हो जाता था। औरत दो-चार बाल्टी पानी और डालती थी। धीरे-धीरे बरामदा और सीढ़ी पानी पीना बंद कर देते थे, और पानी ठहर जाता था। इन्हीं तपती सीढ़ियों वाले क्वार्टर के दो कमरों में से पहले कमरे में औरत-आदमी सोते थे। कमरे में चार पतले-पतले खानों वाली रैक थी, जिनमें “ट्रेन की समय सारणी” और “पांचजन्य” जैसी अवांट-बवांट पत्रिकाएँ ठुंसी होती थीं, चीनी मिट्टी के हाथियों का एक जोड़ा रखा होता था, बाकी रैकें खाली होती थीं।
एक चौकी थी। दीवार से टिकाकर खाट रखी होती थी और बाजू में ही रखा होता था छोटा सा स्टूल। क्वार्टर का एकमात्र पंखा स्टूल पर था।
टेबलफैन का जब स्वीच ऑन होता था, तो वह एकबारगी खूब तेज आवाज में घरघराता था। फिर बेआवाज बिजली की आपूर्ति होते रहने तक हनहनाता रहता था। रात के खाने के बाद आदमी बाहर खड़ी साइकिल को उठाकर अंदर बरामदे में रख देता था।
औरत फिर अपनी खाट बिछा लेती थी।
सुबह, औरत जब नाश्ता-चाय बनाती थी तो आदमी कंघी से बाल काढ़ता था।
औरत पहला कमरा पोंछ लेती थी। फर्श अभी गीला ही होता था, कि आदमी अंदर बरामदे में खड़ी साइकिल बाहर निकाल ले जाता था। गीले फर्श पर साइकिल के पहियों के और पंजों के निशान बन जाते थे।
हांफती हुई औरत अपनी थकान से दोगुना थक जाती थी। औरत चुपचाप बाल्टी के पानी में पोंछन डुबकाती थी और निचोड़ कर फर्श दोबारा से पोंछ लेती थी।
तो आदमी, चौकी पर सोता और औरत रस्सी की उरीची हुई खाट पर। रात में औरत को बड़ी तेज की गर्मी लगती थी। औरत अपने बिस्तर पर पानी छिड़क लेती थी और खाट के पास बाल्टी में पानी रख कर सोती थी।
गहरी रात में औरत हौले से उठकर बाल्टी के पानी से अपने हाथ-पैर भिंगोती थी। हालाँकि ऐसा औरत बहुत एहतियातन करती थी, पर, हल्की सी खट की आवाज हो ही जाती थी। आदमी जैसे,ऐसे ही, किसी क्षण में जाग जाने के लिए ही सोता था। वो तकिये के नीचे टॉर्च टटोलता था और फिर “उंहऽऽऽ” की आवाज कर, करवट फेर लेता था। औरत भीषण अपराधबोध में मुब्तिला हो जाती थी। औरत साँस दाबे चुपचाप पड़ी थी। उसके पास हिसाब भी नहीं था कि उसने इन स्थितियों से बचने के लिए जाने कितनी बार न रोके जा सकने वाले आवेगों को सुबह तक के लिए स्थगित किया था।
औरत फिर खाट के दूसरी तरफ से उतरती थी, और कमरे की इकलौती खिड़की से लगकर खड़ी हो जाती थी। इसी खिड़की से बाहर जबरन बनाया हुआ एक रास्ता गुजरता था जिसपर पीली रौशनी वाली स्ट्रीट लाइट जगमगाती थी।
स्ट्रीट लाइट की रौशनी का कुछ हिस्सा कमरे में भी छिटका था। आदमी गंजी और पायजामा पहने तकरीबन नींद में ही सोता था। बाई करवट में बड़े अंदाज से, चौकी की आधी जगह छोड़कर। औरत का एकदम से मन करता था कि, वो बाकी बची आधी जगह पर जाकर सो जाए, पर आदमी की छाती पर जंगल की तरह उगे हुए काले बालों से उसे बड़ी घिन्न होती थी।
एक बात जो खिड़की के पास खड़ी औरत को कभी समझ नहीं आई कि आदमी ऐसे कैसे सो लेता है, कि सुबह उठने पर, उसके बिस्तर पर एक शिकन तक नहीं होती जबकि औरत का बिस्तर यूँ हुआ रहता जैसे उसे किसी ने बुरी तरह उजाड़ दिया हो।
……………………………………………………………………………………
औरत परेशान हो गई थी।
कभी उसे कुतरी हुई शर्ट मिलती, कभी कुतरी हुई साड़ी। औरत ने आदमी से पहली फरमाईश की थी…
“घर में बहुत सारा चूहा हो गया है, रोजे कुछ न कुछ काट देता है लोग!”
आदमी माथा हिलाकर रह गया था, और ड्यूटी से वापिस आते हुए, एक दुकान से “चूहे मारने वाली दवा” खरीद लाया था।
“एक ठो जीव का हत्या करना ठीक नहीं है!” का तर्क देकर औरत ने चूहेदानी मँगवाई थी। दवा को उसने अन्दर वाले रैक के किसी अँधेरे कोने में रख दिया था।
आदमी, शहर की हाट से लकड़ी की एक मजबूत चूहेदानी ले आया था।
चूहेदानी एक नन्हें बक्से जैसी थी। उस छोटी-सी जगह में हाथ डालकर औरत ने उसमें लटके हुए पतले से तार में, रोटी का टुकड़ा फँसा दिया था। औरत ने काठ की वह चूहेदानी रसोई के ऊँचे वाले ताख पर रख दी और दुनिया भर के कामों में बझ गयी।
तमाम काम निपटा लेने के बाद और आदमी के फर्स्ट हाफ से वापसी के मध्य का समय नितांत निजी और आजाद था।
औरत तेजपत्ता, अदरक और चायपत्ती झोंककर, कड़क वाली चाय बनाती थी। गिलास में चाय लेकर आदमी की चौकी पर बैठ जाती थी। आदमी अभी बाहर था। इसलिए अभी ये सबकुछ औरत का था, या, यह भी कह सकते हैं कि आदमी और औरत का साझा सबकुछ!
औरत ने चाय का घूँट भरा।
खिड़की के पल्लों पर कई तह धूल जम गई थी। औरत ने अपनी तर्जनी से उसपर एक फूल बना दिया। फूल, धूप की हल्की रौशनी में चमकने लगा।
औरत ने बहुत पहले रेडियो पर सुना था कि सूरज आग का गोला है। तब से औरत जब भी सूरज को देखती, सोचने लग जाती कि आखिर इतनी आग जलते रहने के लिए डीजल, जूट, गोइंठा, कोयला, कुछ तो चाहता होगा न भाई? तो इतना सारा सबकुछ कैसे जो आया होगा सूरज के पास? सूरज जलता रहा है, जलता ही जा रहा है। कब खत्म होगा इसका ईंधन?
औरत चाय का आखिरी से ठीक पहला घूँट भरने वाली थी, कि…तभी खूब जोर ‘खटाक’ की आवाज हुई।
औरत चिहुंकी…फिर मुस्कुरा भी पड़ी।
“फंस गए न महाराज!”
उसने बड़े आराम से आखिरी घूँट लिया और गिलास खिड़की की रैक पर रख दिया। अपने खूब लंबे गीले बालों को मुट्ठी में मरोड़ कर उसने जूड़ा बना दिया। चूहेदानी लेकर वह कमरे में आ गई और फर्श पर पसर कर बैठ गई। वो एक अकेला नन्हा सा चूहा था जो चूहेदानी में इधर से उधर उछल रहा था। औरत ने चूहेदानी की जाली से अपनी नाक सटाई, वहाँ सिर्फ काठ की सोंधी सी महक थी और कुछ नही था।
औरत चूहे को छूकर देखना चाहती थी।
जाली के फांक इतने महीन थे कि और किसी भी ऊँगली की गुंजाइश नहीं थी, सिवाय कनिष्ठा के।
कनिष्ठा, चूहे की चिकनी पीठ पर हलके से फिसल कर रह गयी। मासूम चूहा सहम गया और दुबक गया था डिब्बे के कोने में।
“तुम्हारा क्या करें हम, बताओ!”
औरत को प्यास लग आई थी। चूहेदानी को लिए हुए ही औरत ने घड़े से पानी निकाला और गट-गटा-गट पी गई।
“अरे, कितना मजेदार न!”
उसने चूहेदानी को बायीं ओर से तिरछा किया और चूहा बायीं ओर सरक गया। अब उसने चूहेदानी को उलट दिया, नन्हा चूहा जालियों पर लटक गया था और उसकी नन्हीं सूतली जैसी पूँछ जाली से बाहर आ गई। औरत ने उसकी पूँछ को टोहा। नन्हकु कांप गया जरा सा! चूहा चूँकि जाली पर था, इसलिए औरत उसकी देह का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा छू सकती थी। वो बड़ी देर तक टोहती रही। चूहे की नन्हीं सी चिकनी देह।
आदमी की फर्स्ट टाइम की ड्यूटी से वापसी का समय हो रहा था। औरत ने चूहेदानी उलट दी और चूहा काठ की फर्श पर गिर गया था। फिर उसने चूहेदानी का दरवाजा खोल दिया पर सहमा सा चूहा कोने में दुबका रहा…
औरत ने हथेलियों से चूहेदानी को थपथपा दिया, और सरपट भगा चूहा गुम हो गया था, क्वार्टर के किसी बिल में।
अब औरत और चूहे के बीच एक साईं-गोटी थी।
औरत जब जी चाहे क्वार्टर के किसी भी कोने से चूहे को उठा लेती थी और फिर उसे जब जिस कोने में जी चाहे वहां छोड़ देती थी।
…………………………………………………………………………………….
धूल हवा से उतर जाती थी। तब, धूल और पानी का मौसम आता था। धूल पानी में घुल गई थी और थपर-थपर फैल गयी थी पीच वाली सड़क पर, सीमेंटेड सीढ़ियों पर, बरामदों पर, हद हो गयी जी कि कपड़ों पर भी!!
“शायद अब बारिश रुक जाए कि तब बारिश रुक जाए” की संभावना ने सूरज के ढलते जाने की भी परवाह नहीं की थी। आखिरकार इस संभावना को खारिज कर आदमी साईकिल और काला जेंट्स छाता लिए सड़क पर आ गया था। आदमी को रेनकोट लेना औरताना लगता था। कुछ देर पहले जोर-शोर से बरस रहे आसमान का जोश ठंडा पड़ गया था। फुहार थी, जो चेहरे पर गुदगुदी करती थी।
आदमी ने छाता बंद कर बायीं हैंडिल पर टांग दिया था। रात थी, चमकती हुई पीली नारंगी स्ट्रीट लाईट्स थीं, भींगी हुई काली सड़क के ऊपर गहरा आसमान था।
अमूमन शांत न रहने वाली ये सड़क आश्चर्यजनक रूप से सून-सपाट थी।
साइकिल लिए होने के बावजूद मस्ती में पैदल चलता आदमी तीन-चार सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रीट लाईट के नीचे ठहरा था। आदमी ने अपनी गोल डायल वाली घड़ी में समय देखा था। सड़क के दूसरी ओर डैम था…काला-रहस्यमयी चुप्प! हवा इतनी नाजुक थी, कि बस रोयें कर सिहरा कर सरक जाती थी। स्ट्रीट लाईट की पीली रौशनी लकीरों की तरह सोयी पड़ी थी डैम की सघन चुप्प सतह पर। आदमी ने सड़क पर से एक कंकड़ उठाया और दे मारा डैम में। ऊँगली की नोंक भर दरवाजा खुला डैम का, और गोल-गोल कुछ हिलने लगा, जैसे या तो ऊँगली की नोंक भर दरवाजे में समा जाएगा, या बह कर निकल जाएगा डैम की परिधि से बाहर। पर पीली रौशनी की लकीरें सतह पर धीमे-धीमे नाचकर थिरा गईं, हलचल जाने कहाँ बिला गई, किस खोह में?
झींगुर गूँज रहे थे, मेंढ़क की टर्र-टर्र भी!
और एकबारगी आदमी के दिमाग में आया था, क्या होगा इस डैम के अथाह पानी के नीचे? दलदल? निरा गाढ़ा दलदल? दलदल के नीचे ठोस जमीन? ठोस जमीन पर रिसता हुआ डैम का पानी! रिसता हुआ पानी…और रिस-रिस कर तैयार होता दलदल!!
और दलदल के नीचे भी दलदल।
यानि की पृथ्वी के एक छोर पर अगर डैम था, तो उस डैम के नीचे पृथ्वी के ठीक दूसरे छोर पर क्या होगा? दलदल ही न? कंकड़ जो डैम में उछाला गया था, पहुँच चुका होगा अब तक दलदल की पहली परत पर। और दलदल की लजलजी देह में धँसते-धँसते संभव है किसी काल खंड में निकल गिरे दलदल की आखिरी सतह से।
क्या होगा उस एक कंकड़ का?
पृथ्वी के पर्यावरण से निकल कर गुम हो जायेगा अन्तरिक्ष के अंधार में, या चक्करघिरनी की तरह घूमता रहेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में।
“क्या चुतियापंथी है? चोप्प साले चोप्प!!”
हवा थी, पत्तों का डालियों पर डोलना था, सरसराते सांप का गुजरना था, थोड़ी दूर पर नजर आते बाजार की जगमगाहट थी, चेहरे पर हेडलाईटस की रौशनी फेंकते हुए स्कूटर का गुजर जाना था और इन सब के बीच चिरकुट सा जीवन था।
आदमी रुक गया था। अपनी तीसरी छलाँग के बाद एक मेंढ़क साईकिल के सामने आ गया था। चौथी छलाँग में मेंढ़क ने सड़क पार की, आदमी आगे बढ़ गया।
आदमी जब यहाँ आया था तो ताजा-ताजा ही जवान हुआ था। कुल जमा बीस बरस का। आदमी को तब क्वार्टर एलॉट नहीं हुआ था, सो आदमी हट्टन रोड में मंटू घोष के यहाँ किराये पर रहता था।
झड़े चूने और खिया चुके प्लास्टर वाले मंटू घोष के विरासती मकान की खिड़कियाँ सीढ़ीदार आकार में थीं। जिनपर किसी जमाने में सुआपंखी रंग का पेंट चढ़ा होगा।
दिन में भूरे रंग का दिखता वह मकान रात में एकदम स्याह हो जाता था। खुली हुई खिड़कियों के गुलाबी फूलों वाले परदे हिलते रहते थे, और झक पीली रौशनी बाहर गली तक छितराई रहती थी। मकान में एक ब्लैक एण्ड व्हाइट टी०वी० थी जिसपर हर इतवार की साँझ कोई बांग्ला फिल्म आती रहती थी। कभी-कभी उस पर मोटी कलात्मक भवों वाली हिरोईन की फिल्म भी आती थी जो बांग्ला और हिंदी फिल्मों में समान रूप से काम करती थी।
खूब भारी-भरकम दीवार घड़ी का पेंडुलम लगातार दाएँ से बाएँ हिलता रहता था और ठीक उनसठवें मिनट के बाद घड़ी घन्न-घन्न-घन्न नौ बजा देती थी। मंटू घोष फोल्डिंग सोफा पर बैठकर लाल झोल वाली सब्जी के साथ उसना भात चाभता था। खूब पुराने स्टील के गिलास का पानी बुड्ढा घटर-घटर पी जाता था। बुड्ढे की तीन बेटियाँ थीं। बेटा एक ही था जो पार्टीगिरी करता था और झूठमूठ के नारे लगाता था-
आधा रोटी तावा में,
ज्योति बोसु हावा में,
उसकी बड़ी बेटी किसी बांग्लादेशी से शादी करके ढाका भाग गयी थी। मँझली बेटी दिनभर सिलाई करती थी। उसकी सबसे छोटी बेटी दसवीं में पढ़ती थी।
सिलाई करने वाली ये सुन्दर लड़की बरामदे में मशीन में गड़ी सुई में से धागा निकालती थी। लड़की की आँखों में पानी भर आता था, सो लड़की अपनी नजर भटकाती थी।
सामने खड़ा आदमी चेत जाता था।
“वो…घोष बाबू??”
“बाजार…!”
लड़की फिर सूई और कपड़े को जोड़ने वाले धागे को दांत से काटकर सिरा-तोड़ देती थी।
लड़की खटर-खटर बड़ी कुशलता से मशीन चलाती थी। कमीज का किनारा सीती हुई लड़की की लम्बी पतली उँगलियाँ कपड़े के साथ-साथ सूई के करीब चलती जाती थीं। इधर से कच्चा कपड़ा लगाने पर, दूसरी ओर से सिला हुआ कपड़ा गिरता जाता था।
आदमी को हमेशा भय लगा रहता था कि कहीं कपड़े की लहर में लड़की की ऊँगली भी सूई के नीचे ना चली जाए । वो इस बाबत कई बार लड़की को सचेत भी करना चाहता था।
यह तो बाद के दिनों में गौर से देखने पर मालूम हुआ कि, स्टैंड गिराने के बाद कपड़े के अलावा हवा की भी गुंजाइश नहीं होती सूई के नीचे आने की।
लिहाजा आदमी आश्वस्त हो गया था।
तुरपाई और सिलाई के अलावा और ऐसा कुछ नहीं था जो लड़की दुनिया से बटोर पाई थी।
घिरे सांझ तक सिलाई करती लड़की छह बार घन्न-घन्न की आवाज के बाद छोटी बहन के साथ मिलकर सिलाई मशीन कमरे में रख देती थी और शंख फूंकती थी।
आदमी जब ताश की महफिल से वापस आता था तो गर्मी की रातों की तेज हवाएं अपेक्षाकृत कम गति से बहती थीं। आदमी बेहाया के बेढ़ा से टिककर साइकिल लॉक कर देता था। चाबी शर्ट के ऊपरी जेब में डालकर विरासती ईमारत के पिछवाड़े जाने के क्रम में दो खिड़कियों के पश्चात् तीसरी खिड़की रसोईघर की होती थी जहाँ सिलाई करने वाली लड़की कटहल के टुकड़े भूंजती होती थी। लड़की आहट पकड़कर बाहर झांकती थी, बेपरवा आदमी जल्दी से पार हो जाता था। घर के पिछवाड़े पहुंचकर आदमी कुल जमा बीस सीढ़ियाँ चढ़ता था, और अपने कमरे का दरवाजा खोलता था। दिन भर का बंद कमरा आदमी के नथुनों तक एक शिकायती गंध छोड़ता था…अकेलेपन का गंध, दिनभर किसी तरह के बर्तनों की कोई उठा पटक न होने के त्रासदी की गंध, लगातार सोते रहने से उपजी आलस का गंध! वह कमरा बार-बार इतनी उबासियाँ लेता था कि आदमी उब जाता था और कमर से लाल लाइनिंग वाली गमछी लपेट कर खाट पर पड़ जाता था।
देर तक यूँ ही पड़े आदमी की नाक से एक गंध टकराती थी और आदमी भयानक हड़बड़ी के साथ उठ-बैठता था। माड़ स्टोव पर गिरता हुआ फर्श पर फैल जाता था। आदमी पोंछन को चार-पांच बार उलट-पुलट कर माड़ समेट लेता था, धो-गारकर पोंछन को कोने में खूँटी में टांग देता था।
नीचे वाले कमरों से गुजरते हुए आदमी को अक्सर ही कभी अंडे की महक आती थी और कभी भूंजी जाती मछली की। आदमी यद्यपि नाक-मुंह नहीं दाबता था, पर कभी उसके अन्दर कुछ जगा नहीं! आदमी को अपना ननिहाल याद था जहाँ नानी की रसोई से निमकी और अचार की खट्टी-खट्टी महक आती थी। जब भी आदमी को नानी की याद आती थी, उसे गरम भात, अरहर की दाल और निमकी का अचार भी याद आता था। इन सब यादों के बीच सबकुछ इस कदर पच जाता था कि आदमी को तुरत-फुरत में कुछ बनाना बेहद जरूरी हो जाता था।
आदमी को बेहद शुरूआती दिनों में अजय देवगन पसंद था। इतना पसंद था कि आदमी अजय देवगन के पोस्टकार्ड साइज फोटो सहेज-सहेज कर रखता था। यथा, मधु को बांहों में लिए प्यार करता अजय देवगन, अमरीशपुरी से बहस करता अजय देवगन, विलेन्स के छक्के छुड़ाता अजय देवगन और भी तमाम तरह का अजय देवगन।
आदमी जब बिहार में था तो उसके पोस्टकार्ड्स में लौंडा नाच के तमाम सीन भरे पड़े थे। आदमी अपने गाँव से एक कोस दूर मिडिल स्कूल में पढ़ता था और लगन के टाइम में उसने भी एक कोस दूर लौंडा नाच देखने के लिए रात-रात भर गायब हो जाता था।
आदमी का बाप एक बूढ़ा आदमी था जो फूस के पलानी में बैठकर गुड़ की चाय सुड़कता था और भसके हुए आँगन में लाठी टेककर चलता था।
बूढ़े को जब गहरी बात कहनी होती थी तब अपने कत्थई देह में उपजे हुए कत्थई हाथों को अपने चमकते चिक्कन कत्थई टकले पर अंदाज से फिराता था फिर आँखें दो-तीन बार झपका कर थूक निगल लेता था।
“अबकी धान तो बेसी हुआ नहीं!”
“हम्म…!” (कौन सा पहले बेसी होता था)
“घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो…!”
“………………” (आगे)
“आई० टी० आई० कर लोगे तो कइसा रहेगा!”
“ठीक ही है बाउजी!” (ना हमको मास्टरी करनी है)
आदमी की माँ एक टांठ औरत थी जो बुड्ढे के आलस को कोसती थी और फिरकन्नी की तरह आँगन भर में नाचती रहती थी।
आदमी का बाप चोर था।
आदमी का घर एकदम खुला था, बोले तो मेड़ जैसी कोई चीज नहीं थी। दो कमरों के अलावा सारा आँगन खुला निचाट था। अब, दिक्कत यह थी कि टांठ औरत को मुंह धोना, या पेशाब करना जैसे छोटे कामों के लिए भी रात का इंतजार करना पड़ता था, आवेगों को लम्बे-लम्बे घंटों तक स्थगित करने के कारण टांठ औरत कई दफा भीषण पेट दर्द से पीड़ित हो चुकी थी।
आदमी का बाप लोगों के घरों से, या ईंटों के ऊँचे-ऊँचे ढेरों में से अक्सर एकाध ईंटें चुरा लिया करता था और घर के चारों ओर मेंड़ तैयार होती जाती थीं।
यही ताजा जवान हुआ आदमी जब पहली बार आसनसोल स्टेशन पर उतरा था तो अकबका गया था। धीरे-धीरे चलता आदमी, दौड़ने लग गया था। गजब रे वैभव! कि बस में जिस तरफ महिलाएँ लिखा होता था उस तरफ सिर्फ महिलाएँ बैठ सकती थीं। आदमी धीरे-धीरे सूती साड़ी और ताँत की साड़ी में फर्क भी चीन्ह गया था।
इस शहर में इतनी गलियाँ थीं कि यहाँ खोया जा सकता था। प्लास्टिक, कागज, कादो का ढेर होता था किनारे, और बीच सड़क पर रिक्शा पों-पों गुब्बारा बजाता पार हो जाता था।
यह किसी मूक नाटक में चलते दृश्य जैसा था जहाँ हर पात्र के चेहरे पर मास्क था और मजा यह कि मास्क वाले हर चेहरे से एक्प्रेशन्स जाहिर हो जाते थे। यह एक बेहद सीधा-सादा शहर नहीं था, पर आदमी को यह चीन्हने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा की यहाँ गांठें अधिक नहीं थीं। कई बार ये गांठें इतनी ढीली होती थीं, कि आदमी धागा पकड़ कर वहाँ पहुँचने-पहुँचने को होता था कि लो, गाँठ ही खुल गई! अब बताओ?
ऐसे ही धागे का एक सिरा पहुँचकर आदमी वहाँ पहुंचा था जिसे लच्छीपुर कहते थे। कहते थे कि, कलकत्ते के किसी दबंग के हड़काने पर इस पूरी बिरादर ने यहीं अपना डेरा-डंडा जमा लिया था। इस बिरादर में मादाएँ ज्यादा थीं जो पेटीकोट को स्कर्ट की तरह करके पहन लेती थीं। मादाएँ पक्के कमरों के आगे पान चबाती टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी होती थीं। उनकी समूची देह का भार उनके टिके हुए हाथों पर होता था। मादाओं की छातियाँ लटक गई होती थीं, और पेट लटकी हुई छातियों के बराबर निकल आया होता था। वहाँ जलकुम्भी और कादो-कीचड़ से बजबजाता एक पोखर था जिसके एक किनारे लाईन से तीन कनेर के पेड़ खिल आए थे।
आदमी ऐसे ही एक कमरे में उस दिन घुसा था, जब आसमान बिलकुल निर्वस्त्र था। उस दिन सड़ा हुआ धुआं उगलती बहुत सारी मिनी बसें गुजरी थीं।
कोठरी में सड़ती हुई मिट्टी की गंध फैली थी और चप्पलें धरती से चपर-चपर करती हुईं अलग होती थीं। एक कोने के बेहद छोटे से दायरे में थूक और पीक से धरती लाल हुई पड़ी थी। कोठरी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांस बंधा हुआ था जिसपर बसाते हुए कपड़े पटके हुए थे। आदमी के सामने जो औरत थी वो स्थूल थी। ढलकी छातियों वाली इस औरत की देह हवा से फूली हुई थी। उसने लाल रंग की कोई सस्ता हुआ ओंठलाली लगायी थी। चेचक के दागों के बावजूद लाल टीप वाली औरत सुन्दर दिख रही थी।
अनाड़ी आदमी पहली बार कोई रहस्य जानने आया था। औरत फुर्सत में नहीं थी। आदमी हाथ-पाँव मार रहा था। औरत ने सहारा देने की कोशिशें कीं, आदमी था की फिसलता जा रहा था बार-बार। आदमी की नाक में घरेलू पसीने की महक समाई थी, सूती साड़ी के आँचल से स्टील की गीली थाली पोंछकर, परोसी जाती भात की महक, पर औरत की गर्दन के पास जर्दे की इतनी तेज महक थी कि आदमी को लगा उसके होंठ गल जाएँगे और सड़कर चू जाएँगे इस बेकायदा गंधाती छातियों के ढेर में। भयानक रूप से डरे हुए आदमी झटके से दूर खड़ा हो गया। औरत खिसिया कर उठ बैठी,
“बेपार टा की रे बोक्का??”
डरे हुए आदमी ने नंगी चौकी पर पचास का नोट धर दिया, और बाँस की अलगनी से खींचकर शर्ट पहन लिया।
काले पैन्ट पर, काले रंग की महीन खड़ी लाइनिंग वाली सफेद शर्ट पहनने वाला आदमी कभी शर्ट इन नहीं करता था। इस आदमी को हमेशा बेल्ट वाली हाथ घड़ी अच्छी लगती थी।
आदमी खास तरह के प्रयास से चुप रहता था और बंगाल का वैभव निहारता रहता था। शहर था की तमाम पुरानी शाही बिल्डिंग्स से भरा हुआ था। काई जमी हुई दीवारों वाली इन हवेलियों की रेलिंग काठ की होती थी और खिड़कियों के टीन वाले पल्ले सीटीनुमा आकर में होते थे। सबकुछ रहस्यलोक जैसा लगता था और खूब चमकता हुआ दिन बीत जाता था। दिन-ब-दिन मछली की महक तेज होती जा रही थी और यह महक आदमी की निहायत ही जरूरी आदतों में शामिल होती गयी थी।
आदमी को यह शहर एक औरत लगता था, औरत जो बिना कलफ वाली लालपाढ़ की ताँत की साड़ी पहन कर गीले बालों में “हरे रंग की टिन वाली खिड़की” से धूपबत्ती दिखाती नजर आती थी।
शहर था कि आदमी के तईं अलग-अलग खुलता जाता था, और आदमी उसे चपेत-चुपत कर जेब में रखता जा रहा था।
सुंदर लड़की जब मुर्गा लकड़ी के विरासती पलंग पर लेटती थी तो पलंग बिना हिले अजब सी चरर्रऽऽ की आवाज करता था और कमरे में अचानक से कुछ नहीं रह जाता था। लड़की से सटे मेज-कुर्सी, कोने में कपड़ों-गद्दों से लदे ट्रंक के अलावा भी कोई चीज थी। कमरे में जो अब नहीं रही और बिना उसके कमरा खाली हो गया है। बुखार से तपते कमरे में मरी पीली रौशनी टिमटिमाती थी। पंखा घर्र-घर्र इस तरह से नाचता था की पंखुड़ियों पर जमी धूल उसकी गति में नहीं दिखती थी। पंखे की हवा से खिड़की का गुलाबी फूलों वाला परदा जंगले की छड़ों से चिपक जाता था, पर बाहर की ताजा हवा जब धकेलती थी, परदा नाचता हुआ खूब ऊपर तक उड़ जाता था और मेज पर रखी हुई तमाम किताबों में से किसी किताब के पन्ने फड़फड़ा जाते थे। हवा वापस लौटती थी, कमरा सटपट चुप्प हो जाता था और परदा इस कदर लोहे की छड़ों से चिपक जाता था, मानों दो छड़ों की बीच वाली जगह से सरक कर बाहर निकल जाना चाहता हो।
बिछ्कुतिया पूँछ पटकती ऊपर चढ़ जाती थी।
आदमी जिद जैसी किसी अय्याशी वाली चीज के बीच पैदा ही नहीं हुआ था। आदमी ने अपने बूढ़े बाप को बताया भर था की बंगाल नमक वैभवशाली राज्य की एक सुन्दर बंगाली लड़की से वह ब्याह करना चाहता है…कि वह बंगाली लड़की गृहकार्य में निपुण है और चिथड़ों में भी रह लेगी हमारे साथ।
बूढ़ा बाप, अपने कत्थई टकले पर बड़ी देर तक कत्थई उँगलियाँ फिराता रह गया।
टाँठ औरत उस दिन बड़ी देर तक ओखल में मुट्ठी भर धान कूटती रह गई थी। चावल के बुरकन्नी हो जाने तक फिर मिट्टी की दीवार के सहारे पसरकर रोती रही थी। उसी साल की पहली लगन में जिस दिन आदमी आँखों में काजल और पैरों में आलता पोतकर जहानाबाद के एक गाँव में लड़की ब्याहने गया था, हट्टन रोड के उस छोटे से गली-गूँचे वाले मोहल्ले में बात आग की तरह फैली थी कि स्टोव फटने से घोष की मँझली बेटी जल गई।
आनन-फानन में उसे कस्तूरबा गाँधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दाएँ हाथ और पैर के झुलसन के अलावा बाकी लड़की साबुत बचा ली गई थी।
वापस आया आदमी स्तब्ध था। वापसी की शाम ही वो मिला लड़की से।
“तुम लोगों ने स्टोव कब खरीदा?” आदमी बहुत चाहकर भी नहीं पूछ पाया।
“बोउदी कैसी हैं?” लड़की के पास इसके अलावा और कोई संबोधन नहीं था।
आदमी के हाथ में लड़की का दायाँ हाथ था। जिसपर झुलसन के निशान थे। लड़की आदमी की नई घड़ी के चेन से खेल रही थी।
लड़की पिघल जाने से डरती थी, आदमी आँच तेज कर रहा था। आदमी सचमुच चाहता था कि यह लड़की दो बरस की छोटी बच्ची बन जाए, जिसे आदमी अपने कलेजे से लगाकर रख ले।
घने अँधेरे में आदमी हाथ से इशारा करे,
“उ देखो भकऊँआ…!”
अँधेरे में देखती बच्ची डर के मारे अपनी नन्हीं बाहें आदमी के गले में लपेटकर चिपट जाए. आदमी उसे छाती से लगाकर खूब दुलारे,
“अले मेला बाबू ले…!”
सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। लड़की गल गई थी और बूँद-बूँद बड़ी देर तक रिसती रही थी आदमी की छाती पर।
आदमी ने कभी नहीं बताया लड़की को कि उसके पास बस एक बूँद भर आँसू बचा है जिसमें वो अपनी उम्र भर का रोना बहा सकता है।
बादल थे, बारिश थी, धूप थी, बाजार का शोर था, बिन ब्लाउज की ताँत साड़ी पहने साँवली औरत थी जिसके हाथ से फिसल-फिसल कर मछलियाँ सामने बिछे प्लास्टिक पर छितराती जाती थीं. लाल टीप लगाए बाल खोलकर हँसती औरतें थीं, ट्रेन का आगाज था, मालगाड़ी का गुजरना था, शाम के संतरईपन में धुएँ की एक लकीर थी और लो!! पलक झपकते ही सारा दृश्य गायब हो जाता था।
आदमीं रिंच से पटरी का नट-वोल्ट कसता था और धूप की तरफ देखता था तो सात रंग दिखाई पड़ते थे। इर्द-गिर्द, दाएँ-बाएँ छितरे हुए। आदमी हथेली के सबसे नर्म-गुदगुदे कोने से रगड़कर माथे का पसीना पोंछ लेता था। पीठ पर टेरीकॉट की कमीज भींगकर चिपक जाती थी।
आदमी नट कसकर पटरी फलाँगता आता था। कितना कुछ छूटा पड़ा था पटरियों पर…!!
फ्रूटी का डब्बा, मल, प्लास्टिक की बोतल, पत्तों का दोना, मूंगफली और केले के छिलके, प्लास्टिक में बचा हुआ बासी-तिरासी खाना, व इन सब के बीच ट्रेन रुकने और चल पड़ने के बीच का “कुछ क्षण जीवन”!
एक ढकचल कुतिया पटरियों के बीच का बचा-खुचा-फेंका हुआ दुरदुराया हुआ जीवन सूंघती थी। उसी के साथ लगे-लगे दौड़ते नन्हें-नन्हें मरघेवल के पिल्ले थे। बाजार के छोटे- छोटे दिखते रौशनी के कतरे पास आ गए थे। चहल-पहल, भाग-दौड़, बाजार की खुमारी में कहीं कोई कमी नहीं थी।
आदमी का मन तीता खाने का हो गया था। खूब तीता, चटक-मटक! आदमी एक ठेले के पास रुका था।
पकती चाशनी और आलू-चॉप के बीच शहर महकता था और महकती थी प्लास्टिक के शेड से चूती हुई बरस चुकी बारिश की बूँदें! बूँदें गर्म सरसों तेल में पड़कर छनछना जाती थीं। आदमी को पता था की ऐसी ही कोई छनछनाहट औरत को भी पसंद थी। सो तमाम रोटियाँ सेंक लेने के बाद औरत लोटे के पानी में उँगलियाँ डुबाकर गर्म तवे पर छिड़क देती थी।
और बूँदें, उछल कूद कर, छनछना कर खत्म हो जाया करती थीं।
आलू चॉप खरीद कर लौटते हुए आदमी के दिमाग में इन्तजामी औरत आती थी, जो गीले कपड़े सुखाने के लिए बरामदे में तार बांधती होती थी, ताकि बरसात में कपड़ों से बास न आए।
आदमी, औरत के कपड़ों के बाजू में ही अपनी गीली शर्ट निचोड़ कर पसर देता था। आदमी जनता था की औरत सिंथेटिक की गुलाबी साड़ी पूरी तरह सूख जाने के पहले ही उतार लेगी क्योंकि पूरी तरह सूखने पर साड़ी तार से सरक जाती थी और साड़ी के नीचे छुपाकर टाँगे हुए औरत के अंतःवस्त्र नंगे हो जाते थे।
……………………………………………………………………..
कई सारी चीजें बेकार थीं जो बेकार, बेमतलब, बेशऊर थीं कई सारे बिंब थे जो अनायास थे, पर साले सारी जिन्दगी को उघाड़ कर रख देते थे।
नहीं जी, ये सारे कैमरे से क्लिक हुए सीन थोड़ी न थे जो जैसे थे, वैसे ही थे? ये सब तो किसी अनाड़ी चित्रकार के द्वारा फोटो इंजेक्ट पेपर पर फूजी कलर का अकुशल इस्तेमाल था। जो वैसे थे, जैसा उन्हें चित्रकार ने देखा था। चित्र में न रंग सही भरे थे, न छाया का कुशल इस्तेमाल था। चित्रकार के पास कुछ नहीं था, सिवाय उसकी आत्मा के, जिसे जंग खाए टिन की तरह बेकार करार दे दिया गया था।
आत्मा उस चित्र में वैसे ही नजर आती थी जैसे किसी फोटो फ्रेम के सामने खड़े होने पर नजर आता है अपना प्रतिबिम्ब!
वक्त अगर ट्रेन था तो आदमी ट्रेन के भागने वाली दिशा की ओर खिड़की पर बैठा था। विपरीत दिशा वाली खिड़की पर बैठने से सिर्फ आने वाला दृश्य दिखाई देता था, छूटा हुआ नहीं, जबकि ट्रेन की दिशा वाली खिड़की पर बैठे आदमी को ऐन सामने से गुजरा हुआ दृश्य दिखायी पड़ना था, बड़ी दूर तक।
औरत अपने तहखाने में छिपाकर रखे ढेर सारे पोस्टकार्ड निकालती थी और दृश्यों को क्रम से देखती थी।उसकी उँगलियों में यानि कि एक “पॉज” दृश्य होता था, और हर “पॉज” दृश्य के साथ उसकी स्मृति कहानी पूरी कर देती थी।
औरत की उँगलियों में जो पहला पोस्टकार्ड थमा था, उसमें छः साल की बच्ची थी जो अपने फ्रॉक के घेरे को चिमोर-मिमोर कर हाथ में पकड़े एक नंगे खेत में बैठे थी। बच्ची अपनी बत्तीसी का सारा बल जैसे अपने पेट में धकेलती थी और जोर से काँखती थी…”अँह…”। बच्ची नीचे देखती थी, कुछ सकारात्मक परिणाम देखकर पुनः बल की मात्र बढ़ाने की सोचती बच्ची की पीठ पर सटाक से कुछ बजता था। झपटकर खड़ी हुई बच्ची, फट से फ्रॉक का घेरा छोड़ देती थी।
“खाली हगइते रहबे, कि छगरियन के ले जइभी?”
बच्ची एक क्षण नीचे देखती थी और एक क्षण पास खड़े ममेरे भाई को। बच्ची फिर सरपट भागती थी और बकरियों को समेटती घर पहुँच जाती थी।
औरत, तीन साल की बच्ची थी, जब उसका बाप खून उगलते मर गया था। भतार खौकी डायन को तब गाँव वालों ने ईट और पत्थरों से कुचलकर मार डाला था। बच्ची को ननिहाल पहुँचा दिया गया। नरभक्षी डायन किसी की बेटी थी, और बच्ची उस बेटी की एकमात्र निशानी। मूलधन से प्रिय ब्याज होता है। और नानी खूब जतन से सहेज-सहेज कर ब्याज रखती जा रही थी।
बच्ची दिनभर खेतों में घूमती थी, कादो-कीचड़ में सन जाती थी। सरसों के फूलों की नाजुक डंठल तोड़कर उनकी बाली, चूड़ियाँ और हार बनाकर पहन लेती थी। बच्ची जब सारी बकरियों को समेटकर घर पहुँचती थी तो सूरज हांफ रहा होता था। और ईट के मकान में एक औरत, हाथ नचाकर बूढ़ा-बूढ़ी से लड़ती होती थी की डायन की बेटी के ब्याह के लिए आखिर पैसे कहाँ से आएँगे”।
सरसों के फूल मुरझा जाते थे। बच्ची चुपचाप बकरियों को ले जाकर बांध देती थी और चापाकल पेरने लगती थी। बच्ची चापाकल इतना पेरती थी, इतना पेरती थी की घर भर की बाल्टियाँ, बासन, भांडे सब पानी से लबालब हो जाते थे।
नानी रात में चौकी पर बच्ची को छाती से चिपका लेती थी। बच्ची हमेशा सचेत रहती और कभी भी अपनी नाक या आँखें नानी की छाती से नहीं चिपकाती थी। हमेशा अपने कान नानी की छाती से चिपकाकर सोती थी और नानी की धड़कन सुनती रहती थी।
नानी ज्यादा चालाक थी। धीरे से अपना हाथ बच्ची के आँखों के पास रखकर टोहती थी। पर, इससे पूर्व कि टोहने का प्रत्याशित या अप्रत्याशित परिणाम मिलता बच्ची नानी का हाथ झटक देती और निन्दियाई आवाज में कहती थी- “हमरा सुते दा न!!”
नानी शांत हो जाती थी।
जब नानी सो जाती तब बच्ची खूब आहिस्तगी से अलगाती थी खुद को। बच्ची करवट फेर लेती थी और दीवार से चिपक जाती थी। समझदार बच्ची फ्रॉक का एक सिरा गेंद जैसा बनाकर मुँह में ठूँस लेती थी।
बच्ची की किसी सखी, सहेली, बंधु-बाँधवी का नाम सपना नहीं था और इसलिए इस शब्द से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हुए ही बच्ची, औरत हो गयी थी।
…………………………………………………………………………..
औरत बड़ी देर से दाबे बैठी थी जो चीज वह अब धीरे-धीरे खुल रही थी। अंततः उन्मुक्त हो गई थी हवा में।
औरत जानती थी, कि पहले यह जरा सी चीज हवा में घुलेगी फिर पूरे कमरे में फैल जाएगी। जो बदबू औरत के नथुनों तक सबसे पहले पहुंची थी, औरत उसके आदमी की नाक तक पहुँचने और फिर उसकी प्रतिक्रिया के इंतजार में बैठी थी।
आदमी चुपचाप बूढ़े पिता को चिट्ठी लिख रहा था। औरत साफ-साफ देख पा रही थी कि आदमी की पुतलियाँ रेनौल्ड्स पेन के हिसाब से भागती और ठहरती थीं।
औरत को जाने कैसे तो लग गया की बस्स!! अब कुछ पहुँचने ही वाला है आदमी की नाक तक। औरत को ऐसा लगा कि कंठ के ऐन ऊपर कुछ अटक गया है।
औरत उसे उसे निगलती थी खामोशी से! परय शायद अटकी हुई चीज पूरी तरह अन्दर नहीं जा पाई थी और कुछ झिल्लीनुमा बाकी रह गई थी।
औरत होंठ दाबे अटकी हुई चीज को जरा बल लगाकर घोंटती थी और आवाज होती थी-“इ्हम्मऽऽऽ!”
एक बच्चा था जी। ड्यूटी से वापस आते पिता को बच्चा रोज पाँच वर्डमीनिंग्स याद करके सुनाता था। पर उस दिन बच्चा खेलता रह गया था और वर्डमीनिंग्स याद नहीं कर पाया था। बच्चा जानता था वर्डमीनिंग्स नहीं याद करने के एवज में एक बार कनैठी और चार झापड़ तय हैं। बच्चा यह भी जानता था कि चीनी मिट्टी का फूलदान टूटने पर एक कनैठी समेत लम्बी डांट के बाद माफी थी। बच्चा बस फूलदान को, वर्डमीनिंग्स से रिप्लेस कर देने की कोशिश करता था।
बच्चा रबर की गेंद लाता था और फर्श पर पटक-पटक कर खेलता था। ऐसा हुआ कि चौथी बार फर्श पर उछाल के बाद गेंद फूलदान से जा टकराई।
फूलदान गया टूट, पिता गए रूठ!
और बच्चा तब अकबक रह गया था जब पिता ने उसे कुल दो कनैठी, चार झापड़ समेत लम्बी फटकार सुनाई थी।
यानि कि, कोई चीज रिप्लेस नहीं हुई थी अलबत्ता जुड़ गयी थी।
चिठ्ठी में आखिरी पंक्ति लिखते आदमी की कलम “बाकी सब यहाँ ठीक” पर ही ठहर जाती थी। आदमी अपने दोनों नथुने हल्का सा सिकोड़ कर छोड़ देता था। भौहें उचकाता था। चिठ्ठी से सर उठाकर इधर-उधर देखता था।
कमरे में जो चीज फैली थी वह वाकई बहुत भयंकर थी। आदमी चिट्ठी पर किताब रखकर, अंगूठा नथुनों पर मलता बाहर निकल गया था।
औरत,चूहे को छटपटा कर ढूँढती थी। पता नहीं कैसे तो, चूहे को अनुभव हो जाती थी- औरत की छटपटाहट! चूहा फुदक कर बैठ जाता था उसकी गोदी में।
“सुनो रानी एक कहानी
एक था राजा एक थी रानी!”
“चुप्प, चूहा कहीं का!”
“सुनो बताएँ! एक आदमी था।”
“हुम्मऽऽऽ”
“एक औरत थी!”
“तो??”
“दोनों पति-पत्नी थे।”
“अच्छा!!
तो पति चौकी पर बैठा चिट्ठी लिखता होता था, और पत्नी अगल में बैठी मटर, छील रही होती थी।
पति बार-बार डांटता था- “चुप्प रहो, चिट्ठी लिखने दो।” पत्नी हर बार दाँत चियार कर बकबकाना जारी कर देती थी। “और तभी…., फुस्स से कुछ बड़ी भयंकर चीज घुल गयी थी हवा में।”
पति दायीं भौहें चढ़ाकर पत्नी को ताकता था। बेशरम पत्नी आँखें मटकिया कर बताती थी उसके नाना कई बरस पहले धनबाद कोईलरी में काम करते थे। नाना के एक पक्के दोस्त जो भोजपुर क्षेत्र के थे। एक दिन जब ऐसे ही नानी ने बदबू घोली थी हवा में, तब नाना ने पक्के वाले दोस्त की बीवी ने उन्हें एक किस्सा सुनाया था।
किस्से में एक नयी नवेली बहुरिया थी जो आँगन में बैठी साँझ की रसोई बना रही थी। घर के सभी मरद-मानुष खाने बैठे थे।
तभी, एक अवांक्षित सी आवाज के साथ कुछ हवा में घुल गया। सास ने बहू को झिड़का
“यहीं आँगन में तेरे ससुर-भसुर बैठे हैं, तुझे लाज नहीं आई?”
तब घूँघट की ओट से उस नयी नवेली दुल्हनिया ने सास को सुनाया। पत्नी, पति के कंधे पर कुहनी टिकाए बता रही थी।
“ससुर भसुर अंगना”
“बहुरिया कईली टींऽऽऽ”
पत्नी बड़ी अदा से पति की ठुड्डी सहलाती थी,
“ए सास हम कुल निक धिय”
“हम फेर करब टीं….!!”
तिरछा मुस्कुराता पति गरिया देता था- “चुप्प बनेच्चर!”
चूहे की मूँछ से नाक लड़ाती असली औरत पूछती थी,
“अच्छा बताओ, अभी हम खूब भीड़ वाली बस में होते तो ठीक होता न?”
“क्यों?”
“हम बड़े मजे से कह देते ‘राम! राम! पता नइ कोन हथी??”
………………………………………………………………………………………
एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमें नजर आया आईने में, कि हमारा चेहरा अद्भुत लावण्य से चमक रहा है हम सोचने लग गए थे कि ऐसा क्या हुआ था पिछली रात कि इस दुनिया में रहते हुए भी इतनी गाढ़ी नींद आ गई थी। हमें दोबारा भी चाहिए थी ऐसी ही गाढ़ी नींद।
औरत कई सारे यत्न-प्रयत्न कर डालती थी।
पिछले हफ्ते के दूसरे दिन को जब औरत पौने चार बजे फर्श पर पोंछा लगा रही थी, (बेशक यह एक रूटीन से बाहर का काम था) और पोंछा लगाते हुए ही वह चौकी के दाहिने पाये पर पहुँची थी कि, ठीक तभी बाहर गेट खुलने और साईकिल की खड़खड़ाहट साथ-साथ सुनाई पड़ी थी।
जल्दी आया हुआ आदमी हड़बड़ाया नहीं था उस दिन। आदमी ने बाल्टी में रखे पानी से स्नान किया था और बड़े आराम से मीठे बताशे के साथ पानी पी गया था।
चूहे ने बताया था औरत को, कि जब दुनिया में सारे संयोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो घटनाओं की पुनरावृति होती है।
औरत अपने हिस्से से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। रोज ठीक तब जब छोटी सूई तीन और चार के बीच रहती थी, तथा बड़ी सूई आठ पर होती थी औरत क्वार्टर के प्रवेश द्वार से पोंछा लगाना शुरू करती थी। बड़ी सूई के नौ पर पहुँचते ने पहुँचते, औरत को पोंछन समेत चौकी के दाहिने पाये तक पहुँच जाना था। पर, औरत पहुँची थी तब, जब बड़ी सूई नौ को पार कर गई थी।
संयोग पूरा नहीं हो पाया था। आदमी समय से घर पहुँचा था। कभी, ऐसा भी होता था जब, बड़ी सूई आठ और नौ के बीच ही रहती थी, तभी औरत चौकी के दाहिने पाये पर पोंछन लगाती पहुँच जाती थी। वो फिर अपने हिस्से से गलती कर गयी थी।
पर, अब औरत सचेत हो गई थी। औरत ने बड़ी नजाकत से पोंछन को बाल्टी के पानी में निचोड़ दिया था। फिर पोंछन को फर्श पर धीरे-धीरे रगड़ती बढ़ती गई थी। औरत ने घड़ी देखी। छोटी सूई तीन और चार के बीच थी, और बड़ी सूई आठ व नौ के बीच। औरत ताबड़-तोड़ पोंछन लगाती हुई चौकी के दाहिने पाये पर पहुँची थी। औरत ने समय देखा था। बड़ी सूई ठीक नौ पर थी। वहाँ फर्श पर पता नहीं कैसा तो एक दाग था। औरत बड़ी देर तक पोंछन रगड़ती रही। पर, दाग नहीं छूटना सो, नहीं छूटा। तीन पचपन हो गए थे, औरत थक कर आगे बढ़ गई।
औरत अंदर कमरे में गई थी। चूहेदानी की छत से अंदर कड़ियों में फँसी सूखी रोटी लटकी हुई थी और चूहा इधर से उधर दौड़ रहा था।
औरत घुटने मोड़ कर बैठ गई और चूहेदानी को अपने घुटनों पर रख लिया।
“झूठे हो तुम!” औरत को जोर का गुस्सा आया था।
“अरे हुआ क्या?” चूहा आकर चिपक गया चूहेदानी की दीवार से।
“संयोग-फंयोग कुछ नहीं होता, समझे!”
“होता तो है।” चूहे ने पूँछ सरसराई।
“आज क्यों नहीं हुआ तब?”
“उस दिन तुमने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी?”
“हरा!”
“आज क्या पहनी हो?”
“गुलाबी!”
“तो??”
औरत माथा पीटकर रह गयी थी अपनी गलती पर। उसने चूहेदानी का दरवाजा खट से खोल दिया था। चूहा बिला गया था क्वार्टर के किसी अंतड़े-पतड़े में।
आदमी हैरान होता था कि औरत रोज हरी साड़ी पहने रहती थी और आदमी के वापस आते ही साड़ी बदल लेती थी।
……………………………………………………………………………..
मोमबत्ती जलती थी, गलती थी, पर खत्म नहीं होती थी। टप-टप-टप पिघलती हुई मोमबत्ती, एक नयी मोमबत्ती तैयार कर देती थी।
औरत को चीजें बमुश्किल याद रहती थीं। किसी एक चीज को याद रखने के लिए कोई दूसरी चीज याद रखना निहायत अनिवार्य था जैसे!
जैसे मान लो मौसम ही!
आधा-बादल, आधा धूप जैसे किसी मौसम में औरत को मिट्टी के ढेलों से भरा हुआ लंबा-चौड़ा परती खेत याद आता था।
या जैसे की मान लो किसी की चिट्ठी! बिन देखे-सुने की चिट्ठी। अगर गोल-गोल नन्हें-नन्हें अक्षर हों तो सहज ही सुन्दर सलोनी आकृति बनती थी मन में- एक सुंदर सलोनी लजकोकड़ लड़की!
होने के जरूरत नहीं थी, बस ऐसा लगा करता था।
खूब टकाटक घूप सिर पर होने के समय में औरत को अक्सर अपने गाँव के उत्तरी मुहाने पर खड़ा दो कमरों का एक खंडहर याद आता था।
औरत खूब सोचती थी फिर भी नहीं समझ पाती थी कि ऐसा कैसे हो जाता है की अच्छे-खासे मकान के पीछे पीपल का एक पौधा उग आता है। नन्हा पौधा बड़ा हो जाता है, इतना कि उसकी जड़ें ईंटों वाले दो कमरों में जाले की तरह फैल गयीं थीं। खंडहर के पलस्तर इस कदर झड़ गए थे कि अधटूटी छतों वाला ईंटों का ढाँचा भर लगता था।
कभी दोनों पहर झाड़ू-पोंछा लगने वाले कमरों की फर्श पर बबूल की झाड़ियाँ उग आई थीं।
खाली घर संभावनापूर्ण होता। पर उन दो कमरों में इस कदर अबाड़-कबाड़ भरा था कि उस घर को सिरे से खाली करके नयी चीजें भरना असंभावनाओं से परिपूर्ण था।
पर, जिंदगी में एक बड़ी टुच्ची गलती पनप गयी थी।
औरत को समीकरण जल्दी समझ में नहीं आते थे। समझने के फेर वह इतना उलझ जाती थी कि, सबकुछ उल्टा-पुल्टा समझ लेती थी।
औरत, बच्ची थी तब पहली बार स्कूल गयी थी।
मास्टर जी ने सामने “बाल-पोथी” फैला दी और बोले पढ़।
औरत बच्ची धड़ल्ले से ‘क’ से कमल, ‘ख’ से खरगोश, ‘ग’ से गमला पढ़ती गयी थी और आकर अटकी थी “ब” पर।
गुरूजी बोले- “पढ़”!
“बऽऽ कऽऽ रऽऽ” में बड़ी ई की मात्रा “रीऽऽ।”!
“तो??”
“बऽऽ कऽऽ रऽऽ में बड़ी “ई” की मात्रा री!
“उच्चारण बताओ क्या होगा?”
बच्ची मोटी बरौनियाँ उठाकर गुरूजी को ताकती थी फिर जीभ पर जम आई थूक को निगल जाती थी।
बच्ची अपनी तर्जनी “ब” पर जमा देती थी और पूरे उत्साह से शब्द पढ़ना शुरू करती थी।
“बऽऽ कऽऽ रऽऽ में बड़ी ई की मात्रा री…!”
फिर बच्ची अपनी तर्जनी एक चित्र पर रखती थी,
“छगरी!!”
सहसंबंध का समीकरण समझने में सदैव आंशिक असफल होती रही अनाड़ी औरत, दरअसल ड्रामाई जिंदगी को जीते-जीते, ड्रामा जीने की ही अभ्यस्त हो गई थी और जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा तो शुरू हुआ था अब! अड़ोसियों-पड़ोसियों की मदद से औरत जब अपने पति का प्रकरण जान पाई थी तो रोमांच की लहर उसकी नाभि से होती हुई उसके गाल के एकदम महीन भूरे रोओं पर छितरा गयी थी।
औरत को पहला मौका मिला था कुछ जीत लेने का, और वो जीतना चाहती थी। कई सीढ़ियाँ थीं, वो पहली सीढ़ी पर चढ़ी थी। वह चूँकि क्षुद्र नहीं थी, इसलिए उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ना आदमी के माँ-बाप को, ना अपने नाना-नानी को। हालाँकि मन के महीनतम कोने में औरत यह जानती थी कि उन लोगों को बता देने का भी कोई अर्थ नहीं था, बावजूद इसके औरत ने अपना बड़प्पन बनाए रखा था।
औरत के पास बहुत छोटा सा पासपोर्ट साईज का आईना था। इसलिए औरत कभी अपनी पूरी देह नहीं देख पाई थी। पर उसे पता था कि, उसकी साँवली, छरहरी लम्बी देह में एकदम संतुलित नमक था। इतना संतुलित कि नवरात्र के व्रत में इंसान अन्न की कमी से नहीं नमक की कमी से बेचैन हो जाए।
पर आदमी मीठा प्रेमी था सो उसके लिए व्रत उपवास बहुत सुविधाजनक चीजें थीं।
औरत जब आई थी तो निहत्थी थी, पर शीघ्र ही आदमी ने पकड़ लिया कि अब औरत हाथ में हथियार लेकर चलती है। आदमी भी मजबूत ढाल लेकर सजग हो गया था।
पर दरअसल बात यह थी कि अनाड़ी हाथ में पिस्टल लेकर बस कहना जानते हैं- “पास मत आना, वर्ना गोली मार दूंगा।”
चला कभी नहीं पाते।
आदमी ने जल्द ही यह भी सूंघ लिया और ढाल को फिरकन्नी की तरह घुमाकर हवा में उछाल दिया।
ऐसा कभी नहीं होता कि, एक चीज कही जाए तो अगली बात एकदम सटीक समझ ली जाए। जैसे पानी कहने पर प्यास बाद में याद आती है और नदी, नाले, समुन्दर पहले याद आते हैं। और प्यास कहने पर बस लोटा भर पानी याद आता था नदी, नाले, समुन्दर नहीं।
वैसे “मृत्यु” कहने पर मर-जाना पहले समझ में आता है जबकि समझाना चाहते थे हम “भय”!
पिस्टल हाथ में लेने वाले अनाड़ी कभी नहीं जान पाते कि ट्रिगर पर कितना दबाव काम तमाम कर देने के लिए काफी है। डरा हुआ अनाड़ी इंसान, बस और बस डराना ही तो चाहता था। पर, उसे दबाव का अंदाजा नहीं हो पाया था और शूं…….गोली भेजे के पार!!
……………………………………………………………………..
एक नन्हीं सी सुपरिचित खबर यह थी, कि वह चौबीसों घंटे बिजली से सराबोर रहने वाला शहर था और लालटेनें वहाँ गरजने तड़कने वाली इक्का दुक्का रातों में ही जलती थीं।
उन्हीं यदा-कदा के चुनिंदा दिनों में से यह एक चौबीस घंटा भी दिनभर बरसने वाली बारिश का था।
बाहर रात थी, पत्तों से टपकती हुई बची-खुची बरसात थी, मेंढ़क थे, झींगुर थे और फितिंगियों से छपी कांपती हुई लालटेन थी।
औरत उसी एक रात में देख पाई थी, कि बजाए पूरे दिन के या बजाए पूरी रात के, आदमी लालटेन की टकाटक पीली आधी रौशनी में ज्यादा मोहक दिखता था।
आदमी थाली पर झुका था। पीली सुगबुगाती रौशनी की महीन रेखाएँ उसके मूँछों पर बिखरी हुई थीं।
गीले मौसम में औरत ने सूखा खाना बनाया था। सूखी रोटी, सूखी सब्जी और कोने में परोसा हुआ सूखा नून! आदमी कच्चा नून नहीं खाता था और नमक थाली में आखिर तक यूँ ही पड़ा रह गया था।
आदमी रोटी सब्जी खाने के बाद एक गिलास दूध पीता था।
शुरू-शुरू में औरत ने आदमी को गिलास में दूध दिया था। फिर पता नहीं कहाँ से तो उसने एक खूब बड़ा सा स्टील का कप जुगाड़ लिया था। उसी में दूध परोसती थी। हालाँकि कप, धारिता में गिलास का आधा ही था, इसलिए एक बार खत्म होने के बाद औरत दुबारा से कप को भर देती थी। आदमी चाहकर ही इस परिवर्तन का कारण नहीं पूछ पाया था। और सुड़क-सुड़क कर दूध खत्म कर जाता था।
वजह बहुत छोटी सी थी। आदमी रात में चूँकि हड़बड़ाया नहीं रहता था,
इसलिए दूध का बहुत नन्हा सा घूँट भरता था, और बहुत छोटी सी आवाज होती थी-
“सुड़ऽऽऽक!!”
आदमी के होठ जब कप से चिपकते थे, तो गोल हो जाते थे और उसकी पतली लम्बी नाक के नथुने हल्के से फूल जाते थे। ऐसे में आदमी छोटा सा बच्चा मालूम होता था।
“मऽऽ दऽऽ नऽऽ- मदन”
“घऽऽ रऽऽ – घर”
“चऽऽ लऽऽ – चल”
गिलास से दूध पीने पर होंठ ढँक जाते थे।
आसमान तड़ातड़ बरसने लगता था। चाँद होता था पर नहीं दिखता था, वैसे ही, जैसे नहीं दिखती थी हृदय में उठती हुई मरोड़।
औरत को कुछ गीलापन महसूस होता था। वह खाट से उतरी थी। बहुत आहिस्तगी से।
बत्ती गुल थी, और अँधेरा कहता था कि मैं ही हूँ । औरत टॉर्च से ढूँढती थी। आखिरकार आदमी की एक झरी हुई सफेद गंजी मिलती थी। औरत कफन की अदला-बदली कर लेती थी। हाँ सचमुच, औरत को ऐसा ही लगता था कि सफेद, नीले, पीले, छींटदार, कशीदेवाले, धारियों वाले तमाम रंगों और डिजाईन के कपड़ों की तह में औरत सदियों से लाशें फेंकती रही है। नन्हीं-नन्हीं अबोध-अधपकी लाशें। सादे-सुदे कपड़ों की तह में सोई पड़ी ये गाढ़ी-गाढ़ी लाशें कभी भी झट से अपनी आँखें खोल देंगी और लगेंगी हिलक-हिलक कर रोने।
काई से भरा हुआ सीमेंटेड आँगन था। आँगन के एक कोने में “स्नानघर” था और दूसरे कोने में “शौचालय”! स्नानघर से थोड़ी ही दूर पर काठ की एक कुर्सी रखी हुई थी जो कई दिनों से लगातार बारिश में भींग रही थी। गरज-तड़क बरसती काली रात में औरत बाएँ हाथ में एक नन्हीं लाश का बोझ उठाए धीरे से उतरती थी आँगन में। अचानक ऐसा लगा औरत को, कि खूब ढेर सारी नन्हीं-नन्हीं लाशें धीरे-धीरे सुबक रही हैं और अपनी मृत्यु का हिसाब माँग रही हैं।
खूब तेज डरी औरत हांफती हुई कमरे में आई थी, और भरसक संभलती रही थी।
“कुर्सिया दू दिन से बरखा में भिजित हई जी!”
……………………………………………………………………
औरत ने, आदमी के देह की ओर हाथ बढ़ाया था, और उतनी ही तेजी से वापस भी खींच लिया था।
औरत वापस दरवाजे के पास गई थी और खुले (आधा!) दरवाजे को झटके से पूरा खोल देती थी- भड़ाम-भड़ाम!
आदमी चौंक कर उठा।
“उ…. हम कह रहे थे कि कुर्सिया दू दिन से बरखा में भिजीत हई जी!”
आदमी मुंडी झुकाए दो मिनिट बैठा था, फिर टॉर्च जलाकर टाइम देखता था।
आदमी आराम से उठ कर बाथरूम में घुस जाता था। बहुत कम क्षण थे। औरत सर पर सूप से आड़ करके फिसलन भरे आँगन में संभल-संभल कर धीरे-धीरे चलती थी। पिछवाड़े का दरवाजा खोल नाले में लाशें बहा आती थी।
आदमी छाती पर हाथ बाँधे बरामदे में खड़ा था। औरत ने हाथ माँज कर बरामदे के किसी खूँटी में सूप टाँग दिया। उसने आँगन में देखा कि दो दिन से भारिश में भींगती कुर्सी अभी भी भींगती-गलती नजर आ रही थी।
उन दिनों औरत दिनभर हाथ माँजती रहती थी। इन्हीं दिनों को समझदार आदमी अपने आप बूझ जाता था। वह समझ जाता था कि औरत आज चांडालिनी, धोबिन या कि चमारिन की योनि में है।
शुद्ध आदमी, अशुद्ध औरत के हाथ का खाना खाने के बजाय बाहर से ही खाकर आता था।
औरत को नन्हकू चूहे ने एक कहानी सुनाई थी।
कहानी में एक प्यारी सी पत्नी थी और एक खूब अच्छा पति था। प्यारी सी पत्नी दिनभर के कामधाम के बाद खूब अच्छे पति की चौकी के बगल में चटाई बिछा लेती थी।
“ई चटाई इहाँ क्यों बिछाई हो?”
“सोयेंगे न…!”
खूब अच्छा पति हैरानी से ताकता था।
“तुम कुछ समझती तो हो नहीं!”
“क्या?”
“कुछ नहीं!”
“इधर आओ!”
पत्नी मुंडी हिला देती थी- “ना, ना, ना!”
“बुला रहे हैं न हम?”
प्यारी पत्नी लचकती हुई पहुँचती थी खूब अच्छे पति के पास।
“हाँ…! अब बोलो!”
पत्नी, पति की बाँहों के मछलियों पर ऊँगली से गोल-गोल कुछ-कुछ बनाती रहती थी।
“कुछ समझते तो हो नहीं, खाना बनवा कर खा लिए हमसे! पर अब हम सोयेंगे नहीं….”
रिसियाई हुई पत्नी की खीस में एक दुलार होता था।
“क्यों?” खूब अच्छा पति सारे नाटक का पटाक्षेप जानता था।
“पाप लगेगा जी!”
“किसे?”
“हमें…और किसे?”
खूब अच्छा पति चूम लेता था खूब प्यारी पत्नी के होंठ!
“लो, अब सारा पाप हमारा!”
लजाई हुई पत्नी, पति की छाती में छिप जाती थी।
असली औरत खाट पर लेटी थी। वो आँखों से कुहनी हटाकर आदमी को ताकती थी। आदमी चित्त सोया था। औरत मन ही मन उसे गरिया देती थी,
“कठकरेज”
………………………………………………………………………
आदमी के मित्र के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। औरत की खूब प्रगाढ़ पड़ोसिन ने कुछ दिनों पहले उसे हल्के पीले रंग की ताँत की साड़ी उपहार में दिया था। औरत, एकमात्र ताँत की वही साड़ी पहन रही थी। औरत को लग रहा था कि सिंथेटिक की अपेक्षा ताँत की साड़ी में बहुत ज्यादा नखरे हैं। ऊपर का भाँज सही बैठ गया था पर माँड की वजह से नीचे की भाँज बैठती ही न थी और गुब्बारे की तरह फूल गयी थी। औरत ने बहुत कोशिश की और इसी प्रयास में धम्म से गिर भी गई। उसने दरवाजे के पास पर्दे की झिर्री से देखा। शर्ट पैन्ट पहन कर तैयार खड़ा आदमी कलाई में घड़ी की बेल्ट फँसा रहा था।
अचार के जार के पीछे से चूहा दौड़कर आया और औरत के चारों तरफ घूमने लगा।
औरत उँगलियों में फंसाकर साड़ी की भाँज गिनती होती थी और झुँझला कर पूछती थी- “क्या है?”
“जानती हो एक खूब अच्छा जोड़ा था!”
“हूँऽऽऽ”
प्यारी पत्नी खूब अच्छे पति से कहती थी,
“ऐ सुनो! नीचे की भाँज सही कर दो ना!”
पति आँखें दिखाता था,
“अच्छा! अब हम तुम्हारी साड़ी ठीक करें न?”
पत्नी फिर गुजारिश करती,
“ऐ, कर दीजिये न जी!!”
झूठमूठ का खिसियाया हुआ पति भुनभुनाता था और साड़ी के नीचे वाली भाँज खींच-खींच कर सही कर देता था।
असली औरत का भाँज गिनना पूरा हो गया था। औरत “हूँ…!” करती थी और भाँज इकट्ठे करके पेटीकोट में खोंस लेती थी।
असली आदमी ने साड़ी की छितराई हुई प्लेट को देखा कहा, कुछ भी नहीं।
औरत कनैल का फूल लग रही थी।
आदमी हाथ खोले मस्ती में चलता था। औरत को, वे औरतें निहायत ही फूहड़ लगती थीं जो मर्दों की तरह हाथ भांज कर चलती थीं। लिहाजा औरत ने पीठ पर खुले आँचल के किनारी को दूसरे कंधे पर खींच लिया था और दोनों हाथ उसे सँभालने में व्यस्त हो गए थे।
भीड़ की धक्कम मुक्की थी। आगे-आगे चलता आदमी औरत के बराबर आ गया था। आदमी ने अनायास औरत को देखा। औरत कहीं और ताक रही थी।
आदमी डोर सुलझाते-सुलझाते पहुँचा तो पता चला कि वह चाट और गोलगप्पे का एक ठेला था।
साथ चलता आदमी फिर दो कदम आगे बढ़ गया और मजे से चलता हुआ ठेले के पास पहुँचा था। औरत बहुत बार, बहुत कुछ, पूछने-पूछने को होकर भी नहीं पूछ पाती थी। उसने आदमी को देखा और चुटकी भर मुस्कुरा पड़ी। तुरंत अपनी इस मुस्कुराहट पर वह लजा भी गई थी।
आदमी उड़ती नजर से देख रहा था आसमान, धरती, भीड़, बाजार, ठेला और आखिर में औरत पर नजर उड़ाकर आदमी घड़ी ताकने लगा था।
ठीक इसी क्षण जब, आदमी की उड़ती हुई नजर औरत पर से हटी थी, आदमी को ऐसा लगा था कि औरत मुस्कुराई थी। अपनी भ्रम की पुष्टि के लिए आदमी ने औरत को दुबारा से देखा था। लजाई हुई औरत प्यारी लग रही थी।
आदमी को पहली बार अफसोस हो रहा था। दरअसल यह एक “छोड़ी हुई” नहीं, बल्कि “छूट गई” मुस्कुराहट थी।
आदमी और औरत में गहरा अंतर था। आदमी बहुत सी चीजों को उधार के खाते में डाल देता था जबकि औरत तुरत-फुरत नकद लेन-देन कर निश्चिन्त हो जाती थी।
जैसे कि, ले लो मुस्कुराहट ही।
खूब भीड़ वाली सड़क पर चलते हुए कई तरह के नरमुंड दाएँ-बाएँ से गुजरते थे।
ऐसे ही कई तरह के नरमुंडों की भीड़ में आदमी को कोई चीन्हा हुआ नरमुंड दिख जाता था।
आदमी जब तक पहचान को चीन्हता, तक तक वह पहचान वाला चेहरा दृष्टि फ्रेम की परिधि से बाहर चल जाता था। आदमी को याद आता था कि, उस चेहर केे, होठों पर एक महीन सी मुस्कुराहट थी।
आदमी ठहर जाता था और मुड़कर देखता था। पहचान वाला चेहरा दूर निकल गया होता था। आदमी हल्का सा सिर झटकता था, मुस्कुराहट को उधार के खाते में डालकर आदमी आगे बढ़ जाता था।
औरत ठीक उलट थी।
औरत को जैसे ही याद आता था कि एक पहचाने हुए चेहरे पर उगी हुई मुस्कुराहट उससे छूट गई है, औरत ठहर कर मुड़ती थी।
बावजूद इसके कि वह पहचान वाला चेहरा दूर निकल गया होता था। औरत उसके पीछे भागती थी। हांफती, थकती, औरत उस चेहरे के करीब पहुँच कर उसके कंधे पर हाथ रखती थी। चौंक कर चेहरा मुड़ता था, तो औरत भर होंठ दांत चियारती थी। पिछली-बिचली-अगली-पीढ़ियों का हाल-समाचार लेती थी, तब वापिस आती थी।
औरत गोलगप्पों को होठों के पास लायी, तब मालूम चलता था कि गोलगप्पों का आकार होठों की फांक से बहुत बड़ा है।
औरत ने आदमी को कनखी से देखा। आदमी गोलगप्पों में व्यस्त था। औरत चेहरा घुमा लेती थी…और मुंह फाड़ कर गोलगप्पे ठूँस लेती थी।
…………………………………………………………………….
पैरों को हलके सूती चादर से ढँक कर बैठने वाली, रूई सी सर्द शाम थी।
औरत ने उबले हुए आलू को छीलकर उसमें ऊँगली धँसाया और “सीऽऽऽ” करके तुरंत निकाल भी लिया था। फिर पास में रखे लोटे के पानी से ऊँगली धो लिया।
पका हुआ टमाटर-बैंगन, उबला हुआ आलू और कतरे हुए लहसुन-मिर्च औरत ने एक कटोरे में लिया, पर हथेली से सान नहीं पायी।
यद्यपि औरत जानती थी कि हाथ से बना हुआ चोखा ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पर सबकुछ इतना गर्म हुआ था कि औरत ने उनपर नमक और सरसों तेल गिराकर कलछुल से मिला दिया था।
आदमी ने चोखा खाकर धीरे से पूछा,
“चोखा कलछुल से सानी हो क्या?”
औरत ‘हाँ’ करती थी, और हैरान होती थी। यानि कि, हाथ में सचमुच होता है कोई स्वाद।
यानि कि औरत इतना आलतू-फालतू नहीं सोचती थी।
यानि कि आदमी भी वह सोच सकता है जो वह सोचती है।
यानि कि शायद देह में भी होता होगा कोई स्वाद?
यानि कि, यानि कि…क्या? कुछ भी नहीं! कुछ हो भी तो क्या अंतर पड़ता था?
आदमी, चलो मान लो निरपेक्ष न होकर घृणा ही करता था तो भी क्या था?
औरत की माँग में पीला सिन्दूर था, मायका था, आदमी के माँ-बाप थे, गली-कूँचे मोहल्ले थे, महिमामय पूरा भारत-वर्ष था, और इन सब के बीच औरत का एक तरफा प्रेम था।
औरत घर पोंछती थी, और चूहे को ढूँढती थी।
आदमी पटरी के नट कसता था, प्वाइंटर रिपेयर करता था, शेड में खड़े इंजन का ब्रेक ठीक करता था और साँसों की हर अनुलोम-विलोम के साथ बंगालिन लड़की को सोचता था। इन सब के बीच क्षण के सौवें हिस्से भर समय के लिए भी पृथ्वी अपने अक्ष पर ठहरी नहीं थी।
ऐसा लगता था कि कोई उबा देने वाली चीज भी थी, जो धकेलती थी आदमी के पास। औरत के पास उबा देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी थी, सो औरत बार-बार मौत के पास भागती थी।
यह चीज बड़ी लुभावनी लगती थी। चूँकि कुछ भी नया बनाने पर अच्छा लगता था- नयी कविता, नयी कहानी, नया कपड़ा, नया पकवान, या नया दुःख ही!!
वो मरती थी, टहलती थी, खाती थी, खाट बिछाती थी, फिर मरने चूहे के पास आ जाती थी।
औरत बच्ची थी जब, तब जाड़े के दिनों में उसकी उँगलियों में नाखून के आस-पास का हिस्सा सूजकर लाल हो जाता था। बहुत दर्द देता था वह। उस सूजे हुए हिस्से पर किसी नुकीली चीज को चुभोने पर, एक नया दर्द पैदा होता था। और दोनों पीड़ाएं मिलकर एक अद्भुत मजा देती थीं। औरत बच्ची जाड़े भर यह खेल दुहराती थीं।
खूब बड़ी दुनिया के आगे औरत को बड़ा होकर जीना पड़ता था और सुलगते रहना होता था। औरत पड़ोसिनों से हंसती थी, बतियाती थी, उपहारों का पकवानों का लेन-देन करती थी और बड़प्पन से जीती थी- “श्रीमति फलाना परसाद!!”
औरत बहुत खुश थी कि अब उसके पास यह एक नन्हा सा चूहा था। छुद्र सा प्यारा चूहा जहाँ औरत बेखौफ क्षुद्र हो जाती थी और जी भर कर बुराई कर लेती थीं अपने मायके की, ससुराल की, पति की और तमामतर दुनिया की।
……………………………………………………………..
दुपहर के चार बजे थे।
पहाड़ी ट्रेन की सीटी भी,
सूरज को काटती हुई यही कहती है।
मैं दिल को सुनता हूँ इसके हृदयहीन पंखों को,
क्या कोई पक्षी पीड़ा में है?
मैं यह भी नहीं कह सकता मत हिलो,
ठहरो,
पीड़ा को थम जाने दो,
लेकिन वे समझते नहीं,
न दिल,
न उसके भीतर हिलता हुआ पक्षी,
दुपहर के चार बजे।
(निर्मल वर्मा की डायरी “धुंध से उठती धुन” से)
लगातार कई दिनों तक बरसते रहने के बाद आसमान थक कर, थम गया था। आसमान एकदम साफ था, स्टील की थाली में रखे पानी सा चमकता साफ आसमान और खूब कड़ी धूप!!
आदमी सेकेण्ड टाईम की ड्यूटी पर था।
बरसात की दुपहरिया सूखी हुई होने के बावजूद उमस भरी थी। हर कोने से सीलन और गीलेपन की बू उठ रही थी। औरत ने बाहर बरामदे में जहाँ खूब धूप थी, वहाँ अपनी खत डालकर उस पर गद्दे, तोशक, तकिए और घर भर के कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे।
फर्श ठंडा था। औरत ने टेबल फैन फर्श पर रख दिया और सुस्ताने लगी। पंखा पहले पहल घरघराया फिर खूब तेज-तेज चलने लगा। औरत ने अपनी चोटी खोल दी और पीठ पर लंबे गहरे भूरे बाल फैला दिए। उसने छाती से आँचल हटाया और नंगे फर्श पर लेट गई।
चूहा उछलता हुआ आया और उसके बाएँ हाथ को जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ नाखून सूंघकर भाग गया।
वो लेटी हुई आसान ढंग से मुस्कुरायी।
औरत गहरी नींद में थी। पंखा खूब तेज आवाज में घरघराया था। औरत चौंक कर उठी। बीच में शायद बिजली गुल हो गयी थी। और अब दुबारा बिजली आयी थी, तो पंखा शुरूआती घरघराहट कर रहा था। वो इतने गहरे सोई कि उसे बिजली गुल होने की खबर नहीं हुई थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। सवा तीन। दो-तीन उबासियों के बाद औरत ने आँचल को छातियों पर फैला लिया था।
औरत स्वीच ऑफ करने उठी थी ताकि पंखे को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया जाए और सन्नाक रह गई।
छोटा सा बच्चा, टेबल फैन के जालीदार दो कवर जहाँ पर मिलते थे उनकी बीच वाली जगह पर फँसा पड़ा था। सहमी हुई औरत ने झट से स्वीच ऑफ किया। तेजी से हनहनाता पंखा मद्धम पड़ गया। धीरे-धीरे रेंगती पंखुड़ियाँ थिरा गई थीं।
नन्हा चूहा शायद तब, जब बिजली गुल हुई थी, पंखे की जालियों पर चढ़ा खेल रहा होगा। अचानक बिजली आ गयी होगी। उसकी परवल जैसी बीच से चिराई हुई देह जालियों में फँसी चिपकी हुई थी। सुतली जैसी पूँछ बाहर लटक रही थी और पपीते के बीज जैसी आँखें खुली थीं।
औरत चुपचाप बैठी रह गयी थी, आदमी की वापसी तक।
बच्चे के दांत में दर्द था।
बच्चा चायनीज डाक्टर के पास गया। डाक्टर ने अच्छी तरह दांत का मुआयना किया और कहा,
“दांत तो पूरी तरह सड़ गया है। खूब दर्द हो रहा है न?”
बच्चा रिसिया गया। बच्चा सोचता था कि डाक्टर उसके दांत में से गोली जैसी कोई चीज निकल कर अपने दांत में ठूँस ले, और तब बताए,
“ओ माँ…! सच में! बिशो…न बेथा रे!!
एशिया, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, तमाम महाद्वीप, महासागरों के समानांतर एक नन्हीं दुनिया थी जहाँ पठार थे बस। औरत चूहे के साथ मिलकर धीरे-धीरे महासागरों के लिए गड्ढे खोदती रही थी। महासागर के लिए खुदते गड्ढों के अवशेषों से अवसादी चट्टानों के पहाड़ स्वयमेव तैयार होते जा रहे थे।
अब औरत अकेली पड़ गयी थी, इसलिए डर भी गई थी।
औरत पिस्टल ढूँढती थी।
उसे अंदर कमरे की रैक के अँधेरे कोने में “चूहे मारने वाली दवा” मिल भी गई थी।
भाज्य में भाजक से भाग देते हुए एक दशमलव भर बिठाया था, और बेशक खूब बड़ा भागफल मिलते हुए भी शेष शून्य हो जाता था।
…………………………………………………………………….
कहीं कोई खट की आवाज नहीं होती थी।
आदमी की नींद टूट जाती थी। आदमी दो तकियों के बीच से टॉर्च निकलता था, जलाने को होता था, पर जलाता नहीं था।
वापस टॉर्च को दो तकियों के बीच ही रख देता था। चौकी, चार गुटकों पर रखकर ऊँची कर दी गई थी तथा खाट को उसके नीचे ठेल दिया गया था।
आदमी, देह से लिपट कर सोई हुई सुन्दर बंगाली लड़की का दायाँ हाथ सहलाता था और आहिस्ते से उसे चूम लेता था।
लड़की कुनमुनाई तक नहीं थी और बेसुध सोयी रहती थी।
लेटे हुए खिड़की से बाहर झाँकने पर स्ट्रीट लाईट की पीली रौशनी के नीचे दूर तक जाती हुई सूनी पगडंडी दिखाई पड़ती थी।
आदमी को हर एकांत में उस औरत की आखिरी बात परेशान करने लगती है। औरत ने रोते हुए पीड़ा के साथ कहा था,
“हम मरना नहीं चाहते…हम तो बस तुम्हें डराना चाहते थे!”
कोई अभ्यास नहीं था जी!!
बस कोई खट की आवाज नहीं होती थी।
……और आदमी जाग जाता था।
’’’’’’’
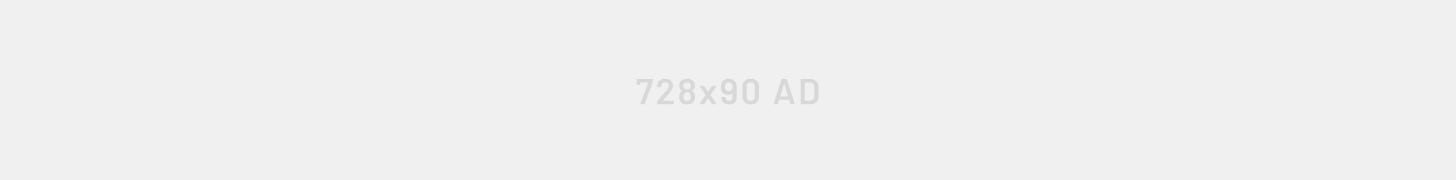
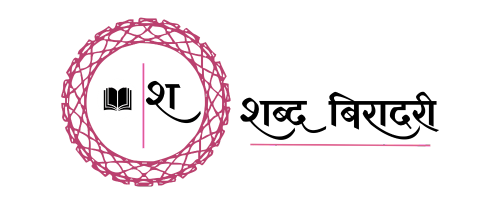

शानदार कहानी
कहानी अच्छी लगी| पढने में समय लगा| इसे हड़बड़ी में पढ़ा भी नहीं जा सकता| चित्रण बहुत अच्छा है| एक घर में रहते हुए भी आदमी और औरत की अपनी-अपनी दुनियां है| माथे में पीला सेनुर भरने वाली औरत की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं| पति उसके तात की साडी की कोर ठीक कर दे, महीने के दिनों में उसका बनाया खाना खा ले, थोडा सा उसे दुलार कर दे, कभी उसे देखकर मुस्कुरा ले| वो अकेलेपन का साथी एक चूहे को बनाती है, तमाम कोशिशे करती है अपनी उदासी को भगाने की और एक दिन पति का ध्यान पाने के लिए अपनी जान दे देती है| औरत का बचपन, उसकी माँ, उसकी नानी, बंगाली लडकी सभी लगता है कि आस पास की औरते हैं| नानी से लगकर सोती छोटी बच्ची नानी को यह एहसास नहीं होने देती की वह रो रही है, औरत भी अपना गम कहाँ ही पता चलने देती है|