
प्रजातंत्र के इस दौर में जबकि तानाशाही अपने पूरे शबाब पर है, तो भी सियासतदां जानता है कि उसे यह निरंतर दर्शाना है कि उससे बड़ा ग़रीबों का मसीहा, समाज और देश का शुभचिंतक कोई हो ही नहीं सकता। तो वह करे कुछ भी, लेकिन समय- समय पर इस बात को कहता रहता है और बार बार दोहराता रहता है। ‘ज़फ़र’ गोरखपुरी ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इस मंज़र को अपने शेरों में बाँधा है:
प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है
बादल अपने घर बरसाया जाता है।
धरती खुद भी खा जाती है फसलों को
चिड़िया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है।
सियासतदानों की फितरत में यह ट्रेंड अक्सर देखने को मिल जाता है। और सरकार के ख़िलाफ़ बोलना, माने देश के ख़िलाफ़ बोलना। सत्तारूढ़ पार्टी के ख़िलाफ़, उसकी सरकार के ख़िलाफ़, उसकी किसी नीति, किसी ज़्यादती के खिलाफ बोलने वाले को देश का ग़द्दार घोषित कर दिया जाता है । इस तर्कहीन, विवेकहीन तुलना को सरकारें जब अपना तरीका बना लेती हैं तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बिना किसी राजनैतिक या व्यक्तिगत मक़सद के, हर ग़लत बात को ग़लत कहने का बीड़ा उठाया हुआ हो । क्योंकि ऐसे लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं होता। किसी प्रकार का राजनैतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त होता नहीं। कानून-वयवस्था भी ऐसे हुक्मरानों के दरबार में प्राय: हाथ जोड़े खड़ी रहती है। और एक तर्कशून्य, विवेकशून्य बड़ी भीड़ तो सिर्फ अपने आकाओं के इशारों पर ऐसे ‘गद्दारों’ को सबक़ सिखाने के लिए हमेशा तैयार बैठी होती है। मुनव्वर राणा का यह शेर ऐसी सोच रखने वाले हुकुमरानों के मुंह पर एक करारा तमाचा है:
जिसे भी जुर्मे-गद्दारी में तुम सब क़त्ल करते हो
उसी की जेब से क्यों मुल्क का झंडा निकलता है।
बशीर बद्र का यह शेर इस फितरत पर एक तगड़ा व्यंग्य है। बेगुनाह व्यक्ति अदालतों में बड़े-बड़े हुनरमंद वकीलों का सामना नहीं कर पाता और बेगुनाह होते हुए भी उसे न्याय नहीं मिल पाता :
शाम के बाद कचहरी का थका सन्नाटा
बेगुनाही को अदालत के हुनर याद आए।
मुनव्वर राणा ने उन शायरों पर भी तंज़ कसा है जो, वह न करके जो उनसे अपेक्षित है, राजमहलों की खुशामद करने में मश्गूल हो जाते हैं:
अजब दुनिया है, नाशायर यहां पर सर उठाते हैं
जो शायर हैं वो महफ़िल में दरी चादर उठाते हैं।
और शायद कुछ लोगों की ऐसा करने की कुछ मजबूरियां भी रहीं हों। इसी ग़ज़ल के एक और शेर में वे यह भी कहते हैं:
ग़ज़ल, हम तेरे आशिक़ हैं मगर इस पेट की ख़ातिर
क़लम किस पर उठाना था क़लम किस पर उठाते हैं।
और जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो वह हुक्मरानों को आगाह भी करते हैं:
बुरे चेहरों की जानिब देखने की हद भी होती है
संभलना आईनाख़ानो कि हम पत्थर उठाते हैं।
सत्ता के पास बहुत तरीके होते हैं हवाओं के रुख को अपनी तरफ़ मोड़ने के लिए। न्यूज़-मीडिया के अलावा भी उन को ऐसे बुद्धिजीवियों की आवश्यकता होती है जो उनके हर-सही ग़लत काम की भूरि-भूरि प्रशंसा करें, अपने सौम्य और प्रभावी लेखन से उनके पक्ष में एक माहौल बनाएं। इसके लिए सत्ता साम-दाम-दंड-भेद किसी भी तरीके को अपनाने से गुरेज़ नहीं करती। पुरस्कार, अवार्ड्स, बड़ी-बड़ी और महत्त्व पूर्ण संस्थाओं के ऊंचे-ऊंचे पद, ये सब ऐसे प्रलोभन हैं जिससे सभी लेखक, कवि-शायर, साहित्यकार बच नहीं पाते। कुछ न कुछ तो सत्ता के इस जाल में फंस ही जाते हैं । बशीर बद्र की एक ग़ज़ल है:
कोई लश्कर है, कि बढ़ते हुए ग़म आते हैं।
शाम के साए बहुत तेज़ क़दम आते हैं।
इस ग़ज़ल का यह शेर देखिए:
मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए
कभी सोने, कभी चांदी के क़लम आते हैं।
चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। ताक़तवर हुकुमरां के एक इशारे पर उनकी महफ़िलों में सितारों की भीड़ लग जाती है । चाहे वो फिल्म-जगत के सितारे हों, या खेल-जगत के, या किसी अन्य क्षेत्र से। कोई दिल से न भी जाना चाहता हो तो भी आला कमान के निमंत्रण को कौन ठुकरा सकता है। और जब सब आ ही जाते हैं तो किसी की क्या मजाल कि वह हुजूरेआला के खिलाफ़ कुछ बोल दे। बल्कि ऐसी महफ़िलों में साहिब की शान में बोलने वालों में, उसकी सभी नीतियों को सही ठहराने की एक होड़ सी लग जाती है । यह सभी के लिए एक विन-विन सिचुएशन होती है । जहां हर सितारे को, वो जिस आसमान पर होता है, उस से और ऊपर के किसी आसमान की तलाश होती है, वहीँ हुकुमरां के पक्ष में अपने चहेते सितारे की बातें सुनकर उसके चाहने वाले गदगद हो उठते हैं और उस सितारे के पाँव और अधिक मज़बूत हो जाते हैं और सीना और अधिक चौड़ा हो जाता है । परन्तु सच्चे शायर को यह सब रास नहीं आता। अदम गौंडवी का तो ऐसी सभाओं में दम घुटने लगता है:
ग़ज़ल को ले चलो अब गाँव के दिलकश नज़ारों में
मुसलसल फ़न का दम घुटता है इन अदबी इदारों में
मुनव्वर राणा जहां अपनी बेबाक़ शायरी से सियासतदानों को बेनक़ाब करते हैं, सोई हुई जनता को जगाने का प्रयास करते हैं और अपनी राह से भटके शायरों/साहित्यकारों को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, वहीं इस चिंता में भी ग्रस्त नज़र आते हैं कि अपने संकीर्ण स्वार्थों में लगे सियासतदां कहीं आने वाली पूरी पीढ़ी को ही नफ़रत की आग में न झोंक दें। उनका यह शेर उनकी इस चिंता का ही इज़हार है कि इस फिरकापरस्ती के माहौल में ये नन्हे-मुन्ने, भोले-भाले बच्चे कहीं अपनी मासूमियत ही न खो दें:
इन्हें फ़िरकापरस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे
ज़मीं से चूमकर तितली के टूटे पंख उठाते हैं।
भारत भूषण आर्य को भी यही चिंता सता रही है कि खौफ़ और दहशत के इस माहौल में बच्चों को सुनाने के लिए कोई कहानियां भी नहीं बची हैं, उन्हें क्या सुनाया जाए:
खौफ़, दहशत, हादसों तक रह गई दुनिया
अब न बच्चों के लिए कोई कहानी है
बशीर बद्र के इन शेरों में भी कुछ ऐसी ही चिंता नज़र आती है:
आस होगी न आसरा होगा .
आने वाले दिनों में क्या होगा।
आसमां भर गया परिंदों से
पेड़ कोई हरा गिरा होगा।
बशीर बद्र के ही एक और शेर पर नज़र डालें:
कभी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं
हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता।
‘बरसात के मौसम में शादाब बेलों का सूख जाना’ अपने आप में कई अर्थ संजोये है, कई तरफ़ इशारे करता है जो बहुत ही स्पष्ट हैं । मेरी नज़र में यह शेर लगभग वही कैफ़ियत लिए है जो हिंदी ग़ज़ल के पुरोधा दुष्यंत कुमार के इस बहुचर्चित शेर में नज़र आती है:
यहां तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियाँ
मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।
सियासतदां अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सियासत की चमक बरकरार रखने के लिए किसी हरे-भरे शजर को भी छितरा-छितरा बिखेर देने में भी कोई संकोच नहीं करते। ‘मख़मूर’ सईदी लोगों के बीच बढ़ती दूरियों और लगातार कम होते भाईचारे का एक मंज़र अपनी इस ग़ज़ल के शेरों में खेंचते नज़र आते हैं:
कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियाँ।
घर कहीं गुम हो गया दीवारो-दर के दरमियाँ।
क्या कहें? हर देखने वाले को आख़िर चुप लगी
गम था मंज़र इख़्तिलाफ़ाते-नज़र के दरमियाँ।
इख़्तिलाफ़ात – मतभेद
बस्तियाँ, ‘मख़मूर’ यूँ उजड़ीं कि सहरा हो गईं
फ़ासले बढ़ने लगे अब घर से घर के दरमियाँ।
यकीनन यह सब सियासतदानों और धर्म के ठेकेदारों का किया-धरा है। ‘अंजुम’ लुधियानवी’ ने भी अपनी इस ग़ज़ल में डर और बे-एतबारी के इस दौर में बनते हालातों के कुछ मंज़र अपने ख़ास अंदाज़ में पेश किए हैं:
एक लम्हे के लिए ये मोअजज़ा* देखा गया।
पत्थरों के शहर में इक आईना देखा गया।
मोअजज़ा* – चमत्कार
आईनाख़ाने में कल उस शख़्स को कोड़े पड़े
जो हवा मुट्ठी में ले कर, घूमता देखा गया।
शहर में हर शख़्स को था, अपने गुम होने का डर
हर कोई साए के पीछे, भागता देखा गया।
सब की सब पगडंडियों पर क़ाफ़िलों की भीड़ थी
अस्ल रस्ते पर न कोई नक्शे-पा* देखा गया।
नक्शे-पा* – क़दमों का निशान
ये आख़िरी शेर, एक तरह से, हुक्मरां पर से उठते विश्वास को बख़ूबी दर्शाता है। कोई उन रास्तों की तरफ़ नहीं जाना चाहता जिन पर हुकुमराँ से सामना हो जाने का खतरा हो। मेरी एक ग़ज़ल का नीचे दिया शेर भी कुछ इस ओर ही इशारा कर रहा है:
हुकुमराँ फिर शहर में निकला है
फिर नया एक हादसा होगा।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष सियासतदां पर बहुत विश्वास रखते हैं और उसे बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा शासक और इंसान मानते हैं । उनकी श्रद्धा की बुनियाद उनके इसी विश्वास पर टिकी होती है । परन्तु अगर कभी उनका यह विश्वास ग़लत निकलता है तो उनकी आशाओं की नींव हिल जाती है, उनके विश्वास की बुनियाद टुकड़ा-टुकड़ा बिखर जाती है। ‘इशरत’ किरतपुरी की एक ग़ज़ल है,
मेरी आहट, मेरी आवाज़ से पर्दा करके।
वो पशीमान है दीवार को ऊँचा करके।
इस ग़ज़ल में उनका एक शेर है जो इस स्थिति को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है:
नाख़ुदा हमको डुबोते तो कोई बात न थी
हम तो डूबे हैं ख़ुदाओं पे भरोसा करके।
और जब-तक असलियत सामने आती है, बहुत देर हो चुकी होती है। इतना ही नहीं, ख़ुदा-न-ख़ास्ता, अगर वे इस सच्चाई को सब के सामने लाने की कोशिश भी करें तो अपने उस ‘भगवान’ के कोप के भागी बन जाते हैं । नसीम अजमल का यह शेर ऐसी स्थिति को हू-ब-हू चित्रित करता है:
क्या ख़बर थी वही दीवार गिरेगी मुझपर
जिसकी तस्वीर उतारी थी सजाने के लिए।
वक़्त की यह मांग है कि इस सब के ख़िलाफ़ न सिर्फ आवाज़ उठाई जाए बल्कि उसे बुलंद भी किया जाए। तभी किसी बड़े परिवर्तन की आशा की जा सकती है। ‘अदम’ गौंडवी ने तो शायरों को साफ़-साफ़ ताक़ीद ही कर दी कि वे इश्क़-मोहब्बत, चाँद-तारों की दुनिया से बाहर निकलें और ठोस ज़मीनी सवालों पर गौर करें:
अदीबो, ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ
मुलम्मे* के सिवा क्या है फ़लक के चाँद-तारों में।
* चमक
कहीं पे भुखमरी की धूप तीखी हो गई शायद
जो है संगीन के साए की चर्चा इश्तहारों में।
अपनी एक और ग़ज़ल में वे सियासतदानों की बढ़ती ख़रीद-फ़रोख़्त पर अटैक करते हैं और सीधे-सीधे ऐलान करते हैं कि इन हालात में जनता के पास सिवाय बग़ावत करने के और कोई चारा ही नहीं बचा। आइये उनकी इस ग़ज़ल के दो शेर देखे लेते हैं:
पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें
संसद बदल गई है यहां की नख़ास* में।
*बाज़ार/मंडी
जनता के पास एक ही चारा है – बग़ावत
यह बात कह रहा हूँ मैं होशोहवास में।
सियासी हलकों में पूँजी और भ्रष्टाचार के दख़ल का सीधा-स्पष्ट उल्लेख इस शेर में किया गया है ।
जमील हापुरी ने अपनी एक ग़ज़ल में सत्ताधीशों के ज़ुल्मात, अस्त-व्यस्त व्यवस्था और इन सबके चलते प्रजा की दुर्दशा का जो मंज़र बाँधा है, वह बहुत ही भयावह और रौंगटे खड़े कर देने वाला है। मेरी खुदा से गुज़ारिश है कि ऐसे मंज़र किसी के दरपेश न आएं:
जिस्म तक बेच डाले गए।
पेट फिर भी न पाले गए।
जश्ने-मक़तल* मनाया गया
सर हवा में उछाले गए।
* क़त्ल करने का स्थान
सर हिलाना ग़ज़ब हो गया
बस्तियों से निकाले गए।
लूट सड़कों पे ऐसी मची
कमसिनों को उठा ले गए।
खिड़कियों से गिराया गया
चाकूओं पर संभाले गए।
शान से जीने वालो, जिओ
जान से जाने वाले गए।
समाज को धर्म-जाति-पंथ आदि के आधार में बाँटने से सत्ता को फ़ायदा तो मिलता है, पर परस्पर वैमनस्य इस क़दर बढ़ जाता है कि सब ओर नफ़रतों के शोले सुलगने लगते हैं। और उन्हें हवा देने वाले तो तैयार बैठे ही होते हैं। फिर जो हालात पैदा होते हैं, उन पर काबू पाना किसी के बस में नहीं होता। जगह-जगह नफ़रतों के विस्फ़ोट होने लगते हैं और मानवीयता धूं-धूं कर जलने लगती है।
भीड़ जब क़ानून को अपने हाथ में लेती है, तो सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती हैं । दंगई भीड़ का चेहरा बहुत खौफ़नाक होता है । फ़िरकापरस्ती की आग भड़काने वाले दूर से तमाशा देखते हैं ।
नासिर काज़मी के इन शेरों में तूफ़ान के बाद की ख़ामोशी कुछ इस तरह देखने को मिलती है:
बाज़ार बंद, रास्ते सुनसान, बे-चराग़
वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई।
गलियों में अब तो शाम से फिरते है पहरेदार
है कोई-कोई शम्अ सो वो भी बुझी हुई.
नसीम अजमल का यह शेर कुछ ऐसे ही एहसासात लिए है:
चमन कल था जो सहरा हो गया है।
अजब रूहों का डेरा हो गया है।
और यह शेर भी:
बर्ग-ओ-शजर सब काँप रहे थे दीवारें चुपचाप खड़ी थीं
वो तो सन से गुज़र गया था फिर ये हवाएँ किसकी थीं।
मेरा यह शेर भी इन तूफ़ानों से पैदा हुए इसी ख़ौफ़नाक मंज़र को कलमबद्ध करने की एक कोशिश है:
अब नहीं मिल पाएंगे उस रेत पर मेरे निशां
मैं चला था जब वहां से चल रहीं थीं आंधियां।
और ये शेर भी:
ख्वाब में मेरे न जाने क्या ख़लल चलता रहा।
इक अजब सा शोर था मैं रातभर डरता रहा।
बंद दरवाज़ों से गलियाँ रात भर लिपटी रहीं
बस्तियों से जाने कैसा शोर सा उठता रहा।
एक और ग़ज़ल से लिए मेरे ये शेर भी देखिए:
सुनी हैं रात भर इतनी सदाएं
अभी तक दिल मेरा सहमा हुआ है।
बड़ी वीरान सी लगती हैं गलियां
कोई बतलाए, आख़िर क्या हुआ है।
मेरा एक शेर है:
उनको मालूम नहीं कौन यहाँ रहता था
किसका घर फूँक के आए हैं जलाने वाले
माने अधिकतर तो ये बलवा करने वाले यह भी नहीं जानते कि जिस घर को वो जला रहे हैं , वह किसका है। बस जो सामने आ जाए, वही फ़िरकापरस्ती की इस आग में स्वाह हो जाता है ।
अदम गौंडवीने अपने एक शेर में साफ़-साफ़ कहा है कि दंगों की आग में झुलसने वाले अक्सर ग़रीब, दबे-कुचले लोग ही होते हैं और दंगे भड़काने वालों के अपने कुछ पहले से सोचे-समझे मकसद होते हैं, कुछ ज़ाती फ़ायदे होते हैं जिनके लिए वो कुछ भी कर गुज़रने से नहीं कतराते :
शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले
कोठियों की लॉन का मंज़र सलौना हो गया
रसूल अहमद साग़र ‘बक़ाई’ ने तो अपनी एक ग़ज़ल में ऐसे सियासतदानों के बारे में अपने ख़्यालात को सीधे-सीधे ज़ाहिर कर दिया है, जो समाज में इतनी नफ़रत फैलाते हैं कि सब-कुछ जल कर ख़ाक हो जाता है। उनकी नज़र में यदि विभिन्न धर्मों के लोग चाहें भी कि वे आपस में प्यार-मोहब्बत से रहें तो भी उनके तथाकथित ठेकेदार यह होने नहीं देते। आइये, उनकी यह ग़ज़ल देखें:
नफ़रतों की आग में यूँ बस्तियाँ रख दी गईं।
घास पर जलती हुई ज्यों तीलियाँ रख दी गईं।
हिन्दू-मुस्लिम ने कभी जब एकता का मन किया
धर्म की दोनों तरफ़ बारीकियाँ रख दी गईं।
हक़ में लीडर के हमेशा हर बजट आता रहा
मुफ़लिसों के रूबरू मजबूरियाँ रख दी गईं।
मैंने छेड़ी जंग जब भी माफ़ियाओं के ख़िलाफ़
मेरे सीने पर तभी कुछ बरछियाँ रख दी गईं।
लिख रहा था वो सियासत की हक़ीक़त इसलिए
काटकर उसकी सरासर उंगलियां रख दी गईं।
समाज के और धर्म के ये ठेकेदार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए काम करते हैं । गरीबों की भलाई करने का ढोंग करते हुए वे और उनके भागीदार चुपचाप मलाई खाते रहते हैं, बेचारी जनता के हिस्से में तो सिवाय मुफ़लिसी के कुछ नहीं आता । और यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति इन बेबस लाचार लोगों के पक्ष में बोलने की हिम्मत करे तो उसे इन ताक़तवर स्वयम्भू ठेकेदारों के कोप का भागी बनना पड़ता है। किसी की क्या मजाल कि कोई सत्ताधीशों की सरपरस्ती में पलने वाले इन ठेकेदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश भी करे। उनके ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के सीनों पर तलवारें रख दी जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ लिखने वालों की उंगलियाँ काट दी जाती हैं ।
रसूल अहमद साग़र ‘बक़ाई’ के ये दो शेर भी हुक़ुमरानों के चेहरे से झूठी नक़ाब नोच के फेंक देते हैं और उनके असली चेहरे से हमें रूबरू करवाते हैं:
सारे शहर में अम्न का चर्चा रहा बहुत।
फिर भी घरों में आदमी डरता रहा बहुत।
वो रहनुमा ही अपना वतन लूटने लगे
जिनकी वफ़ा पे हमको भरोसा रहा बहुत।
सता के इरादों को समझने और उस की हर चाल को सामने लाने वाले शायरों की कोई कमी नहीं है । शैलेन्द्र कुमार पांडेय ‘शैल’ अपने ग़ज़ल-संग्रह ‘परछाईंयों के पाँव’ में लिखते हैं :
आम-ज़न के हक़ की बातें कर रहे जो मंच से
भेड़िये बैठे हैं छुप के मेमनों की खाल में।
आप की इन मसनवी बातों का बोलो क्या करूँ
भूख़ खा कर कब तलक बैठा रहूँ चौपाल में।
उनकी नज़र में हालांकि आम आदमी भी सियासतदानों की साज़िशों को अच्छे से समझता है, पर कुछ बोलता इस लिए नहीं की उसके नज़दीक़ सियासी साज़िशों से भी बड़ा एक मुद्दा है, जिसका हल उसे पहले ढूंढना है और वह मुद्दा है, भूख़!
हर रोज़ वही भूख़, वही रोटियों की दौड़
साज़िश रहे कि पेट बड़ा मसअला रहे।
उनका यह शेर भी शासकों की धूर्तता को एक अनोखे अंदाज़ में ज़ाहिर करता है:
यूँ तो सब इलज़ाम सर कौवों के चस्पा हो गए
लोमड़ी के ख़ून की मक्कारियाँ ज़िंदा रहीं।
पर उनको डरना मंज़ूर नहीं !
पत्थरों से ख़ौफ़ खाना ‘शैल’ ने सीखा नहीं
आईने टुकड़े हुए, बेबाकियाँ ज़िंदा रहीं।
शैल कहते हैं कि अगर हुक्मरानों ने बोलने पर पाबंदियां लगा दी हैं तो क्या हुआ, आँखों की भी तो ज़ुबान होती है:
तख्तों ने बिठाये हैं पहरे जो ज़ुबानों पे
दुनिया को जगाने को आँखों को जुबां देना
वहीं इफ़्तेख़ार आरिफ़ अपनी इस ग़ज़ल में लिखते हैं:
बोलती आँखें चुप दरिया में डूब गईं
शहर के सारे तोहमतगर ख़ामोश हुए।
खेल तमाशा बरबादी पर ख़त्म हुआ
हंसी उड़ा कर बाज़ीगर ख़ामोश हुए।
कच्ची दीवारें बारिश में बैठ गईं
बीती रुत के सब मंज़र ख़ामोश हुए।
दुष्यंत के अनुसार आम आदमी के लिए सियासतदानों की सियासती चालों को समझना संभव नहीं है क्योंकि उसमें अभी तक इंसानियत बाकी है। यानि वह सीधे-सीधे कह रहे हैं कि शिखर तक पहुँचते – पहुँचते अक्सर सियासतदानों के अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका होता है। वे जो भी क़दम उठाते हैं, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मक़सद होता है, अपना सियासती फ़ायदा, चाहे वह किसी भी क़ीमत पर मिले !
मस्लहत आमेज़ होते हैं सियासत के क़दम
तू न समझेगा सियासत तू अभी इंसान है।
मस्लहत आमेज़= भलाई से परे
सियासत के खेल वाकई निराले होते हैं । कहाँ कौन किस के साथ मिलकर क्या खेल खेल रहा है, यह आम आदमी की सोच से बहुत परे होता है । मुमताज़ नाज़ां का यह शेर कुछ इसी तरह की क़ैफ़ियत लिए है :
जो निस्बत मौज से थी, साहिलों से भी वही रगबत
न हम को इल्म था, साहिल से मौजों की है मंसूबी।
भारत भूषण आर्य की नज़र में भी सियासत के खेलों को समझना बहुत मुश्किल है । जो कल तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे कब एक-दूसरे के सुर में सुर मिलाने लगें, क्या पता?
ये सियासी खेल भी क्या खेल है
नेवले-ओ-सांप मिल गाने लगे
सियासतदाँ बहुत चालाक होते हैं। भोली भाली जनता को बहकाने के लिए उनके पास बहुत तरीके होते हैं। वे अक्सर लुभावने नारों और संवेदनात्मक मुद्दों का प्रयोग जनता का ध्यान ज़मीनी हक़ीक़त और अपनी नाकामियों से हटाने के लिए करते हैं। लेकिन उनके ये दुष्प्रयास एक शायर की पैनी नज़र से नहीं छुप पाते। वह आम आदमी को आगाह भी करता है । दुष्यंत का यह शेर देखिए :
आज सड़कों पे लिखे हैं सैंकड़ों नारे न देख
घर अँधेरा देख तू आकाश के तारे न देख।
आदम गोंडवीनेतो सियासतदानों के सभी झूठे दावों को लोगों के सामने लाने कि मानो सौगंध ही उठा रखी हो । सत्ता के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना उनके लिए आम बात है । कौन जाने देश-भर की योजनाएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील आंकड़ों को इकट्टा करना और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर है, उन्हें भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती हो! और अपने आपको सबसे अधिक डेमोक्रेटिक साबित करने में तो कोई भी पीछे नहीं रहता, असलियत चाहे कुछ भी हो:
तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है ।
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है ।
उधर जम्हूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो
इधर परदे के पीछे बर्बरीयत है , नवाबी है ।
अपने आपको जनसेवक कहने वाले शाहों पर तो आदम गोंडवी ने जम कर वार किये हैं । चाहे रोज़-रोज़ नित-नए घोटाले होते रहें, आम जनता लुटती रहे, इन जनसेवकों को कोई फर्क नहीं पड़ता । बस शोहरत के इन तलबगारों की डुगडुगी बजती रहनी चाहिए:
आँख पर पट्टी रहे और अक़्ल पर ताला रहे ।
अपने शाहे-वक़्त का यूँ मर्तबा आला रहे ।
एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए
चार छ: चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे ।
गोपालदास नीरज का यह शेर देखिए। मेरी नज़र में उनका ये शेर काल और देश की सीमाओं के परे भी इशारे करता है:
ज्यों लूट लें कहार ही दुल्हन की पालकी
हालत यही है आजकल हिन्दोस्तान की।
लेकिन संघर्ष के लिए संगठित होना पड़ता है, विशेषकर तब जब संघर्ष एक बेहद ताक़तवर सत्ता के साथ हो। पर मुश्किल यही है कि साहित्यकार अधिकतर अकेला ही होता है। शायर तो और भी अधिक अकेला होता है, कभी-कभी तो वह अपने साथ भी नहीं होता । फिर भी इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है । दुष्यंत को तो बहुत उम्मीद है कि यहीं से कोई रास्ता निकलेगा :
मेरी ज़ुबान से निकली तो सिर्फ नज़्म बनी
तुम्हारे हाथ में आयी तो एक मशाल हुई ।
ऐसे लोगों के लिए, जो देश को एक कर देने के वादे कर के सत्ता में आए, और फिर खुद ही देश को बांटने के काम में लग गए, दुष्यंत ने क्या खूब लिखा है:
आप दीवार गिराने के लिए आये थे
आप दीवार उठाने लगे ये तो हद है।
ख़ामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है
ख़ामोशी शोर मचाने लगे ये तो हद है।
हुकुमरां अपने निजी फायदे के ख़ातिर, सिर्फ लोगों के दरम्याँ दीवारें ही नहीं खड़ी करते, बल्कि उनके दिलों में भी ऐसी दरारें पैदा कर देते हैं जिन्हें भरना बहुत मुश्किल होता है और उनको अपने लुभावने नारों से ढक देते हैं जैसा कि दुष्यंत ने अपने इस शेर में कहा है:
अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार
घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार।
आदम गोंडवी का संवेदनशील मन यही चाहता है कि समाज में सबको न्याय मिले, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सबके लिए रोटी-कपड़ा-मकान की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों । वो सत्ताधीशों को आगाह भी करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी के जज़्बातों से न खेलें :
हिन्दू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िए।
अपनी कुर्सी के लिए जज़्बात को मत छेड़िए।
छेड़िए इक जंग मिल-जुल कर ग़रीबी के ख़िलाफ़
दोस्त मेरे, मज़हबी नगमात को मत छेड़िए।
अदम की नज़र में प्रगति का नाम आकाश को छूना नहीं है । आदमी का विकास चाँद-तारों पर विजय पा लेने भर से नहीं हो जाता । यदि हम अपनी उड़ानों के चलते ज़मीन पर रहने वाले सब से नीचे के आदमी को नहीं देख सकते, तो यह हमारा बड़ा होना नहीं, बौना होना है । यह इंसानियत का विकास नहीं पतन है:
चाँद है ज़ेरे क़दम, सूरज खिलौना हो गया।
हाँ, मगर इस दौर में क़िरदार बौना हो गया।
ढो रहा है आदमी काँधे पे ख़ुद अपनी सलीब
ज़िन्दगी का फ़लसफ़ा जब बोझ ढोना हो गया।
राहत इन्दौरी सियासतदानों की चालों को बख़ूबी समझते हैं और वे और वे इनसे डरने के बजाय बिना किसी लाग-लपेट के उन्हें आईना दिखाते हैं:
लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में
यहाँ पे सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है
हमारे मुँह से जो निकले वही सदाक़त* है
हमारे मुँह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है
*सच्चाई
जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे
किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है
साहित्य का एक काम समाज में व्याप्त घोर निराशा को दूर भगाने के लिए आशा के नित नए दीप जलाना भी है । आईये जमील ‘हापुड़ी’ की एक ग़ज़ल के दो शेर देखते हैं:
क़ातिल का कहीं किरदार तो है।
कागज़ की सही, तलवार तो है।
क़ाबू में नहीं कश्ती न सही
हाथों में अभी पतवार तो है।
जमील इन शेरों में कुछ सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उम्मीद जगाये रखने की कोशिश करते हैं कि हालात से लड़ते हुए, जहां तक जितना हो सके, उतना ही करते चलना भी एक तरह से क्रान्ति की नींव डालना ही है, अन्याय के खिलाफ़ लड़ाई को जिंदा रखना है ।
इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साहित्यकार, चाहे वे किसी भी विधा, किसी भी भाषा में लिखते हों, निराश हुए बिना, निरंतर समाज में व्याप्त विभिन्न बुराईयों के खिलाफ, अपनी ताक़त के मद में चूर सत्ताधीशों के ख़िलाफ़, समाज को टुकड़ों में बांटने वाले स्वयंभू संम्वेदनहीन ठेकेदारों के ख़िलाफ़ लिखते रहें। यदि ऐसा हो जाए, तो हर उस दिल से जो अमन-चैन से रहना चाहता है, अपने देश और समाज का हित चाहता है, सभी वर्गों, जातियों और धर्म के लोगों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है तथा परस्पर प्रेम और विश्वास भरा एक वातावरण कायम करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ निकलेगी जो दुष्यंत के इस शेर में में गूंजती दिखाई देती है:
अब तो इस तालाब का पानी बदल दो
ये कँवल के फूल मुरझाने लगे हैं ।
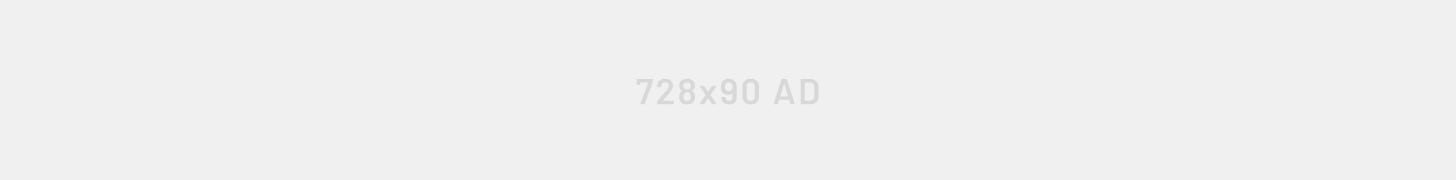
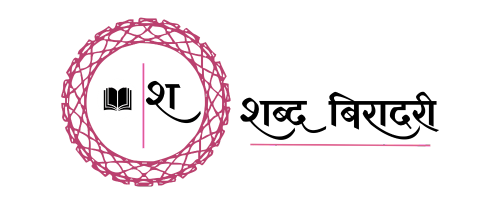

बहुत बढ़िया लेख 🙏🌹
Very well said and articulate with Ghazals/ line of different authors.You are awesome sir.