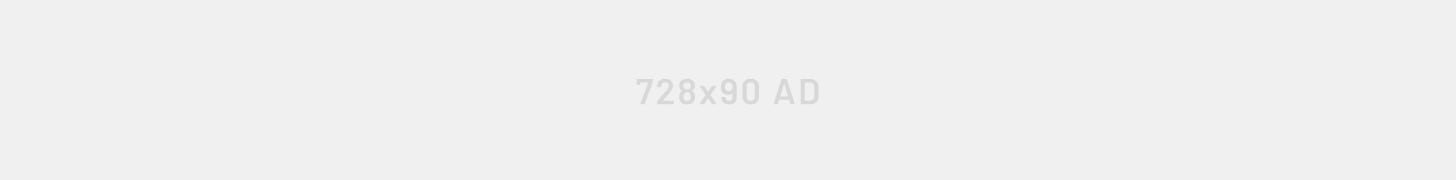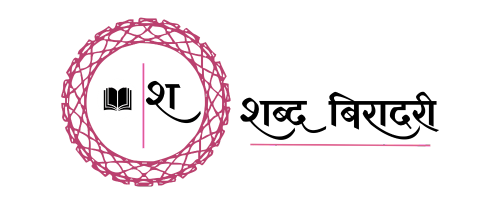जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास से सम्बंधित अनेक तथ्यों का उपयोग किया है. वे जिस दौर में ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना कर रहे थे उस दौर में औपनिवेशिक ढंग से भारतीय इतिहास को समझने-समझाने का क्रम चल रहा था. प्रसाद की विशिष्टता इस मामले में रेखांकित करने योग्य है कि उन्होंने औपनिवेशिक और ओरिएण्टल इतिहास-दृष्टि के बजाए भारतीय ज्ञान-स्रोतों का उपयोग करके अपने नाटकों के कथासूत्र बुने थे.
‘भारतीय चिंतन की बहुजन परंपरा’ पुस्तक के लेखक ओमप्रकाश कश्यप ने आजीवक पर लिखते-पढ़ते हुए पाया कि जयशंकर प्रसाद के नाटक ‘चंद्रगुप्त’ के पात्र-परिचय में आजीवक नाम का एक पात्र है. उन्होंने यह पात्र-परिचय ‘प्रसाद वाङ्मय’ के खंड – दो में देखा था. प्रसाद की जन्मशती के अवसर पर उनके पुत्र रत्नशंकर प्रसाद के समायोजन एवं संपादन में यह ‘वाङ्मय’ पाँच खण्डों में वाराणसी से प्रकाशित हुआ था. ऑनलाइन माध्यमों पर इसकी पीडीफ प्रति मौजूद है.
आज ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक का जो पाठ पुस्तक के रूप में उपलब्ध है उसके पात्र-परिचय की सूची में आजीवक का नाम शामिल नहीं है. यही पाठ ओमप्रकाश सिंह द्वारा सम्पादित ‘जयशंकर प्रसाद ग्रन्थावली’ में भी है. सत्यप्रकाश मिश्र द्वारा सम्पादित ‘प्रसाद के संपूर्ण नाटक एवं एकांकी’ में भी यही पाठ है. कॉपीराइट फ्री होने के कारण ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक का प्रकाशन अनेक प्रकाशकों ने किया है. उन सबमें यही पाठ मिलता है. ओमप्रकाश कश्यप जी ने ‘वाङ्मय’ की पीडीफ प्रति मुझे भेजी और बात भी की. इससे पहले मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी. कश्यप जी इस रहस्य को समझना चाहते थे कि आखिर ‘आजीवक’ को बाद के संस्करणों में क्यों नहीं रखा गया है!
जहाँ तक संभव हो सका मैंने ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक के पुराने से पुराने संस्करण को खोजने और देखने का प्रयास किया. ‘जयशंकर प्रसाद ग्रन्थावली’ के संपादक प्रो. ओमप्रकाश सिंह से भी बात की. उन्होंने भी इस तरह के किसी विवाद के बारे में अनभिज्ञता जतायी.
1957 में हरदेव बाहरी द्वारा निर्मित ‘प्रसाद साहित्य कोश’ का प्रकाशन हुआ था. उसमें प्रसाद साहित्य के पात्रों का भी परिचय दिया गया है. वहाँ भी ‘आजीवक’ नाम का कोई पात्र नहीं मिला. परमेश्वरीलाल गुप्त की पुस्तक ‘प्रसाद के नाटक’ (1956) में ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक के प्रत्येक अंक के प्रत्येक दृश्य का कथा-विवरण दिया हुआ है. उस किताब में ‘चन्द्रगुप्त’ के चार अंक और 44 दृश्य के विवरण मौजूद हैं. इनमें भी ‘आजीवक’ का जिक्र नहीं है.
सब मिलाने पर मैंने पाया कि ‘वाङ्मय’ में तीन दृश्य अधिक हैं. उन्हीं तीन दृश्यों में ‘आजीवक’ की चर्चा है. इनमें चार अन्य पात्र भी हैं जो केवल इन्हीं तीन दृश्यों में हैं – धनदत्त, चन्दन, मणिमाला और माधवी.
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की पुस्तक ‘प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन’ (1949) में इस बात का जिक्र जरूर है कि 1931 में ‘चन्द्रगुप्त’ का पहला संस्करण आया तब इसमें 47 दृश्य थे. दूसरे संस्करण में प्रसाद ने कुछ दृश्यों को मिलाकर कुछ संख्या घटायी थी. मगर शर्मा जी की इस किताब में भी ‘आजीवक’ वाले प्रकरण की कोई चर्चा नहीं मिली.
रत्नशंकर प्रसाद ने ‘वाङ्मय’ की भूमिका में भी इन अतिरिक्त तीन दृश्यों की कोई चर्चा नहीं की है. विभिन्न पुस्तकों में तलाश करते-करते एक सूत्र मिला सिद्धनाथ कुमार की पुस्तक ‘प्रसाद के नाटक’ में. यह पुस्तक 1978 में अनुपम प्रकाशन, पटना से प्रकाशित हुई है. इसका दूसरा संस्करण 1990 का है. इस दूसरे संस्करण की पृष्ठ संख्या 37-38 पर इन अतिरिक्त तीन दृश्यों की चर्चा मिलती है. 1933 में ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक का प्रथम मंचन काशी रत्नाकर-रसिक-मंडल द्वारा 14-15 दिसम्बर को काशी के न्यू सिनेमा हॉल में हुआ था. मंचन की तैयारी और योजना का विवरण बताने के क्रम में राजेन्द्र नारायण शर्मा का एक लंबा कथन उद्धृत किया गया है. शर्मा जी का सन्दर्भ इस प्रकार दिया गया है – ‘लेखक : प्रसाद का अन्तेवासी’, नाट्य प्रशिक्षण शिविर – 1972, वाराणसी की स्मारिका, 1972.
राजेन्द्र नारायण शर्मा के उस लंबे कथन का एक अंश इन अतिरिक्त तीन दृश्यों के बारे में बताता है, “…एक ब्रह्म संकल्प के साथ सबने प्रसादजी के ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक को अभिनीत करने का निश्चय किया. नाटककार से प्रार्थना की गयी कि वे स्वयं नाटक के कलेवर को, उसके आयतन को इस भाँति छोटा कर दें जिससे उसकी रमणीयता और रस सृष्टि रंच मात्र भी कम न हो और उसका अभिनय चार-पाँच घंटों के भीतर सफलता के साथ किया जा सके. प्रसादजी ने संकोच के साथ इसे स्वीकार किया. उनसे यह भी प्रार्थना की गयी कि काल की परंपरा के अनुसार विदूषक के अतिरिक्त उसमें एक प्रहसन की भी रचना आप करने की कृपा करें जो मूल नाटक की कथा के समानांतर एक हास्योत्पादक लघु कहानी के रूप में चले. पारसी रंगमंच की प्रभुता के युग की इस माँग को इच्छा न रहते हुए भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी. स्वयं न लिख कर उन्होंने तटस्थ भाव से बोल कर प्रहसन लिखा दिया. यद्यपि उक्त प्रहसन केवल नाटक के मंचीकरण के हेतु लिखवाया परन्तु उन्होंने इस बात का कितना ध्यान रखा कि प्रहसन के पात्र और उनकी कथा दोनों उसी युग के हों जिस युग का यह नाटक है. प्रहसन का पहला दृश्य इन पंक्तियों के लेखक ने तथा दूसरा और तीसरा दृश्य श्री लक्ष्मीकांत झा ने लिखा है.” (प्रसाद के नाटक – सिद्धनाथ कुमार, अनुपम प्रकाशन, पटना, 1990, पृष्ठ संख्या – 38).
इन्हीं तीन दृश्यों को ‘प्रसाद वाङ्मय’ के खंड – दो में शामिल रखा गया है. चूँकि इन दृश्यों को केवल उस समय के मंचन के लिए बोलकर लिखवाया गया था, इसलिए इसे मूल पाठ में शामिल नहीं किया गया. यह उचित भी है. प्रसाद ने मंचन से जुड़े शुभचिंतकों के प्रेमपूर्ण दबाव के कारण इन तीन दृश्यों को बोलकर लिखवाना स्वीकार किया था इसलिए इन्हें नाटक के पाठ का हिस्सा नहीं माना गया. इन तीनों दृश्यों की भाषा भी अन्य दृश्यों की भाषा से थोड़ी हल्की है. ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इनमें प्रहसन की झलक देनी थी.
प्रथम से लेकर चतुर्थ अंक तक दृश्यों की संख्या क्रमशः 11, 10, 09 और 14 है. कुल मिलाकर 44 दृश्य. ये अतिरिक्त दृश्य प्रथम अंक में पंचम, द्वितीय अंक में दशम और तृतीय अंक में षष्ठ हैं. इनके कारण दृश्यों की संख्या क्रमशः 12, 11, 10 और 14 हो गयी है. कुल मिलाकर 47 दृश्य. इन तीनों दृश्यों को लेख के अंत में शामिल किया जा रहा है.
प्रहसन और मंचन तक का मामला भले ही हल्का-फुल्का मान लिया जा सकता है, मगर इन दृश्यों में ‘आजीवक’ का आना मामूली बात नहीं है. प्रसाद के विभिन्न नाटकों को मिलाकर देखा जाए तो उनमें भारतीय धर्म साधना की अनेक परम्पराओं का उल्लेख मिलता है. ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में बौद्ध और ब्राह्मण संघर्ष को नंद और चाणक्य के बीच देखा जा सकता है. चाणक्य के कई संवाद बौद्धों की निंदा करते हैं और नंद के संवादों में ब्राह्मणों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियाँ हैं. राक्षस भी बौद्ध मतावलंबी है. सुवासिनी के बौद्ध आकर्षण पर व्यंग्य करते हुए चाणक्य कहता है कि वेश्याओं को भी एक धर्म की ज़रूरत थी. दाण्ड्यायन के रूप में प्रसाद ने ऋषियों-मुनियों या संन्यासियों की परम्परा की झलक दी है. राक्षस कॉर्नेलिया को भारतीय संगीत की शिक्षा देता है. जाहिर सी बात है राक्षस की समझ को बनाने में बौद्ध पृष्ठभूमि की भूमिका रही होगी! ‘जन्मेजय का नागयज्ञ’ में नाग, मनुष्य और देवता के संघर्ष को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें सम्प्रदाय, जाति और नस्ल के संघर्ष को कई तरह से देखा जा सकता है.
प्रसाद ने दूसरी रचनाओं में भी इस बात की झलक बार-बार दी है कि भारत की भूमि जन्म-आधारित पहचानों और धार्मिक मान्यताओं से उत्पन्न वैविध्य के बीच संघर्ष की भूमि रही है. यह भी पता चलता है कि इस वैविध्य के साथ भारत का इतिहास विकसित होता रहा है. इस इतिहास को सपाट ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है जिस तरह से औपनिवेशिक दृष्टि पढ़ती रही है. यही काम भारत के वे लोग भी करते रहे हैं जो संस्कृति और धर्म का सहारा लेकर इतिहास की काल्पनिक कहानियाँ गढ़ते रहे हैं! प्रसाद का साहित्य भारत की खोज भारतीय स्रोतों से करने पर ज़ोर देता है. उनके नाटकों की भूमिका और निबंध में पढ़ा जा सकता है कि वे अपने समय की ऐतिहासिक खोजों से परिचित थे. उन्होंने अपने समय के इतिहासकारों को उद्धृत किया है. मगर औपनिवेशिक दृष्टि से विकसित हो रहे इतिहास को वे चुपचाप मान नहीं लेते हैं. संस्कृत और पालि-प्राकृत-अपभ्रंश में उपलब्ध जानकारियों का वे खुले मन से उपयोग करते हैं. उदाहरण के रूप में ‘ध्रुवस्वामिनी’ की भूमिका देखी जा सकती है. सामाजिक परम्परा और लोक मान्यता यही थी कि हिन्दू स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है. स्त्रियों के विरुद्ध ‘स्मृतियों’ को उद्धृत किया जाता रहा है. यह सही बात भी है कि ‘स्मृतियों’ में स्त्री-विरोधी बातें मिलती हैं. मगर इन ‘स्मृतियों’ में भी कई जगह मतभेद मिलते हैं. प्रसाद ने इस नाटक की भूमिका में ‘नारद’ और ‘पराशर’ स्मृति से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हैं जिनमें यह बात साफ़-साफ़ कही गयी है कि एक स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार इन-इन परिस्थितियों में है, ‘नष्ट मृते प्रव्रजिते …’. यदि पति का व्यवहार पतित है या वह नपुंसक है तो वह उसके जीवित रहते हुए भी पुनर्विवाह कर सकती है.
प्रसाद भारत की परम्परागत विविधता को सामने रख रहे थे. ‘दूसरी परम्परा की खोज’ में हजारीप्रसाद द्विवेदी और टैगोर के माध्यम से जिन उत्तर पक्ष के पंडितों की मान्यताओं की बात बतायी गयी है वैसी बात प्रसाद अपनी रचनाओं में बार-बार कर रहे थे.
‘आजीवकों’ के बारे में जितनी बातें ओमप्रकाश कश्यप ने पढ़ी-खोजी हैं उन सबको मिलाकर देखा जाय तो कहा जा सकता है कि 1930 के आस-पास प्रसाद की ऐसी इतिहास-दृष्टि यह बताती है कि हिन्दी के रचनाकार कितने सजग थे! कश्यप जी ने बातचीत में रेखांकित किया कि आजीवकों के बारे में जानकारी प्रदान करने का श्रेय प्रायः अँग्रेज विद्वानों को दिया जाता है. मगर जिस समय प्रसाद आजीवकों के दार्शनिक मतों को प्रकट कर रहे थे वह आश्चर्यजनक है. इससे यह भी पता चलता है कि औपनिवेशिक दौर में जो ज्ञानकाण्ड घटित हुआ उसमें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जानकारियों की घोर उपेक्षा हुई. यह बात भी सही है कि भारतीय भाषाओं में लिखित सामग्री और खासकर साहित्य के जानकार कम ही इतिहासकार रहे हैं.
प्रसाद ईश्वरवादियों और निरीश्वरवादियों की परम्पराओं से खूब परिचित थे. इन परम्पराओं की अभिव्यक्ति भारतीय समाज, संस्कृति में न जाने कितने रूपों में होती रही है. इन परम्पराओं को पढ़ने का मतलब केवल धर्मदर्शन को पढ़ना नहीं है बल्कि भारत के समाज और इतिहास को पढ़ना है.
नोट: उपरोक्त आलेख में वर्णित दृश्यों को पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें
https://drive.google.com/file/d/1rBtNK0UbzLTh7Xbuaa_XKxHSoxpltMw8/view?usp=sharing
कमलेश वर्मा
लेखक का परिचय
कमलेश वर्मा– अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी
पुस्तकें : 1. नागार्जुन की काव्य-भाषा 2. जाति के प्रश्न पर कबीर 3. निराला काव्य-कोश 4. दूसरी परम्परा का शुक्ल-पक्ष 5. प्रसाद काव्य-कोश 6. छायावादी काव्य-कोश
प्रधान सम्पादक : ‘सत्राची’ त्रैमासिक पत्रिका
सम्पादन :1. निराला शब्द कोश (काव्य), 2009 2. सत्राची : वीर भारत तलवार विशेषांक, 2017 3. सत्राची : छायावाद पर केंद्रित विशेषांक, 2018 4. बेटियाँ – जितेन्द्र श्रीवास्तव की बेटियों पर लिखी कविताएँ, 2019 5. दुर्लभ परम्परा के आलोचक : वीर भारत तलवार, 2020 6. असहमतियों के वैभव के कवि श्रीप्रकाश शुक्ल, 2024
पुरस्कार : 1. अयोध्याप्रसाद खत्री स्मृति सम्मान, 2023; 2. राजवल्लभ साहित्य सम्मान, 2020; 3. सीताराम शास्त्री स्मृति पुरस्कार, 2017