
सत्ता और साहित्य के मध्य सम्बन्ध पर बात करने से पूर्व थोड़ी सी बात सत्ता पर कर लेना ठीक रहेगा। सत्ता के विभिन्न प्रकारों तथा सत्ता की प्रकृति पर एक नज़र डालने के पश्चात सत्ता और साहित्य के परस्पर संबंधों को अधिक अच्छे से समझा जा सकता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस में यदि हम अपने आस-पास नज़र डालें, तो हम देख सकते हैं कि किस-किस रूप में सत्ता हमारे आस-पास विद्यमान है। राज्य और राजनीति की सत्ता, पूँजी की सत्ता, पुरुष की सत्ता, बाज़ार की सत्ता, झूठ की सत्ता, मीडिया की सत्ता, धर्म की सत्ता, भ्रष्टाचार की सत्ता, प्रतिष्ठानों की सत्ता इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कालांतर में इन सत्ताओं के प्रभावों और पारस्परिक संबंधों में छुटपुट परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे, परन्तु सत्ता की मूलभूत प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन नहीं के बराबर ही होते हैं। सत्ता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अक्सर कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहती है। किसी के भी द्वारा उस पर उंगली उठाए जाना उसे बिल्कुल गवारा नहीं होता, सवाल पूछे जाने पर वह तिलमिला उठती है। जब बात राजनैतिक सत्ता की हो तो ये कथन और भी अधिक सत्य हो जाता है। और आज के युग में जब राजनीति, पूँजी, धर्म, बाज़ार, मीडिया और झूठ की सत्ताओं ने आपस में हाथ मिला लिए हैं तो वे आपस में इस क़दर घुलमिल गई हैं कि उन्हें एक-दूसरे से अलग कर के देख पाना भी कठिन हो गया है। यह मिली-जुली सत्ता इतनी अधिक मज़बूत हो गयी है कि । ये सब सत्ताएँ एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आप को और अधिक मज़बूत कर रही हैं, और अपनी-अपनी रोटियां सेक रही हैं। यदि यह कहा जाए कि वे एक दूसरे की पूरक हो गई हैं तो यह अतिश्योक्ति न होगी!
दूसरी ओर प्रश्न उठाना साहित्य का मौलिक स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। भाषा, समाज, संस्कृति, परंपरा उसके मूलभूत कार्यक्षेत्र हैं। समाज में जो कुछ घट रहा होता है, वह किसी न किसी रूप में साहित्य में जगह पाता ही है, बल्कि समाज के विभिन्न घटकों के पारस्परिक संबंध, मानव मन की अपेक्षाएं, इच्छाएं, विडंबनाएं, कुंठाएं इत्यादि सभी इसकी विषय-वस्तु में सम्मिलित हैं।
समाज में चल रही कुरीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी साहित्य के कार्यक्षेत्र का एक हिस्सा है। पूंजीवाद के चलते समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों, असमानताओं को उजागर करना लेखकों, साहित्यकारों का परम कर्तव्य है। ग़रीब, दबी-कुचली जनता के लिए आवाज़ उठाना, परिष्कृत वर्गों की तक़लीफ़ों को सामने लाना, ये सब हमेशा से साहित्य के सरोकारों का हिस्सा रहे हैं। यद्यपि कुछ लोगों की नज़र में साहित्य का कर्म-क्षेत्र राजनीति और राजनैतिक सत्ता नहीं है, तो भी अपने अन्य सामाजिक सरोकारों के साथ न्याय करते-करते साहित्य का सामना किसी न किसी रूप में राजनैतिक सत्ता से हो ही जाता है और एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है।
जब कोई रचनाकार दाने-दाने को मोहताज लोगों की भूख़ का मंज़र अपनी रचनाओं में उतारता है या किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार, डरे-सहमे लोगों की ख़ामोशियों को आवाज़ प्रदान करता है, तो वह सीधे-सीधे सरकार की नाकामियों या उसकी ग़लत नीतियों पर ऊँगली उठा रहा होता है, उसके झूठे वादों और खोखले नारों की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है। अब अपनी ताक़त के मद में चूर सत्ताधीशों को यह कैसे मंज़ूर होगा कि कोई उन पर ऊँगली उठाए। वो सिस्टम के ख़िलाफ़ कही हुई हर बात को अपने ख़िलाफ़ कही हुई बात ही समझते हैं। दुष्यंत का यह शेर इस स्थिति का बिलकुल ठीक-ठीक चित्रण करता है:
मत कहो आकाश में कोहरा घना है।
ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।
कभी-कभी लिखने वाले की क़लम से निकले शब्द अनजाने में ही शिखर पर बैठे लोगों को कुछ इस क़दर आहत कर जाते हैं कि वे तिलमिला उठते हैं। उदाहरण के लिए मेरा यह शेऱ देखिए:
रह रह के लहू रिसता रहा आसमान से।
ये तीर कैसा चल गया मेरी क़मान से।
सत्ता, भाषा और साहित्य के बीच का सम्बन्ध गहरा भी है और जटिल भी। इनमें से कौन किसको प्रभावित करता है और किस हद तक, यह ठीक-ठीक तय कर पाना अत्यंन्त कठिन कार्य है क्योंकि इनके मध्य क्लियर-कट सीमाएं तय करना बहुत मुश्किल है। यदि यहां पर गणित की भाषा का प्रयोग करने की इजाज़त हो तो हम सत्ता और साहित्य के मध्य के सम्बन्ध को फ़ज़ी सम्बन्ध कह कर परिभाषित सकते हैं।
फ़ज़ीनेस को समझने के लिए न तो हमें गणित का ज्ञान होने की आवश्यकता है, न ही गणितज्ञों द्वारा दी गयी फ़ज़ीनेस की संकल्पना की तकनीकी परिभाषा को जानने की। फ़ज़ी होने का सामान्य अर्थ अस्पष्ट होना या धुंधला होना होता है। गणितज्ञों ने जब यह पाया कि जिन तत्वों के साथ वो काम करते हैं, जैसे कि समुच्चय, संबंध, फलन इत्यादि, उन के बीच के संबंधों को समझने के लिए हर समय वे संकल्पनाएं समर्थ नहीं होतीं जिन्हें वे पारम्परिक रूप से इस्तेमाल करते रहें हैं; तो उन्हें एक ऐसी अवधारणा की ज़रुरत महसूस हुई जिसके प्रयोग से ऐसे संबंधों का अध्ययन किया जा सके जो पूर्णतया स्पष्ट न हों, अर्थात् फ़ज़ी हों। इस समस्या का निदान तब हुआ जब 1964 में एल.ए.ज़ादे ने फज़ी-गणित की संकल्पना दुनिया के समक्ष रखी। ज़ादे एक गणितज्ञ, कंप्यूटर इंजीनियर, कम्प्यूटर साइंटिस्ट, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर तथा कैलिफोर्निआ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर एमेरिटस थे। ज़ादे का जन्म बाकू, अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य में हुआ था। उनके पिता एक ईरानी थे और माँ एक रूसी यहूदी और एक बाल-रोग विशेषज्ञ ।
ज़ादे की इस संकल्पना ने केवल गणितज्ञों की ही मदद नहीं की, बल्कि उनकी इस संकल्पना के आधार पर जितना फ़ज़ी-गणित विकसित हुआ, उस से ज्ञान के अनेक अन्य क्षेत्रों को भी अत्यधिक लाभ हुआ। शायद कुछ लोगों को ‘सत्ता, भाषा और ग़ज़ल’ विषय पर लिखे जा रहे इस लेख में गणित की बात करना कुछ अप्रासंगिक, बल्कि अटपटा लगे। पर मैंने इसका ज़िक्र किसी विशेष उद्देश्य को लेकर किया है। सबसे पहला उद्देश्य तो साहित्य और सत्ता के बीच के सम्बन्ध को परिभाषित करना था, परिभाषित नहीं तो कम से कम सम्बोधित करने के लिए एक विशेषण या एक शब्दावली की आवश्यकता तो थी ही। सो, मेरी नज़र में इस सम्बन्ध को शब्द ‘फ़ज़ी’ जितना ठीक से परिलक्षित करता है, उस से बेहतर रूप से शायद कोई और शब्द न कर सके। दूसरे जैसा कि मैंने ऊपर ज़िक्र किया कि फ़ज़ी गणित का उपयोग ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में किया गया है। इसमें विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस तथा अर्थशास्र तो शामिल हैं ही, पर साथ ही सोशल साइंसेज़ भी शामिल हैं। यहां तक कि समाजशास्त्र में भी फ़ज़ी गणित का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि समाज के विभिन्न अंगों के बीच सम्बन्ध भी मूलत: फ़ज़ी ही होते हैं। अधिकतर मानवीय सम्बन्ध भी सुस्पष्ट न होकर फ़ज़ी ही होते हैं!
फ़ज़ी-गणित, ज्ञान के इन सब क्षेत्रों में जहां एक ओर सिद्धांतों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि करने में सहायक सिद्ध होता है, वहीं नए सिद्धांतों की खोज करने के लिए भी साधन उपलब्ध करवाता है। आलोचक तथा कहानीकार बिक्रम सिंह ने तो साहित्य तथा संस्कृति को समर्पित प्रसिद्ध पत्रिका ‘अनभै सांचा’ में अपने लेख ‘समकालीन ग़ज़ल का फ़ज़ी सौंदर्य-लोक’ में फ़ज़ीनेस का सफ़ल प्रयोग ग़ज़ल में एक पैरामीटर के रूप में करके यह भी साबित कर दिया कि फजीनेस की संकल्पना साहित्य के विश्लेषण तथा आकलन में भी सहायक हो सकती है। यही नहीं, उन्होंने साहित्य में इस फ़ज़ी-चिंतन के अनोखे प्रयोग को अपनी किताब ‘फ़ज़ी हिंदी आलोचना और नसीम अजमल की ग़ज़ल’ के माध्यम से आगे बढ़ाया। पर इस से पहले कि यह किताब दुनिया के सामने आ पाती, काल के निर्मम हाथों ने कोरोना काल में इस विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा को हमसे छीन लिया। उनके परलोक के महाशून्य में विलीन हो जाने के पश्चात अनभै सांचा के सम्पादक द्वारका प्रसाद ‘चारुमित्र’ तथा हिंदी ग़ज़ल के जाने-माने प्रणेता ज्ञान प्रकाश ‘विवेक’ ने इस कृति को पूरा करने का बीड़ा उठाया तथा वर्ष 2023 में यह महत्वपूर्ण किताब दुनिया के सामने आई। बिक्रम सिंह जी जैसे गंभीर चिन्तक तथा साहित्यकार को इस से अच्छी श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। मेरे विचार में साहित्य से सबंधित प्रत्येक व्यक्ति को उनकी इस महत्वपूर्ण कृति को पढना चाहिए।
आपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब हम थोड़ी बात ग़ज़ल पर कर लेते हैं। ग़ज़ल साहित्य का एक अभिन्न बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ग़ज़ल एक नाज़ुक सिम्त-ए-सुखन है, जिसमें शायर अपनी ग़ज़ल को अपने जज़्बात से सजाता है, ग़ज़ल के रदीफ़ और काफ़िये को निभाते हुए ,एक-एक शेर में एक-एक शब्द को इस तरह पिरोता है कि पूरे शब्द-विन्यास से शेर में एक ख़ास तरह की कैफ़ियत पैदा हो जाती है । मीर-ग़ालिब से लेकर, नासिर काज़मी, फ़राज़, फैज़ के दौर से गुज़रते हुए, दुष्यंत से लेकर आज तक के शायरों तक ग़ज़ल ने जो इतना बड़ा सफ़र तय किया है और जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे ग़ज़ल की मूल बनावट में शामिल वो ख़ास शै है जो उसे किसी भी तरह के एहसासात को बेहद खूबसूरती के साथ पेश करने की ताक़त देती है । लेकिन ग़ज़ल के बारे में कई ग़लतफ़हमियाँ आज भी बरक़रार हैं। अब भी कुछ लोग ग़ज़ल को सिर्फ़ शराब और शबाब से ही जोड़ कर देखते हैं। यह पूर्णतया सही नहीं है ।
यह ठीक है कि ग़ज़ल मूलत: प्रेयसी के आस-पास घूमती थी: पीछे मुड़ कर देखें तो महबूब की रानाइयों के ज़िक्र, उसकी शोखियों, उसके शबाब के चर्चे, उसकी ज़ुल्फ़ों के पेचोख़म, उसकी वफाओं और ज़फ़ाओं के ज़िक्र ही ग़ज़ल की मूल विषय-वस्तु हुआ करते थे। या यूँ कहें कि ग़म-ए-जानां ही उसका केंद्रीय विषय था। पर आधुनिक ग़ज़ल अपने अंदर अनेकों रंग समेटे है। उसमें ग़म-ए-दौरां भी उतना ही शामिल है जितना कि ग़म-ए-जानां। ग़ज़ल जहां एक ओर दिल में उठने वाली उमंगों-तरंगों का, मोहब्बत के हिज़्र-ओ-विसाल से जुड़े एहसासात का खूबसूरत काव्यात्मक चित्रण है, वहीं मानव-मन की आशाओं-निराशाओं का, बनते-बिगड़ते मंज़रों का, टूटते-बिखरते रिश्तों का भी जख़ीरा है। साथ ही ग़ज़लकारों ने हर प्रकार की सत्ता की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, हुक़ुमरानों के ज़ुल्मात के ख़िलाफ़ भी खुलकर आवाज़ उठाई है। ज़ोरों-ज़ुल्म, हत्याओं , दंगों-फसादों, राजनैतिक दांव-पेचों, सियासती षड्यंत्रों में से ऐसा कुछ न होगा जिस पर ग़ज़लकारों ने नहीं लिखा होगा। उदाहरण के लिए नसीम अजमल साहिब, जिन्होंने मुझे ग़ज़ल से रूबरू करवाया और जिन्हें मैं अपना ग़ज़ल-गुरु मानता हूँ, के दो शेर देखिए:
मैं इक पल में बस आसमानों में था
गिरा दी जो उसने क़बा* सामने। *वस्त्र,परिधान
नज़र ख़ौफ़ दर ख़ौफ़ सहमी हुई
लरजता हुआ एक खंडर सामने।
जहां पहला शेर सेंसुअलिटी की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरे शेर में वे मानो जैसे भयावह दंगों के बाद का कोई ख़ौफ़नाक, डर से कांपता एक मंज़र खींचते दिखाई देते हैं।
तो शायर जितनी खूबसूरती से अपने महबूब की खूबसूरती को ब्यान करता है, जितनी नज़ाकत के साथ मोहब्बत का इज़हार कर सकता है, उतनी ही शिद्दत के साथ समाज के गंभीर मुद्दों पर बात कह सकता है। ग़ज़ल एक नाज़ुक सिम्त-ए-सुखन तो है ही पर इसकी नज़ाक़त इसकी कमज़ोरी नहीं, इसकी ताक़त है। अब अगर कुछ लोग यह समझते हैं कि ग़ज़ल सिर्फ कुछ ख़ास तरह के एहसासात को ही ज़ाहिर कर पाती है तो यकीन मानिए कि वे किसी ग़लतफ़हमी के शिकार हैं । राजनेताओं द्वारा दिखाए गए ख़्वाबों के जाल में फँसी भोली-भाली जनता का दर्द, हुक़ुमरानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों का हश्र, क़लमों को खरीद लेने की कोशिशों तथा नफ़रत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने के प्रयासों इत्यादि सब पर शायरों ने भरपूर वार किए हैं। साहित्य की अन्य विधाओं की तरह ग़ज़ल ने भी सत्ता का भरपूर विरोध किया है। इस लेख में हम ग़ज़ल के वो रंग देखेंगे जो शायद उन्होंने पहले देखे न हों । आइये कुछ उदाहरण देख लेते हैं ।
जैसा कि इस लेख के शीर्षक से ही ज़ाहिर है कि हम यहाँ उन ग़ज़लों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सत्ता के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई है । सत्ता की ग़लत नीतियों, उसकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, लेकिन किसी साहित्यकार, किसी शायर की आवाज़ को इन धमकियों से, इन हतोत्साहित करने वाले तौर-तरीक़ों से दबाया नहीं जा सकता। बल्कि ऐसा करने पर उसे और अधिक कहने का मौका मिलता है। शकील शाह का यह अंदाज़ देखिये:
जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ।
मैं इस शहर का सबसे बड़ा फ़सादी हूँ।
यह न सिर्फ उन हुकुमरानों पर कड़ा तंज़ है जो अपने खिलाफ़ उठने वाली हर अवाज़ को ख़ामोश कर देना चाहते हैं , बल्कि यहाँ शायर खुद अपने भी बाग़ी होने का ऐलान करता हुआ हुकुमरां को एक तरह से चुनौती भी दे रहा है ।
शायर, या व्यापक तौर पर कोई भी साहित्यकार चाहे वह किसी भी विधा में रचनारत हो, किसी भी भाषा में लिखता हो, किसी भी देश में रहता हो, सिर्फ़ अपने दर्द को ही बयां नहीं करता, सारे समाज के दर्द उसी के दर्द होते हैं । जो कुछ भी उसके आस-पास घटित होता है, वह उस से प्रभावित होता है, और अगर कहीं ग़लत देखता है तो आहत होता है। यह वास्तव में हर संवेदनशील व्यक्ति के साथ होता है। और शायर अगर संवेदंशील नहीं होगा तो उसे शायर कहलाने का हक़ ही नहीं है । मुमताज़ नाज़ां के इस शेर में शायर की बेचैनी को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है:
मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूँ
हर ग़ज़ल अब सल्तनत के नाम इक ब्यान है।
इस शेर में सीधे-सीधे वो अपनी हर ग़ज़ल को सल्तनत के नाम एक ब्यान घोषित कर रही हैं । और इस शेर में तो वो साफ़-साफ़ कह रहीं हैं कि सब-कुछ देखते-समझते हुए भी चुप रहने से जीना मुहाल हो जाता है, इसलिए अब और ज़्यादा देर तक ख़ामोश नहीं रहा जा सकता:
ये जुबां हम से सी नहीं जाती
ज़िन्दगी है कि जी नहीं जाती।
शुजा ख़ावर का यह शेर
इधर तो दार पर रक्खा हुआ है।
उधर पैरों में सर रक्खा हुआ है।
भी कहीं न कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है कि जहां एक ओर इस दुनिया में अधिकतर लोग आगे बढ़ने के लिए ताक़तवर हुक्मरानों की क़दमबोसी करने से भी नहीं हिचकिचाते, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो सच का साथ देने के लिए, अंजाम की परवाह न करते हुए, हुकुमराँ के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
इसी प्रकार भारत भूषण आर्य के अन्दर का शायर भी इन स्थितियों के चलते, हर वक़्त सच के साथ खड़े रहने के लिए कटिबद्ध है, चाहे परिणाम कुछ भी हो:
साथ सच के हम रहे हरदम खड़े
हश्र क्या होगा कभी सोचा नहीं ।
सिर्फ़ इतना ही नहीं, वे भयंकर आँधियों में भी सत्य की ज्योति को जलाए रखने की अपनी ज़िद पर कायम हैं:
आंधियो! कब तक बुझाओगी मुझे
क्या दिये की ज़िद का अंदाज़ा नहीं ।
‘अली’ अहमद जलीली की नज़र में ख़ामोशी को हमेशा कमज़ोरी समझ लेना बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी हैं। ख़ामोशी एक आने वाली क्रांति का सबब भी बन सकती है। उनका यह शेर देखिए:
यह अलग बात कि लब सी लिए वरना
ख़ामुशी यह मेरी ललकार भी हो सकती है।
अपने ही एक और शेर में वे यह प्रश्न भी हैरत के साथ उठाते हैं कि पूरे शहर में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। कहीं यह शहर वीरान तो नहीं हो गया?
कोई आहट, कोई सदा ही नहीं
क्या कोई शहर में बचा ही नहीं।
नसीम अजमल के ये शेर भी कुछ ऐसी ही स्थिति की बात करते हैं:
वो आहट आज कैसी बेसदा है
ये मुझमें कौन बहरा हो गया है।
मैं जिन सड़कों पे अक्सर घूमता था
वहाँ पर आज पहरा हो गया है।
ओम प्रकाश नदीम भी अपने इस शेर में अपने अंदर के क्रांतिकारी के कहीं गुम हो जाने पर अपनी हैरत का इज़हार करते हैं:
मेरे अंदर एक मुखालिफ़* था जो मुझसे लड़ता था
अब या तो वो चुप रहता है या हाँ में हाँ करता है
- खिलाफ़त करने वाला
यह अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग तो आदतन ही सत्ता से चिपके रहते हैं और सत्ता की जी-हजूरी को ही अपना परम कर्तव्य मानते हैं। परन्तु कुछ लोग, ग़लत को ग़लत कहना जिनकी आदत में शुमार होता है, ऐसे वक़्त में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं ख़ासकर तब जब सत्ताधीश सिर्फ अपनी प्रशंसा वाली, चापलूसी भरी बातें ही सुनना चाहता हो और उसके सामने सच्चाई और उचित सलाह कोई मायने न रखते हों । ऐसा सत्ताधीश जितना ताक़तवर होगा उतना ही ज़्यादा उन आवाज़ों को दबाने के लिए तत्पर होगा जो उसपर ऊँगली उठाती हों । मजबूरन सत्य के पक्षधर या तो चुप्पी साध लेते हैं या वो भी ओर कोई चारा न देखते हुए हां में हां मिलाने में ही अपनी भलाई देखने लगते हैं, मन मारकर ही सही!
और जो फिर भी सच का साथ देने पर अडिग रहते हैं उनको सत्ता की ज़्यादतियों को सहना पड़ता है, एक कठिन जीवन बिताना पड़ता है । वे चाहे कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी रहने लगें, उनका हाल में कोई बदल नहीं होता क्योंकि लगभग सभी जगह सत्ता एक सी ही होती है। हाँ, उनके काम करने के तौर-तरीके थोड़े-बहुत अलग हो सकते हैं । पर सच के साथ खड़े होने वाले भी ग़लत को ग़लत कहने की अपनी यह आदत बदल नहीं सकते । बशीर बद्र कहते हैं कि सच्ची बात कहने वाले को कोई पसंद नहीं करता। सत्ता तो कदापि नहीं। ख़ासतौर पर तब, जब कोई सत्ता के ख़िलाफ़ बोल रहा हो। चाहे वो कहीं की भी सत्ता हो:
दिल्ली हो कि लाहौर कोई फ़र्क़ नहीं है
सच बोल के हर शहर में ऐसे ही रहोगे।
बशीर बद्र की एक और ग़ज़ल है:
कोई काँटा चुभा नहीं होता
दिल अगर फूल सा नहीं होता।
इस ग़ज़ल का यह शेर भी आज के दौर में बोलने पर लगी पाबंदी का हाल का ठीक-ठीक बयाँ करता है:
जी बहुत चाहता है सच बोलें
क्या करें हौसला नहीं होता।
शायद सब मजबूर हैं इस चुप्पी के लिए। उन्होंने इस बेबसी का इज़हार अपने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से किया है:
हमारी बेबसी की इन्तहा है
कि ज़ालिम की हिमायत कर रहे हैं।
अपनी एक और गज़ल में बशीर बद्र ने धूप को ही सरमायादार बता दिया है । मेरी नज़र में यह भी सत्ता पर ही एक तंज़ है:
ख़ून पानी बना के पीती है।
धूप सरमायादार लगती है।
सब्र कर सब्र करने वालों की
बेबसी शानदार लगती है।
अमीर क़ज़लबाश का ये शेर भी कुछ इसी तरह की कैफियत लिए हैं:
तुम्हारे शहर में कुछ लोग इस तरह भी जिए।
किसी ने ज़ख्म छुपाए, किसी ने होंठ सिए।
लोगों को ऐसी चुप सी लग गयी है कि क्या कहें। लोग सब देखते-समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। कौन ताक़तवर राजा से दुश्मनी मोल ले वो भी ऐसा राजा जो असहमति को, डिस्सेंट को सीधा-सीधा बग़ावत करार देता हो। एक शायर ही है जो इतनी हिम्मत कर लेते हैं। शहरयार का यह शेर देखिए:
कहीं ज़रा-सा अँधेरा भी कल की रात न था।
गवाह कोई मगर रौशनी के साथ न था।
अपनी सत्ता को और अधिक मज़बूत करने की फ़िराक में सत्ताधीश मुसलसल, लगातार, संवेदनात्मक मुद्दों की तलाश में रहते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए हवा देते हैं। और उनका ध्यान आम नागरिक की मूलभूत समस्याओं की तरफ जाता ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादें ज़रूरतें हैं आम आदमी की और उन्हें पूरा करने के लिए रोज़गार के साधन मुहैया करवाना सरकारों का सबसे ज़रुरी काम है। राजेश रेड्डी का यह शेर ऐसे हालात पर सीधा-सीधा और तीखा व्यंग्य कसता है:
रोज़ खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूँ मैं।
मुस्कुरा देने हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं।
सत्ता का मक़सद वही रहता है, हाँ, उसे पूरा करने के लिए वह नए-नए तरीके खोजती और अपनाती रहती है। पर शायर की पैनी नज़र से यह सब कहाँ छुप सकता है:
आपका मक़सद पुराना है मगर ख़ंजर नया।
मेरी मजबूरी है ये, लाऊँ कहाँ से सर नया।
‘पारस’ बहराइची ने सत्ताधीशों द्वारा किये जाने वालों ज़ुल्मात पर जैसा वार किया है, वह बे-मिसाल है:
लाख बेजान सही उसका भी मन दुखता है।
ख़ून नाहक हो तो ख़ंजर का बदन दुखता है।
स्थितियां प्रजातंत्र के दौर में भी बहुत अधिक नहीं बदलतीं। हाँ, शासकों के तौर-तरीके थोड़े-बहुत बदल जाते हैं। थोड़ी लुभावनी बातें, जिससे भोली-भाली जनता का मन बहला रहे। वह इसी मुग़ालते में रहे कि इस शासक से अच्छा शासक तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शायर की नज़र, शब्दों के मायाजाल से ज़बरन बिखेरी गयी फूलों की खुशबू के पीछे छुपी श्रोणित की महक को अच्छे से पहचान लेती है। होश नोमानी का यह शेर देखिये:
नुमाइश तो गुलाबों की है लेकिन
फ़ज़ा से ख़ून की बू आ रही है।
सियासतदां अपने निजी फायदे के लिए लोगों को बाँट देते हैं, कभी जात-पात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर । धर्माधीशों का भी उन्हें पूरा-पूरा सहयोग मिलता है और वे अपने आकाओं के इशारों पर कट्टरता और नफ़रत भरा माहौल बनाते हैं। शासक बदले में उन्हें अभयदान देते हैं और दोनों सत्ताओं का कारोबार चलता रहता है। परन्तु इस सब में समाज में नफरत की एक ऐसी आग लग जाती है कि पूरा समाज उस में धूं-धूं कर जलने लगता है । आपसी प्यार-मोहब्बत, रिश्ते, सद्भाव सब इस आग की भेंट चढ़ जाते है, जिसका फायदा सियासी लोग उठाते हैं । नूर तकी नूर के अनुसार यह फिरकापरस्ती सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानों में ही देखी जा सकती है और कहीं नहीं। उनका यह शेर देखिए :
परिंदों में तो ये फ़िरकापरस्ती भी नहीं देखी
कभी मंदिर पे आ बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे।
शायर यह महसूस करता है कि पूरी सृष्टि में केवल इंसान ही है जिसने अपने आपको हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई आदि धर्मों के आधार पर अलग-अलग खानों में बाँट लिया है, बाक़ी सब प्राणी इन जंजालों से मुक्त हैं । और सियासतदानों ने इंसानों के बीच की इन खाइयों को पाटने की कोशिश करने के बजाए इन्हें और गहरा और चौड़ा किया है ।
मज़े कि बात यह है कि सियासतदां अक्सर अपनी मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातों से सभी वर्गों को बेवकूफ़ बनाने में क़ामयाब हो जाते हैं । सभी वर्ग उन्हें अपना-अपना मसीहा समझने लगते हैं । पर वास्तव में वे किसी के नहीं होते । वे जात-पात, ऊंच-नीच, अमीरी-ग़रीबी, धर्म-वर्ण भेद आदि के सवालात सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए उठाते हैं और उन्हें हवा देते हैं। भावनाओं में बहकर लोग उन्हें अपना मसीहा समझ लेते हैं पर अंतत: किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। रौशनचंद ‘तालिब’ बड़े क़रीने से इस शेर में ऐसे सियासतदानों का पर्दाफ़ाश करते हैं:
देखिए अहले-सियासत की सियासत देखिए
शेख़ से मस्जिद गई, पंडित से बुतखाना गया।
अगर यहाँ पर मैं भी अपनी एक ग़ज़ल के दो शेर उद्घृत करूँ, तो अनुचित न होगा:
आज फिर इन्साफ के बाज़ू शिकस्तां हो गए।
क़त्ल सब किसने किए, इलज़ाम ये किसको गए।
जिस तरफ़ भी देखिए, बस नफ़रतों के हैं शजर*
मेरे वतन के बाग़बाँ ये बीज कैसे बो गए। शजर*= वृक्ष
सियासतदां महज़ अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, नित नए-नए राग छेड़ते रहते हैं और न जाने कितनी झूठी-सच्ची ख़बरों को हवा देते रहते हैं । आज के तकनीकी क्रांति के इस युग में तो यह और भी आसान हो गया है । ताक़तवर सियासी लोग अपने असीमित संसाधनों का उपयोग करके इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम समय में किसी भी झूठी खबर को सच और किसी भी सच्ची खबर को झूठ बनाकर फैलाने में कामयाब हो जाते हैं । इसके लिए उन्होंने ने कंप्यूटर विशेषज्ञों की बड़ी-बड़ी टीमें बना दी हैं, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आकाओं द्वारा तय की गयी झूठी-सच्ची ख़बरों को तेज़ी से फ़ैलाना होता है। इन ख़बरों का इस्तेमाल कभी अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए, तो कभी विरोधियों को नेस्तानाबूद करने के लिए किया जाता है । यह काम इतनी तेज़ी से और इतने सुनियोजित तरीके से किया जाता है कि आम आदमी को तो यह समझने का वक़्त ही नहीं मिलता कि क्या सच है और क्या झूठ!
बार-बार देखी-पढ़ी-सुनी ये बातें किसी के भी मानस को इस कदर जड़ कर देती हैं कि वह इन्हें ही सही समझने लगता है । तेज़ी से वायरल होती ये ख़बरें कब हवाओं से आँधियों में परिवर्तित हो जाती हैं पता ही नहीं चलता । और इन आँधियों के पीछे कौन है, इसकी भनक तक भी आम जनता को नहीं हो पाती । हाँ, वह इसका शिकार ज़रूर हो जाती है । अनभै सांचा में छपी मेरी पहली ग़ज़ल का मतला कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए है:
दश्त, पर्वत, घर, समंदर दल रहीं थीं आंधियाँ ।
कौन जाने किस दिशा से चल रहीं थीं आंधियाँ ।
भारत भूषण आर्य अपने इस शेर में आम-जन को आगाह करते हैं कि सियासतदानों द्वारा चलाई जा रही इन हवाओं पर बिलकुल भरोसा न करें, ये हवाएं न जाने कब दिशा बदल लें:
ऐ हवा तेरा भरोसा हो तो कैसे हो
तू दिया इसका कभी उसका बुझाती है ।
अपनी एक और ग़ज़ल के इस शेर में वे कहते हैं कि दिए को मालूम है कि आँधियों में उसका क्या हश्र होने वाला है, तो भी वह छुप कर जलना पसंद नहीं करता और खुद ही अपना पता आँधियों को दे देता है:
हश्र अपना जानते थे आँधियों के सामने
हम दिए फिर भी उन्हें अपना पता देने लगे ।
यही एक शायर की, एक साहित्यकार की विशेषता है, यही उसका परम धर्म भी है ।
मशहूर शायर राहत इन्दौरी देश में धर्म के नाम पर लोगों को बाँट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले सियायती लोगों को अपने इस शेर के माध्यम से करारा जवाब देते हैं :
सभी का ख़ून है शामिल यहाँ की मिट्टी में
किसी के बाप का हिन्दोस्तान थोड़ी है।
सियासती लोगों में एक और हुनर होता है। बड़े नेता अक्सर अपनी बात खुद नहीं कहते, औरों से कहलवाते हैं । ख़ास-तौर पर उन मुद्दों पर जिनके लिए उन्हें यह शक होता है कि मुद्दा बैक-फायर न कर जाए । तो वह अपने कुछ अन्य नेताओं से ऐसे ब्यान दिलवाते हैं जो किसी एक वर्ग के लोगों को आश्वस्त कर देते हैं कि यही दल हमारे हित के लिए काम करेगा और यदि दांव उलटा पड़ जाए तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ।
परन्तु शायर की नज़र से यह सब छुपा नहीं रह सकता । वह जानता है कि किसी छोटे-मोटे नेता की क्या बिसात कि वह कोई ऐसी बात कह सके जिसमें दल के सर्वशक्तिमान आक़ा की मर्ज़ी शामिल न हो। किसी शायर ने इस स्थिति को कितनी खूबसूरती से इस स्थिति को एक शेर में उकेरा है :
रंग यह भी बहुत पुराना है
सोचता कोई, बोलता है कोई।
मुनव्वर राणा कहते हैं कि अगर हुकुमरां को यह मुग़ालता है कि वह डरा-धमका कर लोगों को अपनी तरफ कर लेगा तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ऐसा कदाचित मुमकिन नहीं है:
डरा धमका के तुम हमसे वफ़ा करने को कहते हो
कहीं तलवार से भी पाँव का काँटा निकलता है ?
इसी ग़ज़ल का एक और शेर देखिए जिसमें वे साफ़-साफ़ कहते हैं कि सियासतदां दिलों में दरारें डालने की कितनी भी कोशिश कर ले, उसे क़ामयाबी कभी नहीं मिल पाएगी । फ़ौरी तौर पर उसे चाहे थोड़ी-बहुत सफ़लता मिल भी जाए, पर अंतत: जीत मोहब्बत की ही होगी। आज के नफ़रत भरे माहौल में उनका यह यकीन, सहरा में पानी की हल्की फुहार जैसा आनंददायी प्रतीत है:
फ़ज़ां में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत ने
मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है।
पड़ोसी देशों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर तकरार रहती ही है । ऐसे मुल्कों के सत्ताधीश एक दूसरे के खिलाफ़ बोलकर अपने देश की जनता के सामने यह साबित करने की होड़ में रहते हैं कि बस वे ही अपने मुल्क को पड़ोसी मुल्क के हथकंडों से बचा कर रख सकते हैं; जब तक वे सत्ता में हैं, तभी तक अमन और शांति रह सकती है । निरंतर इस तरह के सुनियोजित कैंपेन के ज़रिये वे एक ओर तो जनता को भटकाए रखते हैं ताकि लोगों का ध्यान अपने देश की मूलभूत समस्याओं की ओर तथा सरकार द्वारा उन्हें हल न कर पाने की तरफ़, उसकी नाकामियों की तरफ़ जाए ही नहीं। दूसरी ओर वे इस कैंपेन को अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ़ हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते हैं । बेशक अपनी-अपनी राजनीति चमकाने के लिए सियासतदानों ने सरहदों पर सियासी दीवारें खड़ी कर दी हों, सरहदों के दोनों और रहने वाले लोगों में मोहब्बत का जज़्बा बाक़ी रहता ही है । यह यकीनन बहुत ही उत्साहवर्द्धक है कि सियासी दीवारों में भी कम से कम कुछ खिड़कियाँ तो ऐसी होती ही हैं जिनसे इंसान के मूल स्वाभाव, प्रेम, की खुशबू लिए ताज़ा हवा की आवा-जाही लगी रहती है । साहित्य भी ऐसी खिडकियों में से एक है । बशीर बद्र ने इस भाव को अपने इस शेर में बहुत खूबसूरती से पेश किया है:
मुल्क तक़्सीम हुए दिल तो सलामत है अभी
खिड़कियाँ हमने खुली रक्खी हैं दीवारों में ।
राजेश रेड्डी ने भी अपनी एक ग़ज़ल में खुलकर कहा है कि आदमी के लालच ने इस दुनिया को बांट कर रख दिया है लेकिन सियासतदानों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता । ताक़त की भूख ऐसी भूख होती है जो ताक़त बढ़ने के साथ और अधिक बढ़ती जाती है। और अपनी सत्ता के मद में चूर हुकुमरां अपने खिलाफ़ उठने वाली हर ज़ुबान को हमेशा-हमेशा के लिए ख़ामोश करवा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें तो अब अम्नो-अमान वाली दुनिया भी अजीब लगती है:
जितनी बँटनी थी बँट चुकी ये दुनिया
अब तो बस आसमान बाक़ी है।
अब वो दुनिया अजीब लगती है
जिसमें अम्नो-अमान बाक़ी है।
सर क़लम होंगे कल यहां उनके
जिनके मुंह में जुबान बाक़ी है।
दीक्षित दनकौरी तो अपने इस शेर में सभी को ताक़ीद कर रहे हैं कि आस-पास हो रहे अन्याय और ज़ुलमात से सीने में उठने वाले आक्रोश को वहीं दबाकर रखिए और कोई चेहरा ओढ़ लीजिए, इसी में ग़नीमत है:
आग सीने में दबाए रखिए।
लब पे मुस्कान सजाए रखिए।
इसी ग़ज़ल का एक और शेर देखिए:
जाग जाएगा तो हक़ मांगेगा
सोये इंसां को सुलाए रखिए।
जिसमें उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के सीधा-सीधा कहा है कि सियासतदां अच्छी तरह जानता है कि जिस दिन आम आदमी सोचने लगा, सचेत हो गया, उस दिन उनके द्वारा रचा ये नफ़रत और झूठ का सियासी किला ध्वस्त हो जाएगा । इसलिए वे झूठे वादों, लुभावने भाषणों की अफ़ीम देकर उसे सुलाए रखते हैं । भोली-भाली, रोटी-पानी-रोज़गार की समस्याओं से जूझती जनता बार-बार सियासती लोगों के वादों पर विशवास करती है, और बार-बार धोखा खाती है; पर फिर से लाचार होती है फिर से किसी न किसी पर विश्वास करने के लिए। उसकी बेबसी, उसके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस स्थिति को शिव ओम अम्बर ने अपने इस शेर बख़ूबी क़ैद किया है:
यह सियासत की तवायफ़ का दुपट्टा है
ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता।
सत्ता में ग़ज़ब का आकर्षण होता है। सत्ता के इर्द-गिर्द इकठ्ठा होने वालों का, सत्ता से चिपकने वालों का हुजूम सामान्यत: बहुत बड़ा होता है। ये लोग हमेशा सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तत्पर रहते हैं, उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उनके जयघोषों में सभी निरीह, असहाय आवाज़ें दब कर रह जाती हैं । इस स्थिति का ब्यान जितनी सटीकता के साथ बशीर अहमद ‘मयूख’ ने अपने इस शेर में किया है, उसकी दूसरी मिसाल ढूंढ पाना मुश्किल है
राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है।
आदमी फुटपाथ पर बेहोश होता है।
और सत्ताधीशों को ख़ुदा मान लेने वालों की कमी नहीं होती। वो उनपर इस क़दर विश्वास करने लगते हैं जैसे किसी भक्त को अपने भगवान् पर होता है। श्रद्धा इतनी कि तर्क, विवेक, बुद्धि, उचित-अनुचित पर चर्चा करने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। और उनका यही अंधविश्वास,जहां एक तरफ़ सियासतदां को ज़रुरत से ज़्यादा ताक़तवर बनाकर, एक गैर-जिम्मेदार तथा निरकुंश शासक बनाती है, वहीं देश और समाज का भी अहित करती है।
इस सबसे कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिसमें कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रह जाता और दबी-कुचली जनता चुपचाप, बिना कुछ कहे अपने हाल में जीने को मजबूर हो जाती है । पर किसी संवेदनशील शायर की नज़र से समाज का यह दमघोंटू माहौल न तो छिपा रह सकता है, और न ही वह इस पर बिना कुछ कहे जिंदा ही रह सकता है । मुमताज़ नाज़ां कहती हैं कि जैसा सियासी माहौल आजकल पैदा हो गया है, उस में सीधा-सच्चा आदमी घुटन महसूस करने लगा है :
हुआ है दुशवार साँस का आना जाना भी अब
अजीब सी इक घुटन शहर की फ़सील* में है।
फ़सील– दीवार हर एक मासूम शख़्स को अब सज़ा मिलेगी नयी रवायत ये आजकल के अदील* में है।
अदील** -न्याय व्यवस्था
‘इशरत’ किरतपुरी की एक ग़ज़ल का यह शेर भी देखिए:
मेरे लिए तो सांस लेना भी मुहाल है
माहौल की ये सारी घुटन मेरे साथ है।
जिसमें शायर हवा में फैलती और लगातार बढ़ती घुटन का ज़िक्र करता है। यह एक तरह से बिगड़ती स्थितियों की पूर्व-सूचना है जिसका एक ही मकसद है कि लोग समय रहते स्थिति को संभाल लें, क्योंकि शायर तो अक्सर समाज में आपसी द्वेष पैदा करने के लिए फैलाई जा रही कोशिशों के चलते, आने वाले हालात की आहट को बहुत पहले ही सुन लेता है।
पर हुकुमरानों के इशारों पर चलने वाला मीडिया जब दिनभर उन्हीं के शान में शंख बजाता रहेगा, उनकी वाह-वाही के ढोल पीटता रहेगा, तो शायर की आवाज़ नक्कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह दब ही जायेगी ना । मीडिया पर दिन-भर चलती प्रायोजित बहसों के चलते, पैसे की चमक-दमक के आगे, किसी एक क़िताब के किसी पन्ने पर लिखी ग़ज़ल के अशार तो नहीं न दिखेंगे । परन्तु इस माहौल में भी शायर हतोत्साहित नहीं होता और अपने लेखक-कर्म को बखूबी, बिना किसी भय के निरंतर निभाता रहता है । मेरे ये दो शेर देखिए:
कहीं कोई ख़ुदा पैदा हुआ है।
उसे इक बार फिर धोखा हुआ है।
मंजीरे, शंख, बाजे, ढोल, ताशे
ये सब मंज़र मेरा देखा हुआ है।
माहौल की यह घुटन केवल वही आदमी महसूस कर सकता है जो अपने आस-पास जो कुछ गुज़र रहा है उसके प्रति संवेदनशील हो । जो व्यक्ति सिर्फ अपने या अपने परिवार तक ही सीमित हो, अव्वल तो वह यह सब देख ही नहीं पाता और अगर देख भी सके तो उसे अनदेखा कर देता है । एक सच यह भी है कि आज के इस कट-थ्रोट कम्पटीशन में अधिकतर लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो इधर-उधर देख भी सकें और शायद वे यह भी अच्छी तरह जान गए हैं कि देखेंगे तो सोचेंगे और सोचेंगे तो तकलीफ़ होगी; और आवाज़ उठाने का मतलब है अपने को और अपने परिवार को मुसीबत में डालना । जहां हमारी अपर-मिडिल क्लास (बेशक अपने सार्थक प्रयत्नों और कठिन परिश्रम के द्वारा) आज जिस मुकाम पर पहुंची है, उसे भोगने में और अपने उस मुकाम पर बने रहने में ही इतनी उलझ गयी है कि उसे बेरोज़गारी, भूख, ग़रीबी किसी गुज़रे ज़माने की बातें लगने लगी हैं, वहीँ लोअर और मिडिल, मिडिल क्लास अपने को अगली श्रेणी में लाने के लिए और अपने परिवार और परिजनों के लिए बुनियादी (मानी जाने वाली) सुविधाएँ जुटाने में दिन-रात इस क़दर उलझी हुई है कि उसे किसी और की हालत पर नज़र डालने की फ़ुर्सत ही नहीं है । उन्होंने शायद अपने-अपने दिल के सभी झरोखों पर मोटे, गहरे रंग के परदे गिरा लिए हैं जिससे बाहर की दुनिया न दिखे, न तकलीफ़ हो । बशीर बद्र ने लोगों की इस फ़ितरत को बड़े ही करीने से अपने इस में ज़ाहिर किया है:
बहुत से लोग दिल को इस तरह महफ़ूज़ रखते हैं
कोई बारिश हो ये कागज़ ज़रा भी नम नहीं होता।
और पूंजीपति तथा कॉर्पोरेट वर्ग के लोगों की तो बात भी क्या कहें । वे तो स्वयं सत्ता का हिस्सा बने हुए होते हैं। जो सत्ता में हों वही उनके आक़ा ! चुनावों में संभावित सताधीशों को पोसना और फिर बाद में उनसे फ़ायदा उठाना, यह आज के कॉर्पोरेट सेक्टर के एक बड़े हिस्से का तरीका भी बन चुका है और चरित्र भी । सरकारें भी अपने इन दोस्तों के मन-मुताबिक़ नीतियाँ बनाने में कतई नहीं हिचकिचातीं । इस मिले-जुले व्यापार में बलि का बकरा बनती है, तो सिर्फ और सिर्फ जनता! पूँजी और सत्ता के इस नापाक गठबंधन की अट्टालिकाओं की नींव बहुत मज़बूत, और दर-ओ-दीवार साउंड-प्रूफ़ होते हैं जिनमें से होकर बेबस-लाचार जनता की आवाज़ हुकुमरानों के कानों तक पहुँच जाए यह लगभग ना-मुमकिन ही होता है ।
साहित्य का एक काम समाज में व्याप्त घोर निराशा को दूर भगाने के लिए आशा के नित नए दीप जलाना भी है । आईये जमील ‘हापुड़ी’ की एक ग़ज़ल के दो शेर देखते हैं:
क़ातिल का कहीं किरदार तो है।
कागज़ की सही, तलवार तो है।
क़ाबू में नहीं कश्ती न सही
हाथों में अभी पतवार तो है।
जमील इन शेरों में कुछ सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उम्मीद जगाये रखने की कोशिश करते हैं कि हालात से लड़ते हुए, जहां तक जितना हो सके, उतना ही करते चलना भी एक तरह से क्रान्ति की नींव डालना ही है, अन्याय के खिलाफ़ लड़ाई को जिंदा रखना है ।
शायर दरअसल चाहता है कि एक मानवीयता की, इंसानियत की, एक परस्पर प्रेम और विश्वास की सत्ता की स्थापना हो। उसकी दिली इच्छा होती है कि कोई तो ऐसा परिवर्तन आए जिस से समाज, देश और विश्व, इस दिशा में कम से कम क़दम बढ़ाता हुआ तो दिखे। और ऐसा करने के लिए शायरों को/साहित्यकारों को ही अपनी क़लम उठानी होती है। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब किसी क़लम से निकली कोई एक पंक्ति, एक क्रांति उठा देती है और एक ऐसी आवाज़ बनती है जो आतताइयों का सिंहासन हिला देती है, चाहे वो कहीं भी हों, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी रूप में। मुझे यहां अपनी एक ग़ज़ल
फूल दिखला के मेरे ज़ख़्म खिलाने वाले।
लौट के आ ऐ मुझे छोड़ के जाने वाले।
का एक शेर याद आ रहा है:
ये सदा अर्श के पर्दों को हिला सकती है
मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले।
और जब यह आवाज़ क्रांति को जन्म देती है, तो ऐसी आंधियां चलती हैं जो निरंकुश शासक के चेहरे से उसका झूठा नक़ाब नोच के फ़ेंक देती हैं और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। और तब, सब से अधिक आहात होते हैं निस्स्वार्थ भाव से उसके साथ जुड़े वो लोग जो उसके साथ सिर्फ इस लिए जुड़े हुए थे कि वो समझते थे कि बस एक वही है जो अन्य शासकों से अलग है और उन्हें सही दिशा में लेकर जाएगा; जिन्हें उस पर विश्वास था और जो उसके प्रति बे-इंतिहा श्रध्दा रखते थे। और जब ऐसे लोग अपने उस ‘देवतुल्य व्यक्तित्व’ को आईना दिखाते हैं, तो उसका तिलिस्म ख़त्म हो जाता है। यहां मेर एक शेर देखिये जो इस स्थिति के बहुत क़रीब है:
अक्स अपना देख कर वो डर गया, घबरा गया
आईने हाथों में लेकर चल रहीं थीं आंधियां।
झूठ की नींव पर खड़ा उसका अभेद्य किला भर्भरा कर बिखर जाता है। ऐसे ही कुछ भाव शायद आपको मेरे इस शेर में भी नज़र आएं:
आज हमने ये सुना कि वो शजर भी गिर गए
जिनके पत्तों के सहारे चल रहीं थीं आंधियां।
डॉ. जगमोहन राय ‘सजल’
नाम: जगमोहन राय ‘सजल’
सम्प्रति: दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य) से 31 जुलाई, 2023 को गणित के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवा-निवृत।
पता: C-45, कुंज विहार अपार्टमेट्स, प्लाट न.-19, सेक्टर–12, द्वारका, नई दिल्ली-110078
ई-मेल: drjagmohanrai@gmail.com
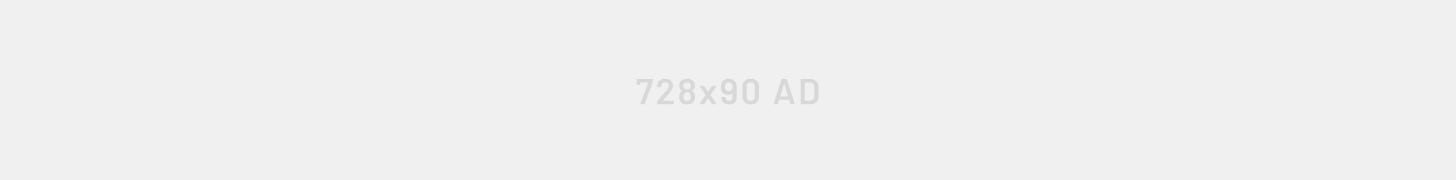
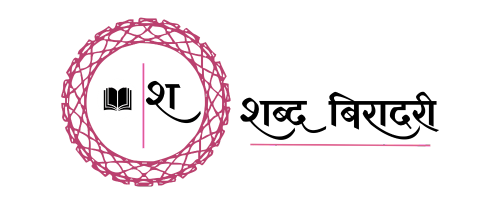

बहुत बढ़िया लेख।
Very beautifully compiled, the complex trilogy of
Power, literature and Ghazal alingwith your passion , Mathematics. Keep on sharing these beautiful works for helping us evolve.
Dr Saheb, very beautifully compiled, the complex trilogy of
Power, literature and Ghazal alingwith your passion , Mathematics. Keep on sharing these beautiful works for helping us evolve.
बहुत अच्छा लेख।
Jagmohan sir, very well done.Collection of Ghazals for writing the actual situation of country. Kindly continue writing along either your collection.
Thanks
Jagmohan sir, very well done.Collection of Ghazals for writing the actual situation of country are excellent. Kindly continue writing along with your collection.
Thanks
ज्ञानवर्धक लेख