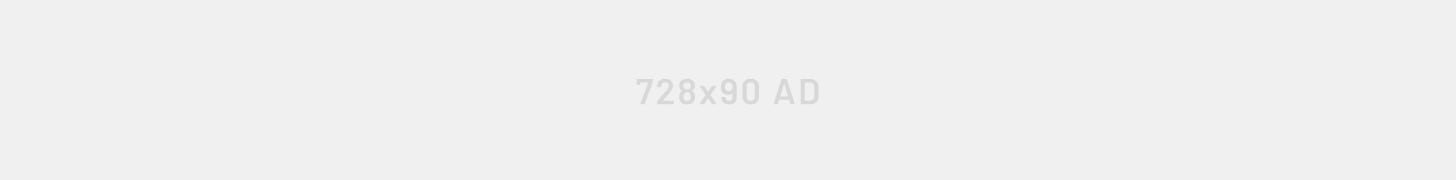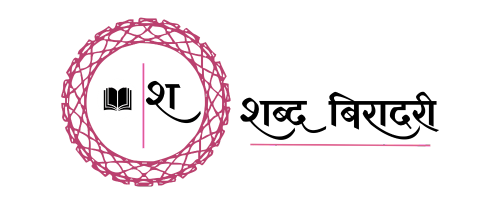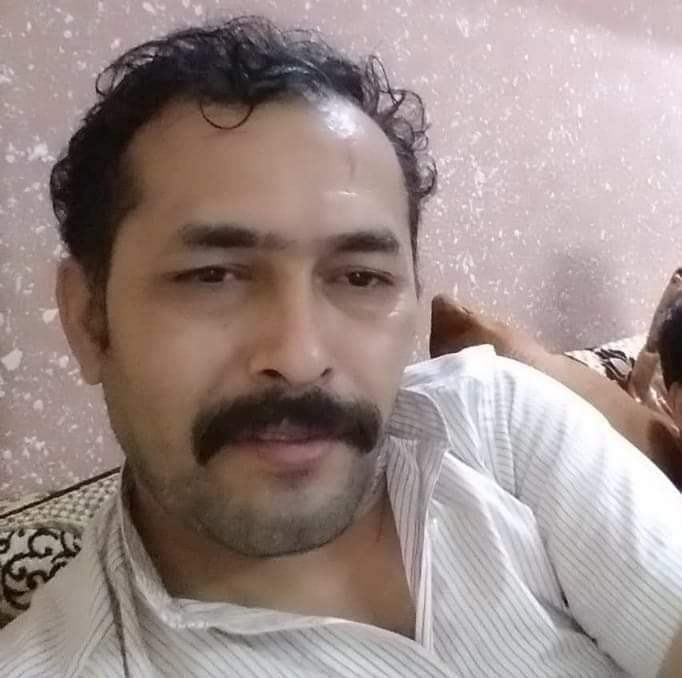
कबीर की पंक्तियाँ हैं, ‘सब दुनी सायानी मैं बौरा/ हम बिगरे बिगरी जनि औरा/’. इन पंक्तियों की जानी-पहचानी व्याख्या को छोड़ दें तो ये पंक्तियाँ एक व्यक्ति के ‘बयान’, उसके ‘स्टेटमेंट’ की तरह भी पढ़ी जा सकती हैं. एक ऐसे बयान के तौर पर, जो तब दिया गया मालूम होता है जब कबीर को उनके अपने सामाजिक वातावरण और भूगोल में एक बौराया हुआ ‘आदमी’ कहा जाने लगा होगा. एक रचनाकार के लिए ही नहीं अपितु सामान्य व्यक्ति के लिए भी अपने परिवेश से विस्थापित कर दिए जाने की पीढ़ा मारक और त्रासद होती है. किसी को ‘बौराया’ हुआ प्रचारित कर देने को, समय और समाज से क्या उसे विस्थापित कर देना नहीं कहा जा सकता! संस्कृत के महान कवि भवभूति को याद कीजिये, जिन्होंने ‘समाज’ द्वारा अपने साहित्यिक (जो उतना ही सामाजिक भी है) नकार और अस्वीकार के जवाब में ‘काल’ को अपना लिया था. कुछ ऐसा ही हमें कबीर में दीखता है जब वो अपनी पत्नी ‘लोई’ को संबोधित करते हुए कहते हैं, ‘इब न रहूँ माटी के घर मैं/ इब मैं जाई रहूँ मिलि हरि मैं’. ‘राम’ को कबीर अपना ठिकाना बना लेते हैं. नया ठिकाना. राम कबीर के लिए ‘अमरपुर’ हैं. एक ऐसा ‘नगर’ हैं जहाँ न पाप-पुन्य की जड़ताएं है, न वेद-कतेब, मंदिर-मस्जिद की सीमाएं हैं. जहाँ “डग-डग रोटी पग-पग नीर” उपलब्ध है. साथ ही उन्हें पागल कहने वाले थोथे समाज से मुक्ति भी है.
कबीर और उनके ‘राम’ का सम्बन्ध आश्चर्यजनक रूप से संभावनाशील है. ये सम्बन्ध जितना भक्त-ईश्वर का सम्बन्ध है, उससे कहीं ज्यादा एक सत्यान्वेषी जीव और गुण-निर्गुण दोनों से परे जो ब्रह्म-तत्व है, उनके बीच निरंतर विकसित होता एक काव्यात्मक सम्बन्ध है. ये सम्बन्ध शुरू ही होता है, इन शब्दों में, – “करता की गति अगम है, तूं चल अपणें उनमान/ धीरैं धीरैं पाँव दे, पहुंचेंगे परवान”. कबीर ने जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध को एक खोजी यात्रा के बिम्ब में उतार दिया है. इसीलिए कबीर के राम जाने-पहचाने और परिभाषित राम नहीं हैं. जिसे राम के नाम से जाना–माना जाता है, उसे कबीर अपना राम नहीं मानते. कबीर कहते हैं, “कहें-सुनें कैसे पतिअईये/ जब लग तहां आप नहिं जईये” जिसे आपने खुद पाया ही नहीं, जहाँ खुद आप कभी गए ही नहीं, उसे अपना कैसे माना जा सकता है. मानने के लिए तो जरूरी है, पहले जाना जाये. कबीर राम को जान लेना चाहते हैं. बिना जाने वो किसी को भी अपना मान लें, ये संभव नहीं है. ऐसे में कबीर राम को खोज और अन्वेषण में बदल देते हैं. रूप से पहले भाव में बदल देते हैं. और रूप से मुक्त हो जाते हैं. राम के रूप से मुक्ति न केवल कबीर को अपितु खुद ‘राम’ को भी संभावनाओं से भर देती है. अब उसे ‘नया’ रूप दिया जा सकता है, एक नहीं अनेक रूप दिए जा सकते हैं, कम से कम इतनी सी सम्भावना तो पैदा हो ही जाती है. कविता रूप की जड़ता के खिलाफ ही ‘रूप’ को रचती है. इसे कबीर की कविता का पाठक खुलकर देख सकता है. कबीर राम के जड़ रूप के खिलाफ ही ‘राम’ को रचते हैं. कबीर हालाँकि ऐसा सामाजिक-वैयक्तिक जीवन के हर पहलू के साथ करते है.
इस आलेख में कोशिश की गयी हैं कि संस्थागत सामाजिक-धार्मिक परिवेश के साथ कबीर के, कवि-व्यक्ति के ‘संबंधों’ और तत्जनित भावात्मक-वैचारिक परिणितियों को रेखांकित किया जाये. इसीलिए कबीर की कविता में से सामाजिक और धार्मिक आचरणों और संस्थानिक रुढियों से जुड़े हिस्सों को ही ज्यादा ‘फोकस’ में रखने का प्रयास किया गया है. धार्मिक-दार्शनिक मान्यताओं और आचरणों की निरर्थकता और इसी निरर्थकता के कारण अर्थहीन और जड़ होते सामाजिक परिवेश को जब कबीर अपना विषय बनाते हैं, तो उदहारण और गवाही दोनों का इस्तेमाल करते हैं. उदहारण वे प्राय: मानवेत्तर जीवन से लाते हैं और गवाही खुद उसकी जिसके ‘नाम’ के पीछे ही इन सारे प्रपंचों को रचा गया है. पवित्रता के सारे ‘प्रतीक’, पुन्य के सारे ‘करम’ पूजा-पाठ, मंदिर-मस्जिद, व्रत उपवास इत्यादि सभी जिस राम के लिए आयोजित किये गए हैं और निरंतर किये जा रहे हैं, वे निरर्थक और बेमतलब हैं, ऐसा सिर्फ कबीर ही नहीं कहते अपितु खुद कबीर के राम भी कहते हैं.
बयान के आलावा ‘गवाहियाँ’ भी कबीर की कविता में सहज ही देखने को मिलती जाती हैं. कबीर ईश्वर को सामने खड़ा कर देते हैं. मानो कह रहे हों इन्हीं से पूछ लो ! कबीर के ‘राम’, पदों और दोहों में क्या इसीलिए खुद सामने आ जाते हैं, ‘मोकों कहाँ ढूंढे बंदे…’ कहते हुए. कबीर की कविता, उन धार्मिक संस्थाओं और आचरणों की पूरी फेहरिस्त देती है, जो ईश्वर-भक्ति के नाम पर चारों तरफ फैले हुए हैं. कबीर भी उन्हें थोथा बताते हैं और कबीर के राम भी. अपने ‘आराध्य’ का ऐसा इस्तेमाल सिर्फ अचरज ही पैदा नहीं करता अपितु उससे आगे जा कर सोचने के लिए आमंत्रित भी करता है.
कबीर एक स्वप्नदृष्टा कवि थे, ऐसा इसलिए भी क्योंकि उन्हें ‘समाज’ जिस रूप में मिला था , उसमें ‘स्वप्न’ ही वो जगह हो सकते थे, जहाँ जीवन के लिए ‘जीवित’ को पाया जा सकता था. अन्यथा, जो था वो तो इतना असहनीय और मारक था कि उसे सहना संभव नहीं.
**
अपने सामाजिक परिवेश का जो व्यक्ति-दृश्य कबीर ने अपने एक पद में खींचा, वो देखा जा सकता है. यह पद कबीर के अपने वास्तविक सामाजिक ‘सन्दर्भ’ को रेखांकित करता है –
“ठग्ग बटमार संसार में भरि रहे, हंस की चाल कहँ काग जानी/
चपल और चतुर हैं बनै वहु चकिने, बात में ठीक पै कपट ठानी/
कहा तिन सों कहों दया जिनके नहीं, घात बहुतें करै बकुल ध्यानी/
काग कुबुधि पावै कहाँ, कठिन कठोर विकराल बानी/
अगिन के पुंज हैं सितलता तन नहीं, अमृत और विष दोऊ एक सानी”
ठग, लुटेरों से यह संसार भरा हुआ है. इन्होने हंस की भाषा और भेष अपना लिया है, लेकिन हंसों को दर-बदर कर दिया है. चपलता, चतुरता और कपटता ही इनका आचरण है. इनमें दया और धर्म का भाव है ही नहीं, उलटे इन्होंने उसे घात करने का हथियार बना डाला है. बदकिस्मती से ये ही वे लोग हैं जो जगत को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं. कबीर कहते हैं, “अति पुनीत ऊंचे कुल कहिये, सभा मांहि अधिकाई./ इनसे दिच्छा सब कोई मांगे, हँसि आवै मोहि भाई.” सामाजिक-मानवीय संबंधों और आचरणों में ‘विपरीतताओं’ का विवेक कुंठित हो गया है. विष और अमृत दोनों एक सामान हो गए हैं. कबीर को हंसी आती है. ये हंसी इन्हीं विसंगत और विपरीत सामाजिक-मानवीय संबंधों और आचरणों को देखकर आती है. जो सहज है, सामान्य है और वास्तविक है, उसे भुला दिया गया है. उसकी जगह पर असहज, असामान्य और आवास्तविक को स्थापित कर दिया गया है.भ्रम और मिथ्या का सकल पसारा है. सामान्य विवेक को तज दिया गया है. जो खुद अंधे हैं, ये जगत उन्ही से दृष्टि मांगता फिर रहा है. जो ‘करतार’ राम बेहद करीब था, समाज ने उसी की मूरतें थाप कर उसे अपने से दूर कर दिया है. और अब जंगल-जंगल उसे खोजने की शिक्षा दे रहा है.
कबीर के शब्दों में, “ दूरहि करता थापिकै, करी दूर की आस” इसी से, “घर की वस्तु निकट नहि आवत दियना बारि के ढूँढत बंदा.” समाज भ्रमों और मिथ्याओं से भर गया है. उसने गलत रास्ते पकड़ लिए हैं. जब रास्ता ही गलत ले लिया गया है, तब सही मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है. कबीर के शब्दों में, “यह जग अँधा मैं केहि समझावों/ एक दुई हों उन्हें समुझावों सब ही भुलाना पेट के अँधा”. समाज पेट के अंधों से भर गया है. इस स्थिति को ‘समाज’ की अवधारणा और उसकी संस्थागत वास्तविकता के साथ जोड़कर अगर देखें तो दो बातें स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं. एक तो ये कि समाज अपनी आदर्श अवधारणा से दूर हो गया है और दूसरी ये कि व्यक्ति के साथ उसके संबंध विपरीत हो चुके हैं. अब समाज प्रकाशवान ‘द्वीपों’ को नहीं, अपितु अंधों को पैदा कर रहा है. तब अंधे समाज को कौन सी दिशा और रास्ता दिखाएंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है. ‘अँधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पडंत’.
समाज अंधों से क्यों और कैसे भर गया है.? कबीर के काव्य-संसार के अपने दायरे में, इस क्यों और कैसे का जवाब ‘दर्शन’ और ‘धर्म’ की संस्थाएं नहीं, तत्कालीन समाज की औपचारिक-अनौपचारिक ‘शिक्षण-संस्थाएं’ ही देती हैं, जिनका एक प्रमुख रूप मंदिर-मस्जिद है. और इसी कारण पंडित-मौलवी को कबीर बार-बार संबोधित करते हैं. कबीर के शब्दों में, “छापा – तिलक बनाई करि, दगध्या लोक अनेक” इन्हीं पंडित-मौलवियों ने भिन्न-भिन्न भेदों को रचकर ‘समाज’ को धधकती भू-देह बना दिया है. और अब ये लोक इसी भेद की आग में जल रहा है. अलग-अलग रूपों और रंगों की आग में जल रहा है. जातियों के भेद, दीन-धर्म के भेद, रूप-रंग के भेद, धन-धान्य के भेद, आदमी-औरत के भेद, और यहाँ तक कि ईश्वर-ईश्वर के भी भेद, ये ही हैं, जो असल बन बैठे हैं. कबीर की दृष्टि में इन्हीं भेदों ने जगत को अँधा कर दिया है. इन्हीं भेदों की आग में समूचा जगत जल रहा है. “ पक्षा पक्षी के कारनै, सब जग रहा भुलान” इन भेदों ने न केवल इस लोक को भटका दिया है, अपितु उस जीव को भी भटका दिया है, जिसको इस जीवन का उपयोग मुक्ति के लिए करना था.
इन्हीं ‘भेदों’ से कबीर का वो समाजिक भूगोल बनता है, जिसमें ‘व्यक्ति’ को (दार्शनिक शब्दावली में जीव को) रहना है. कबीर के कवि-व्यक्ति को इसी सामाजिक-भूगोल की द्वंदात्मकता में देखे जाने की आवश्यकता है. कबीर अपनी तमाम कविता में इस सामाजिक भूगोल में ‘व्यक्ति’ की त्रासद-स्थिति को रचने का काम करते हैं. इस सामाजिक-परिवेश और उसके भेदवादी ‘ज्ञान’ को कबीर भ्रम और माया का जाल कहते हैं. एक ऐसा जाल जो सब को खा रहा है. जीव और जगत दोनों ही भ्रम की मौत मर रहे हैं. ठीक उस ‘बीज’ की तरह जिसे ‘खेत’ ही न मिला हो, “बीज न खेत निवारा”. समाज का ‘परिवेश’ ऐसा बन गया है जो न तो समाज को ही विकसित करता है और न ही व्यक्ति को. उलटे दोनों को ही ऐसे भ्रमों और मिथ्याओं से उसने भर दिया है जिन्होंने इन्हें ‘जीवित-मुर्दों’ का एक विचित्र नमूना बना दिया है. व्यक्ति ही नहीं अपितु समाज की ‘अवधारणा’ भी अपने सामाजिक-परिवेश की ही उपज होती है. दोनों के मध्य ‘मा-बेटे’ का सम्बन्ध होता है. ऐसे में कितना त्रासद और मारक है ये अनुभव कि मां ही अपनी संतानों को खा रही है. कबीर कहते हैं, “यह अपने बलकवै रहै मारि”. सामाजिक वातावरण ही अपने बासिंदों का भक्षण कर रहा है. अपने परिवेश की ऐसी अनुभूति ने कबीर को कितना अजनबी और अकेला बना दिया होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है. अकेलेपन की अनेक छवियाँ कबीर अपनी कविता में दर्ज करते हैं. कबीर की कविता में बार-बार एक विलग स्त्री अपने पिया को ढूँढती नजर आती है. पूरे सामाजिक दायरे में ऐसा कोई नहीं है, जो उसे उसके पिया की खबर दे सके. “मैं कासें बुझों अपने पिया की बात री”. ये अकेलापन खुद कबीर का अपना है. सब तरफ रूप, रंग और दृश्यों की भरमार है लेकिन वो ‘दृष्टि’ कहीं खोजे नहीं मिलती जिससे जीवन प्रकाशित होता है.
कबीर उसे अँधा कहते हैं जो ‘भेद’ को ही ज्ञान, दृष्टि और आचरण मानता और मनवाने की चेष्टा करता है. लेकिन इस बात को भी कबीर के शब्दों में ये भेदवादी समझने वाले नहीं है, “अंध भेदी कहा समझेंगे, ज्ञान के घर तैं दूरा”. कबीर इस भ्रम को सिर्फ जीव की ही भ्रान्ति मानकर चुप नहीं हो जाते हैं, अपितु वो उन लोगों, विचारों और संस्थाओं की भी सामाजिक परिवेश में पहचान करते हैं, जो इन भ्रमों को रचने-गढ़ने और पालने का काम करते हैं. कबीर इसे ‘विष का ब्योपार’ कहते हैं. “सभ पंडित मिलि धंधे परिया,कबीर बनौरी गावै” ये सब भ्रम का व्योपार इन्हीं पंडितों का फैलाया हुआ है. “कहहिं कबीर सुनहु हो पांडे, ई तुम्हरे हैं करमा” ये वही हैं, जिन्होंने कभी साहिब को पाया नहीं, उससे बिना परिचय ही ‘साहिब’ होकर बैठ गए हैं और उसका व्योपार कर रहे हैं.
कबीर की कविता अपने सामाजिक परिवेश में मंदिर-मस्जिद और पंडित-मौलवी के रूप में उन संस्थाओं की पहचान करती है जो विषमता और भेद के संरक्षक ही नहीं अपितु खाद-पानी भी हैं. कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन संस्थाओं का दायरा समाज के धार्मिक-जीवन तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु व्यक्ति की सामाजिकता और उसका सामाजिक अस्तित्व भी इन्हीं संस्थाओं और इनके संरक्षकों द्वारा परिभाषित और नियंत्रित होता रहा है. ऐसे में ‘जीवन’ और ‘जगत’ को जीव के लिए जीवन-मरण का दांव मानने वाले कबीर के लिए, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न धर्म का हो जाता है, उससे कम महत्त्व का सवाल ‘समाज’ भी नहीं रह जाता. कबीर के लिए जीवन और जगत का प्रश्न जितना धार्मिक-दार्शनिक है, उतना ही सामाजिक भी है.
कबीर जीवन को महत्त्व देते हैं. जब जीवन को महत्त्व देते हैं तो जगत की अवहेलना कैसे हो सकती है. इसीलिए जगत के प्रति ‘दृष्टि’ कबीर का मुख्य कथ्य है. भेद-वाद के साथ ही लोलुपता जीवन और जगत दोनों को नष्ट कर देती है. लोलुपता की दृष्टि जीवन-जगत को माया में बदल देती है, अन्यथा जीवन और ये जगत तो ब्रह्म की रचना है, सृष्टि है. जीव के लिए अवसर है, मौका है. एक दाव है, जो चूकना नहीं है. कबीर के लिए जीवन और जगत, ‘फिर न लगै अस दाव’ जैसा महत्त्व रखते हैं. लेकिन भेदवाद और लोलुपता का भ्रमजाल जीव को इस अवसर का फायदा उठाने के विवेक तक पहुँचने ही नहीं देता.
कबीर की कविता अपने श्रोता में इसी विवेक की रचना करने का लक्ष्य लिए हुए है. इसीलिए वे स्वयं भी अपनी कविता को ‘गीत’ नहीं, ‘विचार’ की संज्ञा देते हैं. विचार भी साधारण नहीं, अपितु ‘ब्रह्म-विचार. जिसके दायरे में जीव, जगत और ब्रह्म तीनों आ गए हैं. कबीर का काव्य-विचार इन तीनों के प्रचलित पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता हुआ नए संबंधों का रेखांकन करता है. जीव का जगत के साथ, जीव का ब्रह्म के साथ और ब्रह्म एवं जगत का जीव के साथ क्या असल सम्बन्ध है, इसका रेखांकन कबीर की कविता करती है. इसी के माध्यम से कबीर अपने ‘श्रोता’ जीव में जीवन और जगत के प्रति विवेक दृष्टि पैदा करने का प्रयास करते हैं. जीव अपने जीवन के मूल्य को पहचान सके इसके लिए आवश्यक है, कि वो जगत की भ्रमपूर्ण समझ से मुक्त हो जाये. कबीर की कविता का यह ‘रुझान’,असल में कवि-कबीर द्वारा अपने समय में व्यक्ति और समाज के संबंधों की ‘पुनर्व्याख्या’ की चेष्टा को रेखांकित करता है.
इसके लिए कबीर ने अपने ही सामाजिक परिवेश और परंपरा में विद्यमान दार्शनिक-धार्मिक प्रयुक्तियों का इस्तेमाल किया है. कबीर अपने सामाजिक वातावरण को सपाटता में नहीं, अपितु उसकी तमाम जटिलताओं के साथ देखते हैं. इसीलिए तो वे बार-बार जीव से विवेक की मांग करते है. विवेकपूर्ण चुनाव को, जो जीव को अपने ही अनुभव से हासिल हो सकता है, महत्त्व देते हैं. विवेकपूर्ण चुनाव की आवश्यकता सपाट नहीं, अपितु जटिल स्थितियों में ही हो सकती है. कबीर ऐसे ही नहीं कहते कि ‘सार को पकड़ लेना चाहिए और जो थोथा है उसे छोड़ देना’ चाहिए. इसके लिए एक तरफ कबीर दार्शनिक-धार्मिक ज्ञान-मीमांशा और वर्तमान धार्मिक-आचरणों को एक-दुसरे से टकरा देते हैं, तो दूसरी तरफ ‘मृत्यु’ की वास्तविकता का सामाजिक परिवेश के प्रति दृष्टि के लिए रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं.
दुनिया का कोई भी दर्शन हो, वो मानता है कि एक कोई परम शक्ति है जिसने इस जगत और ब्रह्माण्ड को रचा है. जीव और जगत दोनों ही उसी की रचनाएं हैं. फिर कैसे हमारा सामाजिक परिवेश अनेकों ‘ईश्वरों’ से भर गया है. कबीर सवाल करते हैं, “(भाई रे) दुई जगदीश कहाँ ते आया…अल्लह-राम-करीमा केसो, हजरत नाम धराया” इसी के साथ “हिन्दू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना” कौन सी बात सही है. इस तरह के सवालों से कबीर की कविता भरी पड़ी है. येही वे सवाल हैं जो ‘श्रोता’ जीव के लिए चुनाव, वो भी विवेकपूर्ण चुनाव को आवश्यक बना देते हैं. इसके बाद कबीर जीव-ब्रह्म के उस आध्यात्मिक सम्बन्ध को अपनी कविता में रचते हैं, जिसे हमारा सामाजिक परिवेश भूल बैठा है. कबीर का पद है, “ दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम/ उठे तो नीर है बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम/ उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम.” ब्रह्म और जीव का यही सम्बन्ध कबीर अपनी कविता में रचते हैं. साथ ही यह भी कहते हैं, कि इसे सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, अपितु इसे अर्जित करना होता है. कमाना होता है. ‘दरिया’ और ‘लहर’ में ‘नीर’ का सम्बन्ध है, और इस नीर को हर लहर को अपने में अर्जित करना होगा, तभी वो दरिया को पा सकेगी. और कहने की आवश्यकता नहीं कि ‘अर्जन’ की यह प्रक्रिया तभी संभव है जब ‘जीव’ अपने को उपस्थित सामाजिक-परिवेश और वातावरण से परे ले जाये. अब इसकी एक व्याख्या ये है कि जीव अपने सामाजिक परिवेश से विलग हो जाये. उससे निरपेक्ष हो जाये. उसके प्रति उदासीनता को अपनाना ले. लेकिन असल में कबीर की कविता इस व्याख्या को ख़ारिज करती है. कबीर की कविता अपने सामाजिक-परिवेश से जीव के विलग हो जाने की जगह उसे ‘भेद’ जाने की मांग करती है. यानि कि अपने सामाजिक परिवेश के साथ व्यक्ति के ‘नूतन’ और सकर्मक सम्बन्ध की मांग करती है. अर्जन की मांग ही अपने में सापेक्षता और सक्रियता की मांग करना है, और इसकी शुरुआत कबीर करते हैं जीव और जगत की उस वास्तविकता के साथ जिसे मृत्यु कहा जाता है. जीव को जगत की नश्वरता को आँख खोलकर देखना होगा. तभी वो अपनी वास्तविकता को पहचान पायेगा. कबीर कहते हैं, कि ये जग ठीक वैसा ही है जैसा वो बाजार होता है जिसे व्यापारी सजाता है. फिर शाम ढले उस व्यापारी को वो बाजार समेटना ही पड़ता है. या फिर उस ‘मायके’ की तरह जिसे हर ‘स्त्री’ को छोड़ना ही होता है. ये उदहारण कबीर जग को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इन उदाहरणों से जहाँ एक ओर जग परिभाषित होता है, वहीँ दूसरी ओर इसके साथ जीव का नश्वर सम्बन्ध भी रेखांकित होता जाता है. जीव और जगत का सम्बन्ध ग्राहक और बाजार जैसा है, पेड़ और पक्षी के सम्बन्ध जैसा है. अत: इसका विवेक जीवन में सदैव बना रहना चाहिए. कबीर ‘कुदरत’ को विराट गतिवान चक्की के तौर पर इसीलिए बार-बार रेखांकित करते हैं. जिसमें सभी कुछ नष्ट और मर जाता है. इससे कोई भी नहीं बचा. यही मूल स्वरुप और प्रकृति है जगत की. ऐसे में वो भेदवाद और लोलुपता कैसे बची रह जाएगी, जिसने सकल संसार में अपना विस्तार फैला रखा है. ऐसे में वे पंडे-पुरोहित-मुल्ले-मौलवी, मंदिर-मस्जिद, बेद-कितेब और दीन-धर्म कैसे बचे रह जायेंगे, जो विष और झूंठ का व्यापार करते हैं. कबीर की कुछ काव्य-पंक्तियाँ हैं, “ऐसा भेद बिगुचन-भारी/ बेद-कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी/..को बाह्मन को सूदा/..कहै कबीर एक नाम जपहु रे, हिन्दू-तुरक न कोई/…बिनसि गयां थैँ का नांव धरिहौं,” जो खुद नष्ट हो जाने हैं, उनका क्या नाम धरना. जो खुद नश्वर हैं उनका क्या आचरण और व्यव्हार करना. कबीर विभिन्न मतों-संप्रदायों को ‘नाना रोग’ पैदा करने वाला कहते हैं, “नहीं कुछ ग्यान ध्यान सिधि जोग, ताथें उपजै नाना रोग.”(हिंदी के जनपद संत, पृष्ठ-३०) ऐसे में इनके भरोसे जीव अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता. सबसे पहले उसे इन ‘जग व्यौहारों’ को तजना होगा. जीवन में यही विवेक जीव और जगत दोनों को भ्रम से मुक्त कर सकता है.
कबीर में भक्त बोध से ज्यादा, जीव बोध सशक्त है. जीव ही वो ‘श्रोता’ है जिसे कबीर संबोधित करते हैं. कबीर जिस आत्मबोध की जरुरत को बारम्बार रेखांकित करते हैं वो ‘आतमबोध’ असल में जीव-बोध ही है. जिसके माध्यम से ‘ग्यान’ पाया जा सकता है. या कहें कि जिसे कबीर ज्ञान कहते और मानते हैं, वो असल में ‘जीव’ का आत्म-बोध’ ही है. और जिसने अपने को पहचान लिया. जिसने अपने को पा लिया, वही बचा. उसी को राम मिला बाकी सब बीच दरिया में ही डूब गए. इसीलिए कबीर सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगत व्यवहारों, अंध-दृष्टियों, भेद्ग्रस्त-संस्थाओं और मृत विचारों को ‘आत्मबोध’ के लिए संकट के रूप में देखते हैं. उन्हें अपने कथ्य , यानी ‘जीव’ की मूल समस्या मानते हैं.
अक्सर यह कहा जाता है कि कबीर अपने ‘आराध्य’ को विभिन्न नामों से पुकारते हैं. लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं. क्या सिर्फ इसलिय कि वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्या इसलिए नहीं कि वो असल में ‘जीव’ की एकता में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर से ज्यादा उसके अलग-अलग नामों से बंध गया है. और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है. कबीर कहते हैं, ““खाक एक सूरत बहुतेरी” यही वो जीव है जो असल में तो एक माटी से बना है लेकिन भ्रम के चलते अलग-अलग रूपों के साथ बंध गया है. क्या इसे ‘समन्वय’ की वही चेतना और दृष्टि नहीं कहा जाना चाहिए, जिसका उल्लेख प्राय: तुलसीदास के सन्दर्भ में किया जाता है. कबीर अपने ‘आराध्य’ को सिर्फ विभिन्न संप्रदायों के तथाकथित समन्वय तक ही सीमित नहीं रखते, अपितु विभिन्न धर्मों और उससे भी परे तक लेकर चले जाते हैं और आचरण की भिन्नताओं से बिखरे ‘जीवों’ की मूल ‘एकता’ को रेखांकित करने का समन्वयकारी काम करते हैं. कबीर की ही पंक्ति है, “ऐसे हम लोक बेद के बिछुरे, सुनिहि मांहि समांबहिगे”. कबीर की कविता क्या इसी कारण एक विराट ‘श्रोता-वर्ग’ तक नहीं पहुंची है. यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक-धार्मिक और भाषिक समाजों में कबीर की ‘जीवित’ उपस्थिति निर्मित हुई.
इसी कारण कबीर जीव के लिए किसी भी आचार-विचार अथवा पद्धति को अपनाने भर को महत्वपूर्ण नहीं मानते. एक तरह से वे इन सभी को अनावश्यक ही मानते हैं. फिर ऐसे में कबीर ब्रह्म और जगत को पाने का क्या रास्ता अपने श्रोता के लिए प्रस्तावित करते हैं. कबीर का एक पद है, जिसमें दो स्त्रियों के बीच, इस संवाद को रचा गया है, “परौसनि मांगे कंत हमारा/ पीव क्यूँ बौरी मिलहि उधारा” मुक्ति और मोक्ष का आकांक्षी जीव जिसे पूजता आ रहा है, असल में वो उसका है ही नहीं. ये वैसा ही है जैसे कोई स्त्री बिना पति के ही सुहागिनी का भेष धरे भ्रम का शिकार बनी रहे. या फिर पड़ोसिन के पति को ही अपना भी पति मानकर श्रृंगार करने लगे. लेकिन इससे वो स्त्री अपने ‘पुरुष’ को तो नहीं पा सकती. जीवन भर इसी भ्रम में बनी रहकर वो अपने हीरा-जीवन को नष्ट कर बैठेगी. इस उदहारण को सामाजिक-जीवन की वास्तविकता के साथ रखकर देखिये, तो कबीर जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध को स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की ‘निजता’ दे देते हैं. जीव को अपना ब्रह्म स्वयं अर्जित करना होता है, इसके आलावा और कोई रास्ता जीव के पास नहीं है. जैसे पति आपस में ‘उधार’ नहीं लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही अपना ब्रह्म भी ‘उधारी’ का नहीं हो सकता है. कबीर की कविता सामाजिक-धार्मिक संबंधों में जीव के आत्म और स्व की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करती है. बिना अर्जन के ज्ञान, कर्म और ब्रह्म सभी निरर्थक हैं. गुड्डा-गुडिया के खेल से ज्यादा उनकी अहमियत नहीं है. कोई स्थायित्व नहीं है.
कबीर कहते हैं, “जिहि मिटिया क घर मंह बैठे, तामंह सिस्ट समानी”. जीव जिस शरीर को धारण किये हुए है, उसके बगैर जीव के पास और कोई रास्ता नहीं है इस जगत और इस जगत के कर्ता को पाने का. कबीर जीव और जगत दोनों के भौतिक अस्तित्व को न केवल स्वीकार करते हैं, अपितु उसे ही वो ‘साधन’ मानते हैं, जिससे ब्रह्म को पाया जा सकता है. कबीर का एक पद है, “साधो, सहजै काया सोधो./ जैसे बट का बीज ताहि में पत्र-फूल-फल-छाया./ काया मद्धे बीज बिराजे, बीजा मद्धे काया.”
कबीर के समय में व्यक्ति के ‘समाज-धार्मिक’ सन्दर्भ परिभाषित हैं. न केवल परिभाषित, स्वीकृत और स्थापित भी हैं. ऐसे में ‘व्यक्ति’ का जो सम्बन्ध अपने इन समाजधार्मिक सन्दर्भों और संस्थाओं से बनता है, उसमें ‘आत्मबोध’ की रचना-प्रक्रिया गायब है. इसीलिए अपने सामाजिक परिवेश को एक ऐसी ‘कोख’ के रूप में देखते हैं जो ‘जन्म से अंधों’ को जन्मता है. आत्मबोध-रहित व्यक्ति ‘सर्वनाम’ रह जाता है और संस्थाएं ‘संज्ञा’ की जगह ले लेती हैं. ऐसे में सर्वनाम या फिर कहें सर्वनामों में बदल चुकी मानवीय ‘काया’ को ‘बीज’ के बोध से ही नई भूमिका और स्वप्न के साथ जोड़ा जा सकता है. संस्थाएं, जोकि व्यक्ति को अपदस्थ कर ‘केंद्र’ बन बैठी हैं, उनके प्रति नई दृष्टि भी तभी जन्म सकती है जब व्यक्ति का ‘स्वत्व’ सकर्मक हो. रचनाशील हो. कबीर का उपरोक्त पद ‘जीव’ में निहित संभावनाओं को उजागर करता है. जैसे पेड़ के बीज में ही उसके पत्ते, फूल, फल और वो छाया निहित रहती है, जो सिर्फ पेड़ को नहीं अपितु ‘अन्य’ को भी जीवन और सुकून देने का काम करती है, ठीक वैसे ही कबीर जीव को भी देखते हैं और उससे भी जीवन और जीवन को सुकून देने वाले तत्वों के सृजन की उम्मीद करते हैं.
जिस सामाजिक-धार्मिक परिवेश ने व्यक्ति को भयभीत, निर्बल, अँधा और इतना छिछला बना दिया है कि वो न तो सत्य को खुद पाना चाहता है, और न किसी से अपने विपरीत कुछ सुनना ही चाहता है, उस व्यक्ति की मुक्ति तब तक संभव ही नहीं जब तक उसके ‘परिवेश’ का विखंडन नहीं होता. कबीर की कविता जीव की इसी मुक्ति के स्वप्न को लेकर अपने सामाजिक-धार्मिक परिवेश का एक विखंडन रचती है. साथ ही अपने श्रोता जीव को, उसकी आत्मिक सर्जनात्मक शक्ति के हवाले ,नए मानवीय सामाजिक और धार्मिक परिवेश के निर्माण की दिशा देने का काम करती है. एक ऐसा परिवेश, जिसमें “ साहेब सेवक एक संग, खेलैं सदा बसंत”. एक ऐसा परिवेश जिसमें ‘संस्थाएं’ व्यक्ति के लिए “नांव अभैपददाता” का महत्त्व और आदर्श रखती हों.
***
असल में समाज की लालसा कबीर में अप्रतिम है. वही मूल है. साहित्य ही नहीं अपितु मध्यकालीन जीवनबोध के ‘भाववादी- दार्शनिक’ पैटर्न को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाये, तो साफ़-साफ़ दीखता है कि कबीर की कविता असल में व्यक्ति के समाज-सन्दर्भ की मारक कथा को गाती है. पूरी बेचैनी और व्यग्रता के साथ. सामाजिक जीवन, जिसे व्यक्ति अपने-अपने स्तर और बूते पर जीता है, उस जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों को कबीर की कविता दर्ज करती है. कबीर की कविता में जहाँ एक ओर ‘स्त्री’ का व्यक्ति-वृत्त लगातार चलता है, वहीँ किसान, सौदागर, कारीगर और कोरी-जुलाहा जैसे अन्य जातिजन्य अवमाननाओं के जीवित ‘व्यक्ति-वृत्त’ भी सहज ही दिखलाई पड़ते चलते हैं. लेकिन इन्हीं के साथ एक और ‘आवाज’ है जो लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ सुनायी पड़ती है, और वो आवाज है खुद उस कबीर की जो ‘देह धरे के दुःख’ ठोस और वास्तविक शक्लों में देखता और झेलता है. कबीर कहते हैं कि देह के दुःख सभी को सहने पड़ते हैं. लेकिन देह के दुःख क्यों सहने होते हैं? कबीर की पंक्ति है,- “देह धरे का दंड है, सब काहू को होय”. क्या जीवन के इस ‘दंड’ और दुःख का कारण सिर्फ “दार्शनिक-ज्ञान” है. या फिर इसके कारण समाज और उसके सन्दर्भों में भी निहित हैं. जो दुःख-दंड की पीडाओं को व्यक्ति की ‘जीवन-स्थिति’ बना देते हैं. और व्यक्ति के जीवन से सुख गायब सा हो जाता है. “बासरि सुख ना रैणि सुख , ना सुख सुपिनै माहि” ये स्थिति, सिर्फ स्थित नहीं अपितु एक व्यक्ति की ठोस और वास्तविक ‘जीवन-स्थिति’, किसी दार्शनिक अनुभूति से जन्म नहीं ले सकती. पहले उसे सामाजिक दृश्य होना होगा.
उदहारणस्वरुप कबीर की कविता में अपने पुरुष से विलग एक स्त्री बार-बार आती हैं. जो अपने पुरुष को वापस पाने के लिए तड़प रही है. ये वो पुरुष है जिसके बगैर उस स्त्री का ‘परिवार’ नहीं बस सकता. उसको अपना ‘घर’ नहीं मिल सकता. ये वही स्त्री है जिसके बारे मैं खुद कबीर कहते हैं, “ भई सब कौ हम भारी/ गवन कराय पिया लै चाले, इत उत बाट निहारी/ छूटत गाँव नगर से नाता, छूटै महल अटारी”, वही स्त्री जिसे “घरवां से देत निकारी”, वही स्त्री जो एक बार गौना हो जाने पर फिर जीवन में शायद ही वापस ‘मायके लौट पाती है. अब सोचिये कि इस स्त्री का जीवन और जगत उसके ‘पिया’ और पति के आलावा क्या होगा. उसे हर हाल में पति को पाना ही होगा. वही उसका ठिकाना है. कबीर ब्रह्म से बिछुड़े हुए, जीव को जब कविता में देखते हैं तो जो दिखाई पड़ता है वो ‘स्त्री’ है. संभवत: यही कारण है कि कबीर की कविता में स्त्री का वृत्त बारम्बार उभरता है. कबीर का समाज इस तरह के दृश्यों से भरा हुआ समाज रहा है. इसकी गवाही खुद कबीर की कविता देती है. जाति, धर्म और परिवार की संस्थाओं ने देह के दुःख रचे हैं उनका ‘पाठ’ दर्शन की दृष्टि से नहीं किया जा सकता. लेकिन इन्हीं ने व्यक्ति के वास्तविक जीवन को ‘विकट’ स्थिति में बदल दिया है. अत: जो पीड़ा और बेचैनी देह में बस गयी है उससे मुक्ति के स्वप्न ‘स्वप्निल’ कल्पनाओं में बदल जाते हैं.
अपने सामाजिक-धार्मिक परिवेश के सन्दर्भ में इन ‘स्वप्निल’ कल्पनाओं और स्वप्नों का रेखांकन ही कबीर को एक स्वप्नद्रष्टा कवि बनता है. कबीर के बारे में प्राय: ये कहा जाता रहा है, कि उनके पास वैसा कोई सामाजिक स्वप्न नहीं रहा, जैसा कि तुलसीदास के यहाँ है. ये बात सच है कि तुलसी के राम-राज्य जैसा स्पष्ट स्वप्न कबीर नहीं रचते हैं. लेकिन सच तो यह भी है कि कबीर तुलसी जैसे राम को भी नहीं रचते. तुलसीदास का ‘स्वप्न’ बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या उसे इतना बड़ा भी बना देना चाहिए था, कि समाज के अन्य स्वप्न सुनायी-दिखाई ही न दें.
इस आलेख की शुरुआत में ही यह रेखांकित किया गया कि कबीर एक स्वप्नदृष्टा कवि थे, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ‘समाज’ जिस रूप में मिला था , उसमें ‘स्वप्न’ ही वो जगह हो सकते थे, जहाँ जीवन के लिए ‘जीवित’ को पाया जा सकता था. अन्यथा, जो था वो तो इतना असहनीय और मारक था कि उसे सहना संभव नहीं. कबीर का ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, पूजा-पाठ को लेकर, मुक्ति और मोक्ष को लेकर अर्थात समूची धार्मिकता की भाव संस्था को लेकर एक भिन्न दृष्टि मिलती है. इसके तमाम कारण हो सकते है, लेकिन एक कारण तो ये भी रहा ही है, कि धार्मिक-संस्था अपने प्रचलित और सार्वजनिक रूप में जो भी थी वो कबीर को अनुपलब्ध जरूर थी. कबीर के धार्मिक परिवेश ने उन्हें केवल धार्मिक तौर पर ही “अयोग्य’ परिभाषित नहीं किया था अपितु सामाजिक और मानवीय तौर पर भी ‘छूत’ परिभाषित किया था. जाति-वर्ण-लिंग और प्रभुता की संस्थाओं से ग्रसित अपने सामाजिक-धार्मिक जीवन में ‘रूप’ की ‘अनुपस्थिति’ कबीर के लिए न केवल धार्मिक-आध्यात्मिक सच्चाई है, अपितु असल में तो वो सामाजिक-सांस्कृतिक सच्चाई है. क्या ये कहने की आवश्यकता है कि ‘जिन्हें’ सामाजिक जीवन में ‘समाज’ अपनी रूपात्मक और संस्थागत शक्ल में सहज हासिल नहीं होता, उनकी दृष्टि में जो क्षुब्धता समाज की रूपात्मक संरचना और संस्थानिक ढांचे के प्रति आ जाती है, वो अपने में स्वप्न-धर्मी होती है. कबीर की कविता को देखने समझने की एक कोशिश इस रास्ते भी जरूर की जा सकती है, की जानी चाहिए.
अब भी क्या कोई स्वप्न सचमुच में कबीर के यहाँ नहीं है. कबीर की कविता का सबसे बड़ा स्वप्न ‘आत्मचेतस’ जीव है. एक ऐसा जीव जो अपने ‘स्वत्व’ को अपने अनुभव से रचने का काम करे. स्थापित संस्थाओं ,विचारों और आचरणों के भेदवाद से मुक्त एक ऐसा ‘रागी’ जीव जो धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, धन-प्रतिष्ठा और ऊंच-नीच के भेदों से मुक्त परिवेश का रचनाकार हो. कबीर एक ऐसे ‘रचनाशील’ जीव का स्वप्न अपनी कविता में रचते हैं जो वर्तमान सामाजिक-धार्मिक संस्थागत परिवेश और व्यक्ति के बीच पैदा हो गयी ‘माया-पूर्ण’ खाई को पाट सके. क्योंकि जो विद्यमान है वो खुद कबीर ही नहीं अपितु समाज के बहुसंख्यक के लिए ‘मारक’ और ‘दंड-रूप’ है. सक्षेप में, कबीर की कविता जीव,ब्रह्म और जगत के दार्शनिक ढांचे में अपने समय के व्यक्ति, समाज और उनके बीच उपस्थित हो गए मारक संबंधों को पूरी बेचैनी के साथ स्वप्निल कल्पनाओं के साथ रचने का काम करती है.
*सभी काव्य पंक्तियाँ हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वरा संकलित ‘ कबीर’ नामक पुस्तक एवं हिंदी के जनपद संत’ जो कि शोभी राम संत साहित्य शोध-संसथान द्वारा सम्पादित है. से लिए गए हैं.
*हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी
* हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल