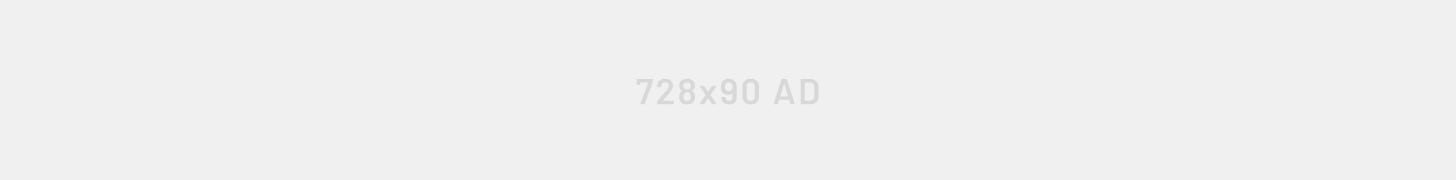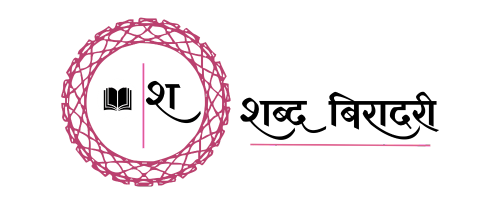राँची
दिनांक : 21.07.2025
महाजनी असभ्यता की क्रूरता
कुछ बातें तत्काल दर्ज नहीं कर पाता हूँ. और बातें हैं कि फांस की तरह अटकीं रहती हैं. हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले बाजार जाना हुआ. मेरा स्वभाव है कि छोटे दुकानदारों से सौदा लेना पसंद करता हूँ. दो-चार बातें हो जातीं हैं. कुछ नए अनुभव लेकर लौटता हूँ. कभी खुशियाँ मिल जाती हैं तो कभी मन थोड़ा दुखी हो जाता है. बाजार में केवल सामान ही नहीं मिलते ज्ञान भी मिलता है. मैं वैसी चीजें खरीदता हूँ जिनका कोई खरीदार नहीं होता. अकसर महिलाएं सब्जियां बेचती हैं. पुरुष भी होते हैं. कभी-कभी पति-पत्नी दोनों. महिलाओं से सब्जी खरीदने पर मेरी पत्नी चिढ़ती हैं. मालूम नहीं,उन्हें क्यों चिढ़ है. मैं उन सब्जी -विक्रेताओं से घर का, उनके बाल-बच्चों का हाल-चाल भी पूछ लेता हूँ. इसमें पैसे तो लगते नहीं हैं. उनके संघर्ष और कामयाबी दोनों का पता चल जाता है. बहरहाल,सब्जियाँ बेचने वाली सड़क किनारे कतार में बैठी हुई थीं. मैं सड़क के दूसरे किनारे स्कूटी लगाकर खड़ा था. पत्नी कुछ अन्य खरीदारी में व्यस्त थीं. इस बीच एक आदमी आया जिसके हाथ में एक रजिस्टर था. वह थोड़ी देर तक उस महिला के पास खड़ा रहा. इस बीच उस महिला ने गला (बटुए) से दो सौ रुपये निकल कर दिया. वह आदमी चलता बना. मेरी उत्सुकता बढ़ गयी. एक समय में सहारा वाले ऐसे ही छोटे-छोटे दुकानदारों से प्रतिदिन वसूली करते थे और उन्हें आश्वस्त करते थे कि उन्हें एकमुश्त मोटी रकम मिलेगी. इसका क्या हश्र हुआ,सब जानते हैं. बहरहाल,यह सहारा समय नहीं बेसहारा समय है. दरअसल ,वह आदमी किसी महाजन का मुंशी था. मैंने इस बाबत उस महिला से पूछा. जो जानकारी मिली ,वह व्यथित करने वाली थी. उस महिला ने अपने बच्चे के एक निजी स्कूल में नामांकन के लिए तीस प्रतिशत मासिक ब्याज पर बीस हजार रुपये का कर्ज लिया था. उसके एवज में वह प्रतिदिन दो सौ रुपये अर्थात माह में छः हजार रुपये का सूद देती थी. मेरा हृदय विदीर्ण हो गया.
एक शब्द हम लोग सुनते आयें हैं-महाजनी सभ्यता. मालूम नहीं इस असभ्यता या क्रूरता को किसने सभ्यता बना दिया. मुझे लगता है श्रेष्ठ शब्द भी तद्भव रूप में सेठ हो गया. इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि जो सेठ अर्थात पूँजीपति है वही श्रेष्ठ है. एक हद तक समाज में यह मान्य हो चुका है कि जो धनवान है,वही गुणवान है,कुलीन है और महान भी. दुर्भाग्य यह है कि इस देश में कलंकित महाजनी प्रथा का अब भी अंत नहीं हुआ है. कुछ कम हुआ है. अशिक्षा के कारण ऐसी स्थिति है. मेरे यहाँ एक कहावत है कि बिना घेंट काटे या पेट काटे धन नहीं होता. ये महाजन गरीबों का ऐसे ही घेंट अर्थात गला काट कर और धनवान बनते हैं. कोई तेज-तर्रार आदमी उस महिला को दोषी बतला सकता है. परन्तु उस माँ को मैं कैसे दोषी मानूँ जो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है. मैं जब भी किसी माँ को उसके बच्चे के साथ स्कूल पहुंचाते या बारिश अथवा धूप से बचाते हुए देखता हूँ, श्रद्धा से भर उठता हूँ. ऐसे दृश्य दुनिया के सबसे मनोहर और सुन्दर दृश्य हैं और सुन्दर दुनिया के सपनों की तस्वीर भी हैं. मैं उस वाकया को भूल नहीं पाता और सोचता हूँ कि इस क्रूरता का कब अंत होगा.
————–
दिनांक:22.07.2025 श्रेष्ठता साबित करने के लिए नीचता पर उतरते लोग
हम सब गौर कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से घर,समाज,प्रान्त,देश,विश्व, राजनीति और यहाँ तक कि कला-साहित्य में भी आक्रामकता बढ़ी है. हम मोटे तौर पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुप हो जाते हैं. हालांकि इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है,फिर भी इस पर सूक्ष्मता से विचार आवश्यक है. यह देखना आवश्यक है कि आक्रामक कौन है. उसके कारण क्या हैं. उसका लक्ष्य क्या है. उसका उद्देश्य क्या है और उसके परिणाम क्या हैं. इतनी बातें विस्तार से पता हो तो ऐसे तत्वों या व्यक्तियों से हम थोड़ी निजात पा सकते हैं. जैसे बम निरोधक दस्ता द्वारा बम को डिफ्यूज कर देने से हमें शान्ति मिलती है. आक्रामक वह है जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है. इस तरह वह पहले से ही स्वयं से पराजित है. पराजित व्यक्ति अपने संतोष के लिए बार-बार आक्रोश प्रकट करता है. दुःख की बात यह है कि हर आक्रोश में वह स्वयं से हारता है. इस तरह आक्रोश, गुस्सा प्रकट करना और क्रोधित होना उसका स्वभाव बन जाता है. उसमें एक घातक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे व्यक्ति किसी के लिए अहितकर होते हैं. वे घर तोड़ेंगे,समाज में अव्यवस्था फैलायेंगे,क्षेत्रीयता का मुद्दा उछालेंगे अर्थात वैसे सारे नकारात्मक काम में संलिप्त हो जायेंगे जिससे नुकसान ही नुकसान होगा. ये किस अनुपात में क्षति पहुँचायेंगे, यह उनकी प्रवृत्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है. दरअसल कुछ हद तक ऐसे लोग विफलताबोध से ग्रस्त होते हैं. गौर करने लायक है कि हीनता बोध से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं का नुकसान करता है जबकि विफलता बोध से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं की श्रेष्ठता निरूपित करने के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है. ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे अलग होना श्रेयस्कर है. यदि ऐसा संभव नहीं हो तो एक न्यूनतम दूरी बनाना ही इसका समाधान होगा. तथापि,ऐसे लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आयेंगे. ऐसे लोग घर-बाहर हर जगह मौजूद हैं. अंग्रेजी में ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहा जाता है. ये पीड़क हैं. पीड़ा पहुंचाना इनका गुण-धर्म है.
————–
दिनांक:23 जुलाई 2025
कहाँ गए वे लोकगीतों वाले दिन
कभी-कभी मेरे मन में एक दृश्य उतरता है. दृश्य-घनघोर बारिश का. चारों तरफ पानी ही पानी. मैं अकेले किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ और कोई पद सुन रहा हूँ-कोई सूफी-संगीत. मुझे आश्चर्य होता है कि जब-तब मैं इस दृश्य की कल्पना में डूब जाता हूँ. इसका रहस्य मुझे स्वयं नहीं मालूम. क्या ऐसा इसलिए होता है कि शर्मा जी मुझे बचपन में पद सुनाते थे. वे संगीतज्ञ नहीं थे लेकिन उनकी टेर में एक जादू था. बाद में जब होश संभाला तो कभी-कभार कीर्तन या लड़कियों के विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों को सुनकर विभोर हो जाया करता था. आज भी जब बेटी की विदाई या सिंदूरदान के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों को सुनता हूँ तो मेरी आँखें नम हो जाती हैं. स्त्रियाँ जब देर रात इन गीतों को गाती हैं और उन्हें सुनते हुए मैं वह दृश्य विजुअलाइज करने लगता हूँ. ध्वनि दृश्य उत्पन्न कर सकते हैं. भले ही यह बात विज्ञान की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती हो लेकिन भावनाओं और संवेदनाओं के तल पर मूर्त रूप ले लेती हैं.
मूल बात की ओर लौटता हूँ. तब आकाशवाणी के सुनहरे दिन थे- अस्सी का दशक .लगभग तब तक मोटे तौर पर रेडियो भी स्टेटस सिम्बल हुआ करता था .गाँव में मुश्किल से एक या दो आदमी के पास होता था. वर्ष 1984 में मेरे घर में दहेज़ के रूप में ही सही,पत्नी के साथ पांच बैटरी वाला रेडियो एक सिको घड़ी के साथ आया. मैं कभी-कभी बहुत तेज आवाज में उसे बजाया करता था. शायद बाल-बुद्धि के कारण लोगों को दिखाता था कि देखो,मेरे पास रेडियो है. घड़ी तो गेंहू के खेत में सिंचाई करने के दौरान पानी में इस तरह भीग गया कि उसने सांस लेना ही बंद कर दिया. बेचारा रेडियो कभी रसद मिलती तो बजता अन्यथा कोने में गुमसुम पड़ा रहता. लेकिन जब भी वह बजता मैं उसे छाती पर रखकर सुनता रहता. कुछ निर्धारित कार्यक्रमों को तो मैं कभी नहीं भूलता. आकाशवाणी पटना के चौपाल,लोकगीत और अनंत कुमार का प्रादेशिक समाचार-वाचन मेरे लिए अविस्मरणीय है. इन प्रस्तोताओं की आवाज में जादू था. विविध भारती और फरमाइशी फ़िल्मी गीत भी ऐसे ही कार्यक्रम थे जो बहुत प्रिय थे पर जिसका जादू सर पर चढ़ कर बोलता था वह था लोकगीत. जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ विंध्यवासिनी देवी, सुदर्शन तिवारी शाहाबादी, संत कुमार सिंह राकेश,मोहिनी देवी आदि के स्वर में लोकगीत प्रसारित होते रहते थे. भोजपुरी,मगही के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओँ के लोकगीत भी प्रसारित होते थे. रेडियो नाटकों का भी मैं मुरीद था. बी बी सी के समाचार तो धर्मराज युधिष्ठिर के शब्द थे.
लोकगीतों के प्रति मेरी दीवानगी दिल में उतरने वाली सरल-सहज भाषा के कारण थी. उसका दूसरा मुख्य कारण इसमें लोक के सुख-दुःख थे, जिन्हें मैं देखा-सुना करता था. यह कहना अधिक सही होगा कि लोक गीत लोक की सबसे विश्वसनीय आवाज है. इसमें कोई मिलावट नहीं है. मैं प्रसारित होने वाले लोकगीतों को कॉपी पर लिख लेता था. कोई पंक्ति यदि छूट जाती थी तो बड़ा पछतावा होता था. लोकगीतों में विषय और शैली की दृष्टि से इतनी विविधता है कि आश्चर्य होता है. जैसे- विभिन्न समयों के लिए अलग-अलग राग- रागिनियाँ हैं ,वैसे ही बारहों महीनों और विभिन्न अवसरों के लोकगीत हैं. सावन में कजरी का आनंद लेते हैं तो आश्विन में देवी गीत. फागुन में फाग गाते हैं तो चैत में चैता. इसमें कोई विचलन मन को नहीं सुहाता और हास्यास्पद लगता है. अपने देश की विविधता में भी विविधता है. इस अर्थ में यह सबसे विलक्षण देश है. हम गाते-गाते रो पड़ते हैं तो फिर आंसू पोंछ कर गाना शुरू कर देते हैं. शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा होता हो. यह उत्सवधर्मिता अन्यत्र आसानी से सुलभ नहीं है. हम उदासी के भी गीत गाते हैं. जागने के लिए प्रभाती तो सोने के लिए दादी,नानी या माँ की मीठी लोरी है. हमारे यहाँ सुख और दुःख दोनों के गीत हैं.
किशोरावस्था में जब लोग फिल्मों के दीवाने होते हैं मुझे फ़िल्मी गीत बहुत पसंद नहीं आते थे. वर्तमान परिवेश में यदि किसी युवक को किसी लोकगीत का मुखड़ा सुनाने के लिए कहा जाए तो न केवल वह चुप रहेगा अपितु प्रश्नकर्ता पर भड़क भी सकता है. उसके लिए लोकगीत पिछड़ेपन का प्रतीक है. ग्रामीण परिवेश लोकगीतों की जन्मभूमि है. वे यहीं जन्म लेते हैं और ग्राम्य कंठ ही इनका पालन-पोषण करते हैं. शहर की मिट्टी इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं है. बहरहाल,आज भी यदि दो अलग-अलग महफ़िल सजाये जाएँ तो मैं फ़िल्मी गीतों को छोड़ कर लोकगीतों की महफ़िल में रात भर बैठना पसंद करूँगा. मेरे लिए इसकी दीवानगी का मुख्य कारण यह है कि यह मेरे दिल के तारों को छेड़ देता है. मैं इसके नशे में डूब जाता हूँ. मैं भिखारी ठाकुर और महिन्दर मिसिर को भूल नहीं पाता. इनके जीवन पर लिखे संजीव के उपन्यासों को मैंने मनोयोग से पढ़ा है. आज भी इनके रचित गीतों को ढूंढ-ढूंढ कर पढ़ता हूँ. कुछ लोग भोजपुरी गायक बलेसर के गीतों पर अश्लीलता का आरोप लगते हैं लेकिन मैं उन्हें घंटों सुनना पसंद करूंगा. वे तत्कालीन भोजपुरी समाज के प्रतिनिधि गायक थे. सवाल यह है कि आप चीजों को ग्रहण किस भाव से करते हैं. जजमेंटल बने से कोई सच्चा आलोचक नहीं हो सकता. आलोचना के लिए नीर-क्षीर दृष्टि अपेक्षित होती है.
मिलावट के इस बुरे दौर में लोकगीतों के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है. हम अपनी विरासत को संभालने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं. भाषणों में विरासत की चर्चा अच्छी लगती है लेकिन सरकार के स्तर पर ऐसा क्या किया जा रहा है जिसे उल्लेखनीय कहा जा सके. माना कि समय बदला और हमें जमाने के साथ चलना चाहिए लेकिन इसका क्या मतलब कि बूढ़े बाप पीछे छूट जाये और हम बेटों के साथ दौड़ने लगें. एक संतुलन तो बिठाना ही चाहिए. इनका संरक्षण होना चाहिए. और होना चाहिए नयी प्रतिभाओं का स्वागत और प्रोत्साहन भी. आज, मैथिली ठाकुर जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने बल-बूते एक शानदार मुकाम पर पहुँची है. तब कहीं जाकर उन्हें आमंत्रित कर सम्मानित किया जा रहा है. सवाल उठता है कि हमारी व्यवस्था ने कितने मैथिली ठाकुर, संजोली पाण्डेय,चन्दन तिवारी आदि के निर्माण के लिए कौन सा ठोस प्रयास किया. जो बने अपने संघर्ष के बल पर कामयाब हुए. लोक ने उन्हें प्यार-दुलार दिया. तब जाकर कहीं उनकी आवाज दिल्ली तक पहुँची. यह किसी एक प्रदेश की बात नहीं है. सभी प्रान्तों और उनके विभिन्न इलाकों के अलग-अलग लोकगीत हैं. उनकी एक समृद्ध परम्परा रही है. कोई भी प्रदेश दूसरे से कम नहीं है. हमारे बौदधिक वर्ग के द्वारा भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है. आने वाले समय में शायद ही कोई यकीन करेगा कि इस देश में कोई देवेन्द्र सत्यार्थी भी हुआ था जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन लोकगीतों की खोज में लगा दिया. पुरानी पीढ़ी के साहित्यकार कभी उन्हें याद भी कर लेते हैं तो नए लोगों का उनसे क्या लेना-देना. खैर, सब की अपनी विवशता या कार्य-प्रणाली है. मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमारी विरासत कहीं विलुप्त न हो जाए. और उससे भी बड़ी चिंता उसके मूल स्वरूप को बचाने की होनी चाहिए. इस अर्थ प्रधान युग में अर्थ के लिए शब्दों के साथ भी बहुत अनर्थ हो रहा है. किसी की टोपी किसी के सर पहनाने का कुत्सित खेल चलता रहता है. कला-संस्कृति की दुनिया की पावनता बनी रहनी चाहिए. निजी लाभ के लिए घालमेल नहीं हो यह हमारी चिंताओं में शामिल होना चाहिए.
हमने कभी यह विचार किया ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इसे धरोहर के रूप में हमें सौंपा है. यह उनका गाढ़ी मेहनत से अर्जित धन है. जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी से सुरक्षित रहती आयी है. चूँकि, हम और हमसे भी कहीं अधिक वर्तमान युवा पीढ़ी लापरवाह है जो इसका महत्व नहीं समझ पा रही है. यह लोक की संपत्ति है,पूंजी है. इसकी पहरेदारी लोक को ही करना पड़ेगा. फिल्मों के लिए बोर्ड का गठन हुआ है. लोकगीतों पर कौन ध्यान देगा. इसे हम कला-संस्कृति विभाग के हवाले छोड़ नहीं सकते. हमने कभी देखा या सुना नहीं है कि किसी नौकरशाह ने क्रांति की हो. क्रान्ति से यहाँ अभिप्रेत मिशनरी भाव से युद्ध स्तर पर किसी काम को पूरा करना. यह सही है कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं है. इसके लिए सब को आगे आना होगा. समर्पण और निष्ठा के बल पर ही हम गीतों वाले उन्हीं पुराने दिनों को लौटा सकते हैं. दिन लौटते भी हैं. हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है- क्यों निराश हुआ जाए. हमें भी निराश क्यों होना. दिन लौटते भी हैं.
———-
राँची
04 जनवरी 2025
सत्तू ,मिर्चा और अचार
आमतौर पर यह माना जाता है कि सत्तू गरीब लोगों का आहार है। बिहार में मेहनतकश मजदूरों का यह भोजन है। वे इसलिए भी इसे खाते हैं कि यह बहुत देर से पचता है। एक जमाने में यह सस्ता भी था। सत्तू खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती। मुजफ्फरपुर में मैंने अधिकांश रिक्शा चालकों को सत्तू खाते देखा है। हल,कुदाल चलाने वाले,चइला फाड़ने वाले अर्थात कठोर शारीरिक श्रम करने वाले इसे खाते हैं। भात-रोटी जल्द पचने वाला आहार है। गरीब लोग दिन भर में तीन बार तो खा नहीं सकते। यह कहूं कि बिहार में वैश्वीकरण के पहले नास्ते का कंसेप्ट नहीं था। अब तो बहुत कुछ बदल गया।चना का सत्तू बिहार का फास्ट फ़ूड है। इसमें कोई झंझट नहीं है। यह रेडी टू ड्रिंक है।
मुजफ्फरपुर में जब मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था,यह मेरा मुख्य आहार था। उस समय पांच रुपये में सौ ग्राम सत्तू मिल जाता था।काला नमक, नींबू और जीरा का चूर्ण डालकर कर जब ठेले वाला लंबे शीशे के गिलास में इसे सर्व करता था तो मन तृप्त हो जाता था। खासकर गर्मी के दिनों में जब कड़ाके की धूप पड़ती थी और लू चलती थी तब इसका स्वाद दिव्य हो जाता था। तब मेरी जेब में इतने पैसे तो होते नहीं थे कि होटल में बैठकर स्वादिष्ट महंगा भोजन कर सकूं।
अब भी घर पर कभी-कभार सत्तू खाता हूं। इसे खाते समय दुरबल मांझी और झोंटी राम जरूर याद आते हैं। ये दोनों मजदूर थे जो मेरे प्रिय थे। उनके लिए मन में कितना सम्मान का भाव है कि वे कभी मेरी स्मृतियां से बाहर नहीं जा सकते। वर्षों से सोचता हूं कि दुरबल मांझी को कविता में उतारूं पर असफल हो जाता हूं। जिस दिन मेरे कविता प्रदेश में इनका पदार्पण होगा, मैं अपना श्रम सार्थक मानूंगा। शायद वे गद्य में ही आयेंगे। आते ही उन्हें आपके सामने उपस्थित करूंगा। झोंटी राम भी गजब का मस्तमौला आदमी था। वह कम्युनिस्ट शब्द को नहीं समझता था लेकिन स्वभाव से वामपंथी था। मैं झोंटी राम के साथ अपने गाछी में समानांतर रूप से कुदाल चलाता था। वे जवानी के दिन थे। झोंटी राम थोड़ा शरीर से कमजोर पड़ गया था और थोड़ी देर कुदाल चलाने के बाद सुस्ताने लगता था। ऐसे दरियादिल लोगों को समाज में काम नहीं मिलता था। आरोप यह कि ये लोग कामचोर हैं और अधिक मात्रा में खाते हैं। जब इनके साथ मैं कुदाल चलाता था,खेत में ही चाय पहुंच जाती थी। हमने इनके साथ सदैव सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। इनकी राम कहानी कभी बाद में।
सत्तू की सात्विकता क्या कहूं? मेरे गांव में एक वैष्णव मठ है। ठाकुर जी का भोग लगता है। वहां एक बंगाली महन्त थे। उनके पुत्र अविवाहित थे लेकिन धुर वामपंथी। पूजा-अर्चना नहीं करते थे। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। जिस दिन मठ पर रसोइया नहीं होता था। वे दोपहर में सत्तू खाते थे। सब लोग उन्हें भाई जी कहते थे। इनकी क्रान्तिकारिता के किस्से भी दिलचस्प हैं।
अब यह सब आप सबको सुनाने का मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं केवल एक आदमी नहीं हूं बल्कि कितने आदमी मुझमें जीते हैं। ये सब मेरी दृष्टि में सच्चे नायक हैं। इन नायकों की जीवन- लीला से कतरा भर भी किसी को कुछ मिल सके तो श्रम सार्थक समझूंगा।
———————————————-
ललन चतुर्वेदी (मूल नाम-ललन कुमार चौबे)
मुजफ्फरपुर(बिहार) के पश्चिमी इलाके में
प्रकाशित कृतियाँ : प्रश्नकाल का दौर , बुद्धिजीवी और गधे (दो व्यंग्य संकलन), ईश्वर की डायरी , यह देवताओं का सोने का समय है एवं आवाज घर (तीन कविता संग्रह) तथा साहित्य की स्तरीय पत्रिकाओं तथा प्रतिष्ठित वेब पोर्टलों पर कविताएं एवं व्यंग्य प्रकाशित।
रांची-834003
मोबाइल न. 9431582801
ईमेल: lalancsb@gmail.com