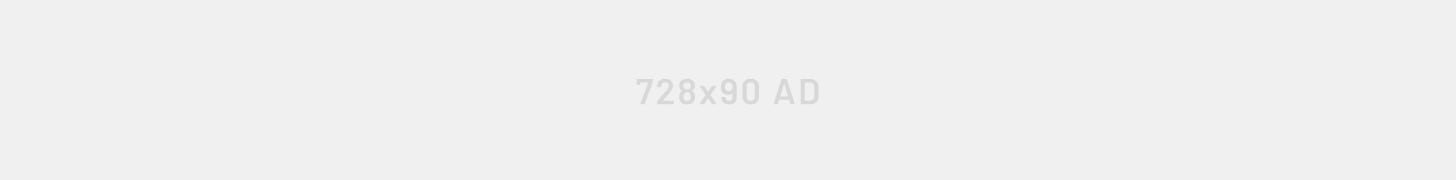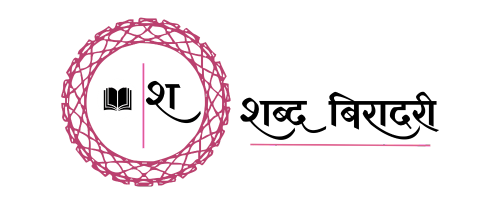सृजन की दुनिया उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी यह दुनिया। मनुष्य जब तक इस सृष्टि में रहेगा, सृजन की दुनिया भी बनी-बनती रहेगी, बसती-उजड़ती रहेगी। सृजन की इस दुनिया का आदि काल से चले आना, इसे इतना महत्वपूर्ण, मार्मिक और दिलचस्प बनाता है, तभी इसको जोखिम ली हुई, लहूलुहान दुनिया भी। बरसों-बरसों से साहित्य और कला का यह व्यापाक संसार, सृष्टि में फैली बुराइयों, हिंसा और अराजकता से संवाद करता आया है, संघर्ष करता आया है। हमारे अपने क्लासिक हों या हमारे देश के बाहर के क्लासिक, हर जगह हमें बुराइयों और अच्छाइयों के बीच सतत चला आ रहा द्वंद्व और संघर्ष दिखता रहा है।
मानवीय संकट, मानवीय पीड़ा का अभिव्यक्त कर रही कृतियाँ भी अंततः आनंद देती रही हैं और सारी दुनिया आनंद और रस के लिए मानवीय क्रीऐशन की तरफ देखती रही है, जो अपने स्वरूप में प्रकृति की तरह भी है और प्रकृति से जुदा भी। सृजन और ध्वंस का एक लंबा सिलसिला जो प्रकृति की अपनी प्रक्रियाओं की ही तरह निरंतर बनता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है।
मुझे कला, साहित्य और सिनेमा से रुचियों के आनंदित होने, आनंद के लिए कला और कविता के पास जाने की बात स्वाभाविक लगती है। इतना जरूर है कि गंभीर साहित्य और सिनेमा, सिर्फ मनोरंजन करने का उद्देश्य लिए हुए ही नहीं रह सकता है। उसे मनोरंजन के परे जाना होता है। मानवीय जीवन के संकटों से जुड़ना होता है। मानवीय मूल्यों के विस्तार में अपनी भूमिका को अदा करना पड़ता है। पर गंभीरता का अतिरेक भी लेखक और पाठक, सिनेमा और दर्शक के रिश्तों को असहज, जटिल बनाता है। मुझे कॉलेज में शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ाने वाले अपने एक अध्यापक की याद आती है। उनकी शेक्सपियर के ‘किंग लियर’ को पढ़ाने के बाद मेरे मन में उनको लेकर यह खयाल उतर करता था कि “He knew everything about Shakespeare except how to enjoy it.” (वे शेक्सपियर के बारे में सब कुछ जानते थे सिवाय इस बात के कि शेक्सपियर को पढ़ने का आनंद कैसे लिया जाये।)
सृजन का यह संसार इतना ज्यादा कल्पनाशील और दिलचस्प हो सकता है कि मशहूर फिल्म निर्देशक चार्ली चैपलिन एक पुलिस, एक पार्क और एक खूबसूरत लड़की को लेकर अपने वक्त की एक कॉमेडी को एक अविस्मरणीय कॉमेडी में जन्म देता है। रुसी लेखक एंटन चेखव एक
कुत्ते के कारण अपने घर के रास्ते को भूल जाते हैं। एक कसबाती इलाके में भटक जाने को लेकर एक आसाधारण कालजयी कहानी की रचना कर पाते हैं। चेखव से चैपलिन तक और इनके आगे भी हमारे लिए दिलचस्प संसार बनता रहा है, बनता रहेगा।
सृजन का यह संसार इतना ज्यादा बहुआयामी और बहुपरतीय हो ही नहीं सकता था, अगर वह सिर्फ और सिर्फ दिलचस्प होने तक खुद को सीमित कर लेता, किसी एक बिंदु, किसी एक मंजिल पर रुकने को अपनी नियति मान लेता। शायद इसलिए भी मशहूर चित्रकार पिकासो कह रहे हैं कि “ईश्वर भी एक दूसरा कलाकार ही होगा, जिसकी अपनी कोई निश्चित और निर्धारित बंधी-बधायी जड़-सी शैली नहीं है।” वह निरंतर कोशिश करता रहता है। कभी अपनी शैली को पाने में सफल हो जाता है और कभी असफल भी। यही है कि कभी वह बिल्ली को रचता है, कभी जिराफ को। कभी उसके हाथों अमलतास का पेड़ खड़ा होता है और कभी चीड़ का। एक दूसरे विचारक हेनरी मतीस कह भी गए हैं- “कलाकार को अपनी खुद की किसी भी छवि का शिकार नहीं होना चाहिए।”
यह लगातार, बार-बार कुछ अलग-सा, नया-सा, अप्रत्याशित-सा खोजने, अभिव्यक्त किए जाने की जरूरत और लालसा कलाकार को थका देती है, लहूलुहान कर जाती है। एक कलाकार के भाग्य में समय काटने की सुविधा उपलब्ध ही नहीं होती है। एक लेखक का पेशा भी, किसी पुरोहित, पुजारी की तरह ही होता है, जिसे चौबीस में से सोलह घंटे तक, रोज ही लगातार नियमित रूप से अपना काम करना पड़ता है। फिर सृष्टि, संसार और साहित्य के तथ्यों को पढ़ना और समझना एक मुश्किल काम ही हो सकता है।
आज तक, किसी भी देशकाल में इस बात को अच्छी तरह देखा जा सकता है कि मनुष्य की धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और वर्ग से खड़ी होती हुई अस्तित्व भले ही बिसरा दी जाये, मनुष्य की सांस्कृतिक अस्तित्व उसके जाने के बाद भी समाज की स्मृति में बनी-बसी रहती है। हमें शेक्सपियर और कालिदास का, उनके लिखे गये का पता जरूर रहता है, लेकिन उनके समय के प्रशासकों, सेनापतियों और राजघरानों की मामूली सी जानकारियों का पता नहीं रहता है।
सृजन के संसार के जोखिम, चुनौतियों और परिणामों के बारे में खोजते हुए, हमारे पुराने लेखकों का इस बात पर ध्यान जाता है कि लेखक, कवि और कलाकार का पेशा एक अंधे आदमी का पेशा भी रहता है, जो अपने देखे हुए को नहीं, अपने महसूस किये जाने को व्यक्त कर सकता
है। गहरी अनुभूतियों, भावनाओं और संवेदनाओं की मानवीय दुनिया को व्यक्त किया जाना । किसी ने कहा भी है कि सच्चे लेखक दोस्तोएव्स्की विचारों, भावनाओं को कुछ उसी तरह महसूस करते रहे, व्यक्त करते रहे, जैसे कोई आदमी ठंड, गर्मी या दर्द को महसूस करता है, व्यक्त करता है।
इसलिए कहा जाता रहा है कि एक कवि इतने गहरे स्तर पर हमारे इस संसार, हमारी इस सृष्टि को महसूस करता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है और फिर भी वह कुछ कहकर निकल जाता है। कविता और कवि की दुनिया का यह रहस्य भी है कि अंग्रेजी कवि-आलोचक टी. एस. एलियट कह रहे हैं कि एक सच्ची कविता खुद को अपने समझे जाने के पहले ही संप्रेषित कर सकती है।
कविता का समझ में आने के पहले ही संप्रेषित हो जाने का यह विचार कितना जादुई, रहस्यमय नजर आता है। पर अब तक हम सृजन के संसार में ऐेसे-ऐसे चमकदार और वरदानी से एक अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि सृजन की इस अलौकिक दुनिया से जादुई दुनिया और कहीं बसती होगी।
इतना जरूरी है कि यह सब जिन कलाकृतियों के बारे में कहा जा रहा है, वे कलाकृतियाँ आंतरिक जरूरतों से जन्म लेती हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ के संवादों से बाहर आती हैं। इनके रचनाकार यह जानते हुए भी सवाल करते रहते हैं कि कुछ सवाल हमेशा से अनुत्तरित रहे हैं। जहां सवाल का उत्तर एक दूसरा सवाल ही रहता आया है। इन रचनाकारों ने उत्तर पाने की हड़बड़ी में सवाल की गंभीरता और मर्यादा का ध्यान रखना नहीं छोड़ा है। इनके लिए ही कभी जर्मनी के दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने कहा होगा कि आदमी अपनी उत्तर देने की क्षमता से उतना नहीं, जितना सवाल खड़ा करने की क्षमता से जाना-पहचाना जाता रहा है।
हिंदी भाषा ने भी खड़ी बोली के अपने साहित्य की बहुत कम उम्र में ही हमें कुछ ऐसे लेखक और कवि मिलें हैं, जिन्होंने निरंतर अपने समय, समाज और संरचना के सामने अपने सृजन के माध्यम से, सवालों और चुनौतियों को खड़ा किया है। इन लेखकों और कवियों में मगर हम मनुष्य के नैतिक आयामों के लिए चिंताओं को देखते हैं। तब मनुष्य के सौंदर्यात्मक आयामों के प्रति इनके सरोकारों को भी। इन लेखकों और कवियों ने सृजन को एक सक्रिय, नैतिक,
जिम्मेदार और मानवीय प्रक्रिया में परिवर्तित किया है। किसी भी अच्छे और सच्चे लेखक के लिए सृजन, जोखिम और जिम्मेदारी लिया हुआ, गंभीर और ईमानदार कर्म ही सकता है।
हमारी भाषा के साहित्य में ऐसे लेखकों और कवियों की कमी नहीं है, जिन्होंने भाषा के प्रति अपने अनुराग, लगाव और चरित्र को लगातार माँजने का भरसक प्रयत्न किया है। वे जानते रहे हैं कि बिना अपनी और अच्छी भाषा के अच्छा सृजन संभव नहीं हो सकता है। एक लेखक सबकुछ होने के पहले अपनी भाषा से लगाव लिया हुआ, अपनी भाषा का गहरा आदर और अनुराग लिया हुआ व्यक्ति ही हो सकता है।
हम जानते आये हैं कि लिखने के क्षण, खुद को किसी एक और एकमात्र बिंदु पर केंद्रित करने के क्षण होते हैं। भाषा की संभावनाओं और सीमाओं को जानने- पहचानने के क्षण। अपने एकांत को पाने और बनाए रखने के क्षण। पर भाषा, जो हमारे औजार की तरह कार्य करती है, वह सार्वजनिक इलाके से सामान्य जीवन और जनों के बीच से आती है। इस भाषा का उपयोग अत्यंत अनर्गल, अश्लील और अराजक ढंग से भी होता रहता है। भाषा को दूषित करने वाले इन तत्वों में राजनीति, धर्म, बाजार और संस्कृति ही नहीं, वह साहित्यिक भाषा भी शामिल होती है जो भाषा को सिर्फ एक माध्यम की ही तरह देखती है। इस परिस्थिति में हिंदी के एक अत्यंत सफरिंग भाषा होने की बात चिंतित करती रही है।
हिंदी ही क्यों, दुनिया भर की भाषाएं निरंतर प्रदूषित होती जा रही हैं। भाषाओं का पतन अपने आप में ही विचार-विमर्श का एक बड़ा इलाका खोज सकता है। यह संयोग नहीं है कि उन्नीसवीं सदी के फ्रांसीसी लेखक फ्लाबेयर हों या बीसवीं सदी के भारतीय लेखक, निर्मल वर्मा, भाषा के प्रति इन दोनों की ही गहरी चिंताएं, चेतावनियाँ को इनके लेखन में जगह-जगह पर देखा जा सकता है।
इन और इनके जैसे जागरूक लेखकों के प्रयास ही रहे हैं कि हमारे समय में भाषा की पवित्रता का सवाल, भाषा की आंतरिकता का प्रश्न सोचने-समझने की दुनिया में, सृजन के संसार में बराबर अपनी जगह बनाए रख सका है। भाषा की इस मानवीय भूमिका को लेखक अगर अपने लिखे गए में, भाषा की गंभीरता और जोर को बनाए रखकर बचा सकता है, तब एक ऐसा समावेशी साहित्यिक परिवेश भी, एक ऐसी साहित्यिक संस्कृति भी, जिसके निर्माण में पत्र-पत्रिकाओं, संपादकों, पाठकों, प्रकाशकों और साहित्यिक संस्थाओं की अहम भूमिका होती है।
यहां लेखक की चिंताओं और जागरूकता के साथ-साथ एक पाठक की आत्मचेतना, एक पाठक के अपने नैतिक आवेग के बारे में सोचने की जरूरत है। जिस तरह शास्त्रीय संगीत को समझ लिया हुआ रसिक अमीर खान के गायन को सच्चे अर्थों में पायेगा। जिस तरह मूर्तिकला का जानकार किसी बौद्ध प्रतिमा को उसकी समग्रता में महसूस कर सकेगा, उसी तरह साहित्य का एक पाठक किसी कविता, कहानी या उपन्यास को उसकी समग्रता में देखते हुए, सृजन के संसार का गहरा, जरूरी और उपयोगी बना सकता है। एक सजग और संवेदनशील पाठक, निराला की कविता ‘राम की शक्ति पूजा’ या प्रेमचंद की ‘पूस की रात’ से कुछ ज्यादा और जरूरी ग्रहण कर सकता है।
मुझे लगता है कि सृजन का हमारा संसार जितना अच्छे लेखकों के अभाव में हमारे लिए गरीब, उजाड़ और आधा-अधूरा बना रहेगा, उतना ही सृजन, संवेदनशील और परिपक्व प्रौढ़ पाठकों के अभाव में।
हम जानते हैं कि हमारा मानवीय जीवन सीमित रहा है। हम यह भी जानते हैं कि सृजन का संसार असीमित रहता आया है। जीवन एक तरफ क्षणभंगुर है और साहित्य में शाश्वत होने का तत्व सदियों से बना रहा है। कहा ही जाता है कि कला, जीवन से लंबी होती है। चेखव हों या हेमिंग्वे, दोनों ही कितना कुछ लिखना चाह रहे थे। कैथरीन मेंसफील्ड अपनी गंभीर जीवन के दिनों में, अपनी कहानियों के बारे में सोचती रही थीं । सृजन के संसार की सीमाएं, बीमारियां और मृत्यु ही तय नहीं करतीं, जीवन भी कभी-कभार सृजन के संसार के लिए सीमाएं खड़ा कर देता है।
आखिर सदियों से तानाशाही साहित्य, कला, सिनेमा और संगीत की दुनिया को तहस-नहस करने की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आती है। राजनीति और धर्म, बाजार और बाजारुपन के आक्रमणों के सृजन के संसार पर होते प्रभावों, परिणामों का एक लंबा, निर्णायक सिलसिला बनता है, जहां समय की सीमा से जा न सकूँगा। अपनी बात का अंत ग्रीक कवि जॉर्ज सेफेरिस की कविता की इन पंक्तियों से करना चाहूँगा –
“The ink grows less
and the sea increases.”
(स्याही कम हो जाती है
सागर फूलता जाता है।)
परिचय :-
जन्म : 25 दिसंबर 1959
शिक्षा : एम.ए. (समाजशास्त्र)
नागपुर विश्वविद्यालय
भारतीय स्टेट बैंक से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति
रचनाएँ : शोकगीत, भारत भवन भोपाल (1990), मरुस्थल, राजकमल प्रकाशन (1998), लाल दीवारों का मकान, कवि प्रकाशन (1998), बारिश, ईश्वर और मृत्यु, वाणी प्रकाशन (2004), चेम्बर म्यूज़िक, वाणी प्रकाशन (2012), इमिज़िंग द अदर (कथा ग्रुप) में कहानी का अंग्रेज़ी अनुवाद, प्रतिनिधि कहानियाँ (2019), गोधूलि की इबारतें (कथेतर गद्य) आधार प्रकाशन (2020), बचपन की बारिश, आधार प्रकाशन (2021), सर्दियों का नीला आकाश, राजकमल प्रकाशन (2022), कुछ दरवाज़े कुछ दस्तकें ( कथेतर गद्य) आधार प्रकाशन (2023), पूर्व-राग: एक पाठक की नोटबुक (कथेतर गद्य), आधार प्रकाशन 2025
कुछ कहानियों के मराठी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेज़ी और पोलिश में अनुवाद प्रकाशित
सम्मान : ‘मरुस्थल’ पर विजय वर्मा सम्मान, ‘बारिश, ईश्वर और मृत्यु’ पर श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, आधार सम्मान (2025) प्राप्त
फ़िल्म सोसायटी मूवमेंट से सम्बद्ध
पता : जयशंकर, शकुंतला, 33, प्रकाश नगर, नियर जीमखाना, गोधनी रोड, नागपुर, 440030
ई मेल : jayshankar58@gmail.com
मोबाइल : 94256-70177