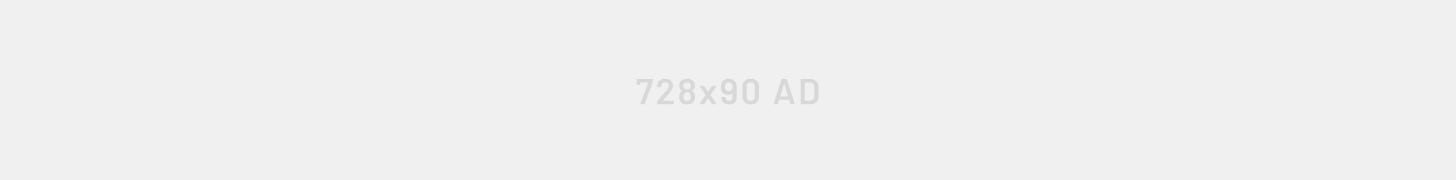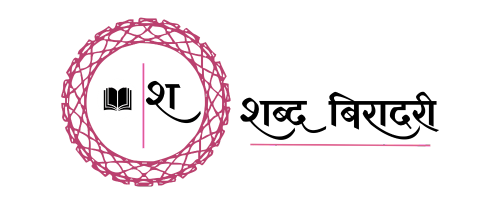बीज– बीज, वह जो तपती धूप, उमस, भरी बारिश और झुलसी हुई धरती में भी धैर्य के साथ खुद को जिलाए रखता है । जिसमें अंकुरण की क्षमता है । फूलने-फलने, बढ़ने और छाया देने की शक्ति है । इस दृष्टि से पृथ्वी और स्त्री भी बीज की तरह हैं, जो बड़ी धीरता के साथ अचल रहकर पूरी मानवता के विकास के लिए उत्पत्ति करती हैं ।
किसान स्वयं बीज है । उसकी रगों में धैर्य, रक्त बनकर बहता है । उसकी पसीने की ख़ुशबू, फसलों में रंग भरती है । उसके तलवे की बिवाइयों में भरी मिट्टी की महक, उसकी साँसो से आती है । अपने चौपाए भाई के जूठन वाला कौर, मुँह में रखते ही अमृत-रस के संचार से उसका खंखर शरीर फिर से जी उठता है ।
वह अपने हल और कुदाल के साथ चौमासा (बरसात) के पहले ही जेठ की उष्ण और फटी धरती के हृदय पर तनकर खड़ा हुआ आसमान में अपने अंकुरण के बिंदु तलाशता है । सूर्य की तेज़ रोशनी से चौंधियाती आँखों के ऊपर बरौनियों पर, अपनी दाहिनी हथेली की छाया रख; पूरा शून्य, वह ख़ुद में उतारकर इसलिए संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शून्य के बाद ही संसार शुरू होता है । उसे यकीन है कि आसमान के साफ माथे पर, किसी दिन उसके माथे के पसीने, बादल बनकर छाएँगे और बूँद बनकर सूखी धरती की प्यास बुझाएँगे ।
पेड़ से फल के रूप में गिर कर मिट्टी तक पहुँचने के क्रम से गुज़रते हुए बीज की तरह किसान का संघर्ष अनवरत चलता रहता है । कभी उस बीज को आंधियाँ साथ ले उड़ती हैं तो कभी बह जाता है वह नदियों के संग, टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों से होकर टकराती लहरों के तटों पर ठोकरें खाते हुए । उसे कोई गुरेज नहीं, किसी चौपाया के उदर का ग्रास बनने से तभी, या तो वह खाद के रूप में धरती को पोषित करता है या मिट्टी के सीने से जा लगने के लिए चबाते दाँतों के किटकिट से ख़ुद को साबुत बचा लेता है । कभी कुछ बूँद पानी के इंतज़ार में वक्त-दर-वक्त आकाश ताकता है; कभी पानी में आकंठ डूबे सड़ने के ठीक पहले तक सूरज तलाशता है तो कभी किसी चिड़िया की चोंच के साथ उड़कर, शहर के कांक्रीट भरे जंगलों में किसी शिखर पर रखे पानी टंकियों के गर्द भरे पाँवों से लिपटकर, पीपल का नन्हा पौधा बनने के इंतज़ार में तपस्या करता है ।
भारत वर्ष में जन्मे लगभग आधे पुत्र अपने पिता के कुछ बीघे खेत के साथ किसान बनकर ज़मीन से जुड़ जाते हैं । सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बंजरता, कीटों के प्रकोप, कई बीमारियाँ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त वह किसान, सरकारी तंत्रों के खोखलेपन, योजनाओं में भ्रष्टाचार, जमींदार के बदले हुए चेहरे से लिए गए क़र्ज़, कुर्की, नीलामी जैसी मानवीकृत समस्याओं से आजीवन जूझता रहता है ।
ज़मीन से जुड़ते ही उस पर बने रहने और उस पैतृक धरोहर को जीवन भर अपने प्राण की तरह संजोए रखने की उसकी कोशिश, उसे बीज बनाती है । धरती माँ की गोद में बीजों के साथ वह अपनी छोटी-छोटी इच्छाएँ बोता है ।
भूमि के सीने में दबे ‘बीज का अंकुरण के लिए संघर्ष’ की तरह वह किसान-पुत्र उनके साथ-साथ उसी भूमि में अंकुरित होने के लिए निरंतर संघर्ष करता है । परिस्थितियों से हार न मानने की जिद, बीजों की तरह किसान की जीवटता का भी आधार है । “भीठ ज़मीन हो या जुताई कम हुई हो, आकाश चुए या बातास जले, पौधे उगेंगे ही ।”4 संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बीज और किसान की प्रथम और पवित्र लालसा अंकुरित हो सकने की होती है ।
अंकुरण– जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो बीज की तरह एक से अनंत के रूप में स्वयं को तब्दील कर पाए । धान का एक बीज मिट्टी में समाकर जब अंकुरित होता है उसमें अनेक कंसे निकलते हैं जितने कंसे उतनी बालियाँ । एक-एक बाली में कई-कई बीज, खुद को परिपक्व बनाने के लिए प्रकृति की हर मार सह कर और उसके एक दुलार पर लरज कर सैकड़ों-सहस्त्रों की संख्या में हवा के साथ खनखनाते हैं; धूसर और बेरंग पड़े खेतों में धानी रंग भर लहलहाते-महमहाते हैं ।
बीज की तरह ही किसान भी सदैव उपलब्ध ज़मीन पर अपनी जड़ें जमाने की पुरज़ोर कोशिश करता रहता है; निरंतर उत्पादन बढ़ाकर पतझड़ी दुनिया के मुँह तक दाने पहुँचाता है; पिता से प्राप्त कम उपजाऊ या बंजर ज़मीन को अपनी मेहनत की चोट से उर्वर बनाकर कोरे संसार के सूने मस्तक पर हरियाली बोता है ।
उसके परिश्रम की चक्की में परमार्थ और प्रेम के दो पाटे हैं । अपने दोनों पाटों को साथ लिए, ज़मीन पर घर्र-घर्र चलती हुई वह चक्की, आसमान में उड़ने वालों की ताक़त का कारण बनती है मगर उन आसमान परस्तों की सामर्थ्य होने का ना उसे इल्म है और ना गुरूर। वह चक्की मिट्टी की व्यथा के साथ जीने-मरने वालों के पसीने की कंठध्वनि है ।
बीजों का ठोस होना किसान की बाजुओं की मजबूती है और बीजों का मिट्टी पर अंकुरण, किसान का अपनी ही ज़मीन पर अंकुरित होना है । जिस तरह खंडहर, अतीत की इमारतों की बुलंदी का इतिहास बताते हैं, उसी तरह साबुत और पुष्ट बीज फसलों की पैदावार का भविष्य बताते हैं ।
किसान के पसीने में किसी पेट की भूख की तृप्ति ठीक उसी प्रकार छुपी रहती है जिस प्रकार धूसर मिट्टी की मलीनता में लहलहाती फसलों की हरियाली छुपी रहती है । मूल्यवान केवल बीज है, ठोस और परिपक्व बीज; बात चाहे भावी उत्पादित फसलों की हो या किसान-जीवन की भावी संतुष्टि और समृद्धि की । बीज की तरह अंकुरित होता किसान भी हमेशा, खुली आँखों से आसमान ताकता है ।
‘नहीं हुआ है अभी सवेरा
पूरब की लाली पहचान
चिड़ियों के जगने से पहले
खाट छोड़ उठ गया किसान।’
क्योंकि ठोस बीजों में किसी किसान का टिकाऊ जीवन निर्भर करता है इसलिए वह खेतों में बीज रोपने के पहले कई तरह से उनका परिक्षण करता है । एक मुट्ठी बीज वह किसी पानी भरे बर्तन में डाल देता है । कितने बीज पानी के भीतर बैठ गए और कितने सतह में तैरते रह गए, इस आधार पर वह अपनी समृद्धि का एक अनुपात तय करता है । एक मुट्ठी में इतने बीज साबुत हैं तो एक बोरी में कितने बीज साबुत होंगे ? और इसी तरह पूरी फसल में साबुत बीजों की संख्या कितनी होगी ? एक दूसरी तरह के परिक्षण में किसान एक मुट्ठी बीज को गिनकर मिट्टी में रोप देता है । कुछ दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं जिन्हें गिनकर वह पूरी फसल में पोपले (बदरा) और ठोस बीजों का अनुपात निकाल लेता है।
प्रकृति भी अपने उपवन में किसान को एक बीज की तरह देखती है । प्रतिकूल होती प्रकृति के मध्य जो किसान बीज की तरह संघर्ष कर खुद को जिलाए रखेगा वही अंकुरित होगा, फूलेगा-फलेगा और बढ़ेगा; न केवल स्वयं में जीवन-रस का संचार करेगा बल्कि पूरे विश्व की जिह्वा में प्राण बन कर संचरित होगा ।
ज़मीन पर पड़े हुए बीजों को अंकुरण के लिए उचित मात्रा में हवा, पानी, प्रकाश और खाद की ज़रूरत पड़ती है । अपनी ज़मीन पर सदैव खड़े रह पाने के लिए किसान को भी हल, कुदाल और साबुत बीज के साथ हवा, पानी, प्रकाश और अर्थ की आवश्यकता पड़ती है । अंकुरण के बाद कोंपलें फूटने तक का बीज का संघर्ष अपनी मिट्टी जेऔर ज़मीन से होता है मगर कोंपलें जब ज़मीन से सिर उठाकर तनों और शाखाओं के रूप में तब्दील होने लगती हैं उसके संघर्ष का दायरा बढ़ कर आँधी, ओला, बाढ़, दुर्भिक्ष से होने लगता है। अंकुरित हुए बीजों को कोंपलों और शाखाओं में बदलते हुए देखना किसान की आँखों की उम्मीद होती है ।
‘हमने चाहा कि
फसलों की नस्ल बची रहे
खेतों के आसमान के साथ
हमने चाहा कि
जंगल बचा रहे
अपने कुल-गोत्र के साथ।’
कोंपलें और शाखाएँ- धरती में जाने के पहले बीज अपने खोल के भीतर होता है । धरती की कोख की उष्णता से जीवन की हरियाली लिए वह अपने खोल से बाहर आता है । वह किसान के हाथों से होकर मिट्टी तक पहुँचने के पहले और उस मिट्टी को फोड़ कर अंकुरित होने की अवधि तक बहुत खुश रहता है; मिट्टी का आँचल ओढ़ता है, अंकुरित होकर पौधा बनने और फूलने-फलने के लिए । मगर कोंपल के रूप में तब्दील हो चुके अंकुरित बीज को जब इस बात का पता चलता है कि उसका तनों और शाखाओं में बदलना अब उतना सहज नहीं है, क्योंकि मिट्टी की नमी तो गिरवी है उन बादलों के पास और उसके मोती सूखे आँसू बन कर आकाश में रुई की तरह बिखर गए हैं ।
इस वास्तविकता का पता तो उसे ज़मीन से फूट निकलने के बाद चलता है; जब स्थितियाँ साथ नहीं देतीं और मानसून की मार सहने वाली वह कोमल कोंपल, शाखाओं और तनों में तब्दील होने की चाह में सोंधी महक वाली हवा, पानी की बौछारें और धूप की हल्की सेंक के लिए शून्य का मुँह ताकती रहती है मगर हासिल होती हैं दरारें, लू और झुलसती उम्मीदें ।
दुनिया में लोगों को विरासत में क्या कुछ नहीं मिलता, किसी को महल, किसी को मुहरें तो किसी को हर मुमकिन भौतिक सुख-सुविधाएँ और पूँजी मगर बीज जब कोंपल के रूप में बाहर आता है उसे विरासत में मिलता है क़र्ज़, जिसे कभी पिता ने अपने पिता से पाया था । पिता के बाद बेटा जब ख़ुद किसान बनकर अपने खेत में पाँव धरता है वह उसकी उष्णता और बंजरता से बेसाख्त रू-ब-रू होता है ।
धीरे-धीरे वह ज़मीन के साथ मिली सारी असुविधाओं और कठिनाइयों से जूझता हुआ ज़मीन में अपनी जड़ें गहरी करने की कोशिश करता है । इस कोशिश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ सामाजिक विपदाओं से भी निपटने का हुनर वह सीख लेता है ।
वह किसान-पुत्र चौपाए साथी के साथ पाँच बीघा ज़मीन पर हल जोतते हुए ऋण की व्यथा बतिया कर, कुछ समय के लिए माथे की चिंता हल की मूठ पर उतार लेता है । पिता के पिता की तरह ही ठेठ देशी बीजों को खेतों में रोपते हुए अपने पूर्वजों की संचित ऊर्जा मुट्ठी में भर लेता है । चौपाए भाई के गोबर से भरे घूर में से खाद ढोते हुए वह भावी फसल की हरियाली की कल्पना कर मुस्करा लेता है । उसे तसल्ली है अपनी ज़मीन से कौर उठा पाने की; सुकून है अपनी और परिवार की भूख की वेदी पर मुट्ठी भर हविष्य डाल पाने का; संतोष है अपनी सीमित चाहनाओं की कमतरीन में असीमित धैर्य धारण कर पाने का । वह स्वावलंबी है… अपनी ज़मीन पर अपने हल, कुदाल, बीज, खाद, चौपाए भाई और परिवार के सभी सदस्यों के साथ खड़ा हुआ । बीजों को कोंपलों में बदलते, कोंपलों को दो से चार और चार से आठ होते देखते और शाखाओं को हरियाते-मोटाते देखते हुए वह अपने सुखद भविष्य की कल्पना में खो जाता है । खेतों की लहलहाती फसलों के साथ उसका मन लहलहा उठता है ।
भूख और संतुष्टि– पीढ़ियों से उस किसान की भूख अपनी पाँच बीघा ज़मीन से उत्पादित अन्न जितनी ही है । वह उस प्राप्त अन्न के सीमित अंश के साथ उसी तरह संतुष्ट रहता है, जैसे कोई बछड़ा दुग्धपान करते हुए अपनी माँ से दूर खींच लिए जाने के बाद भी संतुष्ट हो लेता है क्योंकि माँ के दूध का स्वाद उसकी जिह्वा और मन की तृप्ति का आधार है । उत्पादित अन्न का कितना भाग किसान की जठराग्नि की शांति के लिए है और कितना, बाज़ार उससे लूट लेगा, इसका हिसाब वह नहीं लगाता क्योंकि उसकी खुशी का अवलंब तो खेतों में लहलहाती फसलें हैं । अन्न के प्रत्येक दाने में उसकी उँगलियों की छुअन की आँच मौजूद रहती है । जब उस अन्न के दाने-दाने को दुनिया अपने मुँह में रखती है तो वही आँच उसकी भूख को तृप्त करती है ।
दुनिया की चटपटी जीभ का ख्याल रखने वाले और उसकी पेट पूरी तरह भर देने वाले की भूख में आख़िरकार स्वाद कितना बचा रह गया है यह विचारणीय प्रश्न है ।
वह जानता है कि भूख, पैदावार के साथ-साथ बढ़ती जाती है, मगर उसके पाँच बीघे के कई टुकड़ो में बिखरे खेतों पर ट्रेक्टर के बजाय आज भी हल, कुदाल और फावड़ा चलते हैं । बैल परिवार के किसी सदस्य की भाँति किसान के साथ-साथ जीवन भर उन खेतों में जुतता है और मरने के बाद भी अपनी खाल से बने हुए जुए में तब्दील होकर अपनी संतानों के काँधे पर बँध कर ताकत देता रहता है । उससे जुतकर बछड़े से बैल बनी उसकी संतान को भी किसान-पुत्र की तरह ही वही पाँच बीघा ज़मीन मिलती है, जितने में जुतने वाले उसके संतुष्ट काँधे हल का भार वहन कर मशीनी सभ्यता से भिन्न, प्रकृति और पुरूषार्थ की संस्कृति की मिसाल कायम करते हैं । परिश्रम और विश्वसनीयता के प्रतीक बैल किसान की समृद्धि का आधार है ।
भारतवर्ष में किसान हमेशा से संतोषी प्रवृत्ति का जीव माना जाता है, जिसकी भूख का संबंध अब तक, दो वक़्त की रोटी, तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े और सिर पर अपनी छत से रहा है । मगर समय के साथ-साथ किसान-जीवन की परिभाषा, उसकी भूख और खेती के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है । किसी समय कृषि को हर तरह की नौकरी से श्रेष्ठ समझ कर, मिली हुई नौकरी को भी त्याग दिया जाता था । अब शहरों की चकाचौंध और नौकरी पेशे में रहने वालों की चमकती दुनिया ने किसानों को भी आकृष्ट कर लिया है । मुँह खोलती आवश्यकताओं ने उत्पादन में अधिकता की मांग की । अधिक उत्पादकता ने पर्याप्त पूँजी और उर्वर ज़मीन की मांग की । इन सभी को हासिल कर पाने की कोशिशों ने संकरित बीजों, रासायनिक खाद, विटामिन और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग बढ़ाए, फलत: तरह-तरह के कीटों के साथ मित्र कीट भी समाप्त होने लगे हैं । अब वर्तमान धीरे-धीरे, अपनी बढ़ी हुई भूख की संतुष्टि के लिए पूरे भविष्य को बंजर बना रहा है ।
वसंत– जिनके हलों के फाल ने पीढ़ियों द्वारा खींची गई संस्कृति की लकीरों को गाढ़ा किया; जिनकी जीवन-शैली, सरल स्वभाव, लोकाचार और निस्वार्थ मुस्कान, नदियों के निर्मल जल की भाँति अंतस में उतार लेने जैसी सदानीरा हैं । उन किसानों के जीवन के बियाबान में फागुन, चैत और वैशाख अपनी आधी हरियाली के साथ प्रवेश पाते हैं; उसमें हरी पत्तियों और सुर्ख़ फूलों की तादाद कम होती है मगर महक और लहक के साथ बिखरने में वे कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते । किसानों का आँचल मैला ही सही मगर उसमें अन्न के स्वर्णिम दाने भर पाने की लालसा के कारण, उनके जीवन का वसंत कभी ख़त्म नहीं होने पाता ।
आज भी भारत भूमि में, पाँच बीघे खेत वाले किसानों की संख्या बहुतायत है, जिनके खेतों की जुताई और बुआई, बैलों के गले में बजती घंटी के साथ शुरू होती है । उसी घंटी की आवाज़ के साथ, कई टुकड़ों में बँटे खेतों की उत्पादित फसल उनके घर की चौखट तक पहुँचती है । उन्होंने ट्रेक्टर या हार्वेस्टर के सहारे खेती करना नहीं सीखा, क्योंकि इन कलों की खुराक जितना कौर, उस पाँच बीघे ज़मीन के किसान के खेत में पैदा नहीं होते । वे अपनी हथेलियों की दस उँगलियों की ताकत और चौपाए भाइयों के साथ पर उसी तरह विश्वास करते हैं, जिस तरह चलते-फिरते शरीर को अपनी उठती-गिरती साँसो की थिरकन पर भरोसा होता है ।
कृषि औजारों (हल, फावड़ा, गैंती, कुदाल, टंगिया, कुल्हाड़ी, खुरपी इत्यादि) की पूजा करने वाले उसके हाथ ‘हरेली’ जैसे स्थानीय त्यौहार की परंपरा ढूँढ लेते हैं । सावन के महीने में धरा, हरा आँचल ओढ़ लेती है, तब किसान अच्छी फसल की मंगलकामना के लिए कृषि उपकरणों की पूजा करता है । रसोई की दीवार में मानव-शृंखला के साथ हल और चौपाए पशु के चित्र बनाकर वह कृषि कार्य में पशु-प्रकृति-मनुष्य की परस्पर सहभागिता के दृश्य दिखाता है। संबंधों की प्रगाढ़ता की ये परंपरा अपने काम के प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति है । किसान और लोहार में आपसदारी कृषि और औजार के इसी सहसंबंध का सुंदर नतीजा है ।
पीढ़ी-दर-पीढ़ी किसान अपने पुत्र को उसी तरह खेत सौंपते हैं, जैसे किसान के बैल, अपने बछड़े को बैल बनने के बाद खेतों की जुताई का काम सौंपता है । लोक जीवन से जुड़े ‘पोला’ त्यौहार में किसान अपने चौपाए भाइयों के प्रति मौन स्नेह व्यक्त कर, कृषि कार्य में उनकी अहम् भूमिका को स्वीकार करता है । इस लोकपर्व में किसानों द्वारा की जाने वाली पशु-पूजा, मानव के जीवन में प्रकृति और जीवों की ज़रूरत की पड़ताल करती है । ‘नवाखाई’ का उत्सव किसान अपने परिश्रम के प्रतिफल के महोत्सव स्वरूप मनाता है । नए अनाज, दलहन और तिलहन से पकवान बनाकर और भोजन पकाकर सबके साथ मिल-बाँट कर खाने वाला वह किसान-परिवार प्रकृति से प्राप्त उपादान की साझेदारी की महत्ता स्वीकार करने की सीख देता है ।
भारत वर्ष की कृषि प्रधान संस्कृति में दान-परंपरा की याद दिलाता क्षेत्रीय लोकपर्व ‘छेरछेरा’ फसल कटाई के बाद मनाया जाता है । यह पर्व आपसी मेलजोल और भाईचारे की सेंक से लोकहृदय को आह्लादित भी करता है । बाँटना, उसके अभावों वाले जीवन का स्वभाव होता है । उसकी इसी प्रकृति ने संसार को पोषित किया है । दीपावली के बाद किसान ‘गोवर्धन पूजा’ का पर्व मनाता है । गोठान में अपने चौपाए भाइयों के गोबर से कई छोटी-छोटी कोठियाँ बनाता है, धान की बालियों और सिलीयारी से उन्हें सजाता है । मूक पशुओं की पूजा कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता है । जिस मूक भाई ने वर्ष भर उसकी सेवा की उसको पूजकर वह अपना प्रगाढ़ संबंध उससे जोड़ता है । पशु-पूजा का यह त्यौहार मानव-जीवन में प्रकृति और पशुओं के महत्व को इंगित करता है ।
इन तीज-त्यौहारों के दरमियान उसके होंठों की बरबस हँसी, वीणा के एक तार को छूने जैसी होती है, जिससे दूसरे तारों में अपने आप कंपन पैदा हो जाता है; उस एक चेहरे की हँसी अनेक चेहरों को छू लेती है । कृषक-जीवन का वसंत, उसकी इन्हीं छोटी-छोटी खुशियों की राह चलकर आता है ।
हर तरह के अँधेरों को भूलकर इन त्यौहारों के बीच अपने हिस्से का उजाला तलाश लेने वाला किसान, कभी सिंचाई सुविधा और हाइब्रिड बीजों के प्रयोग के कारण अच्छी पैदावार होने पर खुश हो लेता है, तो कभी सरकार द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने पर कुछ देर इतरा लेता है । कभी पहली बार अपनी ज़मीन पर क़र्ज़ मिलने की खुशी या किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाने का हर्ष उसके कठोर संयमित जीवन में सरसता घोल देते हैं । कभी बिक्री के लिए कृषि उपज मंडी और बाजारों की उपलब्धता के कारण बिचौलियों से कुछ हद तक छुटकारा पाने की राहत तो कभी अपनी ज़मीन की कीमतों में बढ़ोत्तरी की संतुष्टि, उसके शिकन भरे माथे पर सुकून की चिकनाहट पैदा कर देती है।
फागुन, चैत और वैशाख के माह में प्रकृति, पूरी हरियाली के साथ फूलों और फलों से अपना शृंगार करती है; उसी समय खेतों की भरी-पूरी हरियाली और बीजों के भराव से किसानों के जीवन में भी वसंत प्रवेश करता है । प्रकृति में वसंत की हरियाली बीजों की तपस्या के फलस्वरूप होती है और मनुष्य के जीवन में वसंत का उत्सव, किसानों का अटूट मनोबल और अथक परिश्रम का परिणाम है ।
जड़- जड़ का सीधा संबंध बीज से है, जिस बीज की जड़ें जितनी गहरी होंगी उसका पौधा उतना ही पुष्ट होगा, उसकी शाखाएँ और बालियाँ उतनी ही फैलेंगी और फूलेंगी । ज़मीन, जड़, बीज और फसल की कल्पना करते ही ज़ेहन में किसी कौंध की भाँति सिर पर पगड़ी, काँधे पर गमछा और हाथ में हल की मूठ पकड़े किसान का दृश्य उभर आता है । जिस तरह जड़ और बीज का संबंध अन्योन्य है उसी तरह की अनन्यता ज़मीन और किसान के मध्य भी है ।
ठेठ आदिम युग से वक़्त के वर्तमान में दस्तक देने तक कृषि, किसान व पशुपालन का संबंध किसी ज़रूरी व्यवहार की तरह भारत भूमि से जुड़ा हुआ है । मानव की सहज प्रवृत्ति, निर्माण की है; सृजन और सँवार की है । इसी प्रवृत्ति ने उसमें कभी जंगली रही फसलों से बीज एकत्रित करना, एकत्रित बीज से फसलें उगाना और फसलों के उत्पादन की प्रक्रिया में चौपाए बैलों की सहायता लेना सिखाया । उसका बीज, पशुपालन और फसल से उतना ही आदिम संबंध है जितना मनुष्य की भूख का संबंध मिट्टी की गंध से है ।
इसलिए सहस्त्राब्दियों तक मिट्टी के सीने में देशी बीजों की जड़ें इतनी गहरी धँसी हुई थीं कि उसे उखाड़ फेंकना सहज संभाव्य नहीं था । जब तक किसान के पास अपने बीज, पशु, खाद और हल थे, उसे किसी रासायनिक खाद, कीटनाशक या विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि देशी बीज, किसानों की तरह ही अपने सृजन में परिपक्व हुआ करते थे । देशी बीज और खाद से उत्पन्न फसलों के दाने जब किसान के हलक में कौर बनकर उतरते थे, उसकी रगों के रंग, खेतों की हरी-भरी फसल की भाँति अधिक गाढ़ा हो जाया करते थे । तब खेतों पर हल जोतते हुए उसकी पेशानी पर थकावट की नहीं स्वास्थ्य की बूंदें निथरती थीं । तब अपनी जड़ों के ठेठपन से जुड़ा हुआ किसान समूचे संसार को स्वास्थ्य की जड़ों से जोड़ता था ।
जिस प्रकार किसान पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी संतानों के साथ अपनी ज़मीन से जुड़े रह कर, कृषि कार्य में तल्लीन रहता था, उसे अपनी संतानों के भविष्य में नौकरी की जगह, हरियाली से भरे खेत-खलिहान नज़र आते थे, ठीक उसी प्रकार अपने संपूर्ण पुंसत्व के साथ, देशी बीज किसान का हम-कदम बन, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हुए धूसर खेतों को धानी कर देते थे । उसके बीजों में अंकुरण और लहलहाहट की पूरी क्षमता मौजूद रहती थी । वे आज के नपुंसक बीजों की तरह केवल एक फसल के लिए नहीं होते थे, मगर आज समाप्ति की ओर बढ़ रहे उन बीजों का अस्तित्व खतरे में है ।
निर्वंशीय संकर बीजों की तरह ही धीरे-धीरे किसान के वंशधरों का, ज़मीन से जुड़ाव कम होता जा रहा है । कृषि की जड़ें धीरे-धीरे उखड़ रही हैं । कभी खेतों में कलेवा पहुँचाने वाला बचपन, पिता के हल के पीछे-पीछे दौड़ते हुए, कभी अमराई और झरबेरी में ढेले मारते हुए, कभी खेत के मेड़ के सबसे ऊँचे महुआ के पेड़ पर चढ़ते हुए, आम, इमली और तेंदू की ख़ुशबू के बीच बड़ा होता था । पके आम का रस, गदराई इमली की खटाई और लहसते गन्ने की मिठास उसके लहू में रची-बसी थी ।
अब पाठ्यक्रम के बोझ से लदा बचपन, चमकती ख़्वाहिशों के लंबे डंडे के सहारे किसी बड़े शहर या नगर तक छलांग लगाना चाहता है । अपनी जड़ों से उखड़ चुका किसान-पुत्र जब शहरी जीवन की कोमलता को साथ लिए लौटता है; उसके किताब और कलम पकड़ने वाले हाथ, पिता के हल की मूठ नहीं पकड़ पाते ।
भारत भूमि, कृषि और किसानों की भूमि है । इसकी मिट्टी में उगने वाले अनाज, वक्त-दर-वक्त निरंतर लोक-भूमि में हरियाली, लोक-मानस में जीवटता और लोक की धमनियों में रक्त बनकर संचरित होते हैं । यहाँ की संस्कृति पीढ़ियों के श्रम और संस्कारों द्वारा निर्मित है, जहाँ कभी हर किसी के हाथ और माथे पर ज़मीन की ख़ुशबू की धूल जमी रहती थी । यहाँ जड़, ज़मीन और किसान का जुड़ाव परिश्रम के साथ है, इसलिए जड़ें, बीज के साथ और ज़मीन, किसानों के साथ ही बची रह पाएँगी।
पतझड़– मानसून का जुआ कही जाने वाली भारतीय कृषि, आज भी आधी से भी अधिक आबादी के भरण-पोषण का साधन है, उनके जीवन-यापन का आधार है । मगर आधिकाधिक विकास और सुख-सुविधाओं के साथ तेज़ी से पसरते संसार में जहाँ सब कुछ का फैलाव है, सब कुछ की बढ़ोत्तरी है, वहीं, लगातार सिमटती जा रही है ज़मीन । ज़मीन जो किसी समय वृक्षों के हरेपन से रंगी रहती थी, झाड़-झंखाड़ के झुटपुटे से सँवरती थी और फल-फूलों के लदाव से झुकी रहती थी । अब ईंट, बालू-बजरी, कांक्रीट, छड़ और सीमेंट इत्यादि से लदी-पटी ज़मीन, कृत्रिम रंगों से सराबोर होकर, लगातार आसमान छू पाने की भरसक कोशिश कर रही है ।
बढ़ती आबादी की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिकुड़ती ज़मीन धीरे-धीरे अपनी मिट्टी की सोंधी महक खो रही है । दूषित जल, विषाक्त वायु और प्लास्टिक के महीन टूकड़ों ने भूमि की उर्वरता और मिट्टी की वांछित महक को उसी तरह ख़त्म कर दिया है जिस तरह हाईब्रिड बीजों, कीटनाशकों और बाहरी खादों के अत्यधिक प्रयोग ने अनाजों की वाजिब ख़ुशबू और पोषकता को लगभग ख़त्म कर दिया है ।
कभी अपनी मिट्टी और उर्वरता के साथ बीजों की प्रतीक्षा करती ज़मीन, आज विकास की राह चलते हुए कल-कारखानों, उद्योग-धंधों, सरसराती रेल-पटरियों और अनगिनत सड़कों से पट गई है । विकास अपनी लपलपाती जिह्वा से, इर्द-गिर्द फैली हरियाली को समूल निगल लेना चाहता है ।
किसान फसल पैदा करना जानता है, उसमें अपने प्रेम और स्नेह का रस भरने जानता है, उस रस को दोनों हाथों से जगत के बीच उलीचना भी जानता है, नहीं जानता है तो केवल बाजारवादी दोहरा व्यवहार और बर्ताव । उसे अपने ही द्वारा उत्पादित फसलों को अपनी कीमत पर बेच सकने का अधिकार नहीं है, जबकि उन फसलों की खरीद-फरोख्त करने वाले बिचौलिये बाज़ार में उन फसलों के मनमाने दाम वसूलने से बाज़ नहीं आते । वह बाज़ार की पल-पल बदलती नीतियों और नियमों से ठीक उसी प्रकार वाक़िफ नहीं होता जिस प्रकार खेतों में अपनी बालियों के साथ झूमते बीजों को, पकने और भरने के बाद ही गिरने वाले ओलों का पता नहीं लगता । वे तो अपने भराव, फैलाव और धानी रंग की मस्ती में सराबोर रहते हैं, हरहराते खेतों और खनखनाते बीजों को देख मुस्कराते किसानों की तरह ।
तैयार फसलों के बाज़ार में आते ही एक विशेष तबके द्वारा, कम मूल्य में उन फसलों को खरीद लेना और संग्रहित फसलों की आपूर्ति कुछ समय तक रोक कर, उन्हें उन्हीं किसानों और आम जन को उच्च दामों में बेच देना, आज के बाज़ार की और बाज़ार की समझ रखने वालों की मूल प्रवृत्ति बन चुकी है । अपनी ही फसल को उच्च दामों में खरीदने की मजबूरी और अपनी मेहनत का मोल कौड़ी के भाव में पाने की पराधीनता, किसान-जीवन की विडंबना है । न चाहते हुए भी अपने जीवन के वसंत से कटकर पतझड़ी मौसम में जीने की दुर्धर्ष विवशता, उसकी नज़रों में जीवन का मूल्य कम कर देती है ।
पारिवारिक बँटवारे के कारण छोटे-छोटे खेतों में, मशीनों के बढ़ते उपयोग ने सीमांत किसानों की आजीविका छीनने का काम किया है । विदेशों के बड़े-बड़े खेतों की तुलना में भारत भूमि के खेत छोटे हैं । यहाँ किसानी जीवन पर आश्रित बहुतायत लोगों की तरह खेत भी हल और बीज पर आश्रित हैं, मगर वक़्त बीतने के साथ-साथ न केवल खेती की ज़मीन लगातार घट रही है बल्कि जो ज़मीन खेती के लिए बची रह गई है वह भी चार मेंड़ के दरम्यान लगातार सिमटती जा रही हैं ।
जिस कृषि कार्य से जुड़े रह कर, कभी देश की आधी जनसंख्या जीवन-यापन और रोज़गार के लिए खेतिहर गाँवों पर निर्भर रहती थी, आज उस कार्य और उन गाँवों को हेय दृष्टि से देखती है । कभी पारस्परिक सामंजस्य और सहयोग से खेतों के सारे काम निपट जाते थे; लोग-बाग में आपसदारी थी । आज मशीनें दीमक की तरह, कृषि व्यवसाय के उस तालमेल और समरसता को धीरे-धीरे कुतर रही हैं । मशीनीकरण के युग में हाथ की कमाई का मोल नहीं रहा, इसलिए लोग खेतों और गाँवों से हटकर, कल-कारखानों और उद्योग-धंधों से जुड़ने के लिए शहरों की ओर रुख कर रहे हैं ।
कटाव- पहले श्रम की संस्कृति पर भारतवर्ष टीका हुआ था । राजा जनक को हल चलाते हुए सीता मिली थीं । मेहनत करना, हल से ज़मीन जोतना और अपनी जड़ों से जुड़कर रहने की संस्कृति पर भारतवर्ष को नाज़ था । अब की पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, तहसीलदार, कलेक्टर चाहे जो कुछ बनना चाहे पर किसान बनने का स्वप्न वह नहीं देखती । धीरे-धीरे श्रम की संस्कृति की महत्ता ख़त्म हो रही है । नई संस्कृति कुछ और कहती है ।
किसानी कार्य अर्थात् श्रम की अधिकता और लाभ की अनिश्चितता। इसलिए जो जितना अधिक शारीरिक श्रम करेगा, समाज में उसकी स्थिति उतनी ही नीची मानी जाएगी । जब तक श्रम की संस्कृति का सम्मान भारतवर्ष में किया जाता रहा; राजा भी हल की मूठ पकड़ने में गर्व का अनुभव करते थे । अब गोदान के गोबर की तरह युवक गाँव की ज़मीन का मोह त्यागकर, शहर पलायन करते हैं । चाहे वहाँ दूसरों के अधीन तुच्छ-सी कोई नौकरी भी क्यों ना करनी पड़े । किसी तरह यदि किसान गाँव में रह गए तो ‘फाँस’ के किसानों की तरह कठोर और संघर्षपूर्ण जीवन जीने की अपेक्षा मरने का सरल मार्ग तलाशते हैं ।
जीवन में आने वाली प्रत्येक विपदाएँ स्वयं को पहचानने, बदलने और साबित करने का अवसर देती हैं मगर जब व्यक्ति की पहचान, विपदाओं के अंबार तले दबने लगे; विवशता और विपदाओं से उसका साबिका जीवन के हर मोड़ पर पड़ता रहे तो केवल धैर्य की पराकाष्ठा तक खुद को स्थिर रखना शेष रह जाता है और किसान वही धैर्यवान प्राणी है जो समय की पीठ पर सवार होकर भी सदैव, अपनी दशा-दिशा पर स्थिर रहता रहा है ।
सदियों से भारतीय किसानो में दुःख की व्यापकता इतनी रही है कि वह समय-समय पर बयाँ होने के लिए, कभी लोक-जागरण हेतु तुलसीदास की उँगली थामती है । कभी नवजागरण के लिए प्रेमचंद के पीछे-पीछे चलने लगती है और कभी पूर्ण जागृति के लिए आधुनिक कथाकार संजीव के साथ-साथ चली चलती है । मगर प्रत्येक समय की धरातल पर किसान-जीवन का पतझड़ कभी समाप्त होते नहीं दिखता ।
प्रत्यावर्तन- कृषि पर बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव ने एक ओर जहाँ किसानों के जीवन में, अपनी फसल के लिए उचित कीमत और बेहतर उत्पादन की अपार संभावनाएँ पैदा की हैं तो वहीं दूसरी ओर, संकर बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशक और मशीनों पर आश्रित होने के कारण ऋण लेने की समस्या तथा कृषि उपज मंडी और बाज़ारों में बिचौलियों की अनचाही मौजूदगी को भी जन्म दिया है ।
किसानी और व्यापार दो अलग-अलग चीजें हैं । एक के द्वारा खींची गई लकीर मिट्टी कुरेद कर उसे और उर्वर बनती है, तो दूसरे द्वारा खींची गई लकीर, उस मिट्टी से जुड़े लोगों के माथे पर चिंता बनकर झलकती है । इन्हीं (किसानी और व्यापार) के मध्य पनपता है बाज़ार, जिसकी बाँहें गर सहारा दें तो मुरझाए चेहरे मुस्कराने लगेंगे और यदि कस लें तो मुस्कराते चेहरे मुरझा जाएँगे ।
आज आवश्यकता इन बातों की है कि किसानों द्वारा उत्पादित फसलों का उचित मूल्य, उनकी मेहनत और इच्छा के अनुसार निर्धारित किया जाना, अनाजों में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए किसानों को जैविक और पारंपरिक कृषि के लिए प्रेरित करना और जैविक खेती करने वाले किसानों को विशेष सुविधा मुहैया कराना, बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित कर किसानों को शिक्षित, प्रशिक्षित करना, मानसून पर आश्रित कृषि के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाना, उनके जीवन को निरंतर संघर्ष से बचाने का उद्यम करना ताकि उनका, अपनी जड़ों से कटाव के आसार कम हों; उनके द्वारा जिए जा रहे जीवन में जीवित-मृत्यु और आत्महत्या के पतझड़ के बजाय जीवंत-वसंत के लक्षण अधिकाधिक हों, तभी वह खुद को समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख पाएगा और पलायन से परे सुखद जीवन के द्रुत गामी पथ पर अग्रसर हो पाएगा ।
चंद्रिका चौधरी
___________________________________________________________________________________________________________
परिचय
चंद्रिका चौधरी
सहायक प्राध्यापक हिंदी
स्व. राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह
शासकीय महाविद्यालय सरायपाली,
जिला -महासमुंद (छत्तीसगढ़)
Email – drchandrikachoudhary@gmail.com