
मेरे पिता आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व, बुधवार, 9 जुलाई 1980 को इस दुनिया को, हम सब को छोड़ कर चले गए। कभी-कभी मन में ये विचार आता है कि काश वो आज हमारे साथ होते और उन सभी सुख-सुविधाओं का आनंद ले पाते जो ईश्वर की कृपा से आज की पीढ़ी को उपलब्ध हैं। काश वो आज हमारे साथ होते, अपने पोते सूर्यांशु और उसके परिवार पर अपना प्रेम-भरा आशीर्वाद बरसाने के लिए। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें पूर्व-निश्चित होती हैं और हमारे नियंत्रण से परे होती हैं, परन्तु फिर भी कभी-कभी मन में ये विचार कौंध जाता है कि काश वो आज हमारे साथ होते!
हो सकता है यह लेख मात्र उनकी पुण्यतिथि पर मेरे मन में उठा एक भावनात्मक विस्फोट मात्र ही हो, परन्तु अपने मन के भीतर कहीं न कहीं मैं जानता हूँ कि यद्यपि सरकारी नौकरी होने के कारण उनमें इतनी सामर्थ्य तो थी ही कि वे अपने नौ लोगों के परिवार (हम 5 बहनें तथा 2 भाई थे) का भरण-पोषण कर सकें तथा हम सभी बच्चों को शिक्षित करने की व्यवस्था कर सकें, तो भी मैं यह कभी नहीं भूल पाता कि मैंने उन्हें अक्सर घर से मीलों दूर तक रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ऐसा सामान खरीदने के लिए जाते देखा है, जहाँ, उनके अनुसार, वह सामान थोड़े कम दाम पर मिलता था, शायद 5-10 पैसे प्रति किलो ही कम! वह भी पैदल, ताकि बस की टिकट पर खर्च होने वाले 5/10 पैसे भी बचाए जा सकें। हम ओल्ड राजेन्द्र नगर में रहते थे और वे राजेंद्र नगर से केवल सब्जियां खरीदने के लिए ही पुरानी सब्जी-मंडी चले जाते थे जो कि वहां से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर थी, फिल्मिस्तान सिनेमा से भी आगे!
और 2-3 भारी-भरकम थैले लिए, वहां से घर की ओर लौटते हुए, रास्ते में पुल बंगश से मसाले और फिल्मिस्तान के पास स्थित बाड़ा हिंदूराव से मटन खरीदते हुए आते। कई बार वे मुझे भी साथ ले जाते और मुझे भी यह सारा रास्ता पैदल ही चलना पड़ता, जबकि मुझे उनका ये पैदल चलने का विचार कभी पसंद नहीं आया !! इतना ही नहीं, वे प्रतिदिन अपने दफ्तर भी पैदल ही जाते! चाहे गर्मियों का मौसम हो, सर्दियों का या बारिश का! उनका दफ्तर दिल्ली-कैंट में था। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कि वह स्थान हमारे घर से कितनी दूर था, पर बड़ा होने पर मैंने जाना कि राजेन्द्र नगर और दिल्ली-कैंट की दूरी कोई कम नहीं थी।
दिल्ली कैंट के रास्ते में सड़क के दोनों ओर, जामुन के बहुत से बड़े-बड़े पेड़ थे जिन पर मौसम आने पर ढेरों जामुन लगते थे जो तेज़ हवाओं के चलने पर पेड़ों से टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाते थे। जामुन के मौसम में, पिताजी जब दफ्तर से घर की ओर आते, तो हमारे लिए इन जामुनों में से खूब सारे अच्छे-अच्छे जामुन बीन के लाना कभी नहीं भूलते। घर पर माँ इन्हें अच्छे से धो कर, इन पर काला नमक छिड़कती और हम सब भाई बहन इन्हें खूब चाव से खाते। मुझे आज भी याद है कि जब वे गर्मियों की शाम को लगभग 5-6 बजे घर लौटते, तो उन्होंने अपना सर एक रूमाल से ढका होता था, शायद तेज़ लू से बचने के लिए, जिसका एक कौना वो अपने कान के पीछे खोंस लेते थे। रूमाल का दूसरा सिरा वे अपने दांतों से पकड़ कर रखते कि कहीं तेज़ हवाएं उसे उड़ा कर न ले जाएँ। उनके एक हाथ में आमों से भरा एक बड़ा थैला होता और दूसरे हाथ से वो अपने कंधे पर रखे एक बड़े से तरबूज को संभाले होते। मुझे आज भी उनका उस चिलचिलाती धूप में भारी भरकम सामान उठा कर लगभग 8-10 किलोमीटर पैदल चलने से तमतमाया हुआ, सुर्ख लाल हुआ चेहरा इस तरह याद है जैसे कल ही की बात हो!! हम तंगी में, अभाव में रहते थे, इसका आभास मुझे काफ़ी बाद में, बड़ा होने पर हुआ। पिताजी ने हमें कभी इसकी भनक भी नहीं लगने दी थी।
दरअसल मैं बचपन से ही बहुत शरारती लड़का था और लापरवाह भी। और शरारतें भी ऐसी-ऐसी कि माँ-बाप का दिल ही काँप जाए। मैं निर्माणाधीन मकानों/इमारतों में चढ़ जाता और उनकी किसी ऊँची दीवार अथवा पहले माले की छत से कूद जाता। ये वह दौर था जब ओल्ड राजेन्द्र नगर में बहुत से लोग अपने एक मंज़िला कच्ची एस्बेस्टस की शीटों की छत वाले मकानों का पुनर्निर्माण करवाकर उन्हें पक्की छतों के दुमंजिला/तिमंजिला मकानों में बदल रहे थे। हमारे घर के पास ही शंकर रोड पर, सड़क पार एक छोटा सा मंदिर था। उसका भी पुनर्निर्माण हो रहा था, जो मेरे और मेरे कुछ मुझ जैसे ही दोस्तों का क्रीड़ा-स्थल बन गया था। दिन भर भाग-दौड़ करते और एक दूसरे को पकड़ते। पहली मंज़िल की पक्की छत पूरी हो गई तो हमारा खेल बदल गया। सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर जाना और छज्जे के किनारे खड़े होकर नीचे पड़े बालू के ढेर पर कूद जाना। ये खेल लगातार तब तक चलता रहता जब तक हम थककर चूर न हो जाते। मंदिर में आने वाले, थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हमें ऐसा करते देखते तो टोकते भी और डांटते भी! हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते, पर कुछ देर बाद फिर वही खेल शुरू हो जाता। यह हमारा पसंदीदा खेल बन चुका था। धीरे-धीरे हम जान गए कि किस समय पर मंदिर में भक्तगण कम होते हैं, हम अक्सर उसी समय आने लगे और इस तरह हमें इस टोका-टाकी से बचने का तरीका भी मिल गया।
कई बार शंकर रोड पर किसी ट्रैफिक लाइट पर बत्ती लाल हो जाने पर रुकी किसी डी.टी.सी. की बस के पीछे लगी सीढ़ी पर चढ़ जाता, दो-तीन स्टॉप आगे जाकर उतरता और वहां से घर तक पैदल वापिस आता। और भी जाने क्या-क्या अजीब-ओ-गरीब तरह की शैतानियाँ! कई बार मैं बिजली के खम्बों पर चढ़ जाता बिना यह सोचे कि उन के ऊपर लगी तारों में बिजली की तरंगें दौड रही हैं। एक बार तो जब मैं एक बिजली के खम्बे को सहारा देने वाली एक कांटेदार तार को पकड़ कर ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो हाथ की पकड़ ज़रा ढीली पड़ गई और मैं तार के साथ झूलता हुआ नीचे तक आ पहुंचा और बुरी तरह ज़ख़्मी हो गया। घर जाकर चुपचाप सोने का नाटक किया। लेकिन मेरी पीड़ा माँ से ज़्यादा देर तक छिपी न रह सकी। डांट पड़ीं, पर वो मुझे डांट ज़्यादा रही थीं या रो ज़्यादा रहीं थीं, इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल था। इसी प्रकार मैंने कई बार चोटे खाईं। और हर बार मुझे अपने माता-पिता की आँखों में गुस्से के साथ-साथ कुछ अजीब सा भाव भी दिखता, पर मुझे यह समझने में काफ़ी वक़्त लगा कि यह और कुछ नहीं बल्कि मुझे लगी चोटों का दर्द था जो उनकी आँखों को बरबस आंसुओं से भर देता था!! आज अगर पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मैंने बचपन में अपने माता-पिता को जाने-अनजाने कितनी तकलीफ़ें दी थीं।
वे धन के अभाव में अपना परिवार ज़रूर चला रहे थे, तो भी उनके कुछ सपने थे। यद्यपि उन्होंने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया। उनकी एकमात्र इच्छा जो प्रत्यक्ष रूप से ज़ाहिर होती थी, वह ये थी कि उनके बच्चों को बहुत सी चीज़ें खाने को मिलें, उनके खाने-पीने में किसी प्रकार की कोई कमी न हो। यह मुझे बाद में धीरे-धीरे पता चला कि उनके कुछ और सपने भी थे। उनमें से एक जो मुझसे सम्बंधित था, वह यह था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बनूँ। शायद वो चाहते थे कि मैं जज बनूँ। पढ़ने में तो मैं अच्छा ही था पर मेरी सारी प्रतिभा मेरी शैतानियों, जो अक्सर दुस्साहस भरी चुनौतियाँ ही होतीं थीं, के साये के तले दबी हुई थीं। उस समय के जगमोहन को जानने वाले लोगों को मेरे पिता की ये अकांक्षाएं दूर के सपना ही लगते होंगी। पर शायद मेरे पिताजी को प्रारम्भ से ही मेरे अन्दर छुपी इस प्रतिभा का आभास था और यह विश्वास भी कि एक न एक दिन यह प्रतिभा निखर कर सामने आयेगी।
मेरे बचपन से ही वे लगभग प्रतिदिन मुझे सुबह 4 बजे उठा देते थे, अपने हाथ में चाय का एक कप लिए और गाते हुए कि ‘आओ भोग लगाओ मेरे मोहन’। मैं बेमन से उठता, चाय पीता और जैसे-तैसे कोशिश करके पढ़ने बैठ जाता। हो सकता है ऐसे ही सपने उनके मेरे भाई और बहनों के बारे में भी रहे हों, ज़रूर रहे होंगे। पर मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। मुझे भी उनकी इस ख्वाहिश के बारे में पता नहीं चलता अगर उनका तबादला जम्मू में न हुआ होता और अगर मुझे कुछ वर्ष तक लगातार, गरमी की छुट्टियों में लगभग दो-दो महीने तक उनके साथ रहने का मौका न मिला होता! यद्यपि उन्होंने इस विषय में प्रत्यक्ष रूप में मुझ से कभी कोई बात नहीं की, परन्तु जाने कैसे उनकी इस ख्वाहिश को मैं जान गया था। इससे मेरे जीवन में अनायास ही कुछ परिवर्तन आने लगे थे।
मैं एक शरारती और बेपरवाह लड़के से, एक ऐसे लड़के में परिवर्तित होने लगा था जो अपने आस-पास की परिस्थितियों पर ध्यान देने लगा था। पर यह परिवर्तन अत्याधिक धीमा था। अपने प्रति जिम्मेदारी का रवैया जब तक पूरी तरह मेरे जीवन में आया, तब तक मैं स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद अपना एक वर्ष और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी अपना एक वर्ष ख़राब कर चुका था। लेकिन शायद इतना सबक मुझे जागृत करने के लिए काफ़ी था। प्रथम वर्ष की परीक्षा में जब दूसरी बार बैठा तो अच्छे अंक पाकर उत्तीर्ण हुआ। द्वितीय वर्ष का परिणाम भी अच्छा रहा, शायद मैं संभल गया था। पढ़ाई के प्रति मेरी रूचि बढ़ गई थी और मेरे शिक्षक भी मुझसे कुछ अच्छा करने की आशा रखने लगे थे, मुझे इसके लिए प्रोत्साहित भी करने लगे थे।
मैं तब शायद बी.एस.सी. (विशेष) गणित के तृतीय वर्ष में था जब पिताजी का तबादला वापिस दिल्ली में हो गया और पूरा परिवार फिर से एक बार साथ रहने लगा था। पिताजी मेरे प्रथम और द्वितीय वर्ष के परिणामों से बहुत खुश थे और इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये घोषणा कर दी थी कि अब के भी अच्छी मेहनत करना, तुम ज़रूर प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त करोगे! मैंने भी मन ही मन, बिना उनको कुछ कहे, अच्छे से पढ़ाई करने का और उनके इस सपने को साकार करने का अपने आप से वादा कर लिया था। और मैं इसमें सफ़ल भी हुआ। मैं बी.एस.सी.(विशेष) गणित की फाइनल परीक्षा में (उस समय के अनुसार) बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ था। पर तब तक बहुत देर हुई हो चुकी थी!
हुआ यूं कि पिताजी जब जम्मू से वापस दिल्ली आए तो कुछ समय पश्चात् वो बीमार रहने लगे, शायद मई या जून 1980 के आस-पास। कुछ दिन तक उन्हें घर के पास वाली सरकारी डिस्पेंसरी में दिखाया गया, परन्तु कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। उनकी टांगों और पैरों में सूजन आ गई थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। इस पर डॉक्टर ने उन्हें विलिंगडन अस्पताल में, जिसका नाम बाद में बदलकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर दिया गया था, दिखाने को कहा। उन्हें वहां दाखिल कर लिया गया और इलाज चलने लगा। पिताजी की देखरेख के लिए अकसर मैं ही उनके पास रहता था। मेरी फाइनल वर्ष की परीक्षाएं तो समाप्त हो ही चुकी थीं। मेरे छोटे भाई का अपना ही स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता था। घर से अस्पताल का रास्ता लगभग 2-3 किलोमीटर के करीब था, जो अक्सर पैदल ही तय करना पड़ता था। बस तो जाती थी पर उन दिनों बस की सर्विस कोई बहुत अच्छी नहीं थी। घर से अस्पताल के रास्ते में थोड़ा पहाड़ी या यूं कहें कि जंगल-नुमा इलाका पड़ता था, जिस पर चलने वाले लोग कम ही होते थे। ऐसे में माँ मेरी बहनों को, बेशक वे सब मुझसे बड़ी थीं, अकेला भेजना सुरक्षित नहीं समझती थी। और मुझे तो उस रास्तों पर जाना सुहाता ही था। अब तक, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं पिता की देखरेख करने की जिम्मेवारी ओढ़ने के लिए भी तैयार हो चुका था।
मुझे अच्छे से याद है कि मेरा बी.एस.सी. का परीक्षा-परिणाम 9 जुलाई 1980 को आया था। उस दिन बुधवार था। मुझे जैसे ही पता चला कि परीक्षा-परिणाम घोषित हो चुका है, मैं घर से अस्पताल जाने की बजाय, सीधा कॉलेज चला गया यह सोचकर कि कॉलेज से अपना परीक्षा-परिणाम पता कर के, वहीं से सीधा अस्पताल चला जाऊँगा और पिताजी को अपना रिज़ल्ट बता दूंगा। अच्छे नंबर आने की आशा तो थी ही! ओल्ड राजेन्द्र नगर मार्किट के बस स्टैंड पर जैसे ही पहुंचा, रूट नंबर 751 की बस आ गई और मैं लपक कर उस बस में बैठ गया। लगभग आधे घंटे में बस ने मुझे अजमेरी गेट के बस स्टैंड पर उतार दिया। वहाँ से कॉलेज पहुँचने में मात्र 5 मिनट ही लगे। कॉलेज के गेट पर ही एक-दो मित्र मिल गए। वे भी अपना रिज़ल्ट जानने ही आए थे। हम सबका उत्साह देखते ही बनता था। हम लगभग दो मिनट में ही कॉलेज के ऑफिस इंचार्ज सईद साहिब के दफ़्तर के सामने थे। ऑफिस के काउंटर पर बैठे कर्मचारी से पूछा तो पता चला कि सईद सर तो 10 बजे के आस-पास आयेंगे। समय देखा तो पाया कि अभी तो 10 बजने में लगभग तीस मिनट बाक़ी थे। हम अति-उत्साह में कुछ जल्दी ही पहुँच गए थे कॉलेज। यह आधे घंटे का समय काटना हमें बहुत मुश्किल लग रहा था। बार-बार कॉलेज का चक्कर लगाकर आते और फिर पूछते कि सर आ गये क्या? और वही जवाब मिलता, ‘बता तो दिया, 10-10:15 तक आना, उससे पहले सर नहीं आएंगे’ और हम फिर से अपना सा मुंह ले कर चले जाते, कॉलेज का एक और चक्कर लगाने। अंतत:, हमने सोचा कि चलो इस बार 2-3 चक्कर लगाकर ही पता करेंगे कि सईद सर पहुंचे या नहीं। पर अभी हम पहला चक्कर पूरा करके ऑफिस से थोड़ा ही आगे निकले थे कि पीछे से प्रशासकीय ऑफिस के चपरासी की आवाज़ आई, ‘सुनिए, सर आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं’। हम तुरंत मुड़े और सईद सर के ऑफिस के बाहर उस खिड़की पर पहुँच गए, जहाँ से वे विद्यार्थियों से डील करते थे। चपरासी ने हमें एक पंक्ति बनाकर खड़ा होने को कहा तो हम ने तुरंत वैसा ही किया। तब तक हमारी क्लास के ही सात-आठ विद्यार्थी इकट्ठा हो चुके थे और मेरा नंबर पांचवां था।
सईद सर ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। एक-एक विद्यार्थी से उसका नाम और रोल नंबर पूछते गए और उन्हें उनकी मार्कशीट देते गए। साथ ही साथ वे हर विद्यार्थी के रिज़ल्ट पर अपना कोई न कोई कमेन्ट भी देते जा रहे थे, जैसे कि ‘इस बार कुछ कम नंबर आए तेरे, खेल-कूद में ज़्यादा लगा रहा था ना’, या ‘इस बार तो अच्छे नंबर ले आई, पढ़ाई में आख़िर ध्यान लग ही गया तेरा’, इत्यादि, इत्यादि। मानो हर विद्यार्थी का पूरा इतिहास अच्छे से जानते हों। मेरा नंबर आया तो वे एकदम खामोश हो गए और मेरी मार्कशीट हाथ में लिए एक-दो मिनट तक उसे एकटक देखते रहे। मैं काफ़ी डर गया, जाने कैसा है मेरा रिज़ल्ट! मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। फिर वो अचानक अपनी सीट से उठे और मेरी मार्कशीट हाथ में लिए हुए ही कमरे से बाहर निकल कर वहां चले आए, जहाँ हम लोग खड़े थे। मैं बहुत घबरा गया। जाने क्या सामने आने वाला था? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा क्या हुआ सर? इस पर वे मुस्कुराए और मेरी मार्कशीट मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने डरते-डरते मार्कशीट देखी तो मेरी आँखे ख़ुशी से चमक उठीं, मुझे 1000 में से 671 अंक प्राप्त हुए थे और मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ था! मैंने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था!! उन्होंने मेरे दोनों कंधे पकड़ते हुए, बड़े गर्व से घोषणा की ‘हमारे हीरो ने कर दिखाया! ये न सिर्फ़ प्रथम श्रेणी में पास हुआ है बल्कि मेरे कार्यकाल में गणित(विशेष) में इस कॉलेज में इतने अंक लाने वाला पहला विद्यार्थी है! हो जाएँ तालियाँ हीरो के लिए’, उन्होंने वहां उपस्थित विद्यार्थियों तथा स्टाफ़ से मुख़ातिब होते हुए कहा और तालियां बजने लगीं। तालियों की आवाज़ सुन कर जितने भी अन्य विद्यार्थी, कर्मचारी, अध्यापक आस-पास थे, वे भी वहां आ गए और कारण जानते ही वे भी तालियाँ बजाने लगे और तालियों की आवाज़ से पूरा वातावरण गूँज उठा। मेरे लिए यह एक अभूतपूर्व अनुभव था, मेरी ख़ुशी की सीमा नहीं थी। मुझे अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी, पर जो कुछ सईद साहेब ने मेरे रिज़ल्ट के बारे में कहा, उस से मेरे पूरे बदन में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। ‘गणित(विशेष) में इस कॉलेज में इतने अंक लाने वाला पहला विद्यार्थी’ ये शब्द मुझे अविश्वसनीय तो लग रहे थे, परन्तु अत्यंत सुखदायी भी थे। सईद सर अक्सर छात्रों से बहुत अधिक बात नहीं किया करते थे, परन्तु आज जितना स्नेह और सराहना का जो भाव उन्होंने मेरे प्रति दिखाया, उस देखकर मैं हतप्रभ रह गया!
परन्तु मैं अब शीघ्र ही निकलना चाहता था, पिताजी के पास अस्पताल पहुँचने के लिए। पर संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था। मैंने थोड़ा और इंतज़ार करना ठीक समझा। जैसे ही वे अन्दर गए और पंक्ति में खड़े अन्य विद्यार्थियों की मार्कशीट्स उन्हें दे दीं तो मैंने हिम्मत जुटा कर उनसे कहा कि सर क्या मैं जा सकता हूँ? ‘अरे जल्दी क्या है थोड़ा रुको, मिठाई मंगवाते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं तुम सब का’। मैंने क्षमा मांगते हुए उन्हें अपनी मजबूरी बताई कि पिताजी बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं; मैं जल्दी से जल्दी उन्हें अपना रिज़ल्ट बताना चाहता हूँ। यह सुनते ही वे बोले कि तो पहले बताना था न, जाओ जल्दी से दो उन्हें यह खुशखबरी! उनकी यह बात सुनते ही मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मित्रों से विदाई ली और तेज़ी से अस्पताल जाने के लिए निकल गया।
कॉलेज से बाहर निकलते ही मैं समझ गया था कि मुझे पैदल ही जाना होगा। किसी ऐसी बस के बारे में मैं जानता नहीं था जो मुझे वहाँ से सीधा विलिंगडन अस्पताल तक ले जाए और ऑटो रिक्शा में जाने के पैसे मेरे पास थे नहीं। सो, कॉलेज के गेट से बाहर निकलते ही मैं दाएं मुड़ा, दायीं ओर शीला सिनेमा/पहाड़ गंज की तरफ़ जाने वाली पहली सड़क को छोड़ते हुए, दायीं ओर की दूसरी सड़क पर चल पड़ा जो मिंटो ब्रिज के नीचे से होकर सीधे क्नॉटप्लेस के आउटर सर्किल की ओर ले जाती थी। कॉलेज से अस्पताल की दूरी कम नहीं थी और मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। इसलिए मैं जितना संभव था उतना तेज़ चल रहा था, या यूं कहें कि लगभग दौड़ ही रहा था। रास्ते में 40-45 साल के एक साइकिल सवार ने अपनी साइकिल धीमी करते हुए पूछा कहाँ तक जाना है बेटा, काफ़ी जल्दी में लगते हो? मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने साइकिल रोक कर यह कहते हुए मुझे साइकिल पर बैठने के लिए कहा कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ दूंगा। मैं झट से उनकी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गया और उन्होंने मुझे मिंटो ब्रिज से थोड़ा पहले छोड़ दिया, उन्हें शायद बाएं मुड़ कर आई.टी.ओ. की तरफ़ जाना था। मैं उन्हें धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। मेरे लिए इतनी मदद भी काफ़ी थी।
लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर ही क्नॉटप्लेस का आउटर सर्किल था। मैं बायीं ओर मुड़ा और अपनी लक्ष्य की ओर बढने लगा, कभी तीव्र गति से चलते हुए और कभी दौड़ते हुए। हाँ, जब कोई सड़क पार करनी होती तो रुकना पड़ता और सावधानी से ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करना पड़ता। अभी अधिकतम दुकानें/शो-रूम इत्यादि बंद थे। अत: मैं निर्बाध गति से आगे बढ़ते हुए, काफ़ी कम समय में ही रीगल सिनेमा तक पहुँच गया। थोड़ा थक गया था तो पटरी किनारे पड़े एक पत्थर के बेंच पर बैठ गया और अपनी फूली हुई सांस को सामान्य करने का प्रयास करने लगा। मैं लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुका था। ‘अब कुछ ही समय बाक़ी था उस घड़ी के आने में जब मेरी मार्कशीट पिताजी के हाथ में होगी और उनका चेहरा हर्ष से खिल उठेगा’ यह ख्याल आते ही मैं उठ खड़ा हुआ, प्लास्टिक के कवर में से अपनी मार्कशीट निकाली, उसे एक बार पुन: निहारा और फिर से अन्दर रख दिया। थोड़ा और आराम चाहिए था मेरी थकी हुई टांगों को, पर अस्पताल पहुँचने की बेचैनी उठ कर शीघ्र-अति-शीघ्र पिताजी के पास पहुँचने की दरकार कर रही थी।
मैं उठा और एक बार फिर से चलने को तैयार हो गया। बाएं मुड़ते ही कुछ कदम की दूरी पर रिवोली सिनेमा था। सामान्य समय होता तो मैं रीगल और रिवोली सिनेमा के बाहर लगे, उन पर चल रहे और आने वाले चलचित्रों के पोस्टरों को ज़रूर निहारता। पर आज तो मन किसी और ही धुन में था। मानों मैं हवा में उड़ रहा होऊं। मैं हनुमान मंदिर से आगे बढता हुआ कब बंगला साहिब गुरुद्वारे से भी आगे गोल डाकखाने के गोल चक्कर तक पहुँच गया, पता ही नहीं चला! बस अब इसे पार करना था और उसके बाद सामने ही 7-8 मिनट की दूरी पर विलिंगडन अस्पताल का एंट्री गेट! मेरे सब्र का बाँध टूट रहा था। मैंने एक बार फिर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया और ठीक तीन मिनट में ही मैं अस्पताल के गेट पर था। मैं गेट पर पहुँच कर रुका, दो-तीन गहरी साँसें लेकर खुद को ज़रा सामान्य किया, जिस वार्ड में पिताजी का बेड था उस वार्ड की ओर बड़ा, कॉरिडोर में ही अपनी मार्कशीट निकालकर दायें हाथ में ले ली और उसे हवा में लहराते हुए वार्ड में पिताजी के बेड की तरफ़ जाते हुए ख़ुशी से उन्हें पुकारा ‘बाऊजी, मेरा रिज़ल्ट आ…. गया….’। हम भाई-बहन अपने पिताजी को बाऊजी कहकर ही संबोधित करते थे। पर मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, इस से पहले ही मेरी नज़र उनके बेड पर पड़ी, बेड खाली था, उस पर एक सफ़ेद चादर करीने से बिछी हुई थी, जिस पर एक भी सलवट नहीं थी, मानो अभी-अभी बिछायी गई हो। मेरा दायाँ हाथ स्वत: ही नीचे आ गया। मैंने इधर-उधर देखा तो एक वार्ड बॉय नज़र आया, उससे पूछा भैया इस बेड पर जो मरीज़ थे, कहाँ गए! उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया है क्या? वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो फिर वापिस आ गया, उस वार्ड के डॉक्टर-इंचार्ज के साथ। डॉक्टर साहेब से भी मैंने वही प्रश्न पूछा, मेरे पिताजी इस बेड पर थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है क्या? डॉक्टर साहेब अपने दोनों हाथ मेरे कन्धों पर रखते हुए बोले, ‘वी आर वेरी सॉरी यंग बॉय, वी कुड नॉट सेव हिम; क़रीब आधा घंटा पहले उनका देहांत हो गया!’ क्या? नो!! मेरा मुंह खुला का खुला रह गया! ऐसा लगा कि जैसे मैं निष्प्राण हो गया हूँ! खड़ा रहना भी दूभर लग रहा था। पास पड़ी एक कुर्सी का सहारा लिया और फिर धीरे से उस पर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चारों और एक नीरवता सी छा गई हो, कभी न ख़त्म होने वाली एक गहरी खामोशी! डॉक्टर सा’ब कुछ बोल रहे थे पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उन्हें देख रहा था या कहीं और, मुझे नहीं पता था। मुझे होश तब आया जब डॉक्टर सा’ब ने मुझे झकझोरते हुए कहा ‘आपकी ये मार्कशीट नीचे गिर गई है’। मैं झट से खड़ा हो गया। देखा तो मेरी मार्कशीट उनके हाथ में थी और वो उसे गौर से देख रहे थे। मुझे खड़ा देख उन्होंने मार्कशीट मेरे हाथ में थमाई, एक हाथ से मेरी पीठ थपथपाई और बहुत धीमे और संयमित स्वर में ‘आल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर’ कहते हुए वार्ड से बाहर निकल गए।
यह विचार मुझे हमेशा सालता रहा है कि यद्यपि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर पाया पर वह इसे पूरा होते देख नहीं पाए। काश मैं अस्पताल थोड़ी जल्दी पहुँच जाता और वो मेरा रिज़ल्ट देख पाते। पर यह हो नहीं पाया! काश वो थोड़ा समय और रहते हमारे साथ! बरसों तक मुझे इस का मलाल रहा है और रहेगा। अपने माता-पिता को अनेक दर्द और तकलीफें देने के बाद, मैं कुछ समझा, संभला और अपनी जीवन शैली को अनुशासित कर पाया। तब जाकर मैं वहां तक पहुंच पाया जहाँ मैं आज हूँ! काश मेरे पिताजी आज हमारे बीच होते और देख पाते कि मैं वास्तव में बदल गया हूँ और यथोचित रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। माता जी ने तो फिर भी उसके बाद का समय भी देखा और अपने सभी बच्चों की सफलताएं भी देखीं, पर पिताजी इस सब से महरूम रह गए।
वो आज हमारे साथ होते, तो वे भी उन सुविधाओं का आनंद ले पाते जो अगर आज हमें उपलब्ध हैं तो केवल अपने माता-पिता के कठिन परिश्रम और उनके आशीर्वचन की वजह से। वो हमारे साथ हमारी कार की सवारी का आनंद लेते; मेरे पुत्र सूर्यांशू और उसके परिवार से मिलते। वो मेरी पत्नी संतोष से तो मिले थे पर तब तक हमारा विवाह नहीं हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वे आज होते तो संतोष के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना बड़े चाव से खाते। वो कितने आनंदित होते यदि वो देख पाते कि उनके सभी बच्चे सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब देखने के लिए काश वो आज हमारे साथ होते!
__________________________________________________________________
परिचय
डॉ जगमोहन राय ‘सजल’
दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य) से 31 जुलाई, 2023 को गणित के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवा-निवृत।
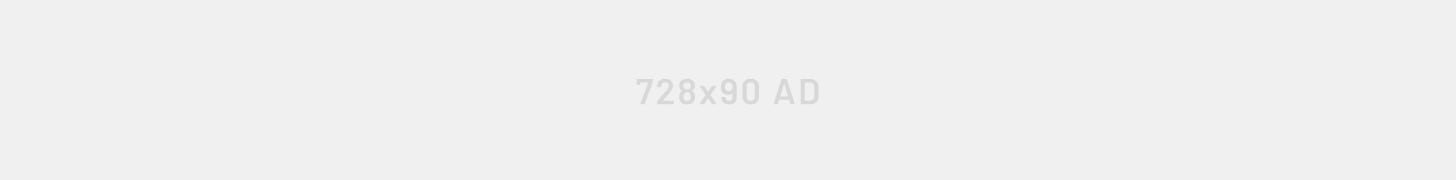
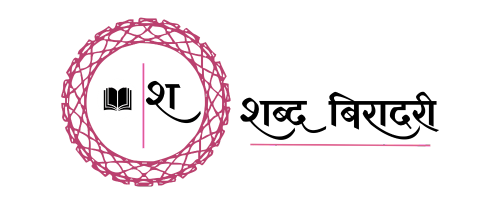

बहुत ही मार्मिक संस्मरण ✨
काश! शब्द काश कहने के लिए ही बना है। आपने बहुत मार्मिक संस्मरण लिखा। आपकी तरह ही हमारा परिवार रहा और माता पिता जी को बहुत मेहनत करते देखा। पिता जी इतना सुख देखकर नहीं गए। आपके पिता जी के संघर्षों को पढ़कर मन द्रवित हो गया। आपके जीवन के अनछुए पहलुओं का परिचय मिला। अक्सर फिल्मों में ऐसी घटनाएं घटते देखते हैं, आपके जीवन का यथार्थ भी वैसा ही रहा। पिता जी की स्मृति को नमन 🙏🙏
काश! शब्द शायद इसी तरह अफसोस करने के लिए ही बना है, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। आपने बहुत मार्मिक संस्मरण लिखा। आपकी तरह ही हमारा परिवार रहा और माता पिता जी को बहुत मेहनत करते देखा। पिता जी इतना सुख देखकर नहीं गए। आपके पिता जी के संघर्षों को पढ़कर मन द्रवित हो गया। आपके जीवन के अनछुए पहलुओं का परिचय मिला। अक्सर फिल्मों में ऐसी घटनाएं घटते देखते हैं, आपके जीवन का यथार्थ भी वैसा ही रहा। पिता जी की स्मृति को नमन 🙏🙏