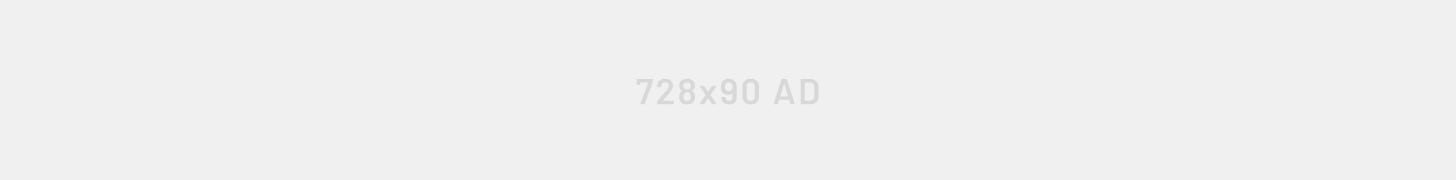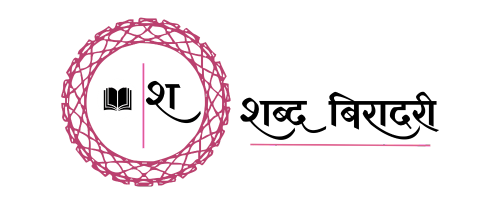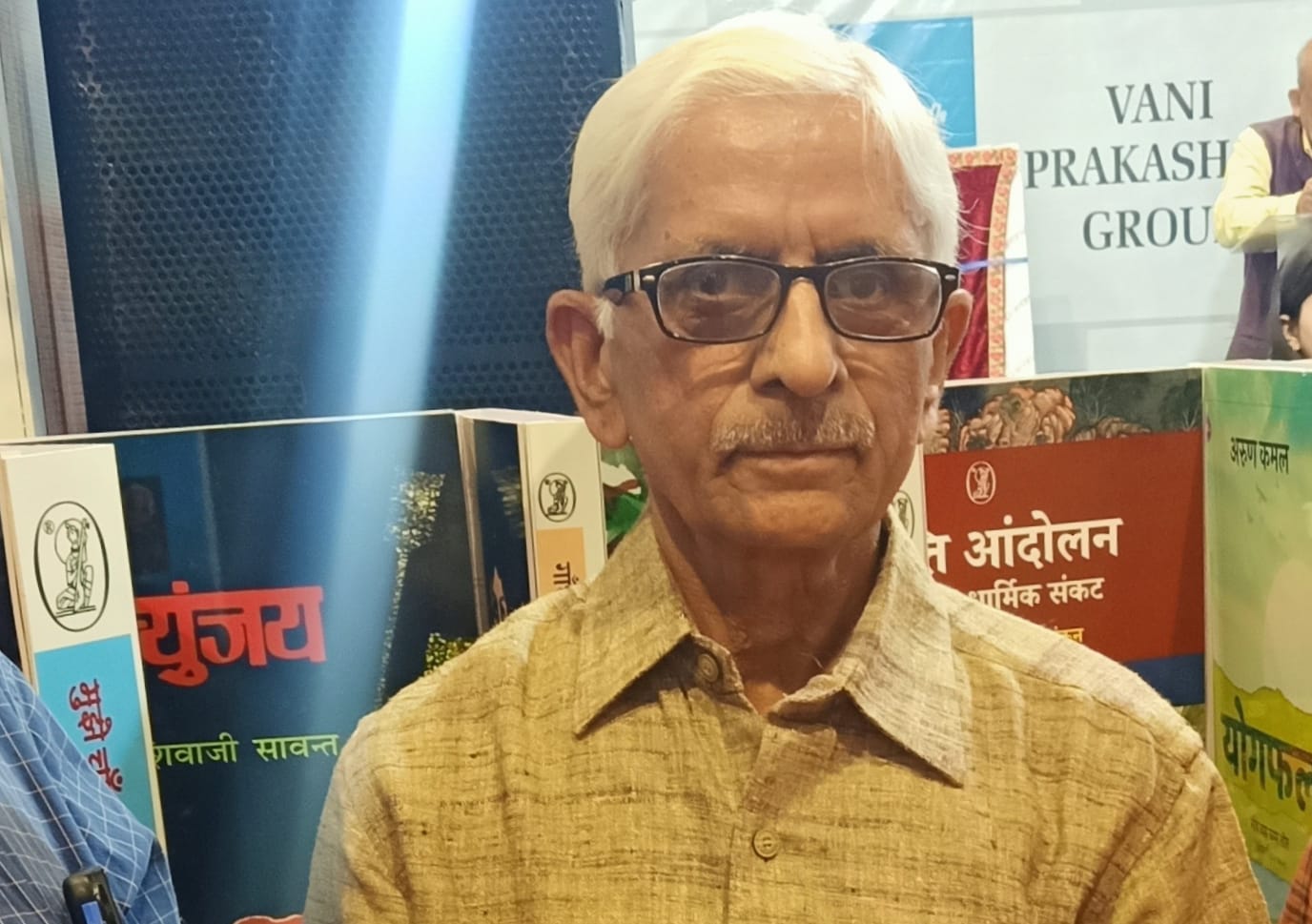
ज़िन्दगी किस शय का नाम है? ज़िन्दगी शायद सफ़र का नाम है। इस सफ़र में चलते हुए सिर्फ जूते ही नहीं घिसते , पाँव की ऐड़ियाँ भी घिस जाती है।
वक़्त के साथ दौड़ने की हसरत और वक्त से पिछड़ जाने की तड़प !
कनॉट प्लेस के खाली बेंच पर बैठा मैं, अकेला और खाली ! खाली जेब जिंदगी की। पता नहीं कहाँ खुशियों का चिल्लर गिरा और कहाँ दुख के खोटे सिक्के !
कनॉट प्लेस के बरामदे में घूमते हुए मैं थक-सा गया हूँ। खाली और अकेले बेंच पर आ बैठा हूँ। यहाँ लोग अकेले होते हैं, बेंच अकेले नहीं होते। बेंच पर लोग बैठे होते हैं, अपने सीने में इच्छाओं के अधबुझे जुगनू लेकर !
लेकिन आज मुझे वो बेंच मिल गयी है जो अकेली है और खाली है।
वक्त अपनी तीसरी आँख से हैरान होकर मुझे देख रहा है। और सोच रहा है कि बेंच ज्यादा अकेली है या मैं।
बेंच जब अकेली और खाली होती हैं तो वो किसी के आने का इंतजार करती नज़र आती हैं।
बेंच को जैसे साथी मिल गया हो और मुझे भी। मैं थका हुआ-सा जब बेंच पर बैठा तो बेंच ने अपनी बाहें पसार कर मेरा स्वागत किया। वो शायद जान गयी थी कि मैं थक गया हूँ। अजीब बात है कि पहले लोग बाहें पसार कर मिलते थे, अब बेंच मिलते हैं।
बेंच बोल सकती तो मैं उससे बातें करता। मैं उसे बताता कि तीस साल पहले मैं यहाँ, दिल्ली में, नौकरी करने आया था और आज रुखसत हो रहा हूँ।
तीस साल पहले जब मैं दिल्ली में आया था, तब मैं अकेला था और आज जब मैं सेवानिवृत हो रहा हूँ तो अकेला हूँ । तीस साल पहले मैं जवान था अब लगभग बूढ़ा ! मैं ही नहीं, मेरी तमाम हसरतें, चाहतें और जिज्ञासाएँ भी बूढ़ी हो चुकी हैं।
वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। तीस साल पहले मेरी जेब में नियुक्ति पत्र था और आज सेवा निवृति का पत्र है।
मेरी कमीज़ की एक जेब में रिटायरमेंट का लैटर है और दूसरी जेब में, कुछ लाख रूपये का चैक। मैं रिटायरमेंट लैटर को कई बार देख चुका हूँ। हर बार इस फंतासी के साथ कि रिटायरमेंट लैटर, अपायंटमेंट में बदल जाए शायद ।
मैं आज के दिन की कल्पना करता तो मन ही मन भयभीत हो जाता। दफ्तर से हमेशा के लिए रुखसत। विदा नहीं, अलविदा !
आज मैं अपने दफ्तर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊँगा। उन स्थानों को छोड़ना कितना कठिन होता है जहाँ आप सालों- साल रहे हों। मैं जानता था एक दिन चल दूंगा कंधे पर झोला टांग कर अपने छोटे से शहर में। शहर, जिसका नाम उम्मीदनगर है।
मैं बेंच से उठा हूँ और कनॉट प्लेस के बरामदे में चला आया हूँ। अकेला घूम रहा हूँ। ज़िन्दगी की रेलगाड़ी के तमाम हमसफर, चेन खींचकर उतर गए हों जैसे।
और मैं साँसों के धागे को दुरूस्त करता । वक़्त के पुराने खतों की इबारत को याद करता। यादों के आतिशदान की राख से खेलता। अपनी नम आँखों के पानी को उँगली के पोर पर रखकर, मुस्कराने की कोशिश करता।
मैं आज रिटायर हो जाऊँगा। हो जाऊँगा नहीं, हो चुका हूँ। मैं जब आफिस में था तो उन्होंने बड़ी रेशमी ज़बान में कहा था कि मैं, लैपटॉप, फाइलें, लैटर सब जरुरी डॉक्युमेंट्स उन्हें डिपॉजिट करा दूं उन्होंने सब कुछ ले लिया था , एक स्टेपलर मशीन मुझे दे दी थी कि मैं कुछ स्टेपल करना चाहूँ तो कर सकूँ ।
यह पुरानी स्टैपलर मशीन, दफ्तर की तरफ से दिया गया गिफ्ट था।
काश, मैं इस स्टैपलर मशीन से, अपने तीस साल का कालखण्ड स्टैपल कर पाता। काश, मैं दिन, महीने, साल, मिनट, घंटे स्टैपल कर पाता। काश, मैं पुराने समय का जज़्बा, दोस्ती की तपिश, चुहलबाज़ियाँ, ठहाके और चाय की चुस्कियों को स्टेपल कर पाता।
ऑफिस की तरफ से दिया गया स्टैपलर अनमोल नजराना था। वो सोच रहे थे कि मैं डॉक्युमेंट्स स्टेपल करूँगा। लेकिन मैं तो तीस साल का कालखण्ड स्टैपल करना चाहता था।
मैं अपने छोटे से शहर उम्मीद नगर से रोजाना दफ्तर आता था। कनॉट प्लेस में कम्पनी के बहुत सारे दफ्तर थे। ट्रांसफर होती रहती। दफ्तर बदलते रहते। दफ्तर बदल जाते। कलीग बदल जाते । वर्किंग बदल जाती और सिस्टम बदल जाता।
मैं डेली अप एण्ड डाउन करता। उम्मीद नगर से नई दिल्ली। मैं छोटे शहर से निकलकर बड़े बहुत बड़े शहर में समा जाता।
इस बड़े शहर की बहुत सारी खूबियाँ थीं।
यह बड़ा शहर, यानी दिल्ली ! दिल्ली ऊँचा सुनती थी। दिल्ली किसीको खातिर में नहीं रखती थी। दिल्ली में जो भी आता अपनी पहचान गुम कर बैठता। दिल्ली, अच्छे भले इंसानों को भीड़ में बदल देती और भीड़, सड़कों पर रेंगती हुई। जैसे कटी पतंगों का लश्कर हो।
कम्पनी का दफ्तर, डिविजनल ऑफिस है, जनपथ पर मैं इसी दफ्तर से सेवा निवृत हुआ हूँ। शाम तक मेरे सारे ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएंगे। मैं हमेशा के लिए दफ्तर छोड़ दूंगा और राजधानी दिल्ली भी।
दफ्तर में मैं कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। मेरे होने का मायने थे लेकिन अचानक क्या हुआ कि मेरी उपयोगिता खत्म हो गई। ऐसा बरताव, जैसे मैं यहाँ कभी था ही नहीं। लैपटॉप, फाइलें, पेपर सब ले लिए गए हैं। मुझे कहा गया था कि किसी फाइल को न खोलूँ।
सुबह ही मेरा पासवर्ड, आईडी लैपटॉप पर ब्लॉक कर दिया गया था। मुझे कहा गया था कि मैं ‘ आई डी’ लॉगइन न करूँ। कम्पनी रूल्स हैं।
थोड़ी देर बाद मेरी टैबल किसी दूसरे एम्प्लोई को दे दी गई थी। मुझे उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया था जो यतीम लग रही थी। कुर्सी यतीम और मैं लावारिस !
जिस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता था और वो कॉर्नर में रखी रहती थी। वही कुर्सी मेरे लिए थी। मैं कुर्सी पर बैठा था सोच रहा था किसीने इस कुर्सी से भी खड़ा कर दिया तो कहाँ बैठूंगा
ऑफिस में सबके सब टेबल पर रखे लैपटॉप के सामने थे। मैं अपने तमाम कलीगों को रूक-रूक कर देख लेता था। हो सकता है उन्होंने भी देखा हो मुझे आज सब बहुत बिज़ी नजर आ रहे थे। कल तक तो सब नॉर्मल था। आज अचानक इतना अधिक ‘वर्कलोड’ ‘कि लैपटॉप से नज़रें ही नहीं हटती थीं।
कल तक यह मेरा दफ्तर था। और आज मैं यतीम कुर्सी पर बैठा था। चीजें कितनी जल्दी छिन जाती हैं। पता ही नहीं चलता। पाँव के नीचे की जमीन और सर के ऊपर का आसमान, कुछ भी अपना नहीं रहता।
कितनी जल्दी ऊब गया हूँ पहले मैं नहीं ऊबता था। आज ऊब गया हूँ । मुझे चार या तीन बजे रिलीव होना है। तब तक यहाँ बैठा हुआ हूँ , अपने आपसे युद्ध लड़ता रहूंगा।
क्यों न कनॉट प्लेस के बरामदे में घूमता रहूँ। इन तीस सालों में मैने हजारों बार, कनॉट प्लेस के बरामदे में चक्कर लगाए।
मैं जब कुर्सी छोड़कर बाहर निकलने लगा था तो कहीं पीछे से धुंधली-सी आवाज़ आई थी “फेयरवैल” फिर वो आवाज डूब गई थी। कई बार आवाजें भी उन कश्तियों की तरह होती हैं, जिन में छेद होते हैं और वो डूब जाती हैं।
क्या पता मेरे आफिस के कलीग फेयरवैल पार्टी करना चाहते हो। खुशफहमियाँ कितनी दिलकश होती है।
मैं कनॉट प्लेस के बरामदे में खड़ा हूँ। एक चक्कर लगा लेने, बेंच पर बैठ लेने के बाद मैं फिर से बरामदे में आ गया हूँ।
कनॉट प्लेस के बरामदे में मैं आखिरी बार घूम रहा हूँ। निरपेक्ष भाव से, सरसरी तौर से, शोरूम की तरफ देखता हुआ मैं, बरामदे में चल रहा हूँ।
पहले मैं बड़ी हसरत से शोरूम के बाहर, शीशे के शो केस देखता था। मैं कनॉट प्लेस के बरामदे में रोज़ाना आ जाता। पहले दफ्तर ट्रॉपिकल बिल्डिंग में था। फिर, राजेन्द्र मेंशन में ऑफिस, फिर सिंघिया हाउस में और बाद में … जनपथ पर ऑफिस !
मैं रोजाना कनॉट प्लेस के बरामदे में चला आता और विस्मित भाव से शो केस देखता रहता ।
मैं अमीर लोगों को देखता रहता। वो अपनी कारें पार्क करके, हिकारत की ऐनक और अहंकार का चेहरा लगा कर, कारों से उतरते। मैं उन्हें देखता रह जाता। वो बड़े लोग। दुख रहित लोग । संवेदना रहित लोग । आत्मीयता रहित लोग। वो गोरे चिट्टे । चमचमाते जूते। चमचमाते चेहरों वाले। वो अंग्रेजी में साँस लेते। अंग्रेजी में छींकते। वो अगर हँसते तो अंग्रेज़ी में हँसते। मर्द परफेक्ट मैन’ की तरह होते और उनके साथ चल रही स्त्रियाँ, खूबसूरत, ब्यूटी पार्लरों से निकली, बेहद कोमल, नाजुक ! ‘हैंडिल विद केयर’ जैसी एहतीयात के साथ-साथ चल रहे मर्द उनको संभालते हुए। वो अमीर लोग किसी शो रूम में चले जाते या फिर, होस्ट, युनाइटिड कॉफी हाउस, वोल्गा विम्पी या रैम्बल में प्रविष्ट हो जाते।
ऐसे बड़े लोगों के लिए, रेस्तराओं के बड़े दरवाजे खुलते । दरवान आदाब बजाते ।
एक दिल्ली, ऐसे बड़े दरवाजों के उस पार थी। और एक दिल्ली वो, जिसमें मैं था, चाहतों के मुचड़े हुए रूमाल पेंट की जेब में रखे हुए।
यह तब की बात है जब मैं जवान था। तब मैं कनॉट प्लेस के बरामदे में दाखिल होता बरामदे के ऐन नुक्कड़ में पनवाड़ी का ठीया था। मैं पनवाड़ी से दो सिगरेटें खरीदता। विल्ज़ नेवीकर, पनामा या कैप्सरन मैं एक सिगरेट जेब में रखता। दूसरी सुलगाता । सिगरेट सुलगाने का अंदाज बड़ा निराला था। पानवाले के ठीये के पास, एक पतली-सी रस्सी सुलग रही होती। सब लोग अपनी सिगरेट को उस रस्सी से सुलगाते। मैं भी अपनी सिगरेट उस से सुलगाता।
मैं कनॉट प्लेस में सिगरेट पीते हुए, धुआँ छोड़ते हुए, मस्त चाल चलते हुए, जवान खूबसूरत स्त्रियों को देखते हुए, कनॉट प्लेस का सर्कल पूरा करता । फिर पलटता। ए ब्लॉक से एन ब्लॉक तक का चक्कर लगा लेता। यह मेरा जवानी का जोश, जश्न और मस्ती भरा खेल होता। मैं बैंगर्ज पेस्ट्री शॉप पर ठिठकता। मैं पोस्ट आफिस के सामने जरा-सा रुकता । पोस्ट आफिस को हिन्दी में ‘डाकघर’ लिखा देख कर मैं मन ही मन मुस्कराता। यानी, चिट्ठियों का घर – डाकघर ।
फिर मैं अपने दफ्तर चला जाता ।
बहुत साल पहले, यही कोई तीस साल पहले मेरी दिल्ली की एक कम्पनी में नौकरी लगी तो मुझे दिल्ली विस्मित करती। बाजार आकर्षित करते। शो रूम डराते। शो केस अपनी तरफ खींचते। सेलर, रैम्बलर, वोल्ग, एम्बेसी, रेस्टोरेंट, होस्ट ,यूनाइटेड कॉफी हाउस मैं बरामदे से गुजरते हुए देखता रह जाता
रेस्टोरेंट, होस्ट, यूनाइटेड कॉफी हाउस, मै बरामदे से गुज़रते हुए देखता रह जाता। कई बार दरवाजा जरा-सा खुलता तो मैं रेस्तराँ के भीतर झाँकने की कोशिश करता।
मेरी जिज्ञासाएँ महानगर को जानना चाहती थीं।
मेरी हसरतें उड़ना सीख रही थीं। मेरी चाहते, मेरे दिल में खलबली पैदा करतीं। मैं सहम जाता।
तब मैं अकेला होता। कनॉट प्लेस के बरामदे में घूमता हुआ, सहसा-सहमा हुआ मैं।
तब मैंने एक तरकीब ईजाद की थी। मैं नौजवान था। मेरी जिज्ञासाएँ प्रबल थीं। मेरी चाहतें अधिक। मेरी तंखा कम थी और मैं अमीरों जैसा दिखना और होना चाहता था। तब, हाँ, तब मैंने एक तरकीब ईजाद की थी। मैं कनॉट प्लेस के बरामदे में आता। दो सिगरेटें खरीदता। कभी विल्ज़ कभी कौर स्केयर, कभी जैसलमेर, कभी इंडिया किंग ! इंडिया किंग की सिगरेट बेशक थोड़ी मँहगी होती। लेकिन ‘किंग’ होने का फितूर तो पैदा कर ही देती की। मैं पफ लेता धुआँ छोड़ता। यह धुआँ मैं तमाम अमीरज़ादों पर छोड़ता जो बरामदे से गुज़रते तो लगता जैसे अहंकार का परफ्यूम मल कर आए हो।
तब, मेरी खस्ताहाल सौ सौ के दो या तीन नोट होते और कुछ चिल्लड़ ।
चिल्हर को मैंने हमेशा जेब में रखा है। पता नहीं क्यों ? शायद इसलिए कि जेब में खनकते सिक्के मुझे अच्छे लगते थे। या फिर इसलिए कि राजधानी में मेरी औकात, चिल्लड़ जैसी थी।
मैं दो सिगरेटें पीते हुए, कनॉट प्लेस के बरामदे का चक्कर लगा लेता था। न कोई मेरी परवाह करता न मैं किसी की।
मैंने ये अंदाज खुद पैदा किया था कि कंगाली के बावजूद, अपने होने का रुतबा पैदा करो। आप सिगरेट पीओ जुएँ से खेलो। और कनॉट प्लेस जैसे बाजार को एहसास करा दो कि फकीरी के ठाठ अद्भुत होते हैं।
बिलकुल शुरू में थोड़ा-सा बरामदे में घूमता। फिर सेंट्रल पार्क के किसी बेंच पर जा बैठता। मेरी रेलगाड़ी साढ़े नौ पहुँच जाती और दफ्तर का टाइम साढ़े दस तक का होता।
सर्दियों में मैं धूपवाले बेंच पर बैठता, गर्मियों में पेड़ के नीचे जो बेंच होता, वहाँ जा बैठता। सुबह का वक्त और तीस साल पहले का समय सेंट्रल पार्क खामोश और लगभग खाली होता। सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस के बीच जो सड़क होती, उस पर भी बहुत कम आमदरफ्त होती।
सेंट्रल पार्क में जाने के लिए थोड़ी-सी एंट्रेंस थी। एक चकरी को घुमाकर पार्क में जाया जा सकता था। चकरी से कई तरह की आवाजें आतीं, जो अच्छी लगतीं।
मैं चकरी के पासवाले बेंच पर बैठता जो अक्सर खाली होती। उधर से पॉलिशवाले लड़के, कुलचेवाले, मसालची, कान साफ करनेवाले, चायवाले, सब उस चकरी को लाँघ कर गुज़रते। जाते हुए वो मुझे देखते, मैं उनको।
एक दिन एक पॉलिशवाले लड़के ने पूछा, ” बाबू, पॉलिश कर दूं जूतों की ?”
मैं जानता था वो सब मँहगे पॉलिशवाले थे। बीस-तीस तो पॉलिश के ले ही लेते थे। लेकिन मैं उसे इन्कार न कर सका। उसने पॉलिश करने में, कम-से-कम दस मिनट लगाए। पुराने खटारा जूते ऐसे चमकाए जैसे नये हों।
मैंने पॉलिश के पैसे पूछे उस लड़के ने एक रूपया माँगा।
“सिर्फ एक रुपया ?” मैं हैरान हुआ।
“बाबू, तुम्हें हम रोज़ देखते हैं। तुम हमारे दोस्त हो।”
“तो फिर एक रूपया किसलिए?”
“ बाबू, बोहनी नई हुई,इसलिए।”
मैंने उसे पाँच रूपये दिए। वो मुस्कराया। पाँच के नोट को उसने माथे से लगाया और चला गया।
आज जब मैं आखिरी दिन बरामदे से गुज़र रहा हूँ और सेंट्रल पार्क को देख रहा हूँ। बहुत भीड़ है। खाते-पीते ,पिकनिक मनाते लोग हैं।
मुझे वो बाकया याद आ रहा है जब सारे के सारे पॉलिशवाले। मालिशवाले, चायवाले, भटूरे-कुलचेवाले, घास पर दायरा बनाकर बैठ गए थे।
वो अपने किसी साथी का जन्म दिन मना रहे थे। और गा रहे की
नित खैर मॅग्गा सोड़ियाँ मैं तेरी दुआ न कोई होर मंगदी
तेरे पैरों विच अरवीर होवे मेरी,दुआ में कोई होर मंगदी
एक लड़के के हाथ में ठीकरियाँ के टुकड़े को वो उन ठीकरियों को उँगलियों में फंसा कर वाद्य यन्त्र का काम ले रहा था।
एक वक्त ऐसा आया जब दस के दस लड़के एकसाथ गा रहे थे- “दुआ न कोई होर मंगदी”!
“सादी खुशियाँ वी लग जाणं सारी, दुआ न कोई है मंगदी”
मुझे उस दिन महसूस हुआ था कि गरीब दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं।
मैंने बीस रूपये पॉलिश वाले को दिए तो वो ज़मीन से उठा। मेरे घुटने को छूकर आभार व्यक्त किया।
पता नहीं वो चायवाला, वो पॉलिशवाला कहाँ होंगे ? आज जब मैं आखिरी बार कनॉट प्लेस के बरामदे में घूम रहा हूँ तो सेंट्रलपार्क के वो पुराने दिन और फ़ाकाकशों का लोकगीत याद आ रहा है “नित खैर मँगा सोंड़ियाँ मैं तेरी दुआ न कोई होर मंगदी।” उस पॉलिशवाले का मेरे घुटनों को हाथ लगाकर जाना मुझे याद आ रहा है। वो मेहनतकश गरीब लड़के, कनॉट प्लेस के बरामदे और सेंट्रल पार्क में घूमते रहते थे । उनकी नजर लोगों के चेहरों पर नहीं, जूतों पर होती थी।
बहुत साल बाद, अब, जब मैं साठ साल का हो चुका हूँ और आखिरी बार, कनॉट प्लेस के बरामदे में घूम रहा हूँ और याद कर रहा हूँ अपनी जवानी के वो दिन जब मैं एक के बाद दूसरी सिगरेट पीता, बिंदास अंदाज में। फिर मुझे सिगरेट पीना बोर करने लगा। मैंने सिगरेट छोड़ दी।
आज मैं छः बीस की रेलगाड़ी से रवाना हो जाऊँगा। मैं तो चला जाऊँगा। मेरा किरदार पीछे रह जाएगा। वो लावारिस किरदार, मुझे ढूँढता रहेगा हमेशा। और मैं उसे छोड़कर, अपने शहर में चला जाऊंगा।
कितना अच्छा लगा है मुझे, बोल्गा रेस्तराँ के बाहर खड़े दरबान ने मुझे नमस्ते की है। कोई तो है जो इस बड़े, भव्य और बेलिहाज़ बाज़ार में मुझे जानता है। उसने कई बार मुझे देखा होगा आज उसने मुझे नमस्ते की है। यह उसकी पहली और आखिरी नमस्ते हैं। जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं राजधानी को छोड़कर चला जाऊँगा। उसकी नमस्ते में, अलविदा की आवाज भी शामिल है।
मैंने मोबाइल को जेब से निकालकर तीन बार देख लिया है। क्या पता अकाउंट्स विभाग ने मेरे ड्यूज़ क्लीयर कर के चैक बना दिया हो। मैं सोच रहा हूँ शायद वो फोन करके बुला लें कि आपका चैक तैयार है। लेकिन, अभी तक फोन नहीं आया।
एक दुर्बल-सी, डरी हुई उम्मीद भी है मेरे दिल में कि क्या पता फेयरवैल पार्टी अरेंज कर रहे हो। बेशक, ऐसी कोई परपंरा तो नहीं है।
अभी तीन महीने पहले एक कलीग रिटायर हुआ था। मैंने अपने सीनियर से कहा था कि फेयरवैल पार्टी अरेंज करते हैं।
उसने गुर्राती हुई नज़रों से मुझे देखते हुए कहा था, बी प्रोफेशनल, नॉट इमोशनल !”
यहाँ लोग, प्रोफेशनल का पाठ इतना रट चुके थे कि जिन्दगी के स्पेलिंग ही भूल गए थे।
किसी कलीग को विदा करते हुए छोटी सी टी पार्टी अरेंज करना क्या इमोशनल होना था। जी हाँ होना था। कोई कलीग हमारे बीच से विदा होकर, चैक जेब में डालकर चला जाए और कोई ऑल दि बेस्ट – बोलते हुए रुक जाए।
मैं जानता हूँ मेरे दफ्तर के मेरी रिटायरमेंट की फेयरवैल पार्टी नहीं करेंगे। किसी कलीग ने हल्की ज़बान में ‘फेयरवेल’ कहा था। पता नहीं कौन था वो । जो था। जो भी था। कोई तो था।
मैं जानकीदास डिपार्टमेंटल स्टोर तक आया हूँ। आगे जनपथ है। यह सड़क बोट क्लब तक जाती है। अब बोट क्लब शायद नहीं रहा।
सामने पालिका बाजार है। जब शुरु हुआ था तो कितना क्रेज़ था इसका। बाद में एहसास हुआ कि आप और कहीं नहीं, दुकानों के बीच घिरे हैं। तब, फव्वारे के लिए फोरसीटर यहीं से चलते थे।
जनपथ नाम की सड़क मेरे दफ़्तर तक जाती है। फिर आगे निकल जाती है। लेकिन मुझे अभी दफ्तर नहीं जाना। मैं वहाँ चला भी जाऊँ तो कटे हुए रिश्ते, टूटे हुए धागे, बिखरे हुए मनके और व्यथर्ता की भावना निरंतर महसूस होगी।
मैं एक बार फिर, कनॉट प्लेस के बरामदे में चक्कर लगा रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं खरीदना बस, आखिरी बार कनॉट प्लेस के इस बरामदे में घूमते हुए, पुराना जमाना याद कर रहा हूँ , जब मैं सेल पर शर्ट, जूते और स्वेटर खरीदता था और बहुत खुश होता था।
अब खरीदने की ख्वाहिश लगभग खत्म हो गई है। कुछ ख्वाहिशें बची है। जिनमें एक ख्वाहिश यह भी है कि कुछ दोस्त होते और वो जाँनिसार होते।
मैं एक बार फिर उन सिनेमाघरों को देख रहा हूँ जहाँ एक मुद्दत पहले मैंने कुछ फ़िल्में देखीं। वो प्लाज़ा सिनेमा को ओडियन सिनेमा !
कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस के बीच एक सड़क जाती है। उपेक्षित-सी सड़क । हर ब्लॉक के पेशाबघर इसी सड़क पर हैं। यहाँ दुकानें कम हैं। यह कनॉट प्लेस का पिछवाड़ा है। यहाँ अहाते हैं। वर्कशॉप हैं और चाय के छोटे-छोटे ठीये हैं।
यहाँ न बरामदा है न सजधज । यहाँ अमीर लोग बिलकुल दिखाई नहीं देते। यहाँ मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्हें लोंग, इलायची , दालचीनी वाली चाय के बारे में पता होता है।
चायवाले ने लकड़ी का पुराना स्टूल दिया है। मैं उस पर बैठा ही था कि उसने थर्माकोल के गिलास में चाय देते हुए पूछा है,” बहुत दिनों बाद आए सॉब
“हाँ, बहुत दिन बाद .. और आखिरी बार ।”
“आखिरी बार ?” वो हैरान सा है।
“मैं आज अपने दफ्तर से रिटायर हो जाऊँगा।
तुम्हारे हाथ की चाय पीने चला आया।”
उसने हाथ जोड़ दिए हैं। वो चुप खड़ा है। जैसे मुझे विदा कर रहा हो, बेआवाज़ ।
कनॉट प्लेस के बरामदे से मैं वापिस जा रहा हूँ। जहाँ कभी टी जी आई एफ था – ‘थैंक्स गॉड इट इज फ्राई डे? मैं चल रहा हूँ और रेस्तरों के नाम को दोहराता जा रहा हूँ । आज नवंबर का आखिरी दिन है। शुक्रवार है। मैंने मन ही मन कहा है ” थैंक्स गाँड इट इज़ फ्राईडे । आलसो ईट इज़ रिटयरमेंट डे।…
दफ्तर में लिफ्ट भी है। लेकिन मैं सीढ़ियों से आ रहा हूँ। साठ की उम्र में, लिफ्ट के होते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। रेलिंग पर हाथ रखते हुए। जैसे रेलिंग को सहला रहा हूँ और उसे अलविदा भी कह रहा हूँ।
उम्र साठ की हो जाए तो आदमी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाँफने लगता है। मेरे हाँफने में, रिटायरमेंट का हाँफना भी है। मेरे हाँफ़ना में तीस सालों का हाँफ़ना भी है। मेरे हाँफ़ने में, रिश्तों के टूट जाने का हाँफ़ना भी है।
पहले जिस शीशे के दरवाजे को धकेलते हुए बाहर निकला था, कुछ घंटे पहले। उस शीशे के दरवाजे को खोलते हुए सकुचा रहा हूँ। तीस साल के लम्बे समय में, ऐसा पहली बार हो रहा है कि दफ्तर का दरवाज़ा खोलते हुए कोई शय मुझे रोक रही है। वो शायद अजनबीयत का हाथ है जो मुझे रोक रहा है।
दफ्तर मेरा अपना दफ्तर। कलीग मेरे अपने कलीग, लैपटॉप, मेरा अपना लैपटॉप , अपनी मेज, कुर्सी, फाइले सब अपना था लेकिन डिप्टी मैनेजर का आदेश था कि किसी चीज को हाथ न लगाऊँ। “नन आफ युअर बिज़नेस” तेज़ चाकू की धार जैसा फिकरा बोला था डिप्टी मैनेजर ने।
मैं अपनी मेज तक आया हूँ। जिसे टेबल इशु की गई है। वो सीट पर नहीं है। कुर्सी खाली है। मैं कुर्सी पर बैठ गया हूँ। जैसे कोई किरायेदार, किराये के मकान में हो और उसने कई महीने का किराया न दिया हो। कुर्सी पर बैठा हूँ और लगता है किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठा हूँ। कुर्सी तक बेगानी हो गई है।
कुछ कलीग ने लैपटॉप से नजरें उठाकर मुझे देखा है हल्का-सा सिर हिलाकर, काग़ज़ी फूलों जैसी बनावटी मुस्कान के साथ। फिर वो काम में मसरूफ हो गए हैं। किसी कलीग का रिटायर होना, उनके लिए ईवेंट’ नहीं है। दफ़्तर का एक एम्पलाई कल से नहीं आएगा और वो उसे याद भी नहीं करेंगे।
लेकिन विडम्बना तो यही है। मुझे न याद करने वाले वो मुझे हमेशा याद आते रहेंगे।
अकाउंट सेक्शन ने मेरे सारे ड्यूज़ क्लीयर कर दिए हैं। नो ड्यूज का लैटर भी इशू किया है और कुछ बचा हुआ अमाउंट भी दे दिया है। मैंने चैक देखा है नो डीयूज़ सर्टीफिकेट देखा है। मैं व्याकुल हो गया हूँ।
क्या ड्यूज़ क्लीयर हो सकते हैं? नहीं, डीयूज़ कभी क्लीयर नहीं हो सकते। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी नहीं उतरते। मैं दफ्तर का कर्जदार रहूँगा और शायद, दफ्तर मेरा कर्जदार रहे।
चैक और सेवानिवृति का पत्र मुझे मिल चुका है। मुझे चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं खड़ा हूँ। कोई मोह का अदृश्य धागा है जो मुझे रोक रहा है। नहीं जाने दे रहा ।
मैं खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ। इन तीस सालों में मैंने, अलग- अलग मेंज़ों पर बैठकर, कोई पटकथा- सी लिखी। विचित्र-सी पटकथा। मेरे पास पटकथा की दो प्रतियाँ हैं। एक पटकथा मैं यहीं छोड़ जाऊँगा। जिसे न कोई देख पाएगा, न पढ़ पाएगा। दूसरी पटकथा दफ्तर कथा, मैं अपने साथ ले जाऊँगा।
सब कलीग हैरान हैं कि मैं क्यों खड़ा हूँ। मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं दफ्तर से बाहर चला क्यों नहीं जाता।
कलीग मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। शीशे के दरवाज़े को मैं खोलते-खोलते रूका हूँ। मैंने पुरकशिश, उदास और कुछ रुँधी हुई-सी आवाज़ में, दरवाज़े के पास खड़े होकर कहा है, “अलविदा मेरे दोस्तो ! दिल से अलविदा !”
अचानक । बिलकुल अचानक ये क्या हुआ है। ये क्या हुआ है कि सबके सब कलीग अपनी सीट से उठ खड़े हुए हैं – वो कह रहे हैं- ऑल दि बेस्ट !.. ऑल दि बेस्ट !
फिर एक उदास-सी आवाज निकली है मेरे दिल से – ” अलविदा दोस्तो।” और मैं दफ्तर से बाहर चला आया हूँ हमेशा के लिए।
ज्ञानप्रकाश विवेक
प्रतिष्ठित कथाकार